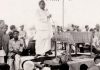— राजकिशोर —
बुद्धिजीवी और विचारधारा का रिश्ता घपले में पड़ा हुआ दिखता है तो इसके कारण दोनों तरफ हैं। कोई भी विचारधारा ऐसी नहीं है जिसकी आड़ में या जिसके नाम पर नृशंसता नहीं की गयी है। जहां नृशंसता का अभाव देखा जाता है, वहां अन्याय को सहने की शिक्षा है या इस पर मौन सहमति तथा आग्रह है। यह भी एक प्रकार की नृशंसता है। ऐसी स्थिति में, कोई सजग बुद्धिजीवी किसी खास विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता का इजहार कैसे कर सकता है?
विचारधाराओं का जन्म बुद्धिजीवियों के ही प्रयास से होता है लेकिन जब कोई विचारधारा संगठित हो जाती है तो उसकी चर्चनुमा सत्ता प्रणाली बन जाती है।
इस प्रणाली में उन्हीं बुद्धिजीवियों की कद्र होती है जो सत्य के प्रति नहीं, संगठन के प्रति उत्तरदायी तथा वफादार हों। बुद्धि का स्वाधीन या स्वतंत्र इस्तेमाल करनेवाले व्यक्तियों से ऐसे सभी संगठनों को खतरा महसूस होता है। यह भी एक कारण है कि हर विचारधारा में बहुत-से संप्रदाय बन जाते हैं और वे सामूहिक रूप से कोई संघर्ष करने के बजाय एक दूसरे की छीछालेदर करने में ज्यादा रस लेते हैं। यह बुद्धि का गैर-बौद्धिक इस्तेमाल है।
विचारधारा की दूसरी समस्या यथार्थ से उसका संबंध है। यथार्थ अपरिमित होता है। हम जितना जानते जाते हैं हमारे अज्ञान का दायरा उतना ही बढ़ा हुआ प्रतीत होता है।
वैज्ञानिक को छोड़कर, जिसे असीम में छलांग लगाते रहने की आदत-सी होती है और जिसका हर विचार उसी के जैसे दूसरे वैज्ञानिक के लिए महज एक प्रस्ताव होता है, बुद्धि के क्षेत्र में काम करनेवाले दूसरे लोगों में इस असीमता से मुठभेड़ करने का साहस नहीं होता। इसलिए वे हमेशा ऐसे ही तथ्य चुनते हैं जिनसे उनकी विचारधारा की पुष्टि होती हो। उदाहरण के लिए, बहुत-से ईसाई अब भी यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह सृष्टि छह दिन में नहीं बनी थी, बहुत-से मुसलमानों का सोचना है कि आदमी चांद पर नहीं उतरा है और अनेक हिंदू स्वर्ग तथा नरक जैसे स्थूल स्थानों की कल्पना को सच मानते हैं। बहुत कम मार्क्सवादी यह मानने के लिए तैयार हैं कि स्टालिन ने क्रूरता भी की थी, जैसे उदार गणतंत्रवादियों को यह दिखाई नहीं देता कि बाजारवाद भुखमरी और आत्महत्याओं का कारण भी बन सकता है।
हर आदमी इस कमजोरी का पुतला होता है कि मैं जो सोचता हूं वही ठीक है या मैं जो चाहता हूं वही काम्य है। यही दुर्बलता विचारधाराओं में विचार-विरोधी हठधर्मिता पैदा करती है। उनका अहं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि दुनिया में ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिनके लिए उनके भीतर कोई गुंजाइश नहीं है।
जैसे ज्यादातर व्यक्ति अपनी विफलताओं के लिए दूसरों को या भाग्य को दोषी ठहराते हैं, वैसे ही विचारधाराओं में भी अपनी कमियों, अपर्याप्तताओं और विफलताओं का वस्तुपरक विश्लेषण करने की शक्ति का अभाव होता है। साम्यवादी व्यवस्थाएं अंततः चरमरा गयीं तो इसमें उनका कोई बड़ा कसूर नहीं था- यह पूंजीवादी षड्यंत्र की सफलता थी।
आश्चर्य की बात यह है कि हर विचारधारा का जन्म अपने समय और इतिहास की आलोचना तथा उस समय तक उपलब्ध व्याख्याओं और विश्लेषणों के असंतोष से होता है, लेकिन वह मुकाम जल्द ही आ जाता है, जब किसी भी विचारधारा को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। उसे अपने आलोचक शत्रु नजर आने लगते हैं। ऐसे बुद्धि-विरोधी वातावरण में कोई सच्चा बुद्धिजीवी कब तक ठहर सकता है?
ऐसे और भी अनेक कारण गिनाये जा सकते हैं जो बुद्धिजीवी को विचारधारा से विरक्त करते हैं। एक जमाना था- और उसे बीते ज्यादा समय नहीं हुआ है- जब बुद्धिजीवी विचारधाराओं की तरफ इस तरह आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खी फूलों की ओर भागती है। कहा जा सकता है कि वह विचारधाराओं का युग था। आज ऐसा नहीं है, तो इसका कारण विभिन्न विचारधाराओं द्वारा मानव समाज के साथ किया गया विश्वासघात है। जैसे-जैसे विचारधाराओं में रूढ़ि प्रबल हुई है, वैसे-वैसे उनसे बुद्धिजीवियों का पलायन बढ़ा है। बुद्धिजीवी प्रश्नों से घिरा होता है। उसे ऐसे उत्तर नहीं चाहिए जो इन प्रश्नों का ही गला घोंटते हों। लेकिन विचारधारा और बुद्धिजीवी के बीच बिलगाव का यह एकमात्र कारण नहीं है। यह भी कह सकते हैं कि यह सबसे बड़ा कारण भी नहीं है।
आज के बहुत-से बुद्धिजीवी विचारधारा से मुख्यतः दो कारणों से भागते हैं। एक कारण है समग्रता में सोच पाने की असमर्थता या अनातुरता। कोई भी विचारधारा जीवन की एक संगठित समझ विकसित करना चाहती है। वह छुटपुट विचारों और स्थापनाओं से संतुष्ट नहीं होती। वह इन्हें एक सूत्र में बांधना चाहती है। यह मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। वह क्षण में नहीं जीता, क्षणों की एक लंबी श्रृंखला में जीता है। आज का बुद्धिजीवी इस श्रृंखलाबद्धता से घबराता है। अपने द्वारा अर्जित सत्यों का कोई अनुशासन विकसित नहीं करना चाहता।
दिलचस्प यह है कि विज्ञान में तो, जिसकी दुनिया सबसे ज्यादा खुली हुई होती है, पदार्थ, सृष्टि और जीवन के बारे में लगातार नए-नए सिद्धांत विकसित हो रहे हैं और उपलब्ध जानकारियों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश होती रहती है,जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ब्रह्मांड विज्ञान है, लेकिन सामाजिक यथार्थ के मामले में विचारधारा विकसित करने की कोशिश से बचा जाता है। क्या इसका कारण मात्र यही है कि लगातार शोध से इतने अधिक सामाजिक तथ्यों का प्रकटन हो रहा है कि सब कुछ अभी द्रवीभूत अवस्था में है और कोई ठोस बात कही नहीं जा सकती? इसमें संदेह नहीं है। विचारधारा से बचने की इच्छा विचारों से ही बचने की इच्छा का पर्याय हो सकती है। ऐसे विश्लेषण किस नाम के, जो किसी विचार तक नहीं पहुंचाते? और, उन विचारों का क्या करें, जिनकी कोई आंतरिक संगति या व्यवस्था नहीं है?
दूसरा कारण इससे ज्यादा ठोस है। कोई भी विचारधारा अंततः एक सामाजिक कर्तव्यशास्त्र भी तैयार करती है- जब तक कर्तव्य से पलायन को ही विचारधारा न मान लिया गया हो।
आज के बहुत-से बुद्धिजीवी सिर्फ बौद्धिक कार्यों में लगे रहना चाहते हैं। वे अपना कोई राजनीतिक या सामाजिक कर्तव्य निर्धारित नहीं करना चाहते। बौद्धिक चर्चा में आनंद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है। राजनीतिक कर्तव्य में जोखिम है, असुविधाएं हैं, त्याग है। इनसे बचने का सम्मानपूर्ण तरीका यही है कि विचारधारा से दूर रहें। जिस तरह भावना अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं होती- उसका कोई न कोई विषय होता है, उसी तरह बुद्धि भी सिर्फ क्रीड़ा करने के लिए नहीं है, उसकी सिद्धि सकर्मकता में ही है। निठल्ला चिंतन एक सीमा के बाद मनोरंजन भी नहीं कर पाता।
मनुष्य अगर एक सामाजिक प्राणी है- यह बहस का विषय है कि वह कितना सामाजिक है- तो उसके बौद्धिक वैभव के सामाजिक पहलू भी होने चाहिए। सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि मैं स्वतंत्रता या समता का उपासक हूं।प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता का विस्तार इतना सीमित क्यों है और उसे व्यापक कैसे बनाया जा सकता है। इसका राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए विचारधारा जैसी चीज की जरूरत होगी। इसी तरह, समता के विचार पर कितनी दूर तक अमल किया जा सकता है और विषमता के मौजूदा रूपों को कैसे खत्म किया जाए, यह बताए बिना समानता के प्रति प्रतिबद्धता का कोई अर्थ नहीं है। विचारधारा से भागनेवाला बुद्धिजीवी विचारों के लोकतंत्र का लाभ उठाना चाहता है, उसकी नागरिक जिम्मेदारियों को कबूल करना नहीं चाहता। माना कि विचार और कर्म के सभी वर्तमान औजार अधूरे हैं लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए उन्हें नदी में फेंक दिया जाए? जिन सदाशयी लोगों को इसमें शक है कि इन्हीं औजारों में से कुछ पर से समय और घटनाओं की धूल हटाकर उन्हें चमकाया जा सकता है और प्रासंगिक बनाया जा सकता है, नये औजारों का निर्माण करना उनकी बौद्धिक जिम्मेदारी है।