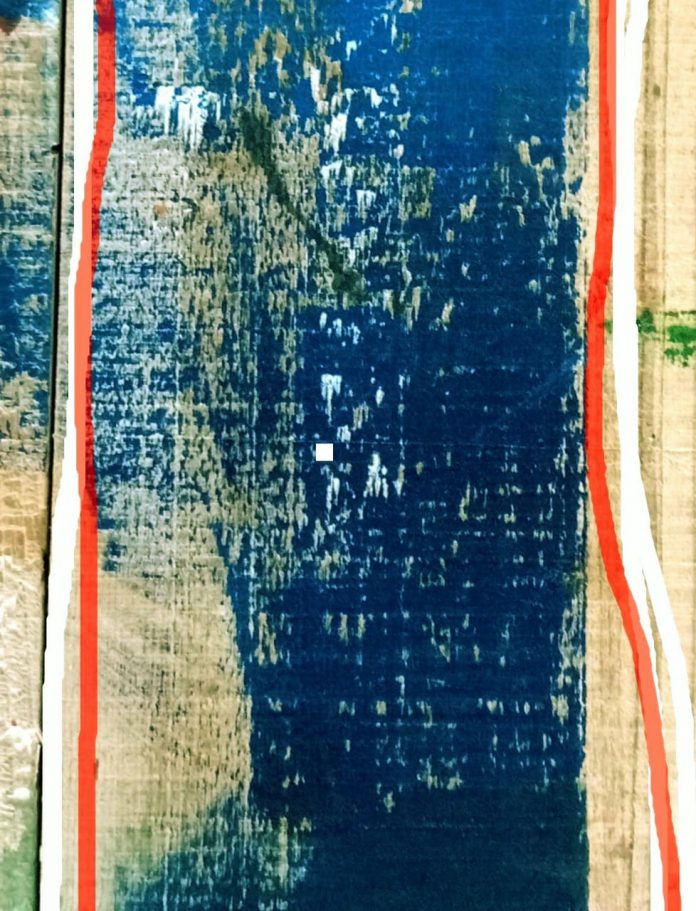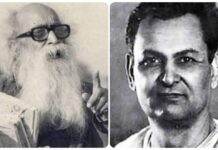— केयूर पाठक —
नजरें उठाकर संगम की तरफ देखा। गंगा और जमुना दोनों को मैंने बेबस देखा। गंगा बह रही थी, लेकिन उसकी धारा में उमंग न दिखी। जमुना भी धीरे-धीरे थपेड़े ले रही थी, लेकिन उसमें भी मिलन का कोई उत्साह न दीखा। मानो स्वर्ग से उतरने के बाद गंगा और जमुना का मिलना एक सतत चलने वाली औपचारिता भर रह गई हो। बस चले तो गंगा भी सीता की तरह धरती में समा जाए, और जमुना भी सरस्वती की तरह अपना मुख मोड़ ले। वैदिक ग्रंथों में वर्णित ‘सर्वश्रेष्ठ माँ, सर्वश्रेष्ठ नदी, सर्वश्रेष्ठ देवी’- ‘सरस्वती’ न जाने कब किन बेबसियों में विलुप्त होने को मजबूर हुई होगी! नदियों की बेचैनी सभ्यता की बेचैनी है, क्योंकि सभ्यताओं की जननी ये नदियाँ ही तो हैं। मानवता जब कराहती है तो नदियाँ भी उदास हो जाती हैं। कुछ सूख कर अपना विरोध दर्ज करती हैं और कुछ डूब कर।
मैं मन ही मन भूपेन हजारिका के गीत गुनगुनाने लगा- “गंगा तू बहती क्यों है रे…।” मैंने गंगा से बात करना चाहा, मैंने जमुना की तरफ भी देखा। लेकिन संगम में मुझे प्रलयंकारी चुप्पी ही सुनाई दी- यह चुप्पी संस्कृतिविहीन चुप्पी थी। मुझे लगा गंगा और जमुना ने अब लोगों से शायद संवाद बंद कर दिया है- या फिर युगों युगों के इस निरंतर प्रवाह से थक गई है। निराश होकर मैं रेत के किनारे बैठ गया कि तभी किसी ने मुझसे धीरे से कहा- “मैं बीमार हूँ…”। मैं चौंक गया, क्या यह आवाज संगम से आई है! लेकिन, यह संगम के संतानों की ही आवाज तो थी।
संगम किनारे खुले बदन रेत पर लेटे हुए एक कृशकाय व्यक्ति ने मुझसे धीमी आवाज में पूछा- “सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है? वहाँ इलाज का पैसा भी लगेगा?…मेरे पास तो कुछ भी नहीं…।” मैं पहले समझ नहीं पाया कि वह कह क्या रहा है, फिर दुबारा मैंने उससे पूछा कि कहाँ से हो और कहाँ जाना है…और क्या चाहिए तुम्हें? उसने लेटे-लेटे ही धीरे से फिर कहा- “बिहार के खगरिया से हूँ। यहाँ मजदूरी करने आया था, बहुत बीमार हो गया हूँ। पेट से शौच के बदले केवल खून निकल रहा है। पैसा नहीं है कि इलाज के लिए जाऊॅं…उठकर चल भी नहीं पा रहा, इसलिए यहाँ आकर लेट गया हूँ….पेट में बहुत दर्द भी है।” मैंने उसे अब ध्यान से देखा। वह वाकई बेहद बीमार था…उसकी आवाज में बड़ी बेबसी थी। उसकी बेबस आवाज ने मुझे भी एक पल बेबस बना दिया। मैं थम सा गया। मैं उसके जीवन की इस असीम निर्जनता को अपने भीतर महसूस करने लगा।
सोचने लगा ऐसे हालात में वह अपने परिवार से दूर कैसे-कैसे मनोभावों से गुजर रहा होगा! संगम नगरी में उसे रेगिस्तानी तूफानों में फॅंसे होने जैसा लग रहा होगा। उसके मन में मानव जाति के लिए, मानवीय सभ्यता के लिए, सत्ता और सरकारों के लिए कैसे-कैसे भाव आते होंगे! उसके लिए धर्म, जाति, राष्ट्र का कितना अर्थ होगा! अब बैठे रहने का मन नहीं किया। उठा और पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ रुपये थे, जो कम बहुत कम थे। फिर भी मैंने उसकी तरफ बढ़ा दिया- और बताया कि सरकारी अस्पताल कैसे जाना है- जहाँ इलाज संभव है बिना पैसा दिए, या फिर शायद बहुत कम पैसे में। सवाल था कि क्या वह निजी अस्पताल में बिना पैसे के जाने की सोच सकता था? शायद नहीं।
ऐसे लोग लाखों हैं- संभवतः करोड़ों हैं जिनके पास निजी अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं होते- दूसरे शब्दों में कहें तो जीवित रहने के लिए पैसे नहीं होते। यह आधुनिक सभ्यता की घृणित त्रासदी है- जहाँ धन का सवाल बेहतर से और बेहतर जीवन से नहीं, बल्कि जीवन का अस्तित्व बचाए रखने से भी है। निजी अस्पतालों में जहाँ मरीजों के इलाज के नाम पर केवल लूटपाट की जाती है वहाँ ऐसे लोग भला जाने की सोच भी कैसे सकते! लगातार तेजी से निजीकृत होती दुनिया में ऐसे लोगों के लिए जगह कहाँ होगी! होगी भी या नहीं! इन सवालों के साथ मैंने फिर से गंगा की तरफ देखा- इस बार वह व्यंग्य से मुस्कुराई और फिर आती हुई लहरों में उसकी मुस्कराहट मिट गई। ऐसा लगा वह कह रही थी- निजीकृत होती अर्थव्यवस्था में गंगा और जमुना भी तो अपनी सामुदायिकता खोती जा रही हैं।
तट पर मछुआरे नौका-विहार का आग्रह कर रहे थे, लेकिन अब मेरे लिए नौका-विहार उदास नदियों का उपहास करने जैसा था। मन संगम में जैसे डूब गया था। बिहार की उस ऐतिहासिक त्रासदी के बारे में मैं सोचने लगा जिसे वह औपनिवेशिक काल से झेलने को अभिशप्त है। बिहारी, पलायन, मजदूरी, अपमान, हिंसा, बेरोजगारी, ये सब कालान्तर में एक तरह से पर्यावाची शब्द बन गए- और कमोबेश पहचान भी। माना जाता है कि मृत्यु के मुख से लौटने के बाद मनुष्य का जीवन दर्शन बदल जाता है। लेकिन ऐसा कोविड महामारी के बाद भी नहीं हुआ- न समाज बदला, न सत्ता, और न उसका चरित्र। लगा था रिवर्स-माइग्रेसन के बाद बिहार से पलायन रुकेगा, रोजगार विकसित होंगे, खेत-खलिहान लहलहाएंगे, गाँवों में सम्पन्नता आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महानगरों से लौटे करोड़ों मजदूर फिर से महानगरों की तरफ ही लौट गए। वे अंधकारपूर्ण अतीत को लेकर आए थे और फिर उसी अंधकार में समा गए।
रेत पर धराशायी इस प्रवासी बिहारी मजदूर को पता था इस महासंकट में उसकी रक्षा शायद माँ गंगा ही कर सकती हैं, तभी तो वह शहर की सभ्यता से दूर प्राचीनता से भरी इस नदी की गोद में आया था। उसे पता था शहर के भीतर उसे कोई जगह भी नहीं देगा, इलाज तो दूर की बात है। उसके इस पलायन में, संघर्ष में बिहार से गंगा उसके साथ साक्षी बनकर प्रयाग तक चली आ रही थी, लेकिन वह एक बेबस माँ की तरह थी- जो अपने साथ-साथ अपनी संतानों की लाचारी पर बस सिसक-सिसक बह सकती थी। मैंने जमुना की तरफ देखा वह अब भी चुप थी, शायद राजधानी में उसकी आत्मा घायल कर दी गई थी- वह क्षत-विक्षत थी। संगम के एक तरफ लाशें जल रही थीं. ये लाशें निश्चय ही मनुष्यता की थीं।