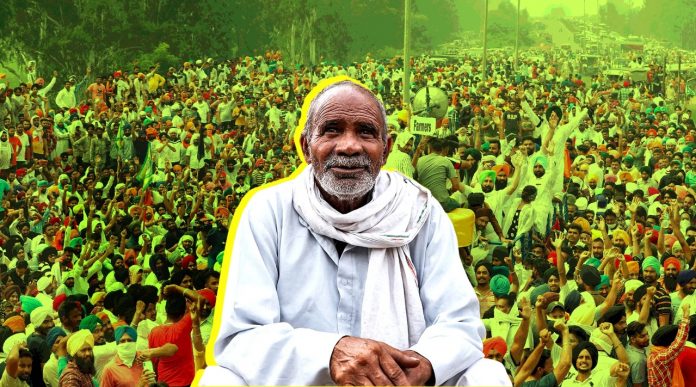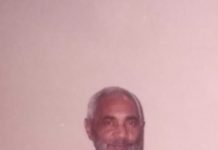अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का सीधा और साफ तात्पर्य यही है कि उसे बाजार के नियमों के अनुसार चलने दिया जाय और उसमें राज्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। लेकिन जब यह कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न हो तब इसका तात्पर्य भी वास्तविक अहस्तक्षेप नहीं, बल्कि ऐसा हस्तक्षेप होता है जो बाजार की स्वतन्त्रता को न केवल सुरक्षित, बल्कि और अधिक मजबूत करता हो। इसीलिए उदारीकरण या आर्थिक सुधारों के नाम पर राज्य अपने को आर्थिक प्रक्रिया से अलग नहीं कर लेता, बल्कि इसके विपरीत ऐसी नीतियाँ और नियम बनाता है जो बाजार की सत्ता को बढ़ाती हैं अर्थात् ऐसी स्थिति में बाजार केवल अपनी प्रक्रिया से संचालित नहीं होता, उसे राज्य का अप्रत्यक्ष, पर प्रभावी संरक्षण हासिल होता है। राज्य का आर्थिक प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए का सीधा तात्पर्य उसकी प्रभुसत्ता को बाधित करता है- उस प्रभुसत्ता को जो उसे अपने नागरिकों से प्राप्त होती है। प्रकारान्तर से इसका अर्थ नागरिकों के हितों पर बाजार के हितों को वरीयता देना है।
लेकिन बाजार का क्या मतलब है? क्या बाजार केवल उत्पादक या बेचने वालों का है? क्या खरीदने वालों के बिना बाजार की कोई कल्पना की जा सकती है? जब बाजार के हित की बात की जाती है तो उसमें आम निवेशक और आम उपभोक्ता का हित भी शामिल होता है या नहीं? और यदि ऐसा नहीं होता तो बाजार की स्वतंत्रता का अर्थ केवल उत्पादक और विक्रेता की स्वतन्त्रता रह जाती है- बल्कि उत्पादक की स्वतन्त्रता, क्योंकि वही तो मूल विक्रेता भी होता है। विक्रय की सारी प्रक्रिया वहीं से तो शुरू होती है।
यह भी उल्लेखनीय है कि जब पहले बाजार की बात की जाती थी तो सामान्यतः लोक हित के क्षेत्र को उससे अलग रखा जाता था अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे ही अन्य कामों को बाजार की प्रक्रिया और उसके नियन्त्रण के अन्तर्गत नहीं समझा जाता था। लेकिन आजकल जीवन की हर गतिविधि को बाजार के नियन्त्रण के अंतर्गत माना जाने लगा है, जिसका मतलब है कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य भी उद्योग माने जाने लगे हैं और इसके चलते उन पर भी बाजार के नियम आयद होने वांछनीय समझे जाने लगे हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को बाजार के नियंत्रण में लाने का सीधा मतलब यह है कि जिसकी क्रयशक्ति जितनी अधिक होगी उसे उतनी ही अधिक गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सकेगी – जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि कम क्रयशक्ति वाले शिक्षार्थी या बीमार को दी जानेवाली शिक्षा या स्वास्थ्य-सेवा गुणवत्ता की दृष्टि से कम प्रभावी होगी।
जब स्कूलों-कॉलेजों या विश्वविद्यालयों और धीरे–धीरे अस्पतालों आदि से भी यह अपेक्षा की जाने लगी है कि अपने लिए आर्थिक संसाधन उन्हें ही जुटाने हैं तो इसमें कहीं यह मन्तव्य भी अन्तर्निहित है कि ऐसी संस्थाओं को अपने ग्राहकों की क्रयक्षमता के मुताबिक सेवा ही उन्हें मुहैया करवानी चाहिए। स्पष्ट हैं कि शिक्षार्थी को अपनी योग्यता और प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा या बीमार को अपनी जरूरत के मुताबिक स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी प्राथमिक शर्त उसकी क्रयशक्ति होगी।
उल्लेखनीय है कि अभी भी किसी मनुष्य के प्राणों की कीमत उसकी आर्थिक हैसियत के अनुसार ही लगायी जाती है। सड़क दुर्घटनाओं में होनेवाली मौतों के मुआवजे का मामला अदालतों में जाता है तो उसका निर्धारण इसी आधार पर होता है कि उसकी आय कितनी थी। रेल और हवाई दुर्घटनाओं में होनेवाली मौतों का मुआवजा भी इसी आधार पर निर्धारित होता है कि मृतक किस साधन से और किस श्रेणी में यात्रा कर रहा था। स्पष्ट है कि एक समान घटना होते हुए भी उस पर मिलनेवाला मुआवजा जरूरत के मुताबिक नहीं, बल्कि मृतक की आर्थिक स्थिति के अनुरूप होगा। किसी बेरोजगार या आयहीन व्यक्ति के प्राणों की कीमत क्या होगी, इसका अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
जिस व्यवस्था में मनुष्य के प्राणों की कीमत भी उसकी आर्थिक हैसियत के अनुरूप हो, वहाँ कम आर्थिक हैसियत वाले को मिलनेवाली शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता किस कोटि की होगी, इसे अलग से समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
बहुत पहले पढ़ा हुआ एक चुटकुला याद आ रहा है। एक मास्टर साहब किसी को घर पर पढ़ाने जाते थे। उन्हें इस काम के लिए पचीस रुपए महीना मिलता था जो बहुत कम था, पर अपनी जरूरत के चलते उन्होंने मान लिया था। एक दिन छात्र ने किसी वाक्य का अनुवाद करने के लिए उनसे ‘जाति हत्या’ जैसे भाव को व्यक्त करनेवाले अंग्रेजी शब्द के बारे में पूछा तो मास्टर साहब ने बताया ‘कलेक्टिव मर्डर’। छात्र के पिता ने वहाँ से गुजरते हुए यह सुन लिया तो उन्होंने मास्टर साहब को टोका कि इसके लिए अंग्रेजी में सही शब्द ‘जेनोसाइड’ है तो मास्टर साहब का, ‘सर, पचीस रुपए में तो ‘कलेक्टिव मर्डर’ ही होगा। जेनोसाइड की कीमत तो ज़्यादा होती है।’
तात्पर्य यह है कि यदि बाजार पर छोड़ दिया जाय तो किसी भी सेवा की गुणवत्ता शिक्षार्थी या बीमार की जरूरत के मुताबिक नहीं, बल्कि उसके द्वारा चुकायी जा सकनेवाली कीमत होगी।
लेकिन यदि ग्राहक भी बाजार का अनिवार्य हिस्सा है तो बाजार के हितों या स्वतन्त्रता के संरक्षण का तात्पर्य ग्राहक के हितों का संरक्षण करना भी होना चाहिए और उसके हित की कसौटी उसके द्वारा चुकायी गयी कीमत नहीं, बल्कि उसकी जरूरत भी होनी चाहिए।
मजे की बात तो यह है कि बाजार का हित इसमें समझा जा रहा है कि यह कीमत भी जरूरतमंद व्यक्ति स्वयं ही चुकाए और इसमें किसी अन्य से उसे कोई सहायता न मिले। जब राज्य से यह कहा जाता है कि वह सभी चीजों पर सबसिडी बन्द कर दे तो इसका निहितार्थ यही है कि जरूरतमन्द व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहीं से इमदाद लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि इमदाद का कोई भी प्रकार बाजार के नियमों के प्रतिकूल है। गरीब को इमदाद से वंचित करना राज्य का उदारीकरण है या अनुदारीकरण- इस पर विचार की आवश्यकता है- उदार शब्द के मौलिक अर्थ के संदर्भ में भी।