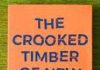— प्रो. राजकुमार जैन —
कोरोना की महामारी से हो रही मौतों के खौफ़ के कारण पुरानी कहावतें भी बेमतलब हो गई हैं। बचपन से सुनते आए हैं, आखि़र में तेरी कपाल क्रिया तो तेरी औलाद ही करेगी। फिल्मों के गानों में भी सुनने को मिलता था ‘तेरा अपना खून ही आखि़र तुझको आग लगाएगा।’ परंतु अब हालात एकदम बदल गए, औरों की बात तो छोड़िए अपनी औलाद ही इतनी खौफजदा हो गई कि मुर्दे के पास जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं रही। कोरोना के कारण इस मजबूरी को समझा जा सकता है। डॉक्टरों की हिदायत भी है कि लाश को जनाजे के लिए बने लबादे (किट) में हस्पताल में पूरी सीलबंदी के साथ घरवालों की मौजूदगी के बिना या एक आदमी को दूर से खड़े होकर दफनाने या जलाने के वक्त देखने की इजाज़त ही होगी।
मगर इस सिलसिले की शुरुआत दूसरे रूप में पहले ही हो चुकी थी। एक वक्त था कि गाँव हो या शहर, इंसान की मौत हो जाने पर घरवालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों के यहाँ मातमी माहौल हो जाता था। गली-मोहल्ले, आस-पड़ोस में जब तक लाश को दफनाने, जलाने गए लोग घर वापिस नहीं आ जाते तथा घर में मौज़ूद औरतों को अपने-अपने घरों में भेज नहीं देते थे, तब तक पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। जिसके घर में ‘गमी’ हुई है उसके घर में तो चूल्हा जलता ही नहीं था। रिश्तेदार, आस-पड़ोस वाले अपने घर से खाना बनवाकर ग़मज़दा घरवालों को ‘कुछ तो खा लो’ कहकर खाने पर मजबूर करते थे।
माहौल में कितना बदलाव आया, नयी नस्ल के लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज हम देखते हैं कि बराबर वाले या पड़ोसी के बर्ताव से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
कोरोना से पहले भी कई बार देखने में आया कि अर्थी उठानेवाले चार आदमी भी मौज़ूद नहीं हैं। एम्बुलेंस वाले को यह कहकर बुलाया जाता था कि लाश तीसरी या चौथी मंजिल पर है, आपको ही उसे उतारना है तथा मुर्दाघाट तक लेकर चलना है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी जानकार का टेलीफोन आया कि भाई साहब आप आ जाओ, हमें नहीं पता कि क्रिया कैसे होगी? सवाल उठता है कि ऐसे हालात कैसे पैदा हुए?
इसी दिल्ली शहर में मैंने देखा है कि गली-मोहल्ले में किसी की मौत हो जाती तो उसकी अर्थी निकलते वक्त ‘राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है’ की आवाज़ घर में बैठा हुआ इंसान सुनता तो तेज़ी से अपनी खिड़की दरवाज़े खोलकर अर्थी के साथ चल रहे किसी आदमी से पूछता कि भाई किसका स्वर्गवास हो गया, अर्थी के पीछे तेज़ कदम से चलता आदमी बताता, फलाने आदमी का, सुनने वाला आदमी फटाफट लुंगी, पायजामा, कमीज, बनियान या जो भी कपड़ा सामने हो पहनता हुआ अपने कंधे पर अंगोछा डालकर घरवालों से कहता कि मैं ‘जमना जी’ जा रहा हूँ (यमुना), जमुना जाने का सीधा-सीधा अर्थ था, मुर्दाघाट क्योंकि वह यमुना के किनारे है। एक-डेढ़ घंटे में लौटूंगा। मोहल्ले के बाहर आते-आते शवयात्रा में तकरीबन, मोहल्ले के सभी लोग शामिल हो जाते, भीड़ बढ़ती जाती तथा उनकी कोशिश होती कि एक बार तो मैं भी अर्थी में कंधा लगा लूं। अपने तो जाते ही थे, परंतु दुश्मन भी शिरकत करते थे। पंजाबी के कवि, गायक आशा सिंह मस्ताना का अति प्रसिद्ध लोकगीत –
“जदों मेरी अर्थी उठाके चलनगे,
मेरे यार सब हुमाके चलेनगे
चलेंगे मेरे नाल दुश्मन भी मेरे
ये वखरी है गल कि मुस्कराके चलनगें।
शमशान घाट में साथ आए हुए लोग, शव को जलाने के लिए अपने हाथों से लकड़ी लगाने की परंपरा को अवश्य निभाते। शमशान घाट पर अर्थी को तोड़कर उसमें लगे लंबे बांस से कपाल क्रिया की जाती। शव के जल जाने के बाद, लोग वापिस अपने घरों को लौटते।
यह आँखों देखा हाल मैंने चाँदनी चौक के हिंदू इलाकों का बयान किया है। यही हाल कमोबेश, मुस्लिम असरियत वाले जामा मस्जिद, बल्लीमारान, बाड़ा हिंदू राव की मुस्लिम बस्तियों की मैय्यत में देखा है।
मोहल्ले में किसी का भी इंतकाल होने पर लोग ‘गमी’ वाले घर पर जुटना शुरू हो जाते थे।
घर के बाहर कुर्सियाँ रख दी जाती थीं। मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाने के लिए लकड़ी से बना मज़बूत तख्तनुमा ‘मसेहरी’ (अर्थी) जिसके चारों तरफ़ हिफाजत के लिए 8-9 इंच की चार दीवारी बनी होती है, जो खोली भी जा सकती है ताकि हिलने डुलने पर भी मुर्दा बाहर की ओर न जा सके। कब्रिस्तान पर दफनाने के बाद यह मसेहरी मस्जिद में आगे के इस्तेमाल के लिए पहुँचा दी जाती है।
हिंदू अर्थी में शव को गिरने से बचाने के लिए सुतली से अच्छी तरह बांधा जाता है परंतु मुस्लिम मुर्दे को बांधा नहीं जाता। मुसलमानों में मजहबी रवायत है कि जनाजे में साथ चलने वाले इंसान को हर एक कदम पर 10 नेकी का सवाब मिलता है अर्थात् 40 कदम साथ चलने पर 400 नेकियों का सवाब मिलेगा। ज्यों-ज्यों जनाजा आगे बढ़ता है हर मुसलमान 40 कदम साथ चलना अपना मजहबी फर्ज समझता है, जिसकी वजह से अच्छे-खासे लोग जमा हो जाते हैं।
कंधे पर ले जा रहे जनाजे पर हर आदमी की कोशिश रहती है कि वो भी कंधा दे। कब्रिस्तान से पहले रास्ते में पड़नेवाली मस्जिद के सामने जनाजे की नमाज पढ़कर मरहूम हुए इंसान के लिए खुदा से दुआ की जाती है कि वो मरहूम के गुनाह माफ कर उसको जन्नत में जगह दे।
मुरदनी में कब्रिस्तान जानेवाला हर इंसान, कब्र में मुर्दे को रखकर अपने दोनों हाथों से तीन बार मिट्टी डालकर दुआ करता है। रवायत है कि 40 दिनों तक मरहूम के घर पर कुरान ख्वानी (पाठ) की जाती है।
कहने का मकसद है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान या किसी और मजहब को मानने वाले पहले दुख की इस घड़ी में कई दिनों तक हादसे वाले घरों में जाकर इस बात का एहसास कराते थे कि तुम अकेले नहीं हो हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं। परंतु आज हालात बदल गए हैं, शहरीकरण व भौतिक जगत की भागदौड़ तथा इंसानों का अपने तक ही महदूद रहने की जहनियत, सर्दी में रजाई, गर्मी में ए॰सी॰ में बैठा आदमी मुरदनी में जाने से कतराता है। पड़ोस में हुए हादसे पर उसका बेरुखी का रुख रहता है। सीधी सी बात है, जब मैं दूसरे के दुख में शामिल नहीं हूंगा तो मेरे दुख में वे क्यों साथ आएँगे।
हालाँकि यह मंजर अधिकतर शहरी सभ्यता में ही देखने को मिलता है। गाँव-देहात में अभी भी काफी हद तक सामूहिकता की परंपरा जारी है। शहरी सभ्यता में एक नई बात भी देखने को मिल रही है हिंदुओं में कमीबेशी हर जात में एक रिवाज रहा है कि तेरह दिन तक मरने वाले की याद और सद्गति के लिए पूजा-पाठ, लोगों का आना-जाना बना रहता था। परंतु आज के व्यापारी तथा नौकरीपेशा तबकों के पास इतना वक्त नहीं है कि तेरह दिन तक वो इंतज़ार करें।
इंतकाल होने के एक-दो दिन के बाद ही अंतिम क्रिया पूरी करके, रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाती है। परंतु आज भी ऐसी जातियाँ/समूह हैं जो पुरानी रवायत को निभाते हैं। दिल्ली की गूजर बिरादरी अभी भी तेरह दिन का शोक मनाती है। 13 दिन मुसलसल रिश्तेदार, पड़ोसी, यार-दोस्त उनके घर आते जाते रहते हैं। घर के बाहर पानी भरी बाल्टी, जिसमें नीम के पत्ते पड़े होते हैं, रखी हुई होती है, आने वाले लोग उस पानी से ‘कुल्ला’ करते हैं। तेरह दिन बाद हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर इस परंपरा का निर्वाह होता है।
बदलती हुई परिस्थितियों, मजबूरियों में इन रीति-रिवाजों में बदलाव होना लाजमी है परंतु सामाजिक संवेदना जिसमें पड़ोसी का दुख मेरा दुख जैसी मैत्री-भावना नहीं है। अगर थोड़ी बहुत है भी तो केवल औपचारिक रूप में। एक और मंजर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। शादी-विवाह, मांगलिक अवसरों पर सैकड़ों-हज़ारों लोगों की हाजिरी व शान-शौकत देखकर लगेगा कि यह शहर का बड़ा रसूख वाला आदमी है, परंतु अगर उसके घर में मौत हो जाए तो रात को मुर्दे के साथ बैठनेवालों में केवल घर के चंद लोग ही मिलेंगे। मुरदनी में भाग लेनेवाले घर पर अर्थी उठाने के लिए नहीं सीधे शमशान घाट या कब्रिस्तान में पता लगाकर पहुँचेंगे कि आखिरी क्रिया में कितनी देर है।
इंसानी रिश्तों में सब कुछ महज एक औपचारिकता बनती जा रही है। मेरे अजीज दोस्त पुरुषोतम दास ने एक ग़ज़ल किसी मौके पर सुनाई थी जिसमें शायर कमर जलालबी का एक शेर है –
दबाके कब्र में सब चल दिये
दुआ न सलाम
ज़रा सी देर में क्या हो गया,
ज़माने को।
तो लगता है कि आज की हक़ीक़त यही है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.