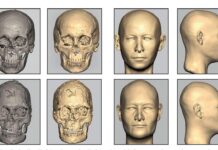— ईशान चौहान —
भाषा हमारे समाज का सबसे अहम हिस्सा होती है। वह हमें संस्कृति से, परम्पराओं से जोड़ती है, हर सीमा से परे हमें हमारे लोगों से जोड़ती है- जाहिर करने का सबसे असरदार जरिया है और न जाने क्या-क्या। लेकिन किसी विपदा के समय उसकी क्या भूमिका होती है? आपदा के बहुरूप होते हैं- ऐसे जो दृष्यंत हों यानी जिनका घटना हमें साफ दिखाई दे- चाहे वह बाढ़ हो या कुछ और ….और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अदृश्य हो, जिनका असर तुरन्त नहीं दिखता और समय के साथ कुछ बदलाव होते हैं, जिसका सबब विपदा के ये असर होते हैं।
जलवायु परिवर्तन एक ऐसी ही विपदा है जिसके असर रोजमर्रा की जिन्दगी में तो शायद न दिखाई पड़ें लेकिन समय के साथ साफ दिखने लगे हैं। सवाल ये है कि उसके भयानक और दीर्घकालीन असरात के बारे में लोगों को अवगत कराने और जलवायु परिवर्तन की तेजी से बढ़ती गति को रोकने के एकजुट प्रयास के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है।
भाषाविद माइकल हैलिडे का मानना है कि हमारी भाषाओं का मानव केन्द्रित व्याकरण ही वह कारण है जिससे यह सोच कि मानव बाकी दुनिया से कुछ अलग और खास है, हमारे सोच में रच-बस गयी है। यही कारण है कि धरती के पदार्थों के लिए द्रव्यवाचक संज्ञा या अगणनीय संज्ञा का प्रयोग होता है जिससे यह प्रतीत होता है कि वे अक्षय हैं।
लेकिन जैसा कि हम अब जानते हैं कि वे अक्षय नहीं हैं और कि मानव क्रिया ही जलवायु परिवर्तन की बिगड़ती स्थिति का कारण है- तो क्या अब भी तटस्थ भाषा का प्रयोग हमारे लिए मुनासिब है?
क्लाइमेट चेन्ज जो आज आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है असल में एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को अमरीकी रिपबलिकन सत्ता ने अलग किया था। हालांकि कहा जाता है कि इस शब्द का ईजाद 1975 में हुआ लेकिन जाहिर है कि जो असर मीडिया पर अमरीकी सरकार का रहा होगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग के मुकाबले कम डर पैदा करनेवाला कुछ विरक्त सा क्लाइमेट चेन्ज इस्तेमाल किया जाने लगा।
फ्रैंक लंट्ज़, जाने हुए राजनैतिक सलाहकार जिसने राष्ट्रपति बुश (2001-08) को यह शब्दावली बदलने को कहा था उन्होंने 2019 में अमरीकी सीनेट की विशेष जलवायु आपातकाल समिति को दिए बयान में यह ऐतरा किया कि उनकी दी हुई सलाह उलटी पड़ गयी, और वे गलत थे। इस विषय पर बहस काफी समय से चली आ रही है और अब कई वैज्ञानिक विशेषज्ञ और ‘द गार्डियन’ जैसे रोजनामे इस विरक्त भाषा का त्याग कर रहे हैं और ऐसी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे लोगों तक इस समस्या की गंभीरता सही मायनों में पहुंच सके।
हिन्दुस्तान पर क्लाइमेट चेन्ज का नहीं क्लाइमेटर इमरजेन्सी यानी जलवायु आपातकाल के कुछ असरात पर नजर डालते हैं और फिर देखेंगे इस बदली शब्दावली के मायने, आखिर हर बात के दो पहलू तो अवश्य होते हैं।
हिन्दुस्तान एक बहुत बड़ा देश है जिसका समुद्री तट 7500 कि.मी. लम्बा है। हाल ही में छपी एक रिपोर्ट ने बताया कि 2050 तक कई शहर जो तट पर हैं वो पानी के नीचे होंगे। हमारी सरकार ने 2020 में 1792 हेक्टेयर की ‘विकास संबंधी कार्यों’ के नाम पर कुर्बानी दे दी- ये अंक भयदायक इसलिए है कि हिन्दुस्तान वैश्वि क जैव विविधता के एक बड़े हिस्से का रखवाला है जिस कारण उसे ‘बायोडायवर्सिटी हाट्स्पाट’ का करार दिया गया है और हाल ही में प्रकाशित एक शोध से सामने आया है कि दक्षिण एशिया के इन 4 हाट्स्पाट्स अपने वनस्पतियों में से 70 प्रतिशत खो चुके हैं।
उपरोक्त तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि हम कितने पानी में हैं। मुनीर नियाजी का एक शेर है -वक्त कितनी तेजी से गुजरा रोजमर्रा में ‘मुनीर’ आज कल होता गया, दिन हवा होते गये। रोजमर्रा में बहुत दिन हवा हो चुके हैं अब और ज्यादा वक्त नहीं है- अभी और आज से ही काम करना होगा। इसमें सबसे बड़ा एक हिस्सा है- आम लोगों को इसके भयानक सत्य से आगाह करना।
इस बदली शब्दावली के जो हामी हैं उनका कहना है कि आज की आम भाषा इससे संबंधित असरात को उनके पूर्ण सत्य के साथ बयान नहीं करती, इसी वजह से आम लोगों में बेपरवाही का नजरिया है, शायद इसलिए भी इसके असर तुरन्त नहीं दिखते।
इस बदली शब्दावली के द्वारा कहा जाता है कि खतरों के बारे में बात न करते हुए उसपर कदम न उठाते हुए, जो फल हमें मिलेंगे उसके बारे में बात की जाए। गंभीरता को महसूस कराने के लिए समस्या को दूर का नहीं निजी बताएं- उसे अपने से असंबंधित सिर्फ एक हमारे बस से बाहर की अवधारणा न बताकर मानवीकरण करें ताकि सुननेवाला उसे अबूझ न समझे।
दूसरा पहलू यह है कि अगर ‘पर्यावरण आपातकाल’ पद का प्रयोग किया जाए तो क्या आज से कुछ समय बाद आम आदमी की सोच में आपातकाल की गंभीरता वैसी ही रहेगी। आदमी कहीं उसके प्रति असंवेदनशील तो नहीं हो जाएगा? अगर हां तो फिर कौन से नए शब्द अपनाने होंगे?
अभी तो यह सोच मेरी समझ में मुनासिब है कि नए शब्दों की तलाश तब होगी जब उनकी आवश्यकता फिर हमें दस्तक देगी। अभी इस शब्दावली को बदलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कोशिश में जोड़ना जरूरी है ताकि हम न्यूनीकरण (मिटिगेशन) और इन मसलों से जूझते हुए पृथ्वी को मानव जीवन निर्वाह के लिए लगातार अनुकूलित करते जाने के प्रयासों में सफलता पा सकें।
इस लेख को पढ़ने पर पाठक के मन में एक सवाल लाजमी है- इसे लिखने के उद्देश्य को लेकर। तो उसका उत्तर साधारण सा है- यह केवल एक अणुमात्र की कोशिश है आमजन में जलवायु परिवर्तन आपातकाल पर बातचीत को बढ़ावा देने की। कहा जाता है कि आगाज मुश्किंल होता है, एक बार हो गया तो फिर उस पथ पर बने रहना कठिन नहीं है, अगर सत्यनिष्ठा हो तो। और जब अपने ही अस्तित्व पर सवालिया निशान हो, तो फिर हर प्रयत्न कम ही है।
संयुक्त राष्ट्र का एक अंग, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने पिछले हफ्ते ही अपनी नयी रिपोर्ट में कोड रेड का परचम बुलंद किया है। महासचिव ने इसपर कहा कि खतरे के सबूत पुख्ता हैं जिन्हें कतई झुठलाया नहीं जा सकता। उनका कहना है कि हल हमारे सामने है बस उसे अपनाने की देरी है। लेकिन शायद सच्चाई का रास्ता इतना भी सीधा नहीं है।
जैसा कि हर बहस के साथ होता है, दो पहलू यहां भी हैं- एक प्रतिक्रिया ये कि कार्बन रिडक्शन से धरती के बढ़ते ताप को कम किया जा सकता है, और दूसरी ये कि इस कमतीकरण पर इतनी निर्भरता ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी तकनीकें अभी आम नहीं हुई हैं। रिपोर्ट का पहला भाग ये कहता है कि धरती का तापमान 2050 तक तो बढ़ेगा ही, चाहे जो भी किया जाए- कितना? यह नियंत्रित किया जा सकता है।
भाषा में बदलाव इस जीवित रहने के संघर्ष में एक छोटी पर अहम कड़ी है। भाषा के प्रयोग से जब तक अत्यावश्यकता का संदेश घर-घर जन-जन तक न पहुंचेगा, तब तक साधारण जनसमुदाय का इस कोशिश में अपना महत्त्वपूर्ण सहयोग दे पाना अंसभव है।
काश, जाँ निसार अख़्तर का कहा कि ‘इतने मायूस तो हालात नहीं, लोग किस वास्ते घबराए हैं” सच होता।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.