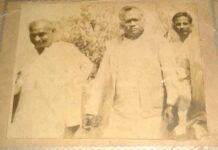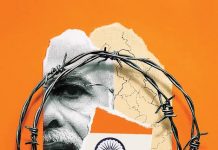अब हम देखें कि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा 1942 के आंदोलन का क्या मूल्यांकन किया गया था, उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वायसराय लिनलिथगो द्वारा सेक्रेटरी आफ स्टेट एमेरी को भेजी गई पहली रपट आत्मतोष की भावना से ओत-प्रोत थी। उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी की कोई खास प्रक्रिया नहीं है और मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। प्रारंभ में बिहार सरकार भी आशावादी थी।
लेकिन दो दिन बात लिनलिथगो का सुर कुछ बदल गया। एमेरी को भेजे गए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि बंबई आंधी का केंद्र दिखाई दे रहा है और गवर्नर रोजर लमली ने बहुत ही निराशाजनक चित्र खींचा है। (ट्रांसफर आफ पावर, खंड 2 पृ. 622)
फिर धीरे-धीरे हिंदुस्तान के अन्य इलाकों से खबरें आने लगीं। एक सप्ताह बीत जाने के बाद लिनलिथगो की यह राय बनी कि बिहार की स्थिति अत्यंत गंभीर है। अब उन्हें महसूस होने लगा कि अशांति का केंद्र बिहार है। ग्रामीण जनता भी आंदोलन में प्रवृत्त हो गई थी। सेबोटेज इतना व्यापक था कि टेलीग्राम, टेलीफोन, रेलवे का यातायात तहस-नहस हो गया। आंदोलन की आग पूर्वी उत्तरप्रदेश में भी फैल गई। जमशेदपुर के इस्पात कारखाने में हड़ताल होने के कारण उत्पादन ठप्प हो गया था और उसका असर युद्ध सामग्री के उत्पादन पर भी पड़ा। (उपरोक्त, खंड 2, पृ. 730, 745, 776)
22 अगस्त को बिहार के गवर्नर स्टुअर्ट ने वायसराय को भेजी अपनी रपट में बिहार में हुए “उपद्रवों का पूरा ब्यौरा दिया था। उन्होंने कहा था कि पटना के सचिवालय पर भीड़ ने लगातार हमले किए और दानापुर से फौजी सहायता आने के बाद परिस्थिति पर कुछ काबू पाया जा सका। विश्वविद्यालय, कालेज, होस्टल आदि बंद कर दिए गए, लेकिन छात्र ग्रामीण इलाकों में फैल गए। गवर्नर ने कहा कि प्रांतीय राजधानी पटना का सभी जिलों से संबंध विच्छेद हो गया, सिर्फ गया को छोड़कर। बाद में शांति और व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के बाद तिरहुत कमिश्नरी में कई पुलिस थानों और चौकियों को छोड़ देना पड़ा।” (उपरोक्त, खंड 2, पृ.787-91)
पूर्वी उत्तरप्रदेश में भी हालत खराब थी। वायसराय ने एमेरी से कहा कि यू.पी. के गवर्नर हैलेट द्वारा आंदोलन को जो विद्रोह की संज्ञा दी गई है, वह सर्वथा उपयुक्त है। जान और माल की अत्यधिक हानि हुई है।
मैक्स हार्टकोर्ट नाम के लेखक ने अपने अध्ययन में कहा है कि उपद्रव से प्रभावित इलाकों का क्षेत्रफल इंग्लैण्ड और वेल्स के बराबर था। बिहार में दस जिले और पूर्वी उत्तरप्रदेश के छः जिले आंदोलन से प्रभावित रहे। उपद्रवों का स्वरूप 1857 में ग्रामीण इलाकों में जो कुछ हुआ, उससे मिलता-जुलता था उसने लिखा है कि 1857 और अबकी बार परिस्थिति में मुख्य फर्क यह था कि इसबार आधुनिक किस्म की व्यवस्था और सत्ता स्थापित करने का विद्रोहियों द्वारा प्रयास किया गया। जो विद्रोही लोग थे वे पूरे इलाके में जय प्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया द्वारा तराईं में जो समानान्तर सरकार स्थापित की गई थी, उसके प्रति आस्था रखते थे। इतना ही नहीं समाजवादियों के माध्यम से इनका संबंध पश्चिम भारत में स्थापित हैडक्वार्टर से था। (कांग्रेस एण्ड द राज, पृ. 316-21)
हाईकोर्ट का मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नाम पर जो केंद्रीय निदेशक समिति की स्थापना की गई थी, उससे था। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, इस कमेटी में गिरफ्तारी से बचे प्रमुख समाजवादी और गांधीवादी नेता थे।
बलिया और आजमगढ़ के जिलाधिकारियों ने अपनी डायरियों और रपटों में थानों और कचहरियों को जनता द्वारा घेर लिए जाने का पूरा ब्यौरा दिया है। कई दिनों तक बंगाल और असम का संबंध बाकी भारत में पूर्णतः कट गया था।
प्रारंभ में रायटर जैसी विदेशी समाचार एजेंसियों द्वारा विद्रोह के खबरें तफसील के साथ भेजी गई थी। इसपर सेक्रेटरी आफ स्टेट एमेरी ने बुरा माना और कहा कि इस तरफ का विस्तृत विवरण प्रकाशित होने के कारण यहां इंग्लैण्ड में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि भारत एक प्रमुख रणक्षेत्र ही बन गया है। इस पर सरकार ने प्रेस पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगा दिए।
वायसराय लिनलिथगो ने प्रधानमंत्री चर्चिल को लिखे पत्र में कहा था कि “इस समय 1857 के बाद हुई इस पहले गंभीर विद्रोह का सामना करने में मैं पूरी ताकत से लगा हुआ हूं। इस विद्रोह की व्यापकता और गंभीरता सुरक्षा संबंधी कारणों को लेकर विश्व से हमने छुपाई हैं। देश के बड़े हिस्से में भीड़ द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही की जा रही है और ग्रामीण इलाके भी इसमें सम्मिलित हैं।” (ट्रांसफर आफ पावर, खंड 2,पृ.853-54)
अगस्त आंदोलन के प्रभाव का जहां तक सवाल हैं, अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया था कि पूर्वी तथा महत्त्वपूर्ण बी.एन.रेलवे कुछ समय के लिए पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गई थी। आंध्र के गुंटूर और विजयवाड़ा जिलों में रेल मार्गों का जो विध्वंस किया गया था। उसकी वजह से कुछ समय तक मद्रास भी उत्तर भारत से कट गया था। वायसराय वेवल, जो 1942 में अंग्रेजी सेना का कमांडर था, और बाद में वायसराय बना, ने गांधीजी को लिखे एक पत्र में स्वीकार किया कि उनकी पूर्वी उत्तरप्रदेश के कुछ जिलों तथा बिहार के एक बड़े भूभाग में अंग्रेजी हुकूमत नष्ट सी हो गई थी। बंगाल में मेदिनीपुर और महाराष्ट्र में कुछ समय बाद सातारा जिला तथा उसके आस-पास के ग्रामीण इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत का अस्तित्व मिट गया था और वहां एक समानांतर सरकार, जिसे ‘पत्री सरकार’ के नाम से साधारण जनता में पुकारा जाता था, कायम हो गई थी।
अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, डॉ. राममनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी जिस तरह समूचे देश में मशहूर हो गए थे उसी तरह समानांतर सरकार की स्थापना से सतारा जिले में श्री नाना पाटिल विशेष रूप से ख्यातनाम हो गए थे। 1942 के अक्टूबर महीने में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण (जो 9 अगस्त के पहले से वहां बंद थे) अपने साथी रामनंदन मिश्र आदि के साथ केंद्रीय जेल की ऊंची दीवारें लांघकर भाग निकले थे। जयप्रकाश नारायण यूं तो पहले से ही एक मशहूर नेता थे, लेकिन इस साहसिक कदम से उनकी ख्याति देश के कोने-कोने में फैल गई। बाहर आने के बाद जयप्रकाश ने आंदोलन में काफी योगदान दिया। डॉ. लोहिया और जे.पी. ने नेपाल को अपना केंद्र बनाकर आंदोलन संचालित किया। भूमिगत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता और जे.पी. में एक प्रश्न को लेकर कुछ बुनियादी मतभेद उत्पन्न हो गए। और जहां ‘न हत्या, न चोट’ वाला प्रतिबंध हमें अपने ऊपर लादने की जरूरत नहीं हैं। अन्य देशों ने जिस तरह हथियारी क्रांति का प्रयोग किया, वैसे ही प्रयोग इस अंतिम चरण में हिंदुस्तान को करना चाहिए। अगस्त आंदोलन में ये मतभेद अंत तक रहे। कुछ लोग अहिंसा को पूर्णतया त्यागने के लिए तैयार नहीं थे।
जे.पी. और लोहिया कुछ समय बाद पकड़े गए और उन्हें लाहौर में डाल दिया गया। वहां उन्हें हर तरह की यातनाएं दी गई। अच्युत पटवर्धन और अरुणा आसफ अली को गिरफ्तार करने में सरकार आखिर तक असफल रही और उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। सुचेता जी, रंगराव दिवाकर आदि गांधीवादी नेता 1943 में गांधीजी के अनशन के बाद जेल चले गए थे। गांधीजी के अनशन के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि ‘न हत्या न चोट’वाला जो विध्वंसकारी कार्यक्रम जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया गया था, वह गांधीजी को पसंद नहीं था। इसलिए गांधीजी में जिनको अनन्य निष्ठा थी उन लोगों ने धीरे-धीरे भूमिगत आंदोलन से अपना रिश्ता तोड़ लिया और प्रकट होकर जेल चले गए।
शिमला सम्मेलन (1945) के कई महीनों बाद जब भारत में केंद्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव का दौर संपन्न हुआ और स्थिति कुछ सामान्य बन गई तब अरुणा जी के वारंट सरकार द्वारा वापस लिये गए और वे अत्यंत जन उत्साह के साथ बंबई में प्रकट हो गईं।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.