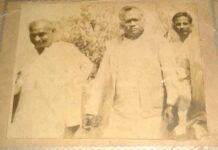सन 1920 तक कांग्रेस के जितने अध्यक्ष हुए उनमें सबसे अधिक संख्या यानी 17 वकीलों की थी। तीन अध्यक्षों का अपने जीवनकाल में शिक्षा से संबंध रहा। तीन भूतपूर्व सरकारी अधिकारी थे और तीन उद्योगपति और व्यापारी। प्रारंभिक काल में तीन चार बार ब्रिटिश नागरिकों ने भी कांग्रेस के अधिवेशनों की सदारत की। इनमें सबसे मशहूर डॉ. एनी बेसेण्ट थीं। एनी बेसेण्ट ने तो भारत को ही अपना निवास स्थान बना लिया था और वे सही मायनों में भारतमाता की पुत्री बन गई थीं।
1920 के अधिवेशन में श्रमिक संघों के निर्माण पर पुनः जोर दिया गया था और सरकार के द्वारा पूंजीपतियों के लिए विशेषकर विदेशी पूंजीपतियों के लिए किसानों की जो जमीनें अधिग्रहित की जा रही थीं, उसकी निंदा की गई थी। अब कांग्रेस में किसानों और श्रमिकों की बाते उठने लगीं। सूत कताई और हथकरघा व्यवसाय को प्रोत्साहन देने संबंधी जो प्रस्ताव पारित हुए थे उनमें इस बात की ओर ध्यान दिया गया था कि भारत में 1/3 फीसदी लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और कृषि व्यवसाय से संलग्न हैं। कृषि से पर्याप्त काम और आमदनी नहीं मिलती। खाली दिनों में सूत कताई आदि काम किए जा सकते हैं। अतः ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण उद्योगों को महत्त्व देना चाहिए, यह बात कांग्रेस के लिए सर्वथा नई बात नहीं थी।
महात्मा गांधी के नेतृत्व के उदय के बाद कांग्रेस उत्तरोत्तर ग्राम और किसान अभिमुख बनने लगी। 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्यों में परिवर्तन किया गया और स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि स्वराज्य की प्राप्ति कांग्रेस का मकसद होगा। इसी अधिवेशन में राजाओं से अपील की गई कि वे अपनी रियासतों में जवाबदेह शासन की स्थापना करने में पहल करें। गांधीजी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करने वाले कांग्रेस के पुराने बुजुर्ग नेताओं में मोतीलाल नेहरू अग्रणी थे। सन् 1921 के लिए मोतीलाल नेहरू, डॉ. अंसारी और राजगोपालाचारी कांग्रेस के महामंत्री पद पर नियुक्त हुए और एक प्रस्ताव के द्वारा यह भी निर्णय किया गया कि कांग्रेस का प्रधान कार्यालय इलाहाबाद में रहेगा। इस तरह गांधी युग के प्रारंभ में ही कांग्रेस इलाहाबाद नेहरू परिवार के कृपा-छत्र के नीचे आ गया था।
असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस संगठन के स्वरूप में आमूल परिवर्तन आया। कांग्रेस में पहले आंग्ल विद्या विभूषित तथा सूट-बूट पहनने वाले उच्च वर्ग के सदस्यों की भर्ती ज्यादा थी, लेकिन जहां गांधी युग प्रारंभ हुआ, वहां यह स्वरूप बदल गया। पश्चिमी वेशभूषा की जगह खादी आई। खादी बन गई त्याग, तपस्या और सादगी का प्रतीक। असहयोग के प्रस्ताव में कपड़े के मामले में सूत कताई और हथकरघा उद्योग के जरिए मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने की बात थी। यह उद्देश्य तो अगले सत्ताईस वर्षों के लगातार प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसमें शक नहीं कि स्वदेशी और खादी आंदोलन की वजह से गांव-गांव में खादी उत्पादन केंद्रों का निर्माण हुआ और इसके जरिये ग्रामीण जनता से संपर्क बनाए रखना कांग्रेस के लिए आसान हो गया। स्वदेशी आंदोलन से भारतीय पूंजीपतियों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हुआ। विदेशी कपड़े के इस्तेमाल का प्रचलन कम होने की वजह से इस अवधि में भारतीय कपड़ा उद्योग का काफी विस्तार हुआ। दवितीय महायुद्ध के दौरान कपड़ों का आयात एकदम घट जाने के कारण देश कपड़े के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया।
असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद गांधीजी के ऊपर केस चलाया गया और उनको 6 साल की सजा फरमाई गई। जैसा कि हमने पढ़ा है, कांग्रेस में नेताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसका प्रारंभ से विधानमंडलों के बहिष्कार के कार्यक्रम में विश्वास नहीं था। गांधीजी के व्यक्तिगत मत और उनकी लोकप्रियता के दबाव में ही कौंसिल बहिष्कार के कार्यक्रम को इन नेताओं द्वारा अपनाया गया था। अतः असहयोग आंदोलन के स्थगित होने का अवसर साध कर इन लोगों ने कौंसिल प्रवेश की राजनीति का दुबारा श्रीगणेश किया। स्वराज्य पार्टी गठित हुई। उसके नाम पर मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने संसदीय कार्यक्रम हाथ में लिया। 1924 में उनके द्वारा एक घोषणापत्र जारी किया गया। इस घोषणापत्र में स्वराज्य पार्टी ने निम्न बातों पर विशेष रूप से जोर दिया :
- असह्य करभार में कटौती।
- सरकार की मुद्रा नीति का विरोध, जिसके चलते रुपए का ऊर्ध्वा मूल्यन हुआ था। पौंड स्टर्लिंग के मुकाबले रूपए का मूल्य ऊंचा रखने कारण कृषि उत्पादन के दामों में गिरावट आ गई थी और किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की आय घट गई थी। सरकारी मुद्रा नीति का स्वदेशी उद्योगों पर भी बुरा असर हुआ था।
- भारत के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना। विदेशी माल की सपर्धा से स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देना स्वराज्य पार्टी की नीति थी। सीमा शुल्क की दीवार खडी करने से स्वदेशी उद्योग जल्दी पनप सकेंगे, ऐसी स्वराज्य पार्टी की मान्यता थी। इकत्तीस करोड़ ग्राहकों के बाजार के संदर्भ में स्वराज्य पार्टी औद्योगिक नीति की ओर देखती थी।
- स्वराज्य पार्टी की मांग थी कि रेल भाड़े की दरों को घटाया जाए जिससे कृषि माल और औद्योगिक माल पर ज्यादा बोझ न पड़े।
- स्वराज्य पार्टी की अंतिम मांग यह थी कि प्रशासन में फिजूलखर्ची को कम किया जाए और सरकारी खर्च में मितव्ययिता अपनाई जाए।
स्वराज्य पार्टी के जमाने में कांग्रेस में असहयोगवादी और कौंसिल प्रवेशवादी नाम से एक तरह की दरार पड़ गई थी। गांधीजी ने अपनी रिहाई के बाद अपने रचनात्मक कार्यक्रम में किसी तरह का समझौता न करते हुए कांग्रेस की बागडोर स्वराज्य पार्टी के नेतृत्व के हाथों सौंप दी। आगे चलकर स्वराज्य पार्टी के आर्थिक कार्यक्रम और कांग्रेस के कार्यक्रमों में कोई अंतर नहीं रहा। स्वराज्य पार्टी के विधानमंडलों के सदस्य हर रचनात्मक कार्यक्रमों का अपने मंच से समर्थन करने लगे।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.