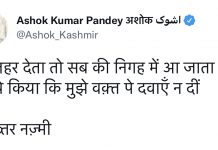— नन्दकिशोर आचार्य —
अक्सर होता यह है कि राज्य में शक्ति और सत्ता का अधिकाधिक केंद्रीकरण नागरिक को राजकीय संस्थानों के समक्ष कमजोर बनाता और अपमानित करता है। यदि एक सामान्य नागरिक पुलिस और कचहरी की तो बात दूर, अस्पताल और यात्रा आरक्षण जैसे दफ्तरों में भी स्वयं को बौना, उपेक्षित और अपमानित महसूस करने लगे, तो सोचना होगा कि उस व्यवस्था को कहाँ तक वास्तविक और नैतिक आधारों पर लोकतंत्र कहा जा सकता है- क्योंकि सत्ता का वास्तविक स्रोत लोक है और वही वहाँ उपेक्षित और अपमानित है। यह सिर्फ कर्मचारियों के व्यवहार का ही नहीं लोकतंत्र को एक महाकाय यंत्र बना देने का परिणाम है।
राजनीति के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हुए अक्सर य़ह मान लिय़ा जाता है कि उसका संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। अधिकांशतः राज्य़ को य़ा तो एक ‘आवश्य़क बुराई’कहकर स्वीकार किय़ा जाता है या उसकी इतनी प्रशंसा की जाती है जैसे वह इस लोक में ईश्वर का साक्षात् रूप हो। आधुनिक कहे जानेवाले बहुत से राजनीतिवेत्ता खासतौर से व्यवहारवादी विश्लेषक न केवल राज्य के आचरण का अध्ययन उसकी दैनिक कार्यप्रणालियों और सत्ता-राजनीति के आधार पर करते हैं बल्कि इन्हीं आधारों पर राज्य के कार्यों और राजनीति की मूल्यहीनता का औचित्य भी सिद्ध करते हैं।
अक्सर यह कहा जाता है कि सत्ता में आने, बने रहने और सत्ता का प्रबंध कर सकने के लिए कुछ व्यावहारिक सीमाओं को मानना आवश्यक है, लेकिन यह भुला दिया जाता है कि व्यावहारिक सीमाओं के नाम पर यदि उन बुनियादी मानव मूल्यों की ही अवहेलना या दमन हो रहा है जिनके पोषण के लिए राज्य को एक अनिवार्य बुराई होते हुए भी स्वीकार किया गया है तो इस तरह की व्यावहारिकता को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अपना वास्तविक प्रयोजन पूरा करने में वह पूर्णतया असफल रही है। किसी बात का घटित होना या होते रहना उसके होने की वांछनीयता प्रमाणित नहीं करता। हम उसके कारणों का विश्लेषण कर उसे समझने की कोशिश करते हैं तो इसलिए नहीं कि उसके औचित्य की आधारभूमि तलाश करें, बल्कि इन कारणों की समझ हमें उसमें से अवांछित को मिटाने और उसे अपनी वांछित दिशा में मोड़ दे सकने का बुनियादी सामर्थ्य देती है।
भारतीय परंपरा में राज्य को अनिवार्य बुराई मानकर उसकी अवहेलना नहीं की गयी। यह माना जाता रहा कि राज्य यानी सत्तासंपन्न एक व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा और विकास के लिए एक अनिवार्य संस्था है और वह वस्तुतः एक अनिवार्य बुराई नहीं बल्कि एक अनिवार्य हितैषी संस्था है। इसीलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र या शांति पर्व में राज्य का अस्तित्व भौतिक और नैतिक-आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक स्वीकार किया गया है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस उद्देश्य की पूर्ति की व्यावहारिक जिम्मेदारी राज्य पर छोड़ते हुए भी तत्संबंधी दिशा-निर्धारण का कार्य राज्य पर नहीं छोड़ा गया है। यह कार्य धर्म का है, यहाँ धर्म किसी संप्रदाय विशेष के अर्थ में नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति और एक नियमसंहिता यानी संविधान के अर्थ में है। राज्य को धर्म के शासन से ऊपर नहीं माना गया है। दूसरे शब्दों में, यह स्वीकार किया गया है कि राज्य को ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें नागरिकों का भौतिक-नैतिक विकास हो सके लेकिन उसे इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करना है।
आधुनिक काल में राज्य के अधिक शक्तिशाली होते चले जाने के कई कारण हैं- लेकिन एक महत्त्वपूर्ण कारण राज्य को नागरिकों की स्वीकृति भी है। अधिनायकवादी व्यवस्था की बात फिलहाल छोड़ दें क्योंकि यह गुंडई का ही एक विकसित और सूक्ष्म रूप है- उसका नैतिक आधार भौतिक शक्ति है, नागरिकों की सहमति नहीं। प्राचीन राजतंत्रीय व्यवस्था को भी नागरिकों की एक प्रकार की परोक्ष स्वीकृति रहती थी क्योंकि तब उसकी शक्ति का, उसके प्रति श्रद्धा का स्रोत धर्म और उस धर्म-व्यवस्था को समाज की स्वीकृति रहती थी। लेकिन आधुनिक काल में अधिनायकवाद का कोई भी प्रकार इस तरह का नैतिक औचित्य प्रमाणित नहीं कर सकता क्योंकि सेना के अंधे बल के अतिरिक्त उसका कोई स्रोत नहीं है, इसलिए अधिनायकवादी राज्य का कोई नैतिक औचित्य प्रमाणित नहीं होता।
समाजवादी उद्देश्यों का दावा करनेवाली और कुछ हद तक उसे अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा व्यावहारिक रूप देने में अग्रणी व्यवस्था का अधिनायकत्व भी नैतिक दृष्टि से संदिग्ध ही रहता है क्योंकि उसकी नीति और कार्य प्रणाली को भी कोई स्पष्ट सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती। यह मान लिया जाता है कि राज्य उनके लाभ के लिए काम करता है, इसलिए वह नागरिकों को स्वीकार होगा ही। लेकिन इस विकास की– और समाज का विकास भौतिक सुविधाओं का ही नहीं, चेतना का विकास है, बल्कि भौतिक सुविधाएँ भी तभी वांछनीय हैं जब वे चेतना के विकास में सहायक हों– वास्तविक नीति और प्रक्रिया के निर्धारण में नागरिकों को खुले रूप से भाग लेने का अवसर देना वांछनीय नहीं समझा जाता। इस कारण अन्ततः राज्य और नागरिक का रिश्ता किसी मूल्यगत और नैतिक स्तर पर नहीं बल्कि सत्ता के समक्ष विवशता के स्तर पर ही बना रहता है।
लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि स्वयं को लोकतांत्रिक कहनेवाली व्यवस्था का आधार सदैव सामाजिक स्वीकृति ही होता है। निस्संदेह इस सामाजिक स्वीकृति का एक वैधानिक या औपचारिक रूप तो उनमें बना रहता है– लेकिन इस स्वीकृति को वास्तविक अर्थों में नैतिक स्वीकृति कहाँ तक कहा जा सकता है?
इसे लेकर संदिग्धता बनी रहती है कि वर्तमान लोकतांत्रिक पद्धतियों में क्या वस्तुतः लोकेच्छा व्यक्त हुई है। क्या एक निश्चित अवधि के लिए चुनी गयी सरकार के प्रत्येक कार्य को उसके चुननेवालों का नैतिक समर्थन प्राप्त है? यदि नहीं है तो उस सरकार को सदैव एक नैतिक व्यवस्था के रूप में किस तरह स्वीकार किया जा सकता है? और यदि व्यवस्था का अपना स्वरूप नैतिक नहीं है तो नागरिक से यह अपेक्षा कहाँ तक संगत है कि वह राज्य की प्रत्येक नीति को स्वीकार कर लेगा और अपने आचरण को उसके अनुसार ढालने का प्रयत्न करेगा? और यदि इस नैतिक आश्वस्ति के बिना भी राज्य समाज पर अपनी आकांक्षा लादता है तो क्या वह ऐसा सिर्फ सैनिक शक्ति के आधार पर ही नहीं करता?
दूसरे शब्दों में, ऐसी परिस्थिति में वास्तविक सामाजिक स्वीकृति के अभाव में लोकतांत्रिक औपचारिकताओं के बावजूद राज्य और समाज के रिश्ते की वास्तविक आधारभूमि अनैतिक या अधिक से अधिक नैतिकता निरपेक्ष ही रहती है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न यह भी है कि यदि राज्य मानवीय चेतना के विकास का ही एक उपकरण है और इसीलिए उसकी नीति और प्रक्रिया का निर्धारण सामाजिक स्वीकृति के ही आधार पर होना चाहिए तो यह भी देखना होगा कि इस प्रक्रिया पर सामाजिक नियंत्रण केवल औपचारिक नहीं बल्कि वास्तविक हो। यह भी देखना होगा कि मानवीय विकास के लिए बनाई गई व्यवस्था के समक्ष वही मनुष्य अपने को बौना या तुच्छ महसूस करने न लग जाए जिसका विकास ही इस व्यवस्था के अस्तित्व का प्रयोजन है।
अक्सर होता यह है कि राज्य में शक्ति और सत्ता का अधिकाधिक केंद्रीकरण नागरिक को राजकीय संस्थानों के समक्ष कमजोर बनाता और अपमानित करता है। यदि एक सामान्य नागरिक पुलिस और कचहरी की तो बात दूर, अस्पताल और यात्रा आरक्षण जैसे दफ्तरों में भी स्वयं को बौना, उपेक्षित और अपमानित महसूस करने लगे, तो सोचना होगा कि उस व्यवस्था को कहाँ तक वास्तविक और नैतिक आधारों पर लोकतंत्र कहा जा सकता है- क्योंकि सत्ता का वास्तविक स्रोत लोक है और वही वहाँ उपेक्षित और अपमानित है। यह सिर्फ कर्मचारियों के व्यवहार का ही नहीं लोकतंत्र को एक महाकाय यंत्र बना देने का परिणाम है।
लोकतंत्र है- लेकिन यदि उसका व्यवहारिक रूप गरिमा का दमन करता हो और मनुष्य को एक चेतनासंपन्न स्वतंत्र व्यक्तित्व समझने की बजाए उसके साथ संवेदनहीन व्यवहार करता और उसे एक यंत्र का पुर्जा बना डालने पर जोर देता हो तो उसके कारणों को समझना और उसके निराकरण की दिशा में सचेष्ट होना हमारी राजनीति की एक वांछनीय अनिवार्यता होनी चाहिए।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.