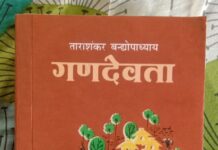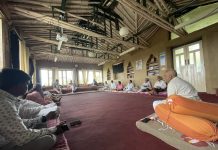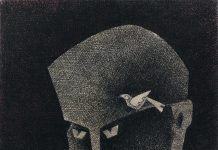— अरमान अंसारी —
हाल में मेधा का काव्य संग्रह ‘राबिया का ख़त’ राधाकृष्ण प्रकाशन से छपकर आया है। संग्रह का शीर्षक राबिया का ख़त अपने आप में अनूठा है। राबिया अल-बसरी मध्यकालीन अरब की सुप्रसिद्ध सूफ़ी साधिका थी। सामाजिक हैसियत गुलाम की थी और दुनिया के सौंदर्य के मानदंडों पर कुरूप। राबिया जन्नत के लोभ और दोज़ख़ के डर से ईश्वर की वंदना नहीं करती थीं बल्कि उनका ईश्वर के प्रति विशुद्ध प्रेम था। ऐसी राबिया को अपने काव्य संग्रह का शीर्षक देना स्त्री के मूल में स्थित प्रेम को अभिव्यक्ति देना व स्थापित करना है।
मेधा अपने काव्य संग्रह की भूमिका में कई महत्त्वपूर्ण संकेत देती हैं। अपने शुरुआती दौर में मेधा रिल्के के विचारों से प्रभावित हो जाती हैं, जिसमें रिल्के एक युवा कवि को पत्र लिखते हैं, जब तक ये न लगे कि लिखे बिना तुम मर जाओगे, तब तक मत लिखना। वे कहती हैं दशकों तक कविता लिखे बिना ही जीवन चलता रहा, उस जीने में मर जाने जैसा अनुभव था। वे कविता लिखने को खुद से साक्षात्कार मानती हैं। मेधा के इस संग्रह की पहली कविता है ‘चाँद की मटकी’। चाँद रूपी प्रतीक का आकर्षण बच्चों से लेकर प्रेमी-प्रेमिकाओं तक का रहा है। मेधा की इस कविता की खूबसूरती यह है कि इन्होंने चाँद रूपी प्रतीक का परंपरागत प्रयोग नहीं किया है। वे ‘चाँद की मटकी’ लेकर अनंत की यात्रा पर जाने की बात करती हैं, एक ऐसी यात्रा जिस पर निकलने के बाद कोई रोकना चाहे भी तो नहीं रोक सकता। इस यात्रा में मेधा अकेले नहीं जाती हैं उनके साथ, उनके भीतर हैं, उर्मिला, यशोधरा और रत्ना भी।स्वयं कवयित्री कहती हैं : “चाँद की मटकी माथे पर रख एक रोज़ निकल पड़ूँगी मैं आसमान की अनंत यात्रा पर/और उस घड़ी तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुक सकूँगी कि मेरे भीतर मैं ही नहीं, उर्मिला, यशोधरा और रत्ना भी रहती हैं।” इस यात्रा की प्रक्रिया में कवयित्री जानती हैं अपनी हद को – “जानती हूँ मैं कि तुम्हारे भीतर न तो सीता जितना समर्पण है न ही प्रेम/ सावित्री सा साहस भी कहां है तुममें।” जिन महिला प्रतीकों का इस्तेमाल कवयित्री ने किया है वे सदियों से भारतीय जनमानस में रचे-बसे हैं। इनका इस्तेमाल भारतीय जनमानस अपने हिसाब से समय-समय पर करता रहता है। इन पात्रों की सीमाएं और सम्भावनाएं दोनों हैं।

संग्रह की दूसरी महत्त्वपूर्ण कविताओं में से एक है ‘कितनी छोटी है कविता’। दरअसल यह कविता दो अलग-अलग स्थितियों में पली-बढ़ी लड़कियों और उनके संघर्ष की है। एक की अपनी काव्यगत साहित्यिक महत्त्वाकांक्षाएं हैं, और दूसरे की चूल्हा जलाने,अपने परिवार के पेट की आग बुझाने की है।पानी से गीला हो चुका चूल्हा है कि जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस कविता में एक जद्दोजहद है जिन्दगी की, आखिर साहित्य का लक्ष्य भी तो जीवन ही है। अपनी कविता की आखिरी पंक्तियों में कवयित्री द्वारा ‘कविता’ छोटी पड़ जाने का स्वीकार’ उन्हें बड़ा कवि बना देता है। “मेरी चिंता है एक अच्छी कविता लिखे जाने की/ और उसकी चिंता है चूल्हा जलाने की/ रोटी सेंकने की पूरे घर को तृप्त करने की/ कितनी कोमल है उसकी चिंता/ मैं लिख रही हूँ कविता वह सेंक रही है रोटी/धुएँ में सनी उसकी आँखों के सामने/ बौनी पड़ जाती है मेरी कविता/ धुएँ और आग से जूझती उसकी जिंदगी के सामने कितनी छोटी है मेरी कविता।”
कवयित्री की एक अन्य कविता है ‘प्रतिरोध’, यह प्रतिरोध एक स्त्री का प्रतिरोध है जो पुरुषवादी मानसिकता के विरुद्ध है।पुरुष को केवल दिखाई देता स्त्री का शरीर और उसके शरीर का भूगोल। लेकिन स्त्री है कि अपनी प्रसव पीड़ा से जन्म दे रही है करुणा और क्षमा को। वह आह्वान करना चाहती है देखने के नए नजरिये को, जिससे देखा जा सके स्त्री को उसके शरीर से परे भी। एक मानव व इंसान के रूप में। वह करुणा को बीज के रूप में देना चाहती है जिससे उसकी फसल लहलहा सके, करुणा का विस्तार हो सके : “सौंप दूँ तुम्हें इस उम्मीद में कि तुम कर सकोगे इस बीज-बूँद से करुणा की खेती/ और एक दिन लहलहाएगी तुम्हारे अंतर में करुणा की फसल/ और कुछ हो न हो, यह लहलहाती फ़सल तुम्हारी चेतना को ले जाएगी देह के भूगोल के पार।” इस कविता में स्त्री विमर्श का एक नया वैकल्पिक रूप दिखाई पड़ता है।
एक दूसरी कविता ‘स्त्री’ में, मेधा का प्रचलित और चलताऊ स्त्री विमर्श दिखने लगता है। वे पुरुष को दंभी, वहशी, अहंकारी, वर्चस्ववादी, प्रेम द्रोही जैसी संज्ञा से सम्बोधित करती हैं। स्त्री विमर्श का यह रूप अपने आप में कोई नया नजरिया पेश नहीं करता उलटे पुरुष को दुश्मन व नकारात्मक चरित्र के रूप में स्थापित करता है। वे कहती हैं : “पुरुष के पास अहंकार का तम था। वर्चस्व की ताक़त। उसने प्रेम के नाम पर वही दिया, जो उसके पास था। स्त्री के पास करुणा का उजास था और क्षमा का आकाश। स्त्री ने भी वही दिया जो उसके पास था। और वह आगे बढ़ गई अपने उजास और आकाश के साथ।”
गांव को देखने के कई नजरिये हैं। कुछ लोग गाँव को रोमानी दृष्टि से देखते हैं तो कुछ लोग गाँव को तमाम समस्याओं की जड़ मानते हैं। गांव के संदर्भ को लेकर ‘राबिया का खत’ संग्रह में दो कविताएं हैं : ‘अंदर वह गाँव’ और ‘ मेरा गाँव’। कवयित्री इन दोनों कविताओं में गाँव को समझने और समझाने की कोशिश करती नज़र आती हैं। उन्हें ‘ठाकुर का कुआँ’ ,’पूस की रात’ और ‘कफ़न’ वाले गाँव याद हैं। वहीं उनके अंतर्मन में बसा हुआ वह गाँव भी याद है जिसे उन्होंने बचपन में टुन्ना साह की चाय की दुकान पर गुलगुले की मिठास के साथ पाया है। वे कहती हैं : “मेरा यह गाँव मेरी साँस है उजास है इसके रूमान से ही शेष है, जीवन में रोमांच।” वहीं गाँव के संबंधों पर दूसरी कविता में गाँव के जीवन का वर्णन मिलता है जहाँ सहजता, सरलता और सरसता जैसे मूल्य हैं। मेधा ‘परवीन शाकिर की मौत पर’ पर श्रद्धाजंलि देना नहीं भूलती हैं। अपनी कविता में उन्हें योद्धा के रूप में रेखांकित करती हैं जिसने नियति के फैसले को चुनौती दी।
संग्रह में ‘बेटी’ शीर्षक से छह कविताएं हैं। इन कविताओं में एक माँ की असीम ममता उमड़ती-घुमड़ती दिखाई पड़ती है जिसकी अभिव्यक्ति बेटी के पूर्व और उसके इस दुनिया में आ जाने के बाद जीवन में हुए बदलाव को रेखांकित करती है। संग्रह में कुछ लोकरंग में रची-बसी कविताएं मिलती हैं, इनमें ‘फगुआ पवन’ एक है। चैत माह में पड़नेवाला फगुआ अरसे से समाज को अपने रंग में रंगता रहा है। मेधा की कविता में उस परंपरा में मनःस्थितियों का चित्रण दिखाई पड़ता है।
संसद द्वारा नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया था।इस कानून को लेकर देशव्यापी आंदोलन हुए। इनमें सबसे चर्चित आंदोलन शाहीन बाग का था। इस आंदोलन की गूँज दुनिया भर में सुनाई पड़ी थी। मूलतः यह आंदोलन महिलाओं द्वारा आयोजित व संचालित था। इसकी केंद्रीय भूमिका में मुस्लिम महिलाएं थीं। जिनके बारे में कई तरह की अफवाहें व भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। मेधा के संग्रह में ‘उम्मीद का एक सितारा – शाहीन बाग़ ‘ नाम की कविता है। यह कविता मूलतः आजादी के आंदोलन और उसके सपने की याद दिलाती है। प्रकारान्तर से यह रेखांकित करने की कोशिश करती है कि मुल्क लोगों से बनता है, लोग हैं जो सदियों-सदियों से साथ रहते आए हैं। लोगों ने नफरत की हर दीवार को गिराया है। सत्ता है कि भेदभाव की नई दीवार बनाना चाहती है। शाहीन बाग़ के आंदोलन ने संविधान और समाज को जिंदा किया है। मेधा कहती हैं : “एक सितारा जगमगाता है ‘शाहीन बाग़’/शाहीन बाग़ से अब भी उम्मीद कायम है/ इस मुल्क की औरतें बनाएगी एक नया मुल्क जहाँ जमीनों की हदें भले ही हो/ दिलों की कोई हद न होगी/ जहाँ गुलों में रंग होंगे तो गालों पर गुलाल भी।” कवयित्री की इच्छा है “क्या ही अच्छा होता कि दुनिया भर की औरतें तब्दील हो जातीं शाहीन बाग़ की औरतों में, और सारी दुनिया बन जाती शाहीन बाग़–’हर जुल्म से टक्कर लेती समता-समानता की नई पौध उगाती-दुनिया।” इस संग्रह कविताओं में और बहुत सारी महत्त्वपूर्ण कविताएं हैं- ‘ईश्वर’, ‘साल का विदा होना’, ‘नियति एक पेड़ की’, ‘मुक्ति’, ‘अभी भी वक़्त है’, ‘मिलन’, ‘विरह’, ‘दुआ’। संग्रह की अंतिम कविता है ‘नया छंद’ जिसमें निर्बाध जीवन और भय के अंत, सहजता और आनंद की कल्पना है।
कवयित्री की यह पहला ही काव्य संग्रह है भले वे कविता काफी पहले से लिखती रही हों। इस लिहाज से संग्रह की कविताओं में भाव व विचार में सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश दिखाई पड़ती है। शिल्प और संवेदना दोनों ही धरातल पर कविता गहरे उतरने की मांग करती है। रामचन्द्र शुक्ल से शब्द उधार लेकर कहें तो कविता हृदय की मुक्तावस्था की अभिव्यक्ति है और मेधा इस अभिव्यक्ति की कोशिश में नजर आती हैं।
किताब : राबिया का ख़त (कविता संग्रह)
कवयित्री : मेधा
प्रकाशन : राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
ईमेल : [email protected]
मूल्य : 299 रु.
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.