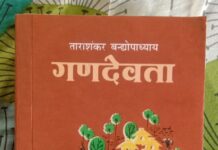— हिमांशु जोशी —
पुस्तक का आवरण अनुप्रिया द्वारा तैयार किया गया है। आवरण चित्र पुस्तक के नाम से मेल खाता दिखता है और पाठकों का ध्यान खींचने में सक्षम है। इसे देख लगता है कि पुस्तक में महिलाओं के विषय में कुछ खास लिखा गया है। पिछले आवरण में सम्पादकों के बारे में लिखा गया है। किताब की शुरुआत में ‘कस्तूरी’ से यह जानकारी मिलती है कि यह किताब कस्तूरी मंच द्वारा आयोजित श्रृंखला ‘फिल्में जो सहेजनी हैं’ में हुई परिचर्चा का संकलन है।
चन्द्रकला त्रिपाठी ने बड़े ही विस्तृत तरीके से किताब की भूमिका लिखी है और इसे पढ़ पता चलता है कि किताब में फिल्मों पर लिखे उन्नीस आलेख हैं। यहां हम समझते हैं कि यह किताब सिनेमा की क्षमता और सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप के आयाम लेकर पुरानी व नई फिल्मों पर जरूरी बात करती है।

चार शुभकामना सन्देशों के बाद किताब का सम्पादकीय दिखाई देता है। गुलजार की पंक्तियों से शुरू हुए सम्पादकीय में लिखा है कि समानांतर सिनेमा ने स्त्री को खुला आकाश दिया है जिसमें आज स्त्रियों की मुक्त भावनाएं अपनी उड़ान भर रही हैं। हिंदी सिनेमा के माध्यम से स्त्री की इन्हीं उड़ानों को देश के विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से सुसज्जित महत्त्वपूर्ण विचारों में संकलित किया गया है, जो इस पुस्तक में देखने को मिल रहा है।
किताब समाप्त करने पर पाठक सम्पादकीय की इन पंक्तियों से स्त्रियों की उड़ान को करीब से समझने में कामयाब हो जाएंगे।
किताब का पहला आलेख साल 1960 में आयी फिल्म ‘मुगल-ए-आजम’ पर लिखा गया है, जिसका शीर्षक बड़ा आकर्षक है। विजय पण्डित के लिखे इस फिल्मी सफर को पढ़ते हुए पाठक एक फ़िल्म के निर्माण की यात्रा में पूरी तरह से खो जाते हैं।
संवादों की जानकारी बड़े ही रोचक तरीके से लिखी गई है। जैसे ‘जब अनारकली कहती है- मुझसे मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे- तो दर्शकों की पीठ पर पसीना उतर आता है।’ आलेख में शामिल ‘प्रेमनिघण्टु’ जैसे शब्द पढ़ते किताब का कद ऊंचा लगता है।
‘तोड़ के बंधन बांधे पायल’ आलेख साल 1965 में आयी फ़िल्म गाइड पर लिखा गया है। किताब पढ़ते हम 1960 के बाद आयी फिल्मों के बारे में पढ़ते हैं, 2022 में लगभग सत्तर साल पहले के सिनेमा को समझना फ़िल्म से लगाव रखने वाले पाठकों के लिए बेहतरीन अनुभव होगा।

निर्देश निधि ने ‘गाइड’ बनने की कहानी लिखने से आलेख की शुरुआत की है। इसके निर्देशन के किस्से से पता चलता है कि फिल्में देश की सांस्कृतिक छवि से कैसे जुड़ी हुई होती हैं। ‘गाइड’ पर लिखा यह आलेख तब की फिल्मों में स्त्रियों की छवि को लेकर महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है।
पृष्ठ 40 पर लिखी पंक्ति ‘शैलेंद्र राजकपूर के खेमे के थे, वे देव आनंद की फ़िल्म के लिए गीत नहीं लिखना चाहते थे’ वर्षों से बॉलीवुड के बंटे होने की जानकारी देती है।
‘सत्यम शिवम सुंदरम’ पर लिखा आलेख मुख्य रूप से इस फ़िल्म के गीतों पर केंद्रित है। इस आलेख के बाद किताब में साल 1975 में आयी तीन फिल्मों ‘अभिमान’, ‘आंधी’ और ‘दीवार’ पर लिखे आलेख शामिल किए गए हैं। ‘अभिमान’ पर लिखे आलेख में डॉ लक्ष्मी शर्मा ने फ़िल्म को पितृसत्ता के चोटिल अहंकार पर केंद्रित बताया है। पृष्ठ 53 की ‘पचास वर्ष पहले बनी अभिमान का विषय भले ही आज के संदर्भ में बेहद सामान्य रह गया हो’ पंक्ति से समाज में महिलाओं की बदली हुई स्थिति का पता चलता है।
फ़िल्म ‘आंधी’ पर लिखे आलेख में शुरुआती पंक्तियां ही फ़िल्म का खाका पाठकों के सामने स्पष्ट कर देती हैं। आलेख की खासियत यह है कि सुधा उपाध्याय ने इसे संदर्भ के साथ लिखा है।
किताब में फ़िल्म ‘दीवार’ पर शामिल आलेख जितेंद्र श्रीवास्तव द्वारा वर्ष 2015 में दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में दिया गया व्याख्यान है। इस आलेख में अमिताभ के अमिताभ बनने की कहानी को लिखा गया है। अमिताभ को इंदिरा गांधी की राजनीति से जोड़े जाना फ़िल्म और देश की राजनीति के बीच के सम्बन्ध को दर्शाता है। पृष्ठ 74 पर नायक और कवियों की तुलना किताब का आकर्षण है।
संतोष गोयल द्वारा फ़िल्म बाजार पर लिखा आलेख ‘सो यास-ए-लहू में नहाकर चले’ किताब के शीर्षक से न्याय करता जान पड़ता है। बाजार फ़िल्म पर लिखते संतोष ने पितृसत्तात्मक समाज की कलई खोली है। ‘औरत का चेहरा दुनिया भर में एक-सा है’ पंक्ति, इसका प्रमाण है। आलेख के अंत में लड़कियों की स्थिति को लेकर पूछा गया प्रश्न पाठकों के हृदय को कुरेद देगा।
1982 में आयी फ़िल्म ‘अर्थ’ पर लिखे आलेख में उर्मिला शुक्ल द्वारा फ़िल्म में नारी के चित्रण पर लिखा गया है। उषा दशोरा का ‘प्रेम रोग’ पर लिखा आलेख साल 1982 और 2022 के बीच महिलाओं की बदली हुई स्थिति की तुलना करता है।
पृष्ठ 100 पर आयी पंक्ति ‘निर्देशक राजकपूर जिस मुहाने पर हमें छोड़ते हैं उससे आगे बस काजल बचाकर रोने का हुनर ही हमारे पास आया’ पढ़ते यह महसूस होता है कि आज इतने सालों बाद भी महिलाओं की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली।
1983 में आयी फ़िल्म ‘मासूम’ पर लिखे आलेख की पंक्ति ‘फ़िल्म में शबाना आजमी को अपने पति नसरुद्दीन को तैयार करते, पति के लिए चाय बनाते दिखाया गया है। एक पुरुष प्रधान समाज में इन दृश्यों से बहुत फर्क पड़ा’ इस बात का उदाहरण है कि समाज में फिल्मों का गहरा प्रभाव पड़ता है।
निवेदिता दिनकर का फ़िल्म ‘उत्सव’ पर लिखा आलेख पढ़ते हुए आपको इस फ़िल्म को देखने की तीव्र इच्छा होने लगेगी। निर्देशक और निर्माता के बारे में बड़े ही निराले अंदाज में लिखा गया है। कलाकारों, गीत संगीत के बारे में पढ़ना भी अस्सी के दशक में पहुंचा देता है। ‘स्त्री’ को कलाकार की प्रेरणा बता लेखिका ने पाठकों को स्त्रियों का महत्त्व बताने की कोशिश की है।
रश्मि रविजा द्वारा फ़िल्म ‘लज्जा’ पर लिखे आलेख का शीर्षक ‘कौन शहर कौन डगर तू चली कहाँ’ है, यह भी हर आलेख के शीर्षक की तरह आकर्षक है और पाठकों का ध्यान खींचने में सक्षम है। आलेख में फ़िल्म ‘लज्जा’ में स्त्रियों से जुड़े हर मुद्दे उठाने के बारे में लिखा गया है। पृष्ठ 138 पर ‘रामदुलारी’ के बारे में जो भी लिखा है वह आज भी घटित हो रहा है और रश्मि ने इसे फ़िल्म के साथ जोड़कर इस किताब की यात्रा को कभी न भूलने वाला बना दिया है।
सम्पादकों ने किताब के लिए ऐसी फिल्मों का चुनाव किया है जिन फिल्मों ने समाज में नारी को लेकर कुछ न कुछ विशेष दिखाया और सिखाया। इन फिल्मों पर लिखे आलेख पढ़ पाठकों को भारतीय नारी की बदलती सामाजिक दशा के बारे में भी जानकारी मिलती रही। प्रज्ञा पाण्डेय की साल 2019 में आयी बदला फ़िल्म पर लिखे आलेख में ‘नैना टॉप क्लास की बिज़नेस वुमन है’ पंक्ति इसका उदाहरण है।
पाठकों को यह किताब पढ़ते हुए भारतीय सिनेमा और उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में जो जानकारी मिलती है, उससे यह स्पष्ट होने लगता है कि कुछ फिल्मों में महिलाओं की स्थिति ठीक वैसी ही दिखाई गई जैसी उस समय के समाज में थी पर कुछ फिल्मों में उनकी स्वतन्त्रता पर इस तरह बात की गई जैसी उस समय के समाज में स्वीकार्य नहीं थी।
यह किताब शुरुआत से अंत तक पाठकों को बिल्कुल नीरस नहीं लगती।
चित्रा माली का संदर्भ सहित लिखा गया आलेख ‘स्त्री प्रतिरोध स्वर : सन्दर्भ हिंदी सिनेमा’ नारीवाद की दूसरी लहर और तीसरी लहर के उद्देश्यों के सिनेमा पर प्रभावों पर केंद्रित है। यह आलेख इस तथ्य को प्रमाणित कर देता है कि सिनेमा समाज को देखने का दर्पण है।
रक्षा गीता द्वारा लिखा गया आलेख ‘ऐतिहासिक फिल्मों में स्त्री अस्मिता’ इस महत्त्वपूर्ण किताब का अंतिम आलेख है।इसमें रक्षा ने 1983 में आयी ‘रजिया सुल्तान’ फिल्म का उदाहरण देकर यह समझाया है कि किस तरह फिल्मों में महिलाओं के सशक्त चरित्रों के साथ छेड़खानी कर पितृसत्ता को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है।
पुस्तक – कितनी गिरहें खोली हैं मैंने
सम्पादक – रश्मि सिंह, विशाल पाण्डेय
प्रकाशन- कलमकार पब्लिशर्स, फोन- 9310562856
मूल्य- 300 रुपए
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.