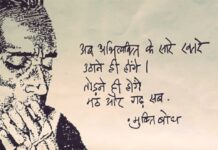— ध्रुव शुक्ल —
आजकल यही बात ज़्यादा चलती है कि सब अपनी विजय चाहते हैं, अपनी हार किसी को स्वीकार नहीं। सारे धर्म अपनी ध्वजा को, व्यापारी अपने मुनाफे को, नेता अपने अहंकार को, गुण्डे अपनी तलवार को, अफ़सर अपने रुआब को, अभिनेता अपने शबाब को, खिलाड़ी अपने छक्के को और मीडिया के लोग अपने हल्लाबोल को ऊंचा देखना चाहते हैं। कोई उस आदमी की तरफ़ देख ही नहीं रहा जो पीछे छूटता जा रहा है। वह अपनी उम्मीद बांधे तो आख़िर किससे?
लोकतंत्र के घोड़े से जनता को नीचे गिराकर सब उस घोड़े को किसी भटकी हुई दिशा में हांक ले जाना चाहते हैं। तरह-तरह के मतान्ध कपटवेशधारी धर्म,जात-पांत, लोभ और कट्टरता की दीवारें खड़ी करके लोकतंत्र के विनाश में भागीदार होकर गरज रहे हैं। बैर और हिंसा को बढ़ा रहे हैं। अपने ही देश के लोगों को अज्ञान की जड़ता में धकेलकर सब अपने-अपने विजयरथ दौड़ा रहे हैं जिनसे उड़ने वाली धूल की धुंध में देश अदृश्य होता जा रहा है।
देश में जीतने और हारने वालों का एक अलग तबका बन गया है जो जनजीवन को हराने पर आमादा है। कोई कैसे भी जीते, स्वार्थवश सब जीतने वाले एक हो जाते हैं और अपने बीच से किसी एक को अपना रिंग मास्टर चुनकर राजनीतिक इण्डियन सर्कस कंपनी चला रहे हैं। अपने-अपने राजनीतिक लालच के पिंजरों में क़ैद युवा चीते और बूढ़े शेर रिंग मास्टर की ग़ुलामी स्वीकार कर रहे हैं। यह खेल खत्म नहीं हो रहा बल्कि इसे तो लोकप्रिय बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कटाक्ष-क्रांति करने वाला समाज अन्याय के ख़िलाफ़ घर से बाहर निकलने में असमर्थ हो जाये, यही कुटिल उपाय करने में सब भ्रष्ट विजेता लगे हुए हैं।
महात्मा बुद्ध कह गये हैं कि अपने जीवन के आयतन को समझो। उससे बाहर न जाओ। अपनी तृष्णा को नाप सको तो इसी में सबकी ख़ैर है क्योंकि इसी से वह हवस पैदा होती है जो किसी को शान्ति से जीने नहीं देती। बुद्ध ने सम्यक वार्त्ता का उपदेश किया है और इस समय देश की वाणी इतनी बिगड़ी हुई है कि उसमें सम्यक संवाद कैसे संभव हो सकेगा?
—–
अकेली किताब के फड़फड़ाते पन्नों जैसा प्रेम
अक्सर उन पुस्तकों के बारे में सोचता हूं जो लम्बे समय तक प्रतीक्षा करती हैं कि कोई उन्हें पढ़े। पुस्तकें कल्पना में बसी उस प्रेमिका की तरह लगती हैं जिससे हमारा अपरिचय ही उसके करीब जाने को बार-बार विवश करता है। करीब आने से प्रिया ऐसे खुलती है जैसे कोई किताब खुल रही हो। प्रेम अकेली किताब के फड़फड़ाते पन्नों जैसा है। उसे एकान्त में थामने के लिए दोनों हाथ और उत्सुक आंखें चाहिए।
जीवन में किसी किताब का आना उस आईने जैसा है जिसमें हम अपनी छबि के अन्तरंग को देख पाते हैं। हमें वह किताब जीवन के उन अंधेरे कोनों में ले जाती है जहां हम कभी गये ही नहीं। जीवन में शब्दों का एकान्त जुगनुओं की झिलमिल जैसा है। हम जब अकेले चल रहे होते हैं तब सितारों की रौशनी के आभास में पगडण्डी दिखायी देती है। कहीं घने वृक्षों पर जुगनुओं का आलोक दिपदिपाता है। किताबें ऐसे ही आलोक से भरकर वाक्यों के बीच शब्दों की राह बनाती हुई हमारे करीब आती हैं।
किताबों से ही यह उम्मीद है कि रोज़-ब-रोज़ थोड़े-थोड़े बढ़ते जाते ॲंधेरे में वे बची रहेंगी और प्रेमिका की तरह किसी न किसी मोड़ पर मिल जाएंगी। वे उत्सुकता से हमारी ओर निहार रही होंगी। किताबों में जीवन की कविता की राहों का नक्शा है जिनके दोनों ओर बिना किसी अतिक्रमण के कहानियों की छोटी-छोटी बस्तियां और उपन्यासों के शहर बसाये जा रहे हैं। किसी चाय की गुमटी पर लेखक अकेला बैठा है। शब्दों में डूबीं स्मृतियां सबके द्वार खटखटा रही हैं।
—–
पुस्तक पढ़ने वाले तितली जैसे होते हैं
शहद को संचित करती मधुमख्खियों को देखकर लगता है कि बड़े धीरज से कोई पुस्तक लिखी जा रही है। जैसे पूर्वजों के स्तवनों से भरे बहुअर्थी शब्द एक-दूसरे के बहुत करीब आकर परस्पर आश्रय में किसी गहरी रसनिष्पत्ति के लिए तप कर रहे हों। यह तप पुस्तक के पाठक के पड़ोस में ही या कभी उसी के मकान के किसी ऊंचे छज्जे पर हो रहा है और हजारों शब्दों के बीच लेखक रानी मख्खी की तरह अदृश्य है। पाठक कृति के पकने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
किसी उपवन में बहुरंगे फूलों को देखकर लगता है कि वे बरन-बरन की कृतियों जैसे हैं और पाठक उन पर तितलियों की तरह ध्यान लगाये हैं। तितलियां एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर बैठ जाती हैं जैसे एक कृति का मर्म दूसरी कृति को बता रही हों। प्रसिद्ध शाइर अख़्तरुल ईमान की एक लम्बी नज़्म ऐसे ही शुरू होती है– ‘तितलियां फूल से फूल पर यों जाती हैं जैसे कोई बात हो जो कान में कहनी है अभी।’
फूलों के आसपास भन्नाते हुए काले भंवरे उन आलोचकों की तरह लगते हैं जो किसी नयी किताब को पढ़कर भनभनाते ज़रूर हैं पर उसके मर्म को उघार नहीं पाते। वे काले गुलाबजामुन की तरह अपने ही पनीले शीरे में डूबे रहते हैं। वे किताब में बसी शब्दों की भांति-भांति की मिठास को अक्सर पहचान ही नहीं पाते। जो कृति में बसे मर्म को पहचान पाते हैं उन्हें ये आलोचक अपनी व्यभिचारिणी बुद्धि के कारण साहित्य की बिरादरी से निर्वासित किये रहते हैं। अक्सर कुछ पाठक भी इन भनभनाते आलोचकों की कथनी में फंसकर श्रेष्ठ कृतियों को पहचान ही नहीं पाते।
अच्छे पाठकों को कृतियां नदियों जैसी लगती होंगी जिनमें वे अपनी नौका डालकर जीवन के बहुरंगी किनारों की थाह ख़ुद ही ले लिया करते हैं।
——

धरती पर बसे साहित्य देश का नागरिक कौन?
धरती को देखो तो लगता है कि सबका जीवन उन शब्दों में बसा हुआ है जिनका उच्चारण करके हम एक-दूसरे को इस धरती पर पुकारते हैं। जीवन के सारे रूप तो नामों में ही बसे हुए हैं। ये रूप शब्दों से ही अपना श्रृंगार करके न जाने कब से एक-दूसरे के करीब सौन्दर्य और प्रेम का डेरा डाले हुए हैं।
धरती साहित्य के देश जैसी लगती है। जैसे कोई असमाप्त महाकाव्य लिखा जा रहा हो। इस महाकाव्य को पढ़कर आत्मसात करने वाले पाठक ही साहित्य देश के नागरिक कहलाएंगे। इस साहित्य देश के विशाल हृदय की भूमि पर कोई गहरा जलाशय है जिससे काव्य-रसों से विभोर जीवन-कथाओं की नदियां बहती चली आ रही हैं। सारे नागरिक पाठक अपने-अपने स्वभाव के अनुरूप जन्म और मृत्यु के बीच बहते जीवन-जल का स्वाद लेकर तृप्त हो रहे हैं।
धरती पर शब्द इतने स्वाधीन हैं कि उन्हें सबका निवास स्थान माना गया है। शब्द आपस में मिलकर अपने आप कोई संकीर्तन रचते रहते हैं। वे बहुरूपी छंदों में साहित्य के इस बहुअर्थी देश को इसी तरह बसाये हुए हैं। वे अकथ कथाओं को भी ऐसे कह देने में समर्थ हैं कि भले ही कोई उन्हें पूरी न कह पाये पर वे हमारी रूह के अहसास में किसी भूली-बिसरी लोकधुन की तरह गूंजती रहती हैं। भले ही कोई किसी का द्वार न खटखटाये पर शब्द हमारी स्मृति के द्वार पर दस्तक देना कभी नहीं भूलते।
धरती पर इस साहित्य के देश को रचने वाले अकेले साहित्य-सर्जक इसे नहीं बचा सकते। इस देश को बचाये रखने के लिए वे पाठक मतदाता भी तो चाहिए जो इसके मर्म में पैठने की चाहत से सदा भरे रहते हैं। इंसानी बिरादरी ने राज्य व्यवस्था रचने का सपना इसी साहित्य देश में बसे प्रजातंत्र को बचाये रखने के लिए देखा था। अब यह उन पाठक मतदाताओं पर ही निर्भर है कि इस साहित्य देश के सामाजिक और राजनीतिक रचाव के लिए वे कौन-सी कृतियां चुनते हैं।
—–
अपने जीवन को कविता बनाना चाहिए
पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कविवर शिवमंगल सिंह सुमन की डायरी में सत्तर साल पहले यह वाक्य लिखा था — ‘अपने जीवन को कविता बनाना चाहिए।’ यह वाक्य नेहरू जी इसलिए लिख पाये होंगे क्योंकि उनकी ‘भारत की खोज’ भारत माता को एक लम्बी कविता की तरह पढ़कर उसका मर्म जानने की रही है। नेहरू विश्व इतिहास की झलक पाकर यह भी पहचान सके कि वहां तो खॅंडहरों के सूनेपन के बीच सितमगरों की समाधियों और कब्रिस्तानों के आसपास मुरझाये जीवन की दास्तान ही ज़्यादा सुनायी देती है। पर जीवन तो निरंतर रची जा रही कविता जैसा ही है।
जीवन कैसे कविता बनता है, यह प्रश्न केवल कवियों से ही नहीं, उन राजनेताओं से भी पूछा जाना चाहिए जो भारत के जीवन को भारत की कविता से दूर ले जाने में संलग्न हैं। सबका जीवन उस कविता के घेरे में ही रह सकता है जिसकी चौपाइयों में उज्ज्वल कमलनियां खिल उठती हैं। जिसमें बहुरंगी कमलों के समूह कई प्रकार के जीवन छंदों में बहुरंगी अनुभूतियों की तरह बसे रहते हैं। जहां भाषा की सुगंध पूरे जीवन पर छाने के लिए आतुर रहती है। अर्थ सौन्दर्य और भावों का पराग-मकरंद सबके मन पर फैलता ही रहता है। यह लम्बी कविता सदियों से पूरे जीवन की उपमा खोज रही है और कह रही है कि जीवन की कोई उपमा नहीं, गुण-अवगुण से सना जीवन तो जीवन की तरह ही है। ऐसे जीवन को परस्पर आश्रय में साधे रहने की कला को ही वास्तविक राजनीति कहा जायेगा।
जीवन को राजनीतिक हठों के किनारों से नहीं बांधा जा सकता। उसे बांधने की कोशिशें देश को विपदा के सागर तक लिये चली जाती हैं। बहुरंगी जीवन के स्वभाव के विरुद्ध उसकी नौका की राह रोकने वाली कोई भी राजनीति काल महासागर की लहरों पर कभी ठहर नहीं पायी है। इतिहास साक्षी है कि सागर उसे बहा ले गया।
कवि, कविता और समूचा जीवन उस अनादि प्रकृति के महाकाव्य में बसे हुए हैं जिसे सदा अर्थपूर्ण बनाये रखने के लिए सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना की जाती रही है। पर अगर समाज और राजनीति ही उससे बेपरवाह होते चले जायेंगे तो जीवन से वह काव्य तत्व खोता चला जायेगा जिसमें सुजल-सुफल से भरी ग्रामवासिनी भारत माता बसी हुई है। यह भारत माता ही वह महाकाव्य है जिसे पढकर और उसका मर्म जानकर सबका जीवन कविता बना रह सकता है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.