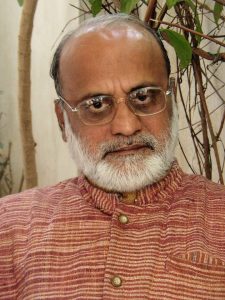— डॉ. सुरेश खैरनार —
26 सितंबर 1932 के दिन, आज से 92 साल पहले, ऐतिहासिक पूना पैक्ट पर एरवडा जेल के अंदर हस्ताक्षर हुए थे। हमेशा की तरह, इस समय भी उस पैक्ट को लेकर कुछ लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं।
मुख्यतः माननीय कांशीरामजी जब पुणे में डिफेंस की नौकरी के लिए कुछ दिनों के लिए रहे, उस दौरान उन्होंने जो भी अध्ययन किया, उसमें से उन्होंने आज से 92 साल पहले के ऐतिहासिक पूना पैक्ट को लेकर बाकायदा एक दलित मराठी भाषी प्रोफेसर और दलित साहित्य तथा जाति व्यवस्था पर मराठी में अधिकारिक रूप से चलते-फिरते संदर्भ ग्रंथ जैसे अध्ययन किए। मेरे मित्र ने मुझे खुद बताया कि “कांशीरामजी जब पूनावासी थे, तब वे दलित सवाल पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मेरे पास आते-जाते थे। एक दिन अचानक उन्होंने कहा, ‘आज मुझे मेरी राजनीति के लिए एक शत्रु मिल गया।’ मैंने पूछा, ‘कौन?’ तो उन्होंने कहा, ‘महात्मा गांधी।’ मैं सुनकर दंग रह गया और पूछा, ‘कैसे?’ तो उन्होंने कहा, ‘पूना पैक्ट।’ तब मैंने कहा, ‘डॉ. बाबा साहब अंबेडकरजी ने अपनी पत्रिका बहिष्कृत भारत के पहले ही अंक में प्रकाशित लेख में कहा है कि काश, महात्मा गांधी जी के साथ मेरे संबंध और पहले बने होते! मैंने तो सिर्फ 71 सीटों का आरक्षण मांगा था, लेकिन गांधीजी के आग्रह पर 148 सीटें मिलीं। यह तो दोगुने से भी अधिक है। और जिस तरह से उन्होंने संपूर्ण देश में अस्पृश्यता के खिलाफ जनजागृति मुहिम शुरू की है, यह ऐतिहासिक महत्व की बात है .
पुणे जेल से रिहा होने के बाद, महात्मा गांधी अस्पृश्यता से हिंदु समाज को मुक्त करने के लिए 12,500 मील लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने हिंदुओं से आग्रह किया कि “वे दलितो के विरुद्ध अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करें,” और उनसे निवेदन किया कि “वे नशीले पदार्थों और शराब का सेवन छोड़ दें।”
महात्मा गांधी जी की 12,500 मील से अधिक की हरिजन यात्रा के दौरान, जिस तरह से सार्वजनिक तालाब, कुएं और मंदिरों के दरवाजे दलितों के लिए खोले जा रहे थे, यह अस्पृश्यता के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था, जो सवर्ण समाज की पहल पर शुरू हुआ। इस आंदोलन ने एक बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत की.
भले ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने दलितों को गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने का नारा दिया हो, लेकिन आज भी बड़े संख्या में दलित गांवों में ही रहने के लिए मजबूर हैं। इसलिए सतत तनाव में रहते हुए गांव में अपनी ज़िंदगी बसर करना आसान नहीं होता। आखिरकार, मिलजुलकर ही रहना यही वास्तविकता है।
महात्मा गांधीजी ने इसे हमेशा पहचाना था। इसलिए उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ सतत अपनी भूमिका समय-समय पर निभाने की कोशिश की। यहां तक कि कांग्रेस के इतिहास में, पहली बार, उन्होंने 1920 में हुए नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, सामान्य प्रतिनिधि होते हुए भी, अस्पृश्यता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किया।
दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत के उनके सभी आश्रमों में, सभी जातियों, धर्मों और विभिन्न देशों के लोग साथ रहते थे। उन्होंने छुआछूत या अस्पृश्यता के खिलाफ काम किया। जिस जाति-व्यवस्था का आधार व्यवसाय था, उसमें बदलाव लाते हुए, उनके आश्रम में लोग खुद पाखाना साफ करने से लेकर मरे हुए जानवरों की चमड़ी निकालने के काम करते थे, जैसे कि कोकणस्थ ब्राह्मण अप्पासाहेब पटवर्धन। आजकल विजय दिवाण भी वह काम बखूबी कर रहे हैं।
महात्मा गांधी जी ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया था और उनके शादी में शामिल भी होते थे. डॉ. बाबा साहब आंबेडकर ने भी कहा है कि “जाति तभी समाप्त होगी जब आंतरजातीय विवाह होंगे।” यही जाति निर्मूलन के लिए सक्रिय कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है। अन्यथा, “जाति न मिटेगी” कहावत के अनुसार, जाति-व्यवस्था बनी रहेगी।
इसलिए मैंने इस लेख में बलराम नंदा की “गांधी और उनके आलोचक” और अंग्रेजी में प्यारेलाल द्वारा लिखित The Epic Fast इन दोनों किताबों का सहारा लिया है। बलराम नंदा की किताब के पृष्ठ 31 से 39 तक के “गांधीजी और जाति-प्रथा” नामक संपूर्ण अध्याय को पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ।
गांधीजी पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें से एक यह भी है कि उन्होंने जाति-प्रथा के पक्षधर के रूप में कार्य किया। कहा गया कि 1932 में किया गया उनका उपवास, अंग्रेजी सरकार द्वारा शूद्रों अर्थात अछूतों के पक्ष में की जा रही एक सकारात्मक कार्यवाही को रोकने के लिए था। तथ्य यह है कि सदियों पुरानी जाति-प्रथा की कमर तोड़ने और हिंदुत्व के माथे से अस्पृश्यता का दाग मिटाने के लिए गांधीजी से अधिक किसी ने प्रयास नहीं किया। यह एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है—जाति-प्रथा का उद्भव, इसके गुण और अवगुण, छुआछूत के विरुद्ध गांधीजी का जीवन पर्यंत संघर्ष, और 1932 में हिंदुओं की इस सामाजिक समस्या को भारतीय राष्ट्रीयता के विरुद्ध एक राजनीतिक हथियार बनाने की साम्राज्यवादी कोशिश।
वैसे तो जाति – प्रथा के आरंभ के बारे में विद्वानों में विवाद रहा है ! लेकिन आमतौर पर यह स्वीकार किया गया है ! ” मूल रूप में इसके व्यवसायगत चार प्रमुख विभाग थे ! और न तो वे अनिवार्यतः वंशानुगत थे, और न ही अपरिवर्तनीय ! इस प्रथा ने लगता है, एक ऐतिहासिक प्रयोजन सिध्द किया था ! कुछ अन्य उपमहाद्वीपो के विजेताओं की तरह ! भारतीय आर्यों ने स्थानीय आबादीयो को न मिटाया ! और न ही उन्हें गुलाम बनाया ! अपनी सर्वोच्चता कायम रखते हुए भी ! उन्होंने मूल निवासियों को एक सामाजिक ढांचे में बांधे रखने का प्रयास किया !
यह जाति – प्रथा के कारण ही संभव हो सका ! “कि उत्तर – पस्चिम से आंक्रमणकारियों, और अप्रवासियो की निरंतर आती लहरें अपनी विशिष्ट पहचान खोए बिना भारतीय समाज में अपना स्थान बना सकी ! राजनीतिक उथल-पुथल के समयों में जाति – प्रथा ने हिंदु समाज को एक निश्चित लचीलापन प्रदान किया और करोडो लोग, शासक, राजवंशों और उनके परिजनों के साथ जो कुछ बीता उससे बेखबर अपना जीवन जीते रह सके ! पर, समय के साथ इस प्रथा में अत्यांतिक रुढता आ गई और यह पूरी तरह वंशानुगत बन गया ; अनेक प्रकार के निषेध और कर्मकांडीय भावना से जुड़े विचार इसमें प्रवेश कर गए ! फलतः जो वर्ग इस सामाजिक भवन की तली में थे वे हीन अत्याचारों के और भेदभाव के शिकार बन गए !
सफाई से लेकर कारागिरी तक के निम्न कार्यो में लगे ‘अंत्यजो ‘की दशा विशेष रूप से दारुण हो गई ! मध्य युग में बसवेश्वर, तुकाराम, गोरखनाथ, नानकदेव, कबीर और चैतन्य जैसे संतो ने और उन्नीसवीं सदी में ज्योतिबा फुले, आंबेडकर, रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार जैसे समाज – सुधारको ने करुणावश इनकी और ध्यान दिया ! लेकिन कट्टरपन की जड़ें इतनी गहरी थी कि उन्हें आसानी से हिलाया नही जा सकता था ! अतंतः जाति – प्रथा की कट्टरता और छुआछूत की बुराईयों के सदियों पुराने जंजाल में फंसे, हिंदुत्व को झकझोर कर बाहर निकालने का काम गांधीजी के जिम्मे आया !
गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है कि कैसे उनके अपने घर में छुआछूत से उनका सामना हुआ। जैसा कि वैष्णव हिंदुओं में सामान्य जातिगत भेदभाव का प्रचलन था, उनकी माता भी इसे मानती थीं। गांधीजी एक आज्ञाकारी बालक थे, लेकिन इन निषेधों पर वे प्रकट रूप से बिदकते थे, उस छोटी आयु में भी। उन्हें छुआछूत की प्रथा में और रामायण के उस मनोहारी प्रसंग में, जिसमें उन्होंने सुना था कि “नायक राम को एक दलित जाति के केवट ने गंगा के पार उतारा,” उन्हें एक असंगति दिखाई देती थी। जैसे-जैसे वे बड़े होते गए, दलितो के प्रति मित्रता की भावना उनमें बढ़ती गई। दक्षिण अफ्रीका में, सभी वर्गों और समुदायों के लोग उनके सहयोगी बने।
1915 में भारत वापस आने के बाद, अहमदाबाद में जो पहला आश्रम उन्होंने स्थापित किया, उसमें एक दलित परिवार को भी रखा। इस बात पर अहमदाबाद के वे धनी व्यापारी बिगड़ उठे, जो आश्रम के लिए धन दे रहे थे। विरोध में कुछ सहयोगी भी साथ छोड़कर गए थे। धन चुक गया, और आश्रम में भी थोड़े लोग रह गए, जो अब तक उनके साथ जुड़े थे। गांधीजी ने सोचा कि “अहमदाबाद की गंदी बस्तियों में जाकर रहा जाए!” तभी एक गुमनाम दानी ने उनके इस विचार को अनावश्यक बना दिया।
दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद, पहले चार वर्षों के दौरान, जब गांधीजी राष्ट्रीय राजनीति के किनारे पर थे, उन्होंने छुआछूत की बुराई के विरुद्ध निरंतर प्रचार किया। इस सुधार को उन्होंने अपने 1920-22 के राजनीतिक अभियान में एक मुद्दा तक बनाया। तीसरे दशक में, अपनी देशव्यापी यात्राओं के दौरान, अपने भाषणों में छुआछूत का बार-बार उन्होंने जिक्र किया। 1931 में लंदन की गोलमेज परिषद में, “यह देखकर उन्हें दुख पहुंचा कि दलित के प्रतिनिधि, प्रतिक्रियावादी, सांप्रदायिक और राजनीतिक तत्वों के हाथों में खेल रहे हैं,” जैसा कि मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के साथ किया गया। दलितो को भी एक पृथक चुनावी समुदाय के रूप में तोड़कर अलग किए जाने का उन्होंने विरोध किया। इस विषय पर उनके विचार कितने दृढ़ थे, यह उस भाषण से प्रकट होता है जो उन्होंने 13 नवंबर 1931 को अल्पसंख्यक समिति की बैठक में दिया था।
” दलितो की विशाल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अपने निजी रूप में करने का दावा मैं करता हूँ। यहाँ मैं सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ही नहीं, बल्कि अपने निजी पक्ष से भी बोल रहा हूँ। मैं दावा करता हूँ कि यदि दलितों का जनमत लिया जाए, तो मैं उनका मत प्राप्त करूंगा और सर्वाधिक मत मुझे ही मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे रजिस्टर और जनगणना में दलितो को एक अलग वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाए। सिख भले ही सिख रहें, मुसलमान मुसलमान रहें, और यूरोपीय यूरोपीय रहें, पर क्या दलित सदा के लिए अछूत ही बने रहेंगे?” यह महात्मा गांधीजी का दलित समस्याओं को एक मां की ममता से देखने का दृष्टिकोण है, जिसे कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अनदेखा कर, गलत तरीके से व्याख्या करते हैं।
महात्मा गांधीजी के मन में अस्पृश्यता को खत्म करके, छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन करते हुए, समस्त दलित समाज को हिंदुओं के बराबरी में शामिल करने का संकल्प था। अन्यथा, छुआछूत के साथ ही जैसे मुसलमान, सिख और ईसाई अपने-अपने धर्मों में बँटे हुए हैं, उसी तरह समस्त दलित समाज भी हिंदू धर्म से टूटकर अलग हो जाएगा। छुआछूत तो बनी रहेगी, लेकिन भविष्य में इस अलगाव से भारत में और विभाजन होंगे। और ऐसे में, भारत के कितने और पाकिस्तान बनेंगे? इस दूरदर्शिता के कारण, उन्होंने अपने जीवन के 63वें साल में अपने प्राणों की आहुति तक देने का संकल्प लिया था।
मार्च 1932 में, जब गांधीजी जेल में थे, तब उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को उस सांप्रदायिक निर्णय के संबंध में एक पत्र भारत सचिव सर सैम्युअल होर को लिखा था, जिसके द्वारा नए संविधान के अंतर्गत विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व की संख्या और विधि निर्धारित की गई थी। उन्होंने होर को बताया, “पृथक चुनाव क्षेत्रों से अछूतों का कोई भला नहीं होगा, बल्कि इससे हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा।” जैसा कि उन्होंने लंदन में कहा था, वही बात उन्होंने पुनः याद दिलाई। उन्होंने कहा था, “दलित वर्गों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र बनाए जाने का वे अपने जीवन की कीमत पर भी विरोध करेंगे।” गांधीजी ने लिखा, “यह बात क्षणिक भावुकता में अथवा वाक्पटुता के रूप में नहीं कही गई थी।”
जब 17 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रकाशित हुआ, तब गांधीजी का डर सही साबित हुआ। दलित वर्गों को दुहरे मताधिकार दिए गए थे – एक उनके निजी पृथक चुनाव क्षेत्रों में और दूसरा आम (हिंदू) चुनाव क्षेत्रों में। लेकिन तथ्य यह रहा कि इन वर्गों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र बनाए जाने थे।
गांधीजी ने तत्काल ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड को लिखा कि “उन्होंने आमरण उपवास का निश्चय किया है!” यह उपवास तभी तोड़ा जाएगा जब इसके दौरान ब्रिटिश सरकार या तो अपने विवेक से, या लोकमत के दबाव से अपना फैसला बदल देगी और दलित वर्गों के लिए जातिगत (पृथक) चुनाव क्षेत्र बनाने की अपनी योजना वापस ले लेगी। “उन्हें जेल से छोड़ देने की स्थिति में भी, उपवास जारी रहेगा।” तीन सप्ताह बाद रैम्से मैकडोनाल्ड ने गांधीजी के पत्र का जवाब दिया और सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि “यह विरोधी दावों को न्यायसंगत रूप में संतुलित करने का प्रयास है।”
ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार गांधीजी के भावनात्मक और धार्मिक दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ रहे। उन्हें लगा कि इस उपवास के पीछे एक राजनीतिक लक्ष्य छिपा है। उन्हें संदेह हुआ कि “सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता से गांधीजी की प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा था, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए यह उनकी एक चाल है।”
ब्रिटिश मंत्रीगण इस विषय पर गांधीजी की भावनाओं की गहराई को समझ नहीं सके। इससे भी अधिक यह कि “जिसे वे एक राजनीतिक समस्या मान रहे थे, उसके समाधान के लिए उपवास करने की नैतिकता को वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए।” (मेरा आकलन है कि ब्रिटिश शासन, गांधीजी की अंग्रेजों की ‘बांटो और राज करो’ की नीति के कारण, सबसे पहले मुसलमानों, फिर सिखों और तथाकथित यूरोपीय लोगों को 1857 के बाद अलग-अलग तरह से इस्तेमाल कर रहा था। अब 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की आड़ में अस्पृश्यों को भी शामिल कर, भारत के कम से कम चार से पांच हिस्सों में विभाजन की नींव डालने की कोशिश कर रहा था।
इस नीति को लागू करते हुए, महात्मा गांधी के उपवास को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा था। यह मेरी राय है – डॉ. सुरेश खैरनार)। ब्रिटिशों को गांधीजी का उपवास एक प्रकार की जोर-जबरदस्ती का छद्म रूप प्रतीत हुआ। गांधीजी के उपवासों पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया को डेविड लो ने अपने कार्टून ‘1933 की भविष्यवाणी’ में बेहतरीन तरीके से चित्रित किया था। इसमें भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंग्डन को भूख हड़ताल पर बैठते हुए दिखाया गया था, क्योंकि 10 डाउनिंग स्ट्रीट का आदेश था कि ‘गांधीजी को नया संविधान स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए।’
क्या उपवास जोर-जबरदस्ती का एक तरीका था? गांधीजी जानते थे कि उनके उपवासों से एक नैतिक दबाव पैदा होता है, लेकिन वह दबाव उनसे असहमत होने वालों पर नहीं, बल्कि उन पर अधिक पड़ता था, जो उनसे प्रेम करते थे और उन पर आस्था रखते थे। वे उन लोगों की आत्मा में पीड़ा उत्पन्न करना चाहते थे और एक अमानवीय सामाजिक अन्याय के कारण अपनी व्यथा उन तक पहुंचाना चाहते थे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनके आलोचक भी वैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे जैसी उनके मित्र और सहकर्मी करते हैं। उनका विश्वास था कि यदि उनका आत्मबलिदान भारत के उन करोड़ों लोगों के सामने, जिनसे वे एकात्म हो चुके थे, उनकी सच्चाई को प्रदर्शित कर सका, तो आधी से अधिक लड़ाई तो जीत ही जाएगी।
एक बार, अमेरिकी मिशनरी ई. स्टेनली जोन्स ने यरवदा जेल में गांधीजी से पूछा: “क्या आपका उपवास जोर-जबरदस्ती का एक रूप नहीं है?” गांधीजी का उत्तर था: “हाँ, है; यह वैसी ही जोर-जबरदस्ती है, जैसे जीसस सलीब से आपके ऊपर करते हैं।” उपवास, सलीब को माध्यम बनाकर मुद्दे को स्पष्ट करने का एक प्रयास है। हालांकि यह प्रकट रूप से तर्क को दबाने जैसा लगता है, पर वास्तव में इसका लक्ष्य उस जड़ता और पूर्वाग्रह को मिटाना है, जिसने सदियों से हिंदू समाज को एक कुत्सित सामाजिक अन्याय सहने के लिए बाध्य किया है।
इस समाचार ने गांधीजी के उपवास करने के निर्णय को एक कोने से दूसरे कोने तक पूरे भारत में हिला दिया। 20 सितंबर 1932, जिस दिन उपवास आरंभ हुआ, देश में उपवास और प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया गया। शांतिनिकेतन में, रविंद्रनाथ ठाकुर ने काले कपड़े पहनकर एक विशाल जनसमूह के सामने उपवास पर और युगों पुरानी कुप्रथा के विरुद्ध लड़ने की आवश्यकता पर भाषण दिया। भावना का एक सहज ज्वार उठने लगा, और मंदिरों, कुओं, तथा सार्वजनिक स्थानों को अछूतों के लिए खोल दिया गया। सवर्ण हिंदुओं और अछूतों का एक सम्मेलन पूना में बुलाया गया, जिसका उद्देश्य एक वैकल्पिक निर्वाचन व्यवस्था की खोज करना था, जो अंग्रेजों के सांप्रदायिक निर्णय के उन प्रावधानों का स्थान ले सके, जिन्होंने गांधीजी को चरम बलिदान के लिए प्रेरित किया था।
एक समझौता हुआ, लेकिन बहुत शीघ्र नहीं। गांधीजी के बिस्तर के पास बैठकर, दलित वर्गों के लिए जो काल्पनिक निर्वाचन व्यवस्था बनाई गई, उसमें कहा गया कि “दलित वर्गों के मतदाता एक प्राथमिक चुनाव करेंगे और हर स्थान के लिए चार उम्मीदवार चुनेंगे। ये उम्मीदवार सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों द्वारा संयुक्त चुनाव के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेंगे।” प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के स्थानों की संख्या, जो
ब्रिटिश निर्णय के अनुसार 71 थी, बढ़ाकर 148 कर दी गई। स्थानों का यह आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक आपसी समझौते से इसे समाप्त नहीं कर दिया जाए। ‘पूना पेक्ट’ के नाम से जानी गई इस निर्वाचन व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया, और गांधीजी ने 26 सितंबर 1932 को रविंद्रनाथ ठाकुर की उपस्थिति में अपना उपवास तोड़ दिया।
बाद में हिंदू नेताओं ने, विशेषकर बंगाल में, गांधीजी की आलोचना की और कहा कि उन्होंने दलित वर्गों को बहुत कुछ दे डाला; पर इस संवैधानिक दृष्टिकोण से उन्हें घृणा थी। वे महसूस करते थे कि “अतीत में सवर्ण हिंदुओं ने अपने कमजोर भाइयों के साथ जो अत्याचार किए हैं, उन्हें देखते हुए वे कुछ भी करके अधिक उदार नहीं कहलाते।”
इस उपवास का कम से कम एक उत्कृष्ट परिणाम निकला कि दलित वर्गों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों की बात खत्म कर दी गई। भारतीय राजनीति में एक कील की तरह गड़े, प्रतिनिधित्व के इस तरीके का छलपूर्ण प्रभाव अगले दशक में पूरी तरह से प्रकट हो गया। 1909 में सुधारों की मोर्ले-मिंटो योजना के अंतर्गत लागू किए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों ने मुस्लिम अलगाववाद के विकास के लिए एक संस्थागत आधार निर्मित कर दिया था। इसके तेईस वर्ष बाद राष्ट्रीय मोर्चे में एक बड़ी दरार डाल देने के ऐसे ही प्रयास को गांधीजी के उपवास ने विफल कर दिया। यदि 1932 में पूना पेक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय में संशोधन नहीं किया गया होता, तो 1945-47 के वर्षों में भारत की राजनीतिक समस्या का
समाधान वस्तुतः जितना कठिन था, उससे अधिक, असाधारण रूप से कठिन हो गया होता। सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत के दौरान, अंबेडकरजी ने दावा किया कि “उनका अनुसूचित जाति संघ पूरी छह करोड़ अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व करता है और केवल वही उनके एकमात्र प्रामाणिक प्रतिनिधि है!” उन्होंने तर्क किया कि “अनुसूचित जातियों को विशेष संरक्षण और अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता की ठीक वैसी ही जरूरत है, जैसी मुस्लिम समुदाय को दी गई है!” ‘सवर्ण हिंदुओं के प्रभुत्व’ की निंदा करते हुए, वे बहुत कुछ जिन्ना के मुहावरे में बोले। उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों और यहां तक कि पृथक चुनाव निर्णयों की मांग की।
अंग्रेजों के मन में अंबेडकर के लिए एक कमजोरी थी। वे 1942 की वायसराय परिषद के सदस्य थे। 1945 में शिमला सम्मेलन में बहस के दौरान, अंतरिम सरकार के लिए बनी सूची में लार्ड वेवेल ने उनका नाम शामिल किया, पर 1946 के प्रारंभ में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए आम चुनावों के बाद स्थिति बदल गई। कांग्रेस ने अंबेडकर के दल को उखाड़ फेंका। अब अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें मान्यता देना सरकार के लिए भी असंभव हो गया। अंबेडकर ने 1946 में संयुक्त चुनाव क्षेत्रों के अंतर्गत हुए चुनावों के परिणामों पर प्रश्न चिन्ह लगाया, सवर्ण हिंदुओं के अत्याचारों के विरुद्ध विषवमन किया और सीधी कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री एटली से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, तो एटली को सलाह दी गई कि “वे अंबेडकर के विरोध की परवाह न करें!”
यदि गांधीजी ने 1932 में उपवास न रखा होता और जातिगत निर्णय में दिए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों को पूना समझौते के द्वारा नहीं बदला गया होता, तो संभवतः मुस्लिम अलगाववाद और रियासतों के हठपूर्ण रवैये के कारण पहले से ही दुरूह बनी 1946-47 की बातचीत की गुथ्थियां, अनुसूचित जातियों की समस्या के अतिरिक्त भार से और भी उलझ जातीं।
संविधानिक व्यवस्था तो संयोगवश अगले तीन वर्षों तक लागू नहीं हो पाई, पर इससे अधिक महत्वपूर्ण थी भावनात्मक विरेचन की वह प्रक्रिया जिससे हिंदू समाज गुजरा। जैसा कि गांधीजी ने माना था, उपवास का प्रयोजन “हिंदू समाज की अंतरात्मा में चुभन पैदा करके, उसे सही धार्मिक क्रियान्वयन की ओर उन्मुख करना ही था!” दलित वर्गों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों की समाप्ति छुआछूत के अंत की शुरुआत बन जानी थी।
इतिहास में समाज सुधार के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन एक राजकीय बंदी ने छेड़ा। गांधीजी ने अपने अनगिनत संवाददाताओं के लिए वक्तव्यों और पत्रों की एक झड़ी लगा दी, ताकि छुआछूत की बुराई से लोगों को अवगत और शिक्षित किया जा सके। उन्होंने इस आंदोलन को गति देने के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका ‘हरिजन’ के प्रकाशन की व्यवस्था की। ‘हरिजन’ शब्द का अर्थ होता है, ईश्वर की संतान। यह नाम गांधीजी ने अंत्यजों, दलितो को दिया था। गांधीजी ने लिखा कि “संसार के सभी धर्मों में ईश्वर को प्रथमतः मित्रहीनों का मित्र, असहायों का सहायक और कमजोरों का संरक्षक बताया गया है।”
अछूत नाम से वर्गीकृत चार करोड़ हिंदुओं से अधिक मित्रहीन, असहाय और कमजोर और कौन होगा? गांधीजी को इस बात में संदेह था कि हिंदू धर्म ग्रंथों में अस्पृश्यता के समर्थन में कुछ भी लिखा गया है। यदि किसी प्राचीन पांडुलिपि में से इस क्रूरता के अनुमोदन में कुछ उद्धृत करना संभव भी हुआ, तो गांधीजी उससे बंधे नहीं। हर धर्मशास्त्र में कुछ चरम सत्य लिखे होते हैं, लेकिन समसामयिक समाज के लिए संगतपूर्ण कुछ निषेधाज्ञाएं भी उसमें रहती हैं। यदि इनसे मानव गरिमा को क्षति पहुंची है, तो इनकी उपेक्षा की जा सकती है। ‘हरिजन’ का एक बड़ा हिस्सा गांधीजी स्वयं लिखते थे। हिंदुओं के अंतरंग से छुआछूत के पाप को बाहर खींच लाने और अछूतों की उस दर्दनाक स्थिति को शब्दचित्र में अंकित कर प्रकाशित करने की पहल गांधीजी ने ही की।
जेल से छूटने के बाद हिंदुत्व को छुआछूत की बुराई से मुक्त करने के लिए वे 12,500 मील लंबी यात्रा पर निकल पड़े! उन्होंने हिंदुओं से आग्रह किया कि वे हरिजनों के विरुद्ध अपने पूर्वग्रहों का त्याग करें और हरिजनों से निवेदन किया कि वे नशीले पदार्थों और शराब का सेवन छोड़ दें, क्योंकि हिंदू समाज में मिलजुलकर रहने में यह आदत सबसे बड़ी बाधा थी! उन्होंने इस अंधविश्वास का मजाक उड़ाया कि कोई व्यक्ति जन्म से ही अपवित्र हो सकता है, अथवा किसी एक मनुष्य की छाया या उसका स्पर्श मात्र दूसरे को गंदा कर सकता है!
हरिजन फंड के लिए धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अपने आपको थका डाला! दस महीनों में उन्हें आठ लाख रुपये प्राप्त हुए। यह राशि वे किसी महाराजा या करोड़पति से उपहार के रूप में ले सकते थे; लेकिन ऐसे धन इकट्ठा करने को वे अधिक महत्व नहीं देते थे! करोड़ों पुरुष, स्त्री और बच्चे जिन्होंने उनके कटोरे में पैसे डालें—छुआछूत के विरुद्ध उनकी लड़ाई में साथी-सैनिक बन गए!
यह हरिजन यात्रा एक विजय यात्रा बिल्कुल नहीं रही! गांधीजी एक युगों पुरानी क्रूरता पर और लंबे समय से स्थापित निहित स्वार्थों पर आघात कर रहे थे, जबकि उन्हें मालूम था कि ये स्वार्थ अपनी रक्षा में किसी भी बात से पीछे रहने वाले नहीं! कट्टरपंथी हिंदुओं ने एक खतरनाक हिंदुद्रोह का आरोप उन पर लगाया, काले झंडे लेकर प्रदर्शन किए, उन्हें बोलने नहीं दिया और उनकी सभाओं को तोड़ने की कोशिश की! 25 जून 1934 को जब वे पुणे में नगरपालिका भवन की ओर जा रहे थे, उनके प्रतिनिधिमंडल पर बम फेंका गया! गांधीजी को चोट नहीं आई, पर सात व्यक्ति घायल हो गए! बम फेंकने वाले अज्ञात व्यक्ति के प्रति उन्होंने गहरी करुणा व्यक्त की। उन्होंने कहा, “मैं शहीद बनने के लिए तिलमिला नहीं रहा हूँ, पर यदि उस अवस्था को कार्यरूप देने में जिसे मैं अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानता हूँ, और करोड़ों हिंदू जिसमें मेरे साथ एकमत हैं, वह मेरे रास्ते में आ ही जाए, तो मैं समझूँगा कि मैंने उसे ठीक ही अर्जित किया है!”
यद्यपि कट्टरपंथी हिंदुओं का विरोध कठिनाई से ढीला पड़ा, और उग्र हरिजन नेता भी उनकी आलोचना करते रहे, तब भी गांधीजी एक अति प्राचीन फोड़े को चीरा लगाने में सफल रहे! अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रीय नेता राजगोपालाचारी ने ‘क्रांति पूरी हुई’ शीर्षक से एक लेख लिखा था: “अब सिर्फ मलवे को हटाना बाकी है!” यह
एक आशावादी उक्ति थी, पर इसमें संदेह नहीं कि सुधारवादियों ने एक अच्छा आरंभ किया था! 1937-39 के कांग्रेस मंत्रालयों ने हरिजनों की कुछ कानूनी अक्षमताओं को दूर कर दिया था, और 1952 में लागू हुए भारत संघ-राज्य के संविधान में छुआछूत को गैर-कानूनी करार दिया गया! एक सामाजिक और आर्थिक सभी मोर्चों पर निरंतर संघर्ष की जरूरत थी, पर इसमें भी संदेह नहीं कि गांधीजी के आंदोलन ने उन सभी मोर्चों को जड़ तक हिलाया!
यद्यपि छुआछूत के प्रति गांधीजी का विरोधात्मक तेवर अविचल और अटल था, पर छुआछूत जिस जाति-प्रथा की विकृत उपज थी, उसके प्रति दक्षिणी अफ्रीका से वापसी के आरंभिक वर्षों में उनका रूख कुछ दुविधापूर्ण था! हिंदू पुराण-ग्रंथों ने उनके सामने प्राचीन भारत की वर्णाश्रम व्यवस्था का एक रोमांटिक चित्र प्रस्तुत किया था! उस काल में इस मूलभूत चतुर्विध विभाजन में जातियाँ व्यावसायिक संघों के समकक्ष थीं, और जन्म ही एकमात्र सामाजिक स्तर एवं प्रतिष्ठा का निर्धारक नहीं था! गांधीजी को लगा कि अपने प्रकट दोषों के बावजूद इस प्रणाली ने उथल-पुथल के उन युगों में बाहरी दबाव को सोख लेने का काम किया है; वे सोचते थे कि क्या इसकी मूलभूत पवित्रता वापस आ सकती है और हिंदू समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप इसे ढाला जा सकता है?
जाति-प्रथा के प्रति उनकी प्रशंसात्मक टिप्पणियाँ, जिन्हें अक्सर उनके विरुद्ध उद्धृत किया जाता है, इसी पृष्ठभूमि में की गई हैं! यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि जाति-प्रथा के अनुकूल जो भी विचार उन्होंने व्यक्त किए, वे उनके विश्वास के अनुसार जैसी वह व्यवस्था उस सुदूर अतीत में थी, उसके बारे में हैं, न कि जैसी वह उनके समय में बन गई, उसके बारे में! भारत के सामाजिक परिदृश्य को प्रत्यक्ष और निकट से देखने पर उन्हें विश्वास हो गया था कि अंधविश्वासों, छुई-मुईवाद, सामाजिक विषमता और भेदभाव ने इस प्रथा को इतना सड़ गया है कि यह सुधार के लायक नहीं रह गई है!
जाति-प्रथा के प्रति गांधीजी का रुख निरंतर सख्त होता दिखाई देता है! दिसंबर 1920 में उन्होंने लिखा था: “मैं सिर्फ इन चार विभाजनों को मूलभूत, नैसर्गिक और आवश्यक मानता हूँ! अनगिनत उपजातियाँ कभी सुविधाजनक हो जाती हैं, पर अक्सर रुकावटें पैदा करती हैं! जितनी जल्दी वे परस्पर घुल-मिल जाएं, उतना ही अच्छा है!” पंद्रह वर्ष बाद उन्होंने घोषणा की कि शास्त्रों में वर्णित वर्णाश्रम आज व्यवहार में अस्तित्वहीन है! आज की जाति-प्रथा वर्णाश्रम से एकदम उलट है! सार्वजनिक राय से इसे जितनी जल्दी समाप्त किया जाए, उतना ही अच्छा है!” उन्होंने सुझाव दिया कि सभी हिंदू स्वेच्छा से अपने आपको शूद्र कहें, वे शूद्र जो सामाजिक सीढ़ी में सबसे नीचे माने जाते हैं!”
उन्होंने इस विचार का खंडन किया कि छुआछूत हिंदू संस्कृति का एक अनिवार्य अंग है! उन्होंने कहा: “यह एक महामारी है जिससे लड़ना हर हिंदू का परम कर्तव्य है!” 1920 के दशक में विभिन्न जातियों के लोगों के एक साथ खाने और परस्पर विवाह करने पर लगे प्रतिबंधों के अनुमोदन के लिए तैयार थे, क्योंकि वे इन्हें आत्मनियंत्रण के माध्यम मानते थे! पर 1930 के दशक में जाति-प्रथा अथवा स्थानीय पूर्वाग्रह से उत्पन्न किसी भी वर्जना की वे खुलकर निंदा करते थे! उन्होंने लिखा है: “कोई व्यक्ति—स्त्री या पुरुष—कहाँ विवाह करता है या किसके साथ खाता है, यह उसकी स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
यदि भारत एक है और अविभाज्य है, तो निश्चय ही इसमें अनगिनत छोटे-छोटे समूहों को जन्म देने वाले कृत्रिम विभाजन नहीं होने चाहिए, जो न एक-दूसरे के साथ बैठकर खाना खा सकें और न परस्पर विवाह कर सकें!” 1946 में गांधीजी ने एक चौकानेवाली घोषणा की कि उनके सेवाग्राम स्थित आश्रम में कोई विवाह-संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक वर-वधू में से एक जन्म से अछूत न हो!
आरंभिक वर्षों में जाति-प्रथा पर सीधी चोट करने में गांधीजी की हिचकिचाहट महज एक राजनीतिक कौशल हो सकती है! 1956 में हंगेरी के पत्रकार टाइबर मेंडे से बातचीत में जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार कहा: “मैंने गांधीजी से बार-बार कहा: आप जाति-प्रथा पर सीधी चोट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि वे आदर्श व्यवसायिक संगठनों में व्यक्त होने वाले रूप के अलावा जाति-प्रथा में विश्वास नहीं रखते! वर्तमान जाति-प्रथा संपूर्णतः अहितकर है और इसे समाप्त करना ही होगा!” उन्होंने कहा: “मैं छुआछूत की समस्या का सामना करके इसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर रहा हूँ!”
इस तरह आप देखते हैं कि किसी एक बात को हाथ में लेने और उस पर ध्यान केंद्रित करने का उनका एक अलग तरीका था! उन्होंने कहा था: “यदि छुआछूत नष्ट हो जाती है, तो जाति-प्रथा भी नष्ट हो जाएगी!”
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.