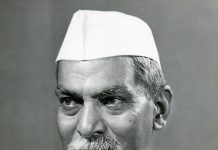दास्तावेज : जनतंत्र का भविष्य
सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में जनतंत्र का भविष्य धूमिल है। 1950 के आसपास अधिकांश औपनिवेशिक मुल्क आजाद होने लगे। उनमें से कुछ ही देशों ने जनतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में अपनाया। अभी भी दुनिया के ज्यादातर देशों में जनतंत्र स्थापित नहीं हो सका है। बढ़ते मध्य वर्ग की आकांक्षाओं के दबाव से कहीं-कहीं जनतंत्र की आंशिक बहाली हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर विकासशील देशों में जनतंत्र का अनुभव उत्साहवर्धक नहीं है। नागरिक आजादी की अपनी गरिमा होती है, लेकिन कोई भी विकासशील देश यह दावा नहीं कर सकता कि जनतंत्र के बल पर उसका राष्ट्र मजबूत या समृद्ध हुआ है या जनसाधारण की हालत सुधरी है।
अगर भारत में जनतंत्र का खात्मा जल्द नहीं होने जा रहा है, तो इसका मुख्य कारण यह है कि पिछड़े और दलित समूहों की आकांक्षाएँ इसके साथ जुड़ गई हैं। अत: जनतंत्र का ढाँचा तो बना रहेगा, लेकिन जनतंत्र के अन्दर से फासीवादी तत्वों का जोर-शोर से उभार होगा। जयललिता, बाल ठाकरे और लालू प्रसाद पूर्वाभास हैं। अरुण गवली, अमर सिंह जैसे लोग दस्तक दे रहे हैं। अगर वीरप्पन कर्नाटक विधान सभा के लिए निर्वाचित हो जाता है तो इक्कीसवीं सदी के लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। यानी जनतंत्र जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। अगर राजनीति की गति बदली नहीं, तो अगले दो दशकों में भारत के कई इलाकों में क्षेत्रीय तानाशाही या अराजकता जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी।
इसका मतलब यह नहीं कि जनतंत्र का कोई विकल्प है। अगर 1947 या 1950 में हम एक जनतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं अपनाते, तो देश की हालत इससे भी बुरी होती। गलती यह हुई कि हम अपने जनतंत्र को सही रूप और चरित्र नहीं दे पाये। भारत के इतिहास, भूगोल, समाज और अर्थनीति को समझते हुए भारत में जनतंत्र का जो मौलिक स्वरूप होना चाहिए था, उसका निरूपण आज तक नहीं हो पाया है। हमारे नेतृत्व का दिवालियापन और बौद्धिक वर्ग की वैचारिक गुलामी इसके लिए दायी हैं। 1947 में उनके सामने सफल जनतंत्र के दो नमूने थे और शासन व्यवस्था की एक औपनिवेशिक प्रणाली भारत में चल रही थी। इन तीनों को मिलाकर हमारे बौद्धिक वर्ग ने एक औपनिवेशिक जनतंत्र को विकसित किया है, जो जनतंत्र जरूर है, लेकिन अंदर से खोखला है। शुरू के दिनों में अन्य विकासशील देशों के लिए भारत की मार्गदर्शक भूमिका थी। जब भारत ही जनतंत्र का कोई मौलिक स्वरूप विकसित नहीं कर पाया, तो अन्य देशों के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया।
पिछले पचास साल में भारत तथा अन्य विकासशील देशों में जनतंत्र की क्या असफलताएँ उजागर हुई हैं, उनका अध्ययन करना और प्रतिकार ढूँढ़ना – यह काम भारत के विश्वविद्यालयों ने बिलकुल नहीं किया है। शायद इसलिए कि पश्चिम के समाजशास्त्र ने इसमें कोई अगुआई नहीं की। पश्चिम से सारे आधुनिक ज्ञान का उद्गम और प्रसारण होता है लेकिन वहाँ के शास्त्र ने भी 1950 के बाद की दुनिया में जनतंत्र की असफलताओं का कोई गहरा या व्यापक अध्ययन नहीं किया है, जिससे समाधान की रोशनी मिले। पश्चिम की बौद्धिक क्षमता संभवत: समाप्त हो चुकी है; फिर भी उसका वर्चस्व जारी है।
1950 के आसपास जिन देशों को आजादी मिली, उन समाजों में आर्थिक सम्पन्नता नहीं थी और शिक्षा की बहुत कमी थी। इसलिए इन देशों के जनतांत्रिक अधिकारों में यह बात शामिल करनी चाहिए थी कि प्रत्येक नागरिक के लिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी होगी और माध्यमिक स्तर तक सबको समान प्रकार की शिक्षा उपलब्ध होगी। अगर ये दो बुनियादी बातें भारतीय जनतंत्र की नींव में होतीं, तो भारत के विकास की योजनाओं की दिशा भी अलग हो जाती। जाति प्रथा, लिंग भेद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विषमता जैसी समस्याओं के प्रतिकार के लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा हो जाता। लोग जनतंत्र को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे।
हुआ है उलटा। सारे समाज विरोधी तत्व जनतंत्र का उपयोग अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए कर रहे हैं। राजनीति पर उन्हीं का अधिकार है। जनतंत्र एक व्यापक राजनीति के द्वारा संचालित होता है। इस राजनीति का चरित्र इतना भयावह होता गया है कि अच्छे लोगों के लिए राजनीति वर्जनीय मानी जा रही है। इसका तार्किक परिणाम है कि राजनीति पर अधिकारियों का अधिकार हो जायेगा। अगर विवेकशील लोगों का प्रवेश राजनीति में नहीं होगा तो भ्रष्ट लोगों का राजत्व अवश्य होगा। इस द्वन्द्व का समाधान कैसे होगा? अच्छे लोग राजनीति में कैसे आयेंगे और वहाँ अच्छे बन कर रहेंगे, इसका कोई शास्त्र या विवेचन होना चाहिए। समाज अगर जनतंत्र चाहता है, तो समाज के ही कुछ तरीके होने चाहिए, जिससे अच्छे लोग राजनीति में आयेंगे और बने रहेंगे। यह सिलसिला निरंतरतापूर्वक चालू रहेगा। अगर वैसा नहीं होता है, तो राजतंत्र क्यों बुरा था? राजतंत्र को बुरा माना गया क्योंकि अच्छे राजा का बेटा अच्छा होगा इसका कोई निश्चय नहीं है। 150 साल के अनुभव से यह मालूम हो रहा है कि जनतंत्र में भी इसका निश्चय नहीं है कि एक बुरे शासक को हटा देने के बाद अगला शासक अच्छा होगा। अत: जनतंत्र को कारगर बनाने के लिए नया सोच जरूरी है। जनतंत्र के ढाँचे में ही बुनियादी परिवर्तन की जरूरत है।
भारत जैसे देश में जनतंत्र को चलाने के लिए हजारों (शायद लाखों) राजनैतिक कार्यकर्ता चाहिए। संसद, विधान सभा, जिला परिषद, ग्राम पंचायत आदि को मिला कर हजारों राजनैतिक पद हैं। प्रत्येक पद के लिए अगर दो या तीन उम्मीदवार होंगे, तब भी बहुत बड़ी संख्या हो जायेगी। इनमें से बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे, जिन्हें पूर्णकालिक तौर पर सार्वजनिक काम में रहना होगा तो उनके परिवारों का खर्च कहाँ से आएगा? भ्रष्टाचार की बात करनेवालों को इस प्रश्न का भी गंभीरतापूर्वक उत्तर ढूँढ़ना पड़ेगा।
पिछले 50 साल की राजनीति पर हम संवेदनशील हो कर गौर करें, तो इस बात से हम चमत्कृत हो सकते हैं कि हजारों आदर्शवादी नौजवान देश के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए परिवर्तनवादी राजनीति में कूद पड़े थे। आज अगर उनके जीवन इतिहासों का विश्लेषण करेंगे, तो मालूम होगा कि उनमें से अधिकांश बाद के दिनों में, जब उनको परिवार का भी दायित्व वहन करना पड़ा, या तो राजनीति से हट गए या अपने आदर्शों के साथ समझौता करने लगे। निजी तथा सार्वजनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू में छोटे-छोटे ठेकेदारों से, भ्रष्ट प्रशासकों से या काले व्यापारियों से चंदा लेना पड़ा। बाद में जब लगातार खर्च बढ़ता गया और प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई, तब बड़े व्यापारियों और पूँजीपतियों के साथ साँठ-गाँठ करनी पड़ी। अगर वे आज भी राजनीति में हैं, तो अब तक इतना समझौता कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार या शोषण के विरुद्ध खड़े होने का नैतिक साहस नहीं है। पिछले 50 साल आदर्शवादी कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक जीवन में पतन और निजी जीवन में हताशा का इतिहास है।
अगर शुरू से ही समाज का कोई प्रावधान होता कि राजनीति में प्रवेश करनेवाले नौजवानों का प्रशिक्षण-प्रतिपालन हो सके, उनके लिए एक न्यूनतम आय की व्यवस्था हो सके, तो शायद वे टूटते नहीं, हटते नहीं, भ्रष्ट नहीं होते। कम से कम 50 फीसदी कार्यकर्ता और नेता स्वाधीन मिजाज के होकर रहते। अगर किसी जनतंत्र में 10 फीसदी राजनेता बेईमान होंगे तो देश का कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर 50 फीसदी बेईमान हो जाएँ, तब भी देश चल सकता है। अब तो इस पर भी संदेह होता है कि सर्वोच्च नेताओं के 5 फीसदी भी देशभक्त और इमानदार हैं या नहीं।
समाज के अभिभावकों का, देशभक्त कार्यकर्ताओं का संरक्षण समाज के द्वारा ही होना चाहिए। सारे राजनेताओं को हम पूँजीपतियों पर आश्रित होने के लिए छोड़ नहीं सकते। समाज खुद उनके प्रशिक्षण और प्रतिपालन का दायित्व लें। इस दायित्व को निभाने के लिए यदि बनी-बनायी संस्थाएँ नहीं हैं, तो सांविधानिक तौर पर राज्य के अनुदान से संस्थाएँ खड़ी की जायें। जिस प्रकार न्यायपालिका राज्य के अनुदान पर आधारित है, लेकिन स्वतंत्र है, उसी तरह राजनेताओं का प्रशिक्षण और प्रतिपालन करनेवाली संस्थाएँ भी स्वतंत्र होंगी। केवल चरित्र, निष्ठा और त्याग के आधार पर राजनैतिक संरक्षण मिलना चाहिए। जो आजीवन सामाजिक दायित्व वहन करने के लिए संकल्प करेगा, जो कभी धन संचय नहीं करेगा, जो संतान पैदा नहीं करेगा, उसी को सामाजिक संरक्षण मिलेगा। जो धन संचय करता है, जो संतान पैदा करता है, उसको भी राजनीति करने, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, लेकिन उसे सामाजिक संरक्षण नहीं मिलेगा। जिसे सामाजिक संरक्षण मिलेगा उसके विचारों पर अनुदान देनेवालों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। सिर्फ आचरण पर निगरानी होगी। निगरानी की पद्धति पूर्वनिर्धारित रहेगी।
यह कोई विचित्र या अभूतपूर्व प्रस्ताव नहीं है। कोई भी राज्य व्यवस्था हो, सार्वजनिक जीवन में चरित्र की जरूरत होगी। किसी भी समाज में समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह चाहिए। आधुनिक युग के पहले संगठित धर्म ने कई देशों में सार्वजनिक जीवन का मार्गदर्शन किया। धार्मिक संस्थाओं ने भिक्षुओं, ब्राह्मणों, बिशपों को प्रशिक्षण और संरक्षण दिया, ताकि वे सार्वजनिक जीवन का मानदंड बनाएं रखें। ग्रीस में और चीन में प्लेटो और कन्फ्यूशियस ने राजनैतिक कार्य के लिए प्रशिक्षित और समर्पित समूहों के निर्माण पर जोर दिया। सिर्फ आधुनिक काल में सार्वजनिक जीवन के मानदंडों को ऊँचा रखने की कोई संस्थागत प्रक्रिया नहीं तय की गई है। इसलिए सारी दुनिया का सार्वजनिक जीवन अस्त-व्यस्त है। सार्वजनिक जीवन का दायरा बढ़ गया है, लेकिन मूल्यों और आदर्शों को बनाए रखने की संस्थाएँ नहीं हैं।
संविधान के तहत या राजकोष से राजनीति का खर्च वहन करना भी कोई नई बात नहीं है। विपक्षी सांसदों और विधायकों का खर्च राजकोष से ही आता है। यह एक पुरानी माँग है कि चुनाव का खर्च भी क्यों नहीं? राजनीति का खर्च भी क्यों नहीं? कुछ प्रकार के राजनेताओं का जीवन बचाने के लिए केन्द्रीय बजट का प्रतिमाह 51 करोड़ रुपये खर्च होता है। करोड़पती सांसदों को भी पेंशन भत्ता आदि मिलता है। इनमें से कई अनावश्यक खर्चों को काट कर देशभक्त राजनैतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक सामाजिक कोष का निर्माण शुरू हो सकता है।
अगर विवेकशील लोग राजनीति में दखल नहीं देंगे तो भारत की राजनीति कुछ ही अरसे के अंदर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के हाथों में चली जायेगी। जो लोग इसके बारे में चिंतित हो रहे हैं, उन्हें एक मूल्य आधारित राजनैतिक खेमा खड़ा करना होगा। इस खेमे के लिए एक बड़े पैमाने का कोष निर्माण करना होगा। आज की संसद या विधान सभा इसके लिए अनुदान नहीं देगी। सामाजिक और स्वैच्छिक ढंग से ही इस काम को शुरू करना होगा।
अन्ना हजारे इस काम को शुरू करेंगे, तो अच्छा असर होगा। यह राजनैतिक काम नहीं है, जनतांत्रिक राजनीति को बचा कर रखने के लिए यह एक सामाजिक काम है। धर्मविहीन राज्य में चरित्र का मानदंड बना कर रखने का यह एक संस्थागत उपाय है। अंततोगत्वा इसे (ऐसी संस्थाओं को) समाज का स्थायी अंग बना देना होगा या सांविधानिक बनाना होगा।
धर्म-नियंत्रित समाजों के पतन के बाद नैतिक मूल्यों पर आधारित एक मानव समाज के पुनर्निर्माण के बारे में कोई व्यापक बहस नहीं हो पाई है। यह बहस अनेक बिंदुओं से शुरू करनी होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.