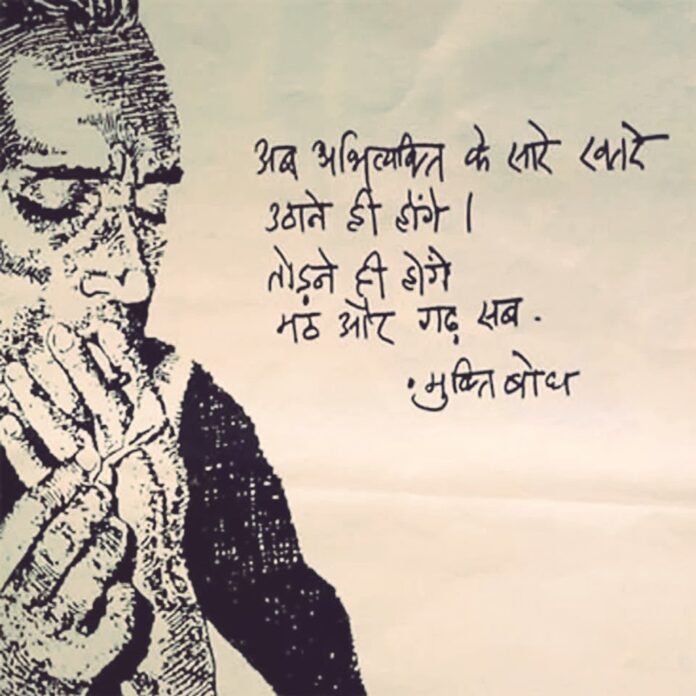आलोचक का प्रथम कर्तव्य है कि वह किसी भी कलाकृति के अंतर्तत्वों को – उसके प्राण तत्वों की भावना – कल्पना को ग्रहण करें और उसमें निहित दशा की ओर प्रभावित गति को और उसकी परिणति को समझें और तदुपरान्त विश्लेषण करें । मुक्तिबोध रचना और आलोचना दोनों स्तर पर किसी कृति का समग्रता में कलात्मक मूल्यांकन को महत्व देते हैं । वे अपने समय के बड़े आलोचक हैं जिन्होंने रचना प्रक्रिया के अन्तःसुत्रों को समझने के लिए तीसरा क्षण नाम से एक नया सिद्धांत और रचनात्मक आलोचना का एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया जो भारतीय काव्य शास्त्र और पश्चिम आलोचना सिद्धांत के लिया एक चुनौती थी । मुक्तिबोध से पहले रचना प्रक्रिया को लेकर कोई पम्परा नहीं थी ।उन्होंने उस समय तक हिंदी आलोचना की जो परम्परा थी, उसका अनुगमन नहीं किया और अपनी आलोचना के लिए नया मुहावरा गढ़ा। निर्मला जैन , मुक्तिबोध के आलोचना कर्म को रेखांकित कराती हुई कहती हैं – ‘’ नए कवि -आलोचकों में वे सबसे प्रखर और गंभीर आलोचक थे। किसी कवि में आलोचना की ऐसी चिंतन शक्ति दुर्लभ ही है ।’’
मुक्तिबोध के रचना काल में तत्कालीन हिंदी साहित्य व्यक्तिपरक और सामाजिकता की दो विरोधी आलोचनात्मक धुर्वों के बोच बटा था । एक पक्ष जहाँ साहित्य में व्यक्ति के आतंरिक सत्य या अनुभूतियों की अवहेलना कर रहा था और सामाजिक सन्दर्भों को अंतिम सत्य के रूप में रूप में देखने का हिमायती था । वहीं दूसरी ओर कुछ आलोचक व्यक्ति स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति के उत्साह में सामाजिकता को नकार कर संवेदना के मूल आधार से दूर हो रहें थे । उन्होंने इसमें समन्वय स्थापित करने की कोशिश नहीं की बल्कि उनका दृष्टिकोण समग्रतावादी है ।
मुक्तिबोध के अनुसार अगर स्वयं की अनुभूतियों या मनोभावों का सन्दर्भ सामाजिक है तो वह जन विरोधी हो ही नहीं सकता है। जो आलोचक अपनी जड़वादी और यांत्रिक सिद्धांतों के माध्यम से केवल क्रन्तिकारी नारों की खोज में रहते हैं , वे अपनी तमाम जनपक्षधरता के वावजूद संवेदना की सामाजिक आधार भूमि से कट जातें हैं । मुक्तिबोध जहाँ एक ओर जड़ मार्क्सवादी और यांत्रिक आलोचना प्रवृति का विरोध करते हैं ,वहीँ नई कविता में व्यक्ति स्वातंत्र्य का नारा उछालने वाले कुंठाग्रस्त और जनविरोधी प्रवृतियों का भी विरोध करतें है । वे कहतें है – ” कोई भी भावना न अपने-आप में प्रतिक्रियावादी होती है ,न प्रगतिशील । वह वास्तविक जीवन संबंधों से युक्त होकर होकर ही उचित या अनुचित ,सांगत या असंगत सिद्ध हो सकती है —- अगर घृणा उचित के प्रति है तो वह स्वयं घृन्य है , यदि अनुचित के प्रति है तो प्रशंसनीय है ।” इस प्रकार वह कविता के किसी खास ढाचें में बंधी होने की मांग करनेवाली प्रवृति का विरोध करतें हैं ।
मुक्तिबोध ऐसे आलोचक हैं जो व्यावारिक आलोचना से शुरुआत करके साहित्य के सौन्दर्य की ओर बढ़तें हैं ।वे काव्यानुभूति या सौंदर्यानुभूति को जीवनानुभूति से अलग नहीं मानते हैं ।
”नए साहित्य का सौन्दर्य- शास्त्र ‘ में वे अपनी आलोचना दृष्टि को स्पस्ट करते हुए लिखते है –
” साहित्य विवेक मूलतःजीवन विवेक है । इसलिए जीवन से दूर अपनी आराम कुर्सी पर बैठा समीक्षक , बड़ा विद्वान् क्यों न हो , जीवन का वैज्ञानिक विवेचन नहीं कर सकता है, फिर उसकी उसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति से विश्लेषण की बात ही क्या ? बगैर जीवन को जाने . बिना पहचाने , जो आलोचक केवल जीवन की गूंजे (साहित्यिक अभिव्यक्ति ) का विश्लेषण करता है ।उसको किसी हद तक यांत्रिकता का सहारा लेना ही पड़ता है ।”
आचार्य शुक्ल ने भी रसात्मक बोध के विविध स्वरूप में काव्यानुभूति या सौन्द्रयानुभूति को जीवनानुभूति का उद्दात रूप माना हैं।
मुक्तिबोध की आलोचना ही नहीं , सम्पूर्ण सर्जनात्मकता की क्रेन्द्रीय संवेदना मानवता के प्रति प्रतिवद्धता है । इसलिए वे कृतियों की आलोचना के लिए केवल साहित्यिक मूल्यों व मापदंडों पर निर्भर नहीं रहते , बल्कि मानवीय मूल्यों की भी अपेक्षा रखते है ।
आलोचना को मुक्तिबोध का सबसे बड़ा प्रदेय रचना प्रक्रिया का विश्लेषण रहा है ।मुक्तिबोध से पहले रचना प्रक्रिया का विश्लेषण उपेक्षित रहा था ।इस प्रकार रचना प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से एक नया सैद्धांतिक पक्ष रखा । ”एक साहित्यिक की डायरी ” में उन्होंने काव्य की रचना प्रक्रिया पर बात करते हुए सृजन के तीन क्षणों की बात करतें है । वे लिखते हैं , ” कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण । दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते – दुखते हुए मूल्यों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैटेंसी का रूप धारण करना , मानों वह फैंटेसीअपने आँखों के सामने खड़ी हो । तीसरा और अंतिम क्षण है फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्णअवस्था तक की गतिमानता ।
मुक्तिबोध जी ने जिन काव्य रचनाओं पर अपनी समीक्षा दृष्टि डाली है उनमे जयशंकर प्रसाद ‘की कामायनी , भारत भूषण की कविता ” ओ प्रस्तुत मन ‘ , भारती जी का ” अँधा युग ” , पंत जी की ‘ चिदंबरा , कांता जी की ” जो कुछ भी देखती हूँ ”, दिनकर जी की ” उर्वशी’ , कुंवर नारायण जी का रचना परिवेश ” हम और तुम ” महत्वपूर्ण हैं ।इसके अलावा उन्होंने शमशेर जी की और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं की भी मीमांसा की है ।
” कामायनी : एक पुनर्विचार ” में मुक्तिबोध कामायनी पर विचार करते हैं और कामायनी की प्रतीकात्मकता में निहित फैंटेसी के माध्यम से प्रसाद जिस यूटोपिया लोक का सृजन करतें हैं , उसका विश्लेषण करतें हैं और इस निकर्ष पर पहुचतें हैं कि कामायनी में बुद्धिवाद के विरुद्ध आस्थावाद और आत्मावाद की प्रतिष्ठा की गई है जो इस काव्य की त्रासदी हैं ।
मैनेजर पाण्डेय के अनुसार- ” कामायनी में मनु और श्रद्धा के चरित्र के माध्यम से श्रद्धावाद की प्रतिष्ठा हुई है ।उन दोनों की मुक्तिबोध ने कड़ी आलोचना की है ।”
श्रद्धावाद के संबंध में मुक्तिबोध स्वयं कहते हैं –
” श्रद्ध्वाद , श्रद्धा के चरित्र से उभरकर यह उद्घाटित करता है कि हमारा तथाकथित भाववाद – आदर्शवाद , अंततः किस प्रकार पूंजीवादी विषमताओं के लिए क्षमाप्रार्थी होकर पूंजीवादी व्यक्तिवादी को सिर्फ नसीहत देता हैं और बाद में उन्हीं से समझौता कर लेता है । यह रहस्यवाद आदर्शवाद , वस्तुत; आत्म विरोधों से ग्रस्त पूंजीवाद और व्यक्तिवाद का दार्शनिक डिफेंस है , और कुछ नहीं ।”
प्रत्येक रचनाकार और आलोचक का इतिहास बोध अलग होता है । मुक्तिबोध का सौन्दर्य बोध प्रसाद से अलग है । वह वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष से संपृक्त हैं इसलिए वे जनपक्षीय दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं। मुक्तिबोध के शब्दों में -” श्रद्धावाद घोर व्यक्तिवाद है । ह्रासगत पूंजीवाद का जनता को बरगलानें का एक जबरजस्त साधन है ।”
रामचंद्र शुक्ल ने भी श्रद्धा और इडा में श्रद्धा को अधिक महत्व देने पर निराशा व्यक्त की है । मुक्तिबोध इडा के चरित्र को कामायनी का सबसे उज्जवल चरित्र कहा है – ” इडा का व्यक्तित्व चरित्र बहिर्मुख ,सकर्मक , विज्ञानवादी
और वैयक्तिक स्वार्थ से नितांत रहित है । इडा स्वप्न द्रष्टाभी है – ऐसी स्वप्न द्रष्टा जो अपनी विधायक बुद्धि व रचनात्मक कार्य से इस स्वप्न को वास्तविकता में परिणत कर देती है ।”
वास्तव में कामायनी के सृजनात्मक बोध और मुक्तिबोध की आलोचना बोध के पीछे वह दोनों की अलग -अलग दृष्टि और युगबोध है । प्रसाद जहाँ ऐतहासिक – पौराणिक परंपरा के सापेक्ष पराधीन भारत में रचना कर रहें थे, वहीँ मुक्तिबोध आधुनिक युग की जटिलताओं और विषमताओं के सदर्भ में इस काव्य कृति का मुल्यांकन करते हैं । नामवर सिंह जी कहते हैं – ” एक नए सृजनशील कवि के नाते मुक्तिबोध काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में छायावाद के प्रतिक्रियावादी मूल्यों क खिलफ संघर्ष करना अपना कर्तव्य समझते थे . इसलिए उन्होंने विशेष रूप से कामायनी के भीतर घुसकर उन ऐतहासिक – सामाजिक शक्तिओं को उदघाटित किया ।
सुभद्रा कुमारी चौहान को वे हिंदी काव्य के प्रथम भावोल्लास के कवियों में मानते हैं, जिन्होंने अपनी कविता से जनता को उत्स्फूर्त किया तथा प्रेम और देशभक्ति के रंग से सराबोर कर दिया है। शमशेर को वे शिल्प की दृष्टि से हिंदी का अद्वितीय कवि मानते हैं।
भारत भूषण की कविता ‘ओ अप्रस्तुत मन’ पर दृष्टि डालते हुए वे कहते हैं कि इन कविताओं में कोई चीज नहीं है, कोई चमत्कार पूर्ण भंगिमा नहीं है। कोई मसीहाई ठाट नहीं है, कोई कवि सुलभ स्वप्ननलिप्तता भी नही है। रास्ता चलते जो कुछ मिल जाता है, या जो कुछ खुल जाता है, उसी ने भारतभूषण के काव्य का रूप धारण कर लिया है। असल में ये मामूली आदमी की कविताएँ हैं। हमारे देश का एक सचेत मामूली आदमी अपनी जिंदगी के रास्ते पर चलते हुए जो तजुर्बे हासिल करता है और नतीजे निकालता, वही यहाँ काव्य-रूप में सामने आया है। उनकी आत्मसमीक्षात्मक कविता का एक उदाहरण द्रष्टव्य है –
रस तो अनंत था,
अँजुरी भर ही पिया
जी में वसंत था,
एक फूल ही दिया
मिटने के दिन आज
मुझको यह सोच है
कैसे बड़े युग को,
कैसा छोटा जीवन जिया।
भारतभूषण का काव्य द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर मध्यमवर्गीय विकास की एक रेखा को प्रतिबिंबित करता है। यह उसका ऐतहासिक मूल्य है। (ज्ञानोदय 1959 में प्रकाशित)
‘अंधा युग’ की समीक्षा करते हुए वे लिखते हैं कि स्वाधीनता-संघर्ष के बाद दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती गई तो दूसरी ओर सामाजिक ह्रास के चिह्न दिखाई देने लगे। इस सामाजिक ह्रास में चरित्र के क्षेत्र में, व्यक्तिगत धरातल पर नैतिक भावना व व्यवहार की कमज़ोरी परिलक्षित होती है। इससे आघात-प्रत्याघात अपना इतिहास बनाने लगे। यही सामाजिक हास जो आज के युग की वास्तविकता है, उसकी कुछ विशेषताओं को एक फ़ैटेसी के ज़रिए धर्मवीर भारती जी ने ‘अंधा युग’ के माध्यम से पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है।
इस फ़ैटेसी का भावनात्मक केंद्र है मौजूदा सभ्यता (यथार्थ) की समीक्षा, जो महाभारत काल के कुछ चरित्रों के अंकन के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसमें चरित्रों के माध्यम से आघात प्रत्याघात द्वारा जो मानव दृश्य प्रस्तुत किया गया उसकी प्रभावकारिता और दृश्य द्वारा सभ्यता की जो आलोचना की गई, इन पहलुओं का आपसी संबंध द्रष्टव्य है। वे मानते हैं कि मौजूदा सभ्यता या समाज का यथार्थ-जैसा कि वह है- से किसी मानव प्रगति की आशा नहीं की जा सकती है। मौजूदा सभ्यता के मसीहा जिस वर्ग या श्रेणी या तबके से निकले हैं, उनके नेतृत्व में चलने वाली सभ्यता या समाज का विनाश अवश्यंभावी है। वे इस फ़ैटेसी को सफल, विचारणीय, द्रष्टव्य और विचारणीय मानते हैं। चूँकि प्रस्तुत काव्य रचना समाज की एक ढंग से आलोचना है इसलिए इसकी सीमाएँ और क्षमताओं का भी मूल्यांकन ज़रूरी है। उनका मानना है कि भारती जी ह्रास के लक्षणों और उनके कारणों को कन्फ्यूज कर देते हैं और उनके पूरे मनोलोक में समाजशास्त्रीय जिज्ञासा का अभाव है। इसलिए सभ्यता और समाज की प्रचंड उपस्थिति उनके मन में होते हुए सभ्यता और समाज के स्वरूप पर सोचने के लिए तत्पर नहीं हैं। फिर भी भारती जी ने सभ्यता और अपनी फ़ैटेसी के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा उभारे गए जिन निष्क्रिय सत्यों, तटस्थ सत्यों और अर्ध सत्यों को उद्घाटित किया है। ऐसी प्रवृत्तियाँ आज के समाज व नेतृत्व वर्ग में है। मुक्तिबोध जी, डॉ. देवराज द्वारा ‘अंधा युग’ की तुलना ‘कामायनी’ से करने पर कहते हैं कि ‘अंधा युग का लेखक दार्शनिक नहीं है। जबकि ‘कामायनी’ में विचारों और अनुभवों के सामान्यीकरण का दर्शन है और भारती जी की आलोचना उत्पीड़न विवेक का विस्फोट है। प्रकृति, दिशा और जीवन अनुभवों की दृष्टियों से ये दोनों कवि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और स्तरों के हैं। वे ‘अंधा युग’ को एक मूल्यवान कृति मानते हैं और चाहते थे कि इस पर व्यापक बहस हो । ( ‘वसुधा’ दिसंबर, 1958 में प्रकाशित)
सुमित्रानंदन पंत के काव्यों की मीमांसा करते हुए वे कहते हैं कि पंत जी में वास्तव के प्रति विशेष उन्मुखता रही। प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें केवल उपमाएँ और रूपक नहीं देता। वह पूरे रूपाकार के साथ उनके सम्मुख होता आया। उनके यौवनोन्मेष काल में प्राकृतिक सौंदर्य उनके लिए वातावरण स्थिति और परिस्थिति लेकर आया। उनमें कोमल संवेदनाओं से आत्मतृप्त एक विशेष प्रकार की अंतर्मुखता भी थी। वे संवेदनाओं के मूल बाह्य स्त्रोतों के प्रति उन्मुख थे। जिस विशेष अर्थ में पंत जी प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं, उस अर्थ में प्रसाद जी नहीं है। वे पंत की प्रसाद जी से तुलना करते हुए कहते हैं कि प्रसाद जी जिस अर्थ में अंतर्मुख कवि हैं। उस अर्थ में पंत जी नहीं। अंतर्मुखता के बिना अपने ही भावों का स्पष्ट दर्शन, उनकी जटिलता और समग्रता का आकलन, उनकी विश्लेषित व संश्लेषित अभिव्यक्ति असंभव है। ऐसी अभिव्यक्ति प्रसाद जी के पास है, पंत जी के पास नहीं। उनकी अंतर्मुखता क्षीण है। पंत जी के काव्य का यौवनोन्मेष काल प्रदीर्घ है।
उनके काव्य में नवीन भंगिमा रही आई किंतु दसियों साल बाद, उनकी कविताओं में पुरानी गूँज सुनाई दी। पुराने भाव संशोधित रूप में सामने आए और पुराने चित्र व पुरानी शैली कुछ फेरफार के साथ अवतरित हुए। लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने जो प्रयोग किए और उनमें ताज़गी है। प्रयोगों में कवि का साहस और अग्रसर होने वाली प्रतिभा की सूचना भी मिलती है। वे मानते हैं कि ‘चिंदबरा’ में संकलित बहुत सी मनोदशात्मक या प्रकृति चिंतात्मक कविताओं में वह पुरानी प्रभाव क्षमता नहीं है। तब यह प्रतीत होता है कि मनःस्थिति व्यंजक कविताओं में भी भावों के केवल रूपरेखा उपस्थित करने के बजाय कुछ और चाहिए, केवल निवेदनात्मक शैली से काम नहीं चल सकता। ‘चिदंबरा’ में वे कई स्थानों पर मात्र एक दृष्टि, एक रुख और एक झुकाव प्रकट करने लगे हैं। फलत: पंत का बहुत सा काव्य मात्र झुकाव का काव्य बनकर रह गया है। वह मात्र दृष्टि काव्य बनकर रह गया है, मर्म काव्य नहीं। ‘चिदंबरा’ की बहुत सी कविताएँ मात्र शुभेच्छाएँ और कल्याण कामनाओं की कविताएँ हैं। इस श्रेणी में बहुत सी उद्बोधनात्मक कविताएँ भी है। कुछ लोग इसे विचारों की उच्चता भी कहते हैं लेकिन यह काव्य का उच्चतम नहीं है। इन कविताओं में छंदों का अनुसरण, चमत्कारपूर्ण, भाव संगीत प्रस्तुत करने के बजाय उबानेवाली एकरसता उत्पन्न करता है। (काव्य प्रभाव की दृष्टि से ) –
लेकिन समग्रता : पंत जी के काव्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्योंकि वह जीवन को समृद्ध बनाता है। इसमें ऐतिहासिक जागरूकता है तथा मनुष्यवादी और जनवादी चेतना से उद्दीप्त है।
उनका अभिमत है कि पंत जी निराला के बाद अपनी विशुद्ध, ऐतिहासिक अनुभूति के कारण जनता के साथ हैं। वे कहते हैं कि नई कविता के कुछ क्षेत्रों में जनवाद काव्य अभिरुचि के बाहर समझा जाता है। लेकिन पंत जी दृढ़ता, साहस और धैर्य के साथ अपना कदम बढ़ा रहे हैं तथा द्विधा से बचकर एक ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, वह होगा जनमार्ग। (जनवरी, 1960 में प्रकाशित, नई कविता का आत्मसंघर्ष में संकलित )
मुक्तिबोध जी ने दिनकर जी की ‘उर्वशी’ की बहुत ही व्यापक व सूक्ष्म आलोचना की है। यह आलोचना मनोवैज्ञानिकता, ऐतिहासिकता और दर्शन को केंद्रबिंदु मानकर की गई है।
‘उर्वशी’ की मनोवैज्ञानिकता पर विचार करते हुए वे कहते हैं कि ‘उर्वशी’ का कामात्मक अध्यात्म एक अत्यंत कृत्रिम मनोवैज्ञानिक व्यापार पर स्थित है तथा शृंगार की श्रेणी से बाहर चला गया है। ‘उर्वशी’ में कोई रोमांटिक उन्मेष, शृंगार की ताजगी तथा स्फूर्ति नहीं है। इसके विपरीत उसमें बासी फूलों का सड़ापन है। छंद विधान एकरस है। इसमें रोमांटिक चंचलता नही है। पुरुरवा और ‘उर्वशी’ के वार्तालाप में भावों की आवृत्ति और पुनरुक्ति भी उबा देती है। उनका मत है कि ‘उर्वशी’ में कामुक अहंवाद का उग्ररूप उद्घाटित हुआ है। भले ही यह अहंवाद अध्यात्म का बाना धारण कर ले। वे मानते हैं कि ‘उर्वशी’ अपने सामाजिक क्षेत्र में पश्चगामी काव्य है। भगवतशरण उपाध्याय ने ‘उर्वशी’ की जो आलोचना अप्रैल, 1963 की ‘कल्पना’ में की थी उसको ध्यान में रखकर वे कहते हैं कि भगवतशरण उपाध्याय ने ‘उर्वशी’ को बाहर से भीतर की यात्रा माना है और इस यात्रा के खतरे है, वे कहते हैं कि ‘उर्वशी’ के कथातत्व या ऐतिहासिकता को लें तो हम पाते हैं कि दिनकर ने बहुत ही समारोहपूर्वक अपनी कृति ‘उर्वशी’ में चारों ओर एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आलोचना स्थापित करने का प्रयत्न किया है। दिनकर का प्रयास है कि पुरानी सांस्कृतिक परंपरा से अपने को जोड़ें, किंतु वेद-पुराण, कालिदास आदि के पास कामरहस्य (रहस्यवादी दर्शन) नहीं है जो उर्वशी में पाए जाते हैं।
पुरुरवा और उर्वशी के कथानक ने लेखक कल्पना को झकझोर दिया है। ‘उर्वशी’ एक बृहद् कल्पना-स्वप्न है, जिसके द्वारा और जिसके माध्यम से, कवि कामात्मक स्पृहाओं का आदर्शीकरण करता है और उन्हें एक सर्वोच्च आध्यात्मिक औचित्य प्रदान करता है। कथानक की ऐतिहासिकता केवल एक भ्रम है।
‘उर्वशी’ की दार्शनिकता पर विचार करते हुए वे कहते हैं कि ‘उर्वशी’ का दर्शन काव्यात्मक संवेदनाओं की आध्यात्मिक परिणति के द्योतन के लिए उपस्थित एक दार्शनिक आडंबर है।
भगवतशरण उपाध्याय द्वारा दिनकर की इन पक्तियों की आलोचना से वे सहमत हैं – “एक घाट पर किस राजा का रहता बँधा प्रणय है।” अथवा ‘रोमांचित संपूर्ण देह पर विगत चुंबन की’ अथवा ‘भारी चुंबन की फुहार’। वे कहते हैं, यह आलोचना उन लोगों को पसंद नहीं आएगी जो दिनकर के अंधभक्त हैं। लेकिन गोपाल राय इसे भगवतशरण उपाध्याय का अनर्गल प्रलाप मानते हैं। ‘उर्वशी’ को वे प्राचीन जीवन के मनोहर वातावरण की कवि प्रणीत कल्पना को बृहत् रूप देने का प्रयत्न मानते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं कि मुक्तिबोध जी ने अपने समकालीन रचनाकारों की जिन काव्यकृतियों की समीक्षा प्रस्तुत की है वह वस्तुगत, तथ्यपरक, वैज्ञानिक तथा यथार्थवादी है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.