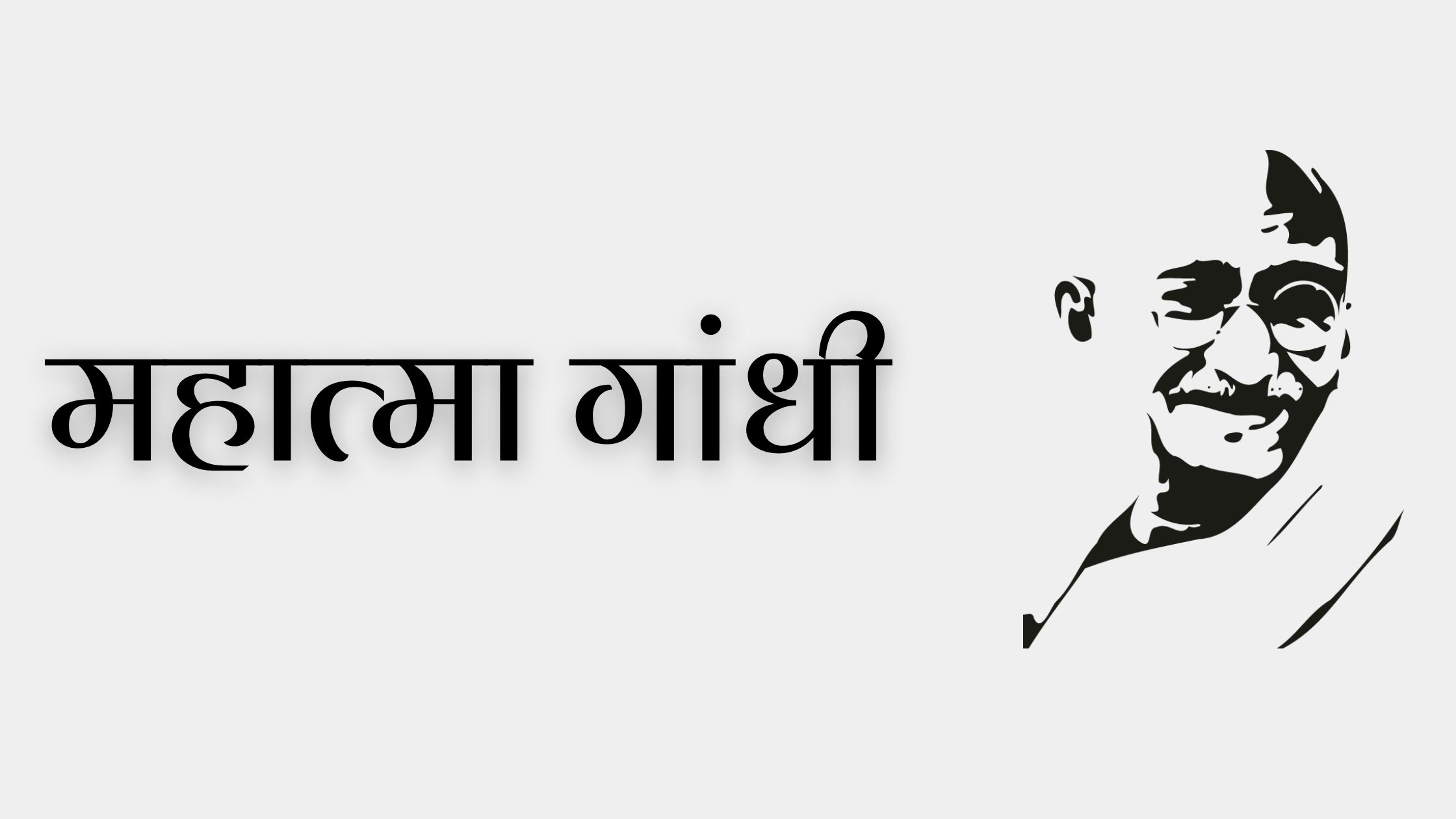— अरुण कुमार त्रिपाठी —
दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में 28 सितंबर यानी शहीदे आजम भगतसिंह के जन्मदिन पर शाम को खयालों को रौशन करनेवाली एक रोचक गोष्ठी हुई। इस गोष्ठी के केंद्र में थे महात्मा गांधी के पोते और मशहूर जीवनीकार व पत्रकार राजमोहन गांधी। हालांकि गोष्ठी के केंद्र में कोई किताब नहीं थी लेकिन यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि हाल में आजादी के अमृत महोत्सव को लक्ष्य करते हुए उनकी एक किताब भी आई है। उसका शीर्षक है—इंडिया आफ्टर 1947: रिफलेक्शन्स एंड रिकलेक्शन्स। किताब के कवर पर गांधी का चित्र है और उसका मूल संदेश यही है कि चर्चिल की बिखर जाने की भविष्यवाणी के बावजूद भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो उसकी नींव में गांधी का प्रेम का संदेश है।
महात्मा गांधी की गोद में खेलकर बड़े हुए राजमोहन गांधी से जब महात्मा गांधी के प्रति दुनिया भर में बढ़ते आदर और भारत में बढ़ती नफरत के बारे में तमाम प्रश्न किए गए तो उनका कहना था कि अगर लोग गांधी को खारिज करना चाहते हैं, उनका अपमान करना चाहते हैं और उन्हें भूल जाना चाहते हैं तो वैसा हो जाने दीजिए। आप गांधी को बचाने की लड़ाई मत लड़िए। अगर लड़ना है तो नफरत को मिटाने की लड़ाई लड़िए। किसी से नफरत मत कीजिए सिवाय नफरत से नफरत करने के। परिस्थितियां गंभीर हैं, मैं नहीं जानता कि हम में से कितने लोग कुछ दिनों बाद जेलों में होंगे या बाहर होंगे। लेकिन याद रखना होगा कि 1947 में गांधी के सामने इससे भी ज्यादा गंभीर स्थितियां थीं। तब देश आजाद नहीं हुआ था और बॅंटवारा सिर पर खड़ा हो गया था, सांप्रदायिकता का दानव भारत के सिर पर सवार हो गया था। लेकिन गांधी ने किसी से नफरत न करने और किसी से भयभीत न होने के सिद्धांत के तहत उसका सामना किया। इस लड़ाई में प्रेम और अभय उनका हथियार बना। आज भी अगर नफरत की इस लड़ाई के पार जाना है तो अहिंसा के उन हथियारों में विश्वास पैदा करना होगा।
उस गोष्ठी में मौजूद इस लेखक के अलावा राहुल देव, चंद्रभूषण, संतोष भारतीय, राजेश जोशी, विनोद अग्निहोत्री, हरिमोहन मिश्र और अपूर्वानंद जैसे कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्राध्यापकों की राजमोहन गांधी से यह जानने की बेचैनी थी कि आखिर इस दौर की नफरत कैसे मिटेगी और इस उद्देश्य को पाने में महात्मा गांधी का जीवन और विचार कैसे मददगार हो सकता है। इस पर राजमोहन गांधी ने एक अमरीकी लेखक का हवाला देते हुए कहा कि उनका मानना है कि बीसवीं सदी का बड़ा आविष्कार आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत और परमाणु बम नहीं है बल्कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह है।
गांधी का सत्याग्रह क्या है और उसे कैसे और कौन कैसे कर सकता है? यह एक गंभीर सवाल है। क्या ईश्वर में विश्वास न करनेवाला व्यक्ति भी सच्चा सत्याग्रही हो सकता है? क्योंकि गांधी ने तो उसके लिए आस्थावान होने की शर्त लगाई है। इस संदर्भ में क्या राहुल गांधी सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या उनकी पदयात्रा सफल होगी? राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े और पुराने समाजवादी विजय प्रताप का यह सवाल पूरे माहौल को गंभीर कर गया। इस सवाल पर राजमोहन गांधी ने पहले तो यह संकेत करते हुए चर्चा को बढ़ाना चाहा कि आस्तिक भी सत्याग्रही हो सकता है और नास्तिक भी। लेकिन फिर उन्होंने हथियार डालते हुए कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। यह एक बड़ी वजह है जिसके नाते डा राममनोहर लोहिया जैसा गांधी का अनुयायी भी अनशन और सत्याग्रह करने से संकोच करता था।
सत्याग्रह के जो नियम गांधी ने बनाए थे उन पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उनकी ईश्वर में जितनी अगाध आस्था थी उतनी इस युग में उनकी भी नहीं है जो तमाम देवी-देवताओं के मंदिरों और जन्मस्थानों के बहाने अपनी राजनीति खड़ी करते हैं। इसलिए हमें सत्याग्रह के उस अर्थ की ओर देखना होगा जो गांधीजी ने हिंद स्वराज में बताया है। उन्होंने सत्याग्रह को दयाबल कहा है, आत्मबल कहा है और फिर बाद में सत्याग्रह कहा है। इसे समझाने के लिए उन्होंने तुलसीदास का वह दोहा भी प्रयोग किया है —-
दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान।
तुलसी दया न छांड़िए जब तक घट में प्रान।।
सत्याग्रही के लिए ईश्वर में आस्था रखने का मतलब उस समय बदल जाता है जब गांधी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। हालांकि वे पहले कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है। सत्य और ईश्वर की इस प्रकार अदला बदली के बाद दी गई ऐसी परिभाषा से उन्होंने यह गुंजाइश बना दी थी कि प्रयोगशाला का वैज्ञानिक भी सत्याग्रह कर सके और नास्तिक व्यक्ति भी। क्योंकि सबके अपने अपने सत्य होते हैं।
प्रोफेसर अपूर्वानंद का यह कथन सबको खामोश करनेवाला था कि असली सत्याग्रह तो मुस्लिम समाज कर रहा है। उमर खालिद और शलजील इमाम जैसे युवा जेलों में सड़ रहे हैं और उनके अधिकारों पर राजनीतिक दलों की चुप्पी है। लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं लेकिन उसकी या तो वाहवाही हो रही है या खामोशी है। यह चुप्पी बहुसंख्यक समाज की ओर से है। लोकतांत्रिक संस्थाओं ने उनकी ओर न्याय की दृष्टि डालनी बंद कर दी है। उनके प्रति कब न्याय होगा कहा नहीं जा सकता। इस अन्यायपूर्ण स्थिति में गांधी के स्मरण से बहुत काम चलनेवाला नहीं है।
गांधी तो खामोश हैं अब उनको क्यों परेशान किया जा रहा है। उनकी हत्या के बाद का अंधेरा गहरा गया है। सन्नाटा लंबा हो गया है। उनके कथन से सहमति जताते हुए राजमोहन ने जो प्रतिप्रश्न किया वह गोष्ठी में और सन्नाटा पैदा करनेवाला था। राजमोहन गांधी ने पूछा था कि क्या इस गोष्ठी में कोई मुस्लिम भाई भी हैं। किसी भी कोने से आवाज नहीं आई। यह बात राजमोहन को उसी तरह अखरने वाली थी जैसे कि आखिरी दिनों में गांधी की प्रार्थना सभाओं की स्थिति होने लगी थी। लेकिन गांधी को न छेड़ा जाए इस टिप्पणी पर गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत का कहना था कि वो तो कह गए हैं कि मैं कब्र से बोलूंगा। जब वह बोलेंगे तो उन्हें कौन रोकेगा।
राजमोहन गांधी ने ‘मोहनदास—स्टोरी आफ ए मैन, हिज पीपुल एंड अम्पायर’ जैसी गांधी की चर्चित जीवनी लिखी है। यह पुस्तक 2019 में गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती पर प्रकाशित हुई थी। ‘हिंद स्वराज’ पर केंद्रित उनकी पुस्तक `व्हाई गांधी स्टिल मैटर्स’ 2017 में आई थी। वे सरदार पटेल की जीवनी `पटेल अ लाइफ’ शीर्षक से लिख चुके हैं। `फंडामेंटल्स आफ मुस्लिम माइंड’ शीर्षक से छपी उनकी किताब इस उपमहाद्वीप के मुस्लिम चिंतन को समझने में सहायक है। ‘कानफ्लिक्ट एंड रिकानसिएलेशन्स’ नामक उनकी पुस्तक विभाजन की त्रासदी और इस उपमहाद्वीप के भविष्य को लेकर की जानेवाली चिंताओं और उम्मीदों पर केंद्रित है। गांधी पर ही केंद्रित उनकी पुस्तक ‘अ गुड बोट्समैन’ मोहनदास वाली पुस्तक का पूर्वाभ्यास लगती है। वे गांधीजी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी के पुत्र हैं। उनकी मां लक्ष्मी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बेटी थीं। देवदास गांधी हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। राजमोहन गांधी इंडियन एक्सप्रेस के बंबई संस्करण के संपादक भी रहे। वे 1989 में राजीव गांधी के विरुद्ध अमेठी से चुनाव भी लड़े थे। एक बार वे पूर्वी दिल्ली से भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे। वे लोकसभा का चुनाव तो नहीं जीत सके लेकिन राज्यसभा के सदस्य रहे। उनके एक भाई रामचंद्र गांधी थे जिन्हें लोग प्यार से रामू गांधी कहते थे। उनकी छवि एक दार्शनिक की थी। रामू गांधी अब इस दुनिया में नहीं हैं। राजमोहन के एक और भाई गोपाल कृष्ण गांधी पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। वे भी अन्य भाइयों की तरह लेखक और विचारक हैं।
मानवाधिकारों का मुकदमा लड़ने वाले एक सिख वकील ने यह कहकर सत्याग्रह का झंडा इतिहास की गहराई में गाड़ दिया कि अगर सत्याग्रह की बात 1869 में पैदा हुए गांधी कर रहे थे तो चार सौ साल पहले 1469 में पैदा हुए नानक भी प्रेम की बात कर रहे थे। यानी यह सिलसिला लंबा है और इसीलिए महात्मा गांधी का यह कथन महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि हिस्टरी इन अच्छी बातों को दर्ज नहीं करती। वह तो राजाओं महाराजाओं की मारकाट और विजय पराजय को दर्ज करती है। लेकिन अगर सारा मानव इतिहास हिंसा और नफरत से भरा होता तो अब तक मानव सभ्यता नष्ट हो गई होती। एक भी इंसान जिंदा न बचता। इसलिए इतिहास में जितनी हिंसा की घटनाएं हैं उससे कहीं ज्यादा अहिंसा और प्रेम का सिलसिला है।
पत्रकार राहुल देव का सुझाव उचित था कि नफरत फैलानेवाले जिन लोगों से हम लड़ रहे हैं उनके प्रति हमें कड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनसे भी प्रेम और विनम्रता से संवाद करना चाहिए। इससे नफरत कम करने में मदद मिलेगी। यहां गांधी का आदर्श काम आ सकता है। वे किसी के प्रति बहुत कटु नहीं होते थे। यहां तक कि अंग्रेजों के प्रति भी। इस पर कुमार प्रशांत का कहना था कि गांधी निजी तौर पर कटु भले न होते हों लेकिन जिन विचारों और प्रवृत्तियों का विरोध करते थे उसके लिए कठोर वचन कहने में भी झिझकते नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि पैगम्बर मोहम्म्द की सीख के अनुसार यह सभ्यता शैतानी सभ्यता है। आउटलुक के संपादक हरिमोहन का कहना था कि नफरत है लेकिन माहौल इतना कठिन और डरावना भी नहीं है। हिंदुत्ववादियों के दुष्प्रचार के चलते ही बहुत सारे गांधीविरोधी भी गांधी की ओर आकर्षित हुए हैं। उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और गांधी के प्रति आदर विकसित किया है। उनमें मार्क्सवादी भी हैं और आंबेडकरवादी भी। यह गांधी का प्रभाव ही है कि अब हिंदुत्ववादी खुलेआम गांधी को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करता। वह जो भी करता है परोक्ष रूप से या छुपकर करता है। एक चुनाव की बात है, नफरत करनेवाले खामोश हो जाएंगे।
गांधी स्मारक निधि के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ गांधीवादी रामचंद्र राही ने कहा कि निश्चित तौर पर इस तरह की चर्चाओं को बंद कमरों से बाहर सड़क और चौराहों पर ले जाने की जरूरत है। हमारी सीमाएं हैं इसलिए हम संस्थानों के हाल में बहसें करते हैं। लेकिन हम अपनी खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं।
राजमोहन गांधी ने गोष्ठी की शुरुआत इस बात से की थी कि 1922 में जब गांधी को राजद्रोह के आरोप में छह साल की सजा हुई तो उन्होंने अपना व्यवसाय बुनकर और किसान लिखवाया था। उन्होंने जीवन में कई भूमिकाएं निभाईं लेकिन एक पत्रकार के रूप में उनकी बड़ी भूमिका थी। बहुत सारे पत्रकार और लेखक उनसे सीख सकते हैं क्योंकि वे अपने पास आनेवाले पत्रकारों को रिपोर्ट कैसी लिखी जाए, यह सिखाते भी थे। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रकार विलियम शरर की तरह कहा कि गांधी एक साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने जो किया वह हम में से कोई भी कर सकता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम में से ही कोई एक दिन वैसा बड़ा काम करेगा। लेकिन विलियम शरर ने इसी बात को थोड़ा अलग ढंग से कहा था। उनका कहना था कि गांधी, बुद्ध, ईसा और सुकरात जैसे लोग अपने को बेहद साधारण व्यक्ति मानते थे। यह उनकी विशेषता थी। इसीलिए वे समझते थे कि वे जो काम कर रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन यही उनकी भूल थी। (क्योंकि साधारण व्यक्ति वह कर नहीं सकता।) राजमोहन गांधी ने विश्वास दिलाया कि आज भले ही नफरत का दौर है लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा, एक दिन जरूर प्रेम की जीत होगी।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.