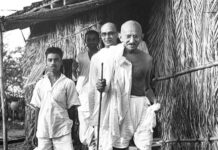— अरविन्द मोहन —
जिन राममनोहर लोहिया को आज पण्डित नेहरू का सबसे बड़ा ‘दुश्मन’ माना जाता है, वे खुद को कुजात गांधीवादियों का सरदार मानते थे। यह भी तथ्य है कि नेहरू ही कभी उनके नेता थे। अब उन्होंने नेहरू से गांधी तक का सफर कैसे तय किया, यह बहुत लम्बी चर्चा की माँग करता है लेकिन इतना कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस बदलाव में न तो कोई न्यस्त स्वार्थ काम कर रहा था, न कोई व्यक्तिगत द्वेष था और न ही लोहिया किसी महत्त्वाकांक्षा के वश में होकर ऐसा कर रहे थे। इसी के चलते नेहरू-लोहिया टकराव में काफी सारे लोग नेहरू-गांधी का टकराव भी देखते थे और हैं। यह बात असलियत में काफी करीब है इसलिए लोहिया की आलोचना का तब भी बहुत वजन रहा और आज भी उनका मान इसलिए है कि उन्होंने समय रहते अपने उस्ताद नेहरू को टोकने में, उनका विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
पर आज इस टकराव को याद करनेवालों का स्वार्थ निश्चित रूप से अलग है। वे अपने रास्ते में गांधी के विचारों को तो बाधक मानते ही हैं और उनका नाम सिर्फ कर्मकाण्ड के तौर पर लेते हैं। पर उनको नेहरू का कद भी परेशान करता है। और इस भारी मूरत को तोड़ पाना भी उनके वश का नहीं है। सो, वे लोहिया के हथौड़े से ही इस मूर्ति पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। पर बिना साधन और मुट्ठीभर सहयोगियों के साथ अगर लोहिया का हथौड़ा नेहरू को चोट पहुँचा रहा था, उनको विचलित कर रहा था, उनकी तब बन गयी वटवृक्ष सी छवि को तोड़ रहा था तो इसका कारण लोहिया की ईमानदारी, निस्वार्थ भावना और सच के साथ खड़े रहना था। लोग उनपर भरोसा करते थे, गांधी जितना न भी हो तो उन्हीं की तरह का भरोसा। लोहिया घर फूँक तमाशा देखने वाले थे।
और एक दौर था जब लोहिया का मानना था कि मूल्क में डेढ़ लोग ही हैं, एक गांधी और आधा नेहरू। नेहरू ने अपने से छोटे और बाद में आजादी की लड़ाई में शामिल, नयी पढ़ाई करके आए लोहिया ही नहीं जे.पी., के.एम. अशरफ और जेड.ए. अंसारी जैसे युवकों को सीधे कांग्रेस के मुख्यालय में बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ देकर काफी लोगों को चौंकाया।
लोहिया के जिम्मे कांग्रेस का विदेश विभाग था। इन सबको इलाहाबाद रहना था पर जमकर रहे सिर्फ लोहिया। वे कृपलानी परिवार के साथ रहे जिनकी नयी शादी हुई थी। कृपलानी जी के दावे को मानें तो लोहिया के मन से गांधी को लेकर बनी भ्रांतियां मिटाने और साम्यवाद से मोड़ने में उनकी और सुचेता जी की भी कुछ भूमिका थी। इस दौरान लोहिया ने कांग्रेस की विदेश नीति के कामकाज को व्यवस्थित करने और उसकी दिशा को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाई। नेहरू खुद नीति के जानकार थे और हमारी आजादी की लड़ाई उपनिवेशों से भरी दुनिया के लिए एक बड़े आकर्षण का केंद्र थी। इस आकर्षण का लाभ लेते हुए लोहिया ने पचासों देशों से सीधा संबंध विकसित किया और अपनी खास राजनीतिक दृष्टि से यूरोप, अमरीका और सोवियत संघ से बराबर दूरी रखने की गुट-निरपेक्ष नीति की शुरुआत करायी, जो लंबे समय तक हमारी विदेश नीति का मुख्य सूत्र थी। पर 1946 से जिस तरह नेहरू समेत अधिकांश शीर्ष नेता सत्ता के बँटवारे में लगे उससे लोहिया उनसे दूर होते गये।
विभाजन और सांप्रदायिक मारकाट के दौर में भी लोहिया पूरी तरह गांधी के साथ रहे, दंगाग्रस्त जगह पहुँचकर शांति कायम करने की मुहिम में थे और स्वाभाविक तौर पर सरकार से शिकायत लिये रहे लेकिन नेहरू के खिलाफ खुलकर बोलना उन्होंने 1949 से शुरू किया। धीरे-धीरे यह हालत हो गई कि सिर्फ वही बोलते थे। और हालत यहाँ तक पहुँची कि चुनाव में बुरी तरह पिटी और बार-बार विभाजित पार्टी का नेता होने के चलते नेहरू के खिलाफ लोहिया की आवाज शुरू में अनसुनी की गई। उनको पगला माना जाता था। तब नेहरू और कांग्रेस का जलवा था। यह चलन भी था कि बड़े नेताओं के खिलाफ विपक्ष उम्मीदवार ही नहीं उतारता था क्योंकि उनका संसद पहुँचना जरूरी माना जाता था। मगर लोहिया ने इस परंपरा को तोड़ा और खुद उस फूलपुर से नेहरू से खिलाफ उतरे जहाँ उनका कोई काम न था। नेहरू न सिर्फ वहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री थे बल्कि 30 के दशक से उस इलाके को अपने चुनाव क्षेत्र के तौर पर सींच रहे थे लेकिन चुनाव में लोहिया हारकर भी जीत गये। उन्हें नेहरू से आधे वोट मिले। फिर लोहिया एक उपचुनाव जीतकर संसद पहुँचे। उनकी जीत की खबर के साथ ही ‘स्टेट्समैन’ ने कार्टून छापा : ‘बुल इन द चाइना शाप’।
सचमुच लोहिया ने संसद पहुँचकर काफी हंगामा किया और सारी व्यवस्था को उलट-पुलट दिया। उन्होंने किन-किन विषयों को बहस के लिए उठाया, किन-किन सरकारी नीतियों और फैसलों पर सवाल खड़े किये, संसद चलाने के किन-किन प्रावधानों का पहली बार इस्तेमाल करते हुए सरकार को घेरा, विपक्ष को एकजुट किया और संसद में हिन्दी में बहस शुरू करा के मुल्क को किस तरह जुबान दी यह पूरी कहानी बहुत बड़ी है लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के खर्च और आम जन की आमदनी (दो आना बनाम 20 हजार), तिब्बत का सवाल, हिन्दी का सवाल, राज्यों में लोकतान्त्रिक ढंग से चुनी सरकारों को गिराने का मसला और सबसे बढ़कर चीनी हमले पर सरकार को घेरकर अच्छा-खासा बवाल मचाया और पण्डित नेहरू की सारी चमक धूमिल की। इस चक्कर में नेहरू को अपने प्रिय मित्र कृष्ण मेनन की बलि देनी पड़ी। संसद में डॉ. लोहिया और उनके मुट्ठीभर साथियों की भूमिका ने उन्हें और समाजवादी दल को विपक्षी राजनीति का केंद्र बनाया और गैर-काँग्रेसवाद की दरम्यानी राजनीति परवान चढ़ी। नतीजा देखने के लिए नेहरू जीवित न थे लेकिन हिन्दी पट्टी से काँग्रेस की जड़ें 1967 में ही हिल गयीं।
लोहिया 50 के दशक में अमरीका गये तो उनका नेहरू विरोधी सुर कुछ नरम था। उनकी छवि से परिचित और सनसनी में ज्यादा भरोसा करने वाले अमेरिकी पत्रकारों ने उनसे तरह-तरह के प्रश्न किये और मुख्य रूप से नेहरू के खिलाफ उनको भड़काना चाहा। विदेश में अपने प्रधानमंत्री की सीधी आलोचना से जब डॉ. लोहिया बचते रहे तो न्यू हैम्पशायर में सीधा यही प्रश्न आया कि आप नेहरू का इतना विरोध क्यों करते हैं? अब उनका बचना मुश्किल था। सो, उन्होंने कहा कि मैं पण्डित नेहरू से सबसे ज्यादा स्नेह करता हूँ, इसीलिए क्रोध भी ज्यादा करता हूँ।
संयोग से जब पण्डित नेहरू की मौत हुई तब भी लोहिया अमरीका में ही थे और उनके नाम पर ऊटपटांग बयान भी चला जिसका बाद में खण्डन-मण्डन होता रहा। लेकिन 50 के दशक वाली यात्रा में डॉ. लोहिया जब आइंस्टीन से मिलने गये तब उन तक भी यह सूचना थी कि लोहिया किस तरह नेहरू की आलोचना करते हैं। सो, उन्होंने लोहिया से वस्तुस्थिति जानी और फिर यह भी पूछा कि नेहरू में ऐसा बदलाव क्यों हुआ। नये और पुराने नेहरू में क्या फर्क है? डॉ. साहब ने कहा, ‘नेहरू एक श्रेष्ठ सवार हैं। घोड़ा अब भी वही है लेकिन लगाम थामने वाला चला गया है। गांधी होते तो उन्हें रास्ते से इस तरह भटकने नहीं देते।’
डॉ. लोहिया और नेहरू के बारे में एक और प्रसंग की चर्चा करके इस कहानी को समाप्त किया जाए तो बेहतर होगा। डॉ. लोहिया आजीवन अकेले रहे, परिवार नहीं बनाया, घर नहीं बनाया, जमीन-जायदाद के नाम पर एक बक्सा किताब और दो-तीन जोड़ी कपड़े। कोई बैंक खाता नहीं, कोई जमा राशि नहीं। अनियमित जीवन, भारी बौद्धिक तनाव से ब्लड प्रेशर हो गया। तब लोग इस मर्ज से कम डरते थे, इसके एक दुष्प्रभाव, लकवा से ज्यादा डरते थे। कभी दोस्तों के साथ बेठकों में इसी समस्या पर बात हो रही थी। किसी ने पूछा कि अगर आप लकवा का शिकार हुए तो कहाँ जाएँगे?आपको सबसे अच्छी देख-रेख कहाँ होने की उम्मीद है? साथ बैठे सभी लोगों को उम्मीद थी कि वे हैदराबाद के अपने व्यवसायी मित्र बदरीविशाल पित्ती का, फारबिसगंज और कोलकाता के अपने बालसखा बालकृष्ण गुप्त जैसे किसी का नाम लेंगे। पर डॉ. लोहिया ने पण्डित नेहरू का नाम लेकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, ‘जब अपना कोई वश नहीं रहेगा तो मैं उसी नेहरू पण्डित के घर जाऊँगा क्योंकि मेरी उससे अच्छी देखरेख कहीं और नहीं हो सकती।’ तो यह था पण्डित नेहरू और डॉ. लोहिया का रिश्ता।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.