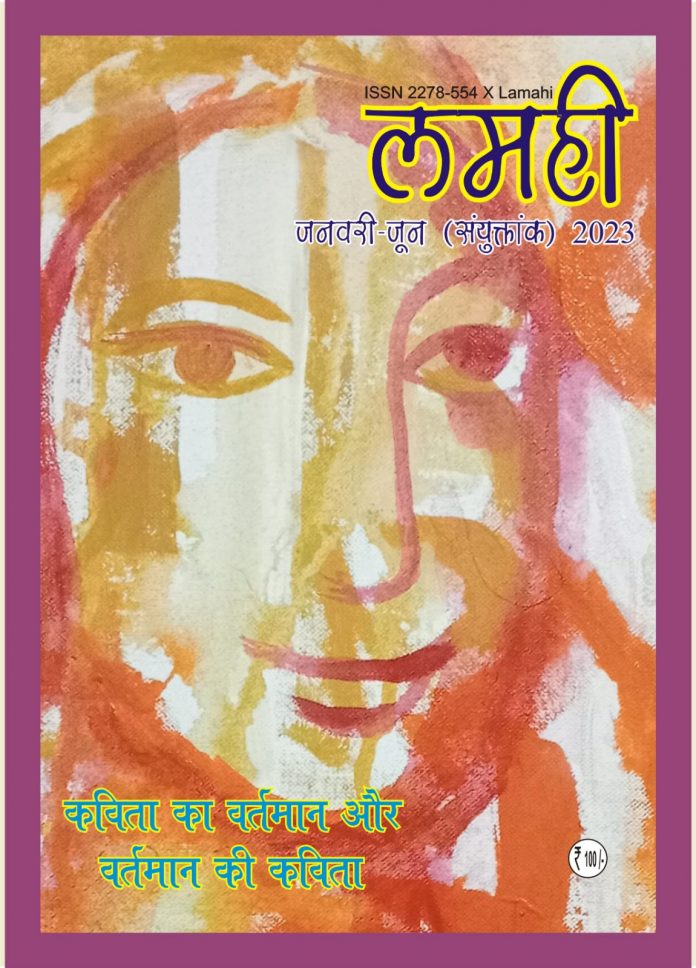— संजय गौतम —
पिछले वर्षों में लमही (संपादक – विजय राय) ने अपने विशेषांकों से खासी प्रतिष्ठा अर्जित की। कोविड समय में संसाधनों की कमी के चलते इसका मुद्रित संस्करण बंद हुआ, लेकिन ऑनलाइन संस्करण जारी रहा। नाटनल पर उपलब्ध इस पत्रिका के अमृत राय, प्रबोध कुमार, साहित्य में संयुक्त मोर्चा विशेषांक बहुचर्चित रहे। सामग्री की गुणवत्ता से अंकों को किताब के रूप में प्रकाशित कराने की जरूरत महसूस होती है। इसी क्रम में ‘लमही’ का यह अंक ‘कविता का वर्तमान और वर्तमान की कविता’परंंंंं केंद्रित है। अंक के अतिथि संपादक हैं शशिभूषण मिश्र।
लगभग दो सौ पृष्ठों के इस अंक को दो खंडों में बॉंटा गया है। पहले खंड में परिचर्चा रखी गई है और दूसरे खंड में कविता पर विचारपरक तीस से अधिक आलेख प्रस्तुत किए गए हैं। ‘परिचर्चा’ के लिए कवियों के समक्ष जो सवाल रखे गए हैं वे हैं–कविता के वर्तमान को आप किस तरह देखते हैं? कविता के समक्ष आज की प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? बीसवीं सदी के अंतिम दशक में उपजी कविता के प्रस्थान बिंदु क्या हैं? इक्कीसवीं सदी की कविता के सामने प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? क्या लक्ष्यों को लेकर कवियों में कोई साझापन दिखता है? क्या आप जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र कई तरह के दबावों में है? क्या इससे कविता पर भी दबाव पड़ा है? इससे कविता में क्या कोई बदलाव आए हैं? हमारी सभ्यता में जिस तरह हिंसा की जगह बढ़ती जा रही है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? ऐसे में कविता और कवि की क्या भूमिका हो सकती है? सूचना प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया और वर्चुअल माध्यमों में कविता की भाषा, अभिव्यक्ति और शिल्प पर क्या प्रभाव पड़ा है? इन माध्यमों से कविता के प्रसार और प्रभाव में किस तरह के बदलाव आए हैं? क्या कविता के समक्ष सम्मुख आलोचना मौजूद है? कविता की समकालीन आलोचना पर आपकी क्या राय है?
इन सवालों के जवाब दिए हैं–अनामिका, अशोक वाजपेयी, विजय कुमार, हरीश्चंद्र पांडेय, ए. अरविंदाक्षन, अरविंद त्रिपाठी, असद जैदी, विनोद दास, कात्यायनी, प्रियदर्शन, नरेश सक्सेना, राजेश जोशी, अरुण कमल, रघुवंश मणि त्रिपाठी, शिरीष कुमार मौर्य, अरुण देव, जितेंद्र श्रीवास्तव, कुलदीप कुमार, सविता सिंह ने।
इन सवालों के परिप्रेक्ष्य में उल्लिखित सभी कवियों, साहित्यकारों द्वारा जवाब दिए गए हैं। ये जवाब हमारे सामने वर्तमान संकट, चुनौतियों, आशाओं, आकांक्षाओं का व्यापक परिदृश्य रचते हैं। वर्तमान समय में लोकतंत्र के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों क ह्रास सभी की चिंता के मूल में है। सभी की दृष्टि में कविता अपनी तरफ से प्रतिपक्ष रच रही है और हिंसक होते समय में मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना के विस्तार का अपनी तरह से प्रयास कर रही है। अशोक वाजपेयी कहते हैं- ‘इस परिस्थिति में कवि और कविता दोनों ही तटस्थ या मूकदर्शक नहीं रह सकते। उन्हें अपनी और कविता की मानवीयता और प्रासंगिकता की रक्षा करने के लिए ऐसा ही होना चाहिए। सौभाग्य से कवि और कविता दोनों ही अधिकांशत: इन शक्तियों के पाले में नहीं गए हैं, जो लोकतंत्र को हिंसा, हत्या, बलात्कार, विस्मृति और प्रतिशोध की भावनाओं से विकृत कर रही हैं पर जिन्हें व्यापक हिंदी समाज के एक बड़े और निर्णायक हिस्से का समर्थन प्राप्त है’।
दूसरे खंड में तीस से अधिक आलेख हैं, जो कविता को विविध कारणों से देखते परखते हैं। हालाँकि अंक का उद्देश्य बीसवीं सदी के आखिरी दशक की कविता को प्रस्थान बिंदु बनाकर कविता के वर्तमान को परखने का है, लेकिन लेखकों ने समकालीनता के दायरे में और पहले के समय को भी विचार की सीमा में लिया है और बदलती हुई प्रवृत्तियों को परखा है। बीसवीं सदी का आखिरी दशक यानी उन्नीस सौ नब्बे-बानवे के बाद का समय इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसी समय भूमंडलीकरण की शुरुआत होती है। इसके पहले सोवियत संघ का विघटन हो चुका रहता है और एक बड़ा सपना टूट गया होता है। भारत इसी समय मिश्रित अर्थव्यवस्था को पीछे करते हुए उदारीकरण के रथ पर सवार होता है। इसी समय विदेशी पूंजी, विनिवेश, निजीकण, बाजारीकरण, उदारीकरण, मल्टीनेशनल जैसे शब्द गूंजने शुरू होते हैं और गूंजते चले जाते हैं, सकारात्मक अैर सुंदर शब्द जीवन में नकारात्मक अर्थ भरते चले जाते हैं। इसी समय अस्मितावादी विमर्श अपने-अपने समुदायों के भीतर जागृति का संचार करते हैं। दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक उठ खड़े होते हैं और अपना हिस्सा पुरजोर तरीके से मांगते हैं, जीवन में भी, साहित्य में भी। इसी समय सांप्रदायिकता का नया ज्वार आता है, और भारतीय समाज के व्यापक ‘हिंदूकरण’ की शुरुआत होती है।
इक्कीसवीं सदी का दो दशक बीतते-बीतते लिखने पढ़ने वालों के मन में निराशा का बोध गहरा होता जाता है, क्योंकि जैसा भी हो बीसवीं सदी में देखा गया स्वतंत्रता, समता और न्याय का सपना नए अर्थतंत्र के वैभव, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आगे चूर होता दीखने लगता है, वह भी लोकतांत्रिक माध्यमों का प्रयोग करके। साहित्यकारों के सामने न कोई बड़ा सपना बचा रहता है, न पक्ष-प्रतिपक्ष की सरल रेखा की पहचान बचती है। हर आदमी के भीतर ऐसा पक्ष उभरता है, जो प्रतिपक्ष में खड़ा है। लक्ष्यहीनता और बेचैनियों का समय है। इन्हीं बेचैनियों के बीच कवि-साहित्यकार संवेदान का राग और आग बचाए रखने के लिए प्रयासरत हैं।
इन आलेखों में यह व्यापक परिदृश्य उभरता है और हम कवियों, आलोचकों की चिंता और चिंतन से रूबरू होते हैं। विनोद शाही ने ‘समकालीन कविता की बीजभूमि’, आमिष वर्मा ने ‘दलित कविता का वर्तमान’, पार्वती तिर्की ने आदिवासी कविता का परिदृश्य, मृदुला सिंह ने ‘श्रम का लोकपक्ष : आदिवासी कविता का वर्तमान’, अंजन कुमार ने ‘विकास की आंधी में उजड़ते लोग’, अंकिता तिवारी ने ‘प्रतिरोध और प्रेम के बहाने स्त्री कविता के वर्तमान’, विकास कुमार यादव ने ‘समकालीन कविता में पर्यावरणीय विमर्श’, अंजन कुमार पांडेय ने ‘नवगीत विधा का सामयिक संघर्ष’ जैसे विषयों से अंक को समृद्ध किया है। कुमार अंबुज का आलेख ‘समकालीनता : अनुभव, संघर्ष और आशा का समुच्चय’ हमें स्मृति के माध्यम से कविता के संघर्ष और उम्मीद की यात्रा कराता है। वह कहते हैं, ‘समकालीन कविता की जगह प्रतिपक्ष की बेंच है। यह उसका स्थायी अड्डा है। वह सदैव जो है उससे बेहतर चाहिए की कल्पना में इस तरह शामिल है कि जीवन में उसे लागू किया जा सके। इस तरह वह एक सक्रिय कार्यवाही भी है। वह सत्ता संरचनाओं के विरुद्ध है और वंचित मनुष्यों के, उपेक्षित समाज के साथ स्वाभाविक रूप से खड़ी है। ये सब कारण और लक्षण मिलजुलकर ही उसे ‘समकालीन कविता’ बनाते हैं’।
अच्युतानंद मिश्र की समकालीन कविता से शिकायत है, ‘संपूर्णता में कविता का कोई प्रभाव अब निर्मित नहीं होता। किसी एक विषय की कविता किसी दूसरे विषय की कविता से जुड़ सकती है, किसी तकनीकी तर्क के माध्यम से किसी एक कवि की कविता के टुकड़ों को किसी दूसरे कवि की कविता के टुकड़ों के ऊपर आरोपित कर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तरह कविता की संपूर्णता एवं प्रभावोत्पादकता का अंत हो चुका है। कविता के टुकड़े एक गतिशील चाक्षुष माध्यम का प्रभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में संप्रेषणीयता को ही प्रभाव मान लिया जाता है।’ बसंत त्रिपाठी ने कविता की भाषा में बदलाव को रेखांकित करते हुए विस्तार से लिखा है तो अनुराधा सिंह ने कविताओं के कुपाठ पर चर्चा की है।
इस अंक में सोशल मीडिया के माध्यम से उपजी कविता की तात्कालिकता पर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है। हजारों की संख्या में रोज लिखी जा रही, पोस्ट की जा रही और लाइक-शेयर की जा रही कविताओं में से बेहतर कविता की तलाश एक चुनौती है, लेकिन सकारात्मकता इस बात में है कि रचना का लोकतंत्र वृहत्तर हुआ है।
इस ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि वर्तमान समय में अधीरता के कारण कविता की बुनावट, शिल्प, कविता के दर्शन, कहन पद्धति, लय, छंद, अमूर्तन, प्रतीक, बिंब जैसे विषयों पर अनुशीलन, चिंतन, मनन, लेखन नहीं के बराबर हो रहा है। संपादकीय में यह शिकायत दर्ज की गई है कि इन विषयों पर बहुत प्रयास करने के बाद भी स्वतंत्र आलेख नहीं मिले। कविता के इन पक्षों पर चिंतन न करने और स्वसंपादन की दक्षता की कमी के चलते ही कविता का अधिसंख्य हिस्सा ब्योरों से भरता जा रहा है और हमारी स्मृति का हिस्सा नहीं बन पा रहा है।
इस अंक के पाठ से हम इन सभी विषयों पर गहन विचार-विमर्श में भागीदार होते हैं। यह अंक कविता पर विमर्श को एक कदम आगे ले जाता है।
पत्रिका – लमही
संपादक – विजय राय
अतिथि संपादक – शशिभूषण मिश्र
मूल्य – ₹100 मात्र
www.notnul.com पर उपलब्ध
मो.- 9454501011
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.