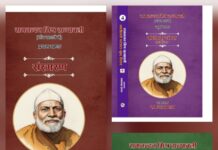9 सितम्बर 1947। भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन दिल्ली की हवा आज़ादी की खुशबू नहीं, बल्कि खून और बारूद की गंध से भरी थी। हर जगह शरणार्थियों की लंबी कतारें थीं—किसी का घर छिन गया, किसी का परिवार बिछुड़ गया। दर्द, गुस्सा और अविश्वास ने दिल्ली को घेर लिया था।
इन्हीं हालात में गांधी 9 सितंबर 1947 को नोआखली और कोलकाता का मिशन पूरा कर दिल्ली आए। सरदार पटेल ने कहा—“बापू, इस बार आप अपनी आदत के मुताबिक दलित बस्ती में नहीं ठहर सकते। वहां भी शरणार्थी भरे पड़े हैं। आपके लिए बिड़ला हाउस तय किया गया है।”
गांधी दो सादे कमरे और बरामदा वाले बिड़ला हाउस में रुकते हैं। गांधी समझ चुके थे कि इन हालातों में दिल्ली हाथ से निकलने वाली है। वे अपने चुनिंदा साथियों के साथ रोज़ पैदल निकलते—कभी शाहदरा, कभी पुरानी दिल्ली, कभी करोल बाग। वे किसी मंत्री की तरह भाषण नहीं देते, वे किसी धर्मगुरु की तरह उपदेश नहीं करते। वे बस चुपचाप लोगों के बीच जाते और उनकी पीड़ा को अपने भीतर उतार लेते।
फिर आया महरौली का दिन। जैसे ही गांधी पहुंचे, हजारों की क्रुद्ध भीड़ ने गांधीजी को घेर लिया। गालियाँ बरसने लगीं—“तुम्हारे कारण हमारी ये हालत हुई है… किस मुँह से आए हो?”
मीरा बेन सहम गईं—“अब बापू बचेंगे नहीं।”
किसी ने तो उन पर थूक भी दिया। लेकिन गांधी ने बिना विचलित हुए पास की मिट्टी के टीले पर चढ़कर सबको चुप रहने का इशारा किया और खुद वहीं बैठ गए। उनकी शांति में एक अजीब शक्ति थी।
कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। तब उन्होंने कहा “मैं तुम्हारे दुख बढ़ाने नहीं, उन्हें सोखने आया हूँ। मुझ पर भरोसा रखो।” इतना सुनना था कि जो भीड़ अभी तक आग उगल रही थी, वही भीड़ आंसुओं में बहने लगी। गांधी ने थूक को भी “प्रसाद” कहकर स्वीकार कर लिया— “थूकने वाले ने अपने भीतर का ज़हर बाहर निकाल दिया। है।”
मीरा बेन लिखती हैं कि कुछ ही क्षणों में पूरी भीड़ जो अभी तक उनको गालियां दे रही थी, वो रोने लगती है। क्योंकि असहायता का, क्रोध का, उन्माद का जो अंतिम बिंदु है वह पश्चाताप है। वहां तक मनुष्य को ले जाना जिससे वह खुद को देखने ,खुद के अंदर झांकने की स्थिति में पहुंच जाए उसको महात्मा गांधी कहते हैं।
लोगों की पीड़ा को समझना, उस पीड़ा से जुड़ने की कोशिश करना ये गांधीजी की सबसे बड़ी देन है जो उन्हें हर दिन नया बना देती है और जो हर दिन उनको हमारे आज से जोड़ देती है।
यही गांधी की ताक़त थी—वे आक्रोश को करुणा में बदल देते थे, हिंसा को आत्मचिंतन में। वे हमें सिखाते थे कि सच्ची शक्ति तलवार से नहीं, सहनशीलता और आत्मबल से आती है।
आज जब समाज बार-बार अविश्वास और नफ़रत की आग में झुलसता है, तो गांधी का यह प्रसंग हमें याद दिलाता है—नेता वह नहीं जो भीड़ को और भड़का दे, नेता वह है जो भीड़ का गुस्सा अपने ऊपर लेकर उसे आंसुओं में बदल दे। नेतृत्व का अर्थ है घाव झेलकर भी मरहम बनना। नेता वही, जो घाव सहकर भी मरहम बने।
किसी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं –
“जब भीड़ पागलपन में खो जाए,
कोई तो हो जो ख़ुद पर चोट लेकर भी सबको संभाले।”
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.