
— देवेन्द्र मोहन —
मेरे पास वो तीन गोले नहीं हैं जो सआदत हसन अली मंटो की नजर के दायरे में थे- शायर ‘मीरा जी’ की शख्सियत की पड़ताल के सिलसिले में…
एक और उदाहरण है मेरे सामने- चार्ल्स डिकिंस के उपन्यास ‘पिकविक पेपर्स’ का। एक किरदार पढ़ता है- ‘चायनीज ऐंथ्रोपॉलोजी’ – दो शब्द। ये क्या बला है, वह सोचता है और फिर एक डिक्शनरी उठा लेता है। डिक्शनरी से पता चल जाएगा, उसे लगता है। उसे इन दो शब्दों का अर्थ ढूंढ़ निकालना है, पता करना है इनके मायने क्या हैं।
पहले तो वह ‘सी’ में जाकर ‘चायनीज’ शब्द का अर्थ समझ लेता है। उसे आधा ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब बारी आती है, ‘ऐंथ्रोपॉलोजी’ की। वह दोबारा ‘ए’ अक्षर की ओर दौड़ता है। ‘ऐंथ्रोपॉलोजी’ का अर्थ भी समझ लेता है। अच्छी तरह। अब उसका ज्ञान पूरा हो चुका है।
ऊपर बताया गया किस्सा डेढ़-एक सौ साल पुराना होगा। होता रहे। सवाल किस्से का नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने का है। मंटो के पास देखने के लिए तीन गोले थे, सामने मेज पर रखे हुए और वे स्वयं रू-ब-रू थे महान कवि मीराजी के सामने- एक ऐसे कवि के सामने जो एक नयी चेतना, नयी भाषा के साथ उर्दू काव्य में एक नयी सोच की सृष्टि कर रहे थे।
आज पचास या पता नहीं बावन-तिरपन साल के बाद कथाकार-रचनाकार प्रबोध कुमार का जिक्र उठा है, तो अक्सर भड़भड़ा कर लौट आनेवाली यादों की परेड में कई व्यवधान आ रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक है क्योंकि प्रबोध कुमार आम टी हाउस/क़ॉफी हाउस या वोल्गा के हस्ब-मामूल लेखकों की तरह नहीं थे। उनके दोस्त कई रहे होंगे, यार कम ही थे- घनिष्ठता तो और भी थोड़ों से रही होगी।
लेकिन चूँकि गया वक्त है कनॉट प्लेस के गलियारों में टहलती, फिरती अधिकतर शख्सियतें परछाइंया भी नहीं रहीं- कृष्णा सोबती, श्रीकांत वर्मा, कमलेश और अशोक सेकसरिया। दो नाम और हैं : प्रयाग शुक्ल और दक्षिण अफ्रीका में जा बसे रमेश गोस्वामी, जिनके हाफ़िज़े में प्रबोध कुमार की कई सारी यादें बदस्तूर कायम हैं।
अशोक सेकसरिया के हवाले से कितनी सारी चीजें स्मृति पटल पर छा जाती हैं। उन्होंने जाने कितने लोगों को ढूंढ़ निकाला, उनकी इधर-उधर डोलती धड़ों पर चेहरे बिठाये, उन्हें पहचान दी- और ये सब खुद को गुमनामी के अंधेरों में रखते हुए।
अशोक खूब पढ़ते थे- आदि शंकराचार्य की तर्ज़ पर ‘किंचित्धीता’ की तरह- कम लिखते थे या पता नहीं बहुत ही कम छपवाते थे – और सब तरह की चीजें पढ़ते थे। दुनिया का कोई भी विषय ले लो। फुटबॉल हो, एबी हो या दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर बेसिल द’ ऑलिवेरा हों – अशोक सेकसरिया को हर खेल, हर खिलाड़ी की गहन जानकारी थी। उन्होंने कई सालों तक खेल पत्रकारिता भी की थी। लगभग ऐसा ही कुछ था प्रबोध कुमार के साथ भी। अशोक ने एक अर्से तक गुणेंद्र सिंह कंपानी के नाम से कहानियाँ लिखी थीं, प्रबोध कुमार ने सारी रचनाएँ शायद अपने ही नाम से लिखी थीं और छपवायी भी थीं।
एक समय ऐसा आया जब अशोक सेकसरिया ने खुद तो कहानियाँ लिखनी बंद कर दीं (नहीं कीं तो उसकी जानकारी मुझे नहीं), लेकिन अक्सर नयी पौध को प्रोत्साहित करते नजर आते। कइयों को इस्लाह देते। भाषाओं, खासकर हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। उनकी लेखन शैली भी कमाल की थी।
प्रबोध कुमार में वे सब गुण मौजूद थे जो अशोक सेकसरिया में थे। दोनों में त्याग की गजब की भावना थी। खुद को छिपाकर रखो, पर औरों के हमेशा काम आओ। लेकिन अशोक सेकसरिया और प्रबोध कुमार में एक असमानता रही है, दिखने और न दिखने की।
अशोक जब-जब दिल्ली में होते थे, वे नियमित रूप से टी हाउस आते थे, देर शाम तक वहां बैठकर लोगों से मिलते थे; साहित्य, खेल, सिनेमा और राजनीति की चर्चाओं में शरीक होते थे, अपना मंतव्य देते थे।
प्रबोध कुमार का एक वक्फे के बाद दर्शन दुर्लभ हो गये थे। वो कब दिल्ली में हैं या ऑस्ट्रेलिया या पोलैंड या यूरोप के किसी अन्य देश में, इसका पता सिर्फ उन्हीं मित्रों के पास होता था जिनसे पत्रों के जरिये उनके संपर्क बने हुए थे।
एक और दिक्कत थी : उनके रचना कार्य की लगातार गिरती रफ्तार। कई बार पता ही नहीं चल पाता था कि वो हिंदुस्तान में हैं भी या नहीं। वैसे भी ज्यादातर लोग उनके बारे में, या यूं कहिए उनके अस्तित्व के बारे में भी पूरी तरह बेखबर थे। ऐसे में उनकी लेखनी के बारे में जाननेवाले ही कहां रहे होंगे?
उनकी लेखनी भी आठ या नौ साल ही रही होगी। कइयों का कहना होता था उन्होंने सन पैंसठ के बाद कुछ नहीं लिखा या नहीं छपवाया। कुछ (अब दिवंगत) मित्र कहते थे, लिखते हैं पर छपवाते नहीं। फिर लिखने, न लिखने और न छपने-छपाने का यह फासला बढ़ता ही गया। वे स्वयं भी अदृश्य-से होते जा रहे थे। बहुत थोड़ों को उनका पता था। बहुत थोड़ों को उनकी याद रही। वे संपादक-लेखक ‘मित्र’ भी जो उनकी रचनाओं के लिए उनका इसरार करते रहते थे उनकी संख्या भी कम होने लगी थी।
फिर ऐसा समय भी आया जब नयी पौध के ‘सलोने’ लेखकों को यह भी पता नहीं था कि प्रबोध कुमार नामक कोई कथाकार हुआ भी था। प्रेमचंद का नाती होने का गौरव उन्हें था, लेकिन जब नयी पौध वालों को- ‘प्रेमचंद? हां, कुछ सुना हुआ नाम सा लगता है’ – बहुत कुछ का नहीं पता तो ‘प्रबोध का बोध’ होना भी मजाक सा लगता है।
एक बार मनोहर श्याम जोशी जो स्वयं प्रबोध कुमार से बतौर लेखक बहुत प्रभावित थे, बता रहे थे कि एक दिन प्रबोध कुमार नाम का एक नया कहानीकार ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ के दफ्तर में उनसे मिलने आया और आते ही कहने लगा, “प्रबोध कुमार नाम का एक नया लेखक और भी आ गया है…नाम सुना है आपने?”
जोशी जी का जवाब था : “नाम भी सुना है, मिला भी हूँ कई बार। नये नहीं पुराने लेखक हैं, बड़े लेखक हैं। अब आप अपना नाम बदल लीजिए और प्रबोध के आगे जो भी शर्मा, वर्मा, सिन्हा, सक्सेना जो भी नाम हो लगा लीजिए। पर प्रबोध कुमार नाम से अपनी रचनाएँ मेरे पास मत लाइए मेरे सामने…।”
वही कहानियाँ दोबारा लौट आती हैं : मंटो के सामने वाले गोले और सामने बैठे ‘मीरा जी’; फिर डिकिंस वाली वही दास्तान जिसके जरिये ‘चाइनीज ऐंथ्रोपॉलोजी’ की तलाश।
कई बार सोचता हूँ जिस प्रबोध कुमार को मैंने देखा था, और बहुत ही थोड़ा जाना था- और वह भी ऐसे समय पर जब खुद मुझे मेरे वजूद की हल्की सी भी जानकारी नहीं थी। कुछ कहानियाँ पढ़ी थीं इधर-उधर पत्रिकाओं में और जब कुछ उनके बारे में जानना चाहा तो वही थोड़े से लोग थे – कृष्णा सोबती, अशोक सेकसरिया, प्रयाग शुक्ल, रमेश गोस्वामी, कवि कमलेश बस। दो-चार और रहे होंगे जिनसे मेरी या तो मुलाकात नहीं थी या बहुत थोड़ी रही होगी। अठारह-उन्नीस की उम्र में किसी व्यक्तित्व के बारे में कुछ ‘खोज’ निकालना बड़ी ही नहीं, ‘दुष्कर’ सी बात थी। आखिर, मैं कौन? खामख्वाह! एक अपरिपक्व नौजवान जिसका लेखकीय जोश पुरजोर तरीके से कागज पर ठाटें मार रहा था और अक्सर किसिम-किसिम के पर्चों में शाया होकर खुद से गलबहियां की मुद्रा में मुब्तिला टी हाउस में नुमाया होता था।
सोलह एक साल की उम्र में मेरी कुछ कविताएँ हिंदी की पत्रिकाओं में छप गयीं। अंग्रेजी कविताएं भी लिखता था। सत्रह साल होते-होते तक अंग्रेजी में भी कई कविताएं लिख मारी थीं और इन ‘लिख मारने’ वाली चीजों को अंग्रेजी पत्रिका ‘थॉट’ में जगह मिली बराय मेहरबानी केशव मलिक के, जो एक नामचीन कला समीक्षक के अलावा अंग्रेजी के कवि भी थे और जिनसे अनंतर प्रगाढ़ सी मित्रता भी हो गयी थी।
उस समय मैं क्या हिंदी क्या अंग्रेजी, हर तरह के प्रकाशन में छपने लगा था- मैं कुछ भी लिख सकता था और ई.डी. गलगोतिया की दुकान से एक किताब खरीदकर पढ़ने के बाद खुद को Arthur Rimbaud समझने लगा था क्योंकि उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं सत्रह की उम्र में ही लिख ली थीं।
मंटो और मोहन राकेश की कहानियों से प्रेरणा लेकर कहानियाँ भी लिखनी शुरू कर दीं। शुरुआत में देवेन्द्र सत्यार्थी और ब्रजेश्वर मदान की कृपा से कुछ ‘अविस्मरणीय’ (अब अविस्मृत) कहानियाँ पत्रिकाओं में छपीं- कुछ अपने और कुछ गैर-नामों से छपवायीं और किसी-किसी पत्रिका में तो तीन-तीन कहानियाँ, कविताएं भी छपीं। आलम ये हो गया कि धर्मवीर भारती, कमलेश्वर और ज्ञानरंजन के इसरार भरे खत आने लगे- “कृपया अपनी रचना भेजकर अनुगृहीत करें।”
उसी जमाने में टी हाउस के एक अनन्य मित्र हरवंश कश्यप जो ‘सारिका’ तथा ‘कहानी’ आदि पत्रिकाओं के कथाकार के रूप में जाने जाते थे, कहने लगे : “पत्रिकाओं में तलाश करो…प्रबोध कुमार की कहानियाँ पढ़ने को मिल जाएं तो मजा आ जाएगा। और कुछ नहीं तो कमलेश या रमेश गोस्वामी से पूछ लो। कृष्णा सोबती जी से भी पूछ सकते हो उनकी कहानियों के बारे में। उन्होंने प्रबोध कुमार की छपी चीजों को सहेज कर रखा होगा…।”
कमलेश ने उसी समय टी हाउस में प्रवेश किया था और सोफे में विराजमान हुए ही थे कि मैंने उन्हें घेर लिया। कमलेश और प्रबोध कुमार की अच्छी छनती थी।
कमलेश का जवाब था : “प्रबोध कुमार की कहानियाँ तो क्या, खुद हमें प्रबोध कुमार की तलाश रहती है…।” पता चला कि प्रबोध कुमार तो शायद अब लिखते ही नहीं हैं। छपना-छपाना तो दूर की बात रही। “अकैडमिक्स की ओर ज्यादा ध्यान रहता है उनका…He has become a rare quantity now…”
एक तवील जमाना गुजर जाने के बाद बात समझ में आयी। दुनिया अजीबो-गरीब है यह तो सबको पता है, लेकिन कितनी यह किसी को नहीं मालूम!
कोई कह रहा है कुछ…अजीबो-गरीब ही अंदाज में : “Professor Prabodh Kumar has professed to remain a professor all his life, and nothing else!”
मतलब?
कहानीकार कहां गया?
कहां गयीं कहानियाँ?
खुद को गुमनाम रखने की क्या तरकीब है यह, और क्यों? जो किसी जमाने में किसी और का नहीं तो निर्मल वर्मा के समकक्ष था, अब कहानियाँ लिखना तो दूर कहानी पर बात करने को भी तैयार नहीं…।
कई फोन किये, एक ही जवाब था : “ अजी, छोड़ो भइया, कहानी-वहानी की ये सब बातें…क्या होता है कहानी लिख कर? हम कहां के दाना थे? पहले भी क्या हासिल कर लिया भैया हमने…?”
इस आंत भर, दांत भर की गयी बातों को बड़े साल हो गये। बहुत पुरानी बात है। Once upon a time… जैसी!
बाद के सालों तक प्रबोध कुमार की कोई किताब, कोई संग्रह नहीं। छपने-छपाने की इच्छा भी जाहिर नहीं। उनका पता ठिकाना भी नहीं। कमलेश के पास कुछ पत्र-पत्रिकाएं रही हों तो रही हों। लेकिन अब तो कमलेश को गए हुए भी कई साल हो चुके हैं…किसी दूसरे दोस्त के पास भी कुछ नहीं है…तो फिर प्रबोध कुमार की तलाश कैसे की जाए?
आठ-दस साल पहले, या कुछ और पहले, सुनने में आया था कि प्रबोध कुमार हर चीज से निवृत्त होकर गुड़गांव में आ बसे हैं और शायद कुछ लिखने की दिशा की ओर भी प्रवृत्त हो रहे हैं…
मतलब यह कि अब शायद कंठ से निकलने वाली आवाज को दोबारा वो चेहरा वापस मिल जाएगा। कागज पर कलम फिसलती या तेज रफ्तार से चलती नजर आएगी…लेकिन, कब?
ठीक से याद नहीं कब, शायद पंद्रह-बीस साल पहले दिल्ली में बसे हुए दोस्तों से फोन पर बात हो रही थी। एक चौंकानेवाली सी मगर अच्छी खबर मिली : प्रबोध कुमार के जेहन में कई किरदार उछल रहे हैं। यें किरदार शायद कुछ अफसानों की शक्ल भी ले लें।
बहुत अच्छा लगा जानकर, लेकिन कब? हम जैसे कई हैं जो प्रबोध कुमार को पढ़ने के लिए किसी हद तक उतावले भी रहे हैं मगर उनकी लेखकी से महरूम रहे शायद उनकी वाबस्तगी के लिए उनकी तरफ रुख कर पाएंगे?
जेहन में कई खयालात हैं उनके – पंचतंत्रनुमा चरित्र और चंद एक कहानियों के खाके जिनमें वयस्क पात्र कम होंगे, बच्चे ज्यादा। अलअमां!
लेकिन फिर एक अजीब सी घटना हो जाती है।
प्रबोध कुमार एक और रूप में नुमाया होते हैं- एक उद्धारक के रूप में। उनकी शिनाख्त का जरिया भी एक हैरतअंगेज शक्ल में नुमाया होता है : वे अपने घर में काम करनेवाली तीन बच्चों की माँ को अक्सर किताबों को उलटते पलटते देखते हैं।
पता करते हैं औरत की दिलचस्पी का सबब। पता चलता है वह थोड़ा बहुत लिख भी लेती है और अपनी जिंदगी की दास्तान बयां करना चाहती है।
“लिखो”, वे कहते हैं, “अपनी दास्तान लिखो।”
वह औरत लिखना शुरू करती है। उसकी दास्तान में ‘दम’ है। फिर लिखने में उसकी सहायता, सहायता और जरूरी ‘इनपुट्स’ का इसरार। पांडुलिपि मित्रों को दिखाते हैं। बातों-बातों में प्रकाशकों को एक नयी ‘प्रतिभा’ के बारे में जानकारी मिलती है। प्रकाशन होता है। लेखिका बेबी हालदार का नाम सबकी जुबान पर आ चढ़ता है।
वह छपती है, कई जबानों में, ख्याति अर्जित करती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम छपने लगता है। प्रबोध कुमार खुश हैं।
उनकी ‘खोज’ की काया पलट हो गयी है। अब वह एक ‘नाम’ बन चुकी है। हवाले के तौर पर प्रबोध कुमार, संजय भारती और रमेश गोस्वामी का जिक्र होने लगता है।
लेकिन वही दिक्कत है- प्रबोध कुमार की शिनाख्त का जरिया उनकी अपनी लिखी चीजें नहीं हैं, बल्कि बेबी हालदार है।
प्रबोध कुमार को इससे कतई परेशानी नहीं। वे अब दानवीर दधीचि की तरह नजर आने लगे हैं।
बेबी हालदार प्रकरण के बाद उन्होंने दोबारा कलम उठा ली है- पैतालीस-पचास साल बाद। लेकिन वे अब भी अपनी लेखनी, रचनात्मकता के बारे में बात नहीं करते, नहीं करना चाहते…। प्रबोध कुमार : तलाश में हम सभी…।
तो फिर, कैसे करे कोई तलाश उनकी? इस सवाल का जवाब नहीं मिलनेवाला। अब तो वे जा चुके हैं बहुत दूर। हम सबसे परे।
“हम रूह-ए सफर हैं
हम नामों से न पहचान”
मंटो के वो तीनों गोले अब हमारे सामने हैं। मीराजी भी हमारे सामने नहीं।
कोई दोबारा ‘पिकविक पेपर्स’ हाथ में थामे कुछ तलाश कर रहा है। उसे अब भी ‘चायनीज’ और ‘ऐंथ्रोपॉलोजी’ का अर्थ जानने की दरकार है।
जवाब मिल पाएगा भी, पता नहीं…
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

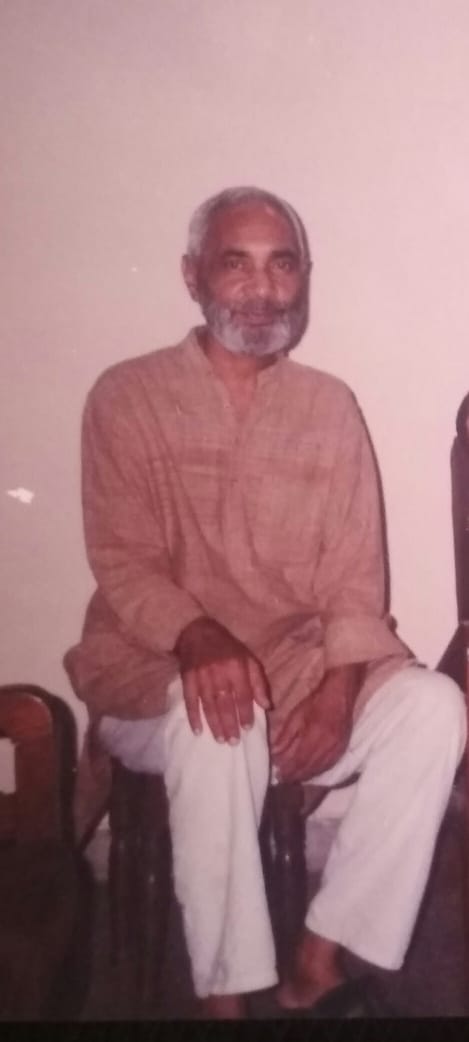
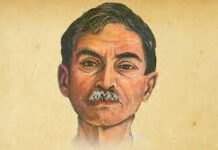















स्मृति लेखा और स्मृति खेला! दोनों की छटा और व्यथा है देवेन्द्र मोहन के यहां। ‘अपने को अप्रकाशित करते हुए’ मलयज की ही तरह अशोक सेकसरिया और प्रबोध। संजय भारती ने कांचरापाडा से अपने रोशनाई प्रकाशन से बेबी हालदार की आत्म कथा छापी तो प्रबोध कुमार ने उसे जगत भर में रौशन करा दिया। पर बड़ी मुश्किल से खुद अपना कहानी संग्रह ‘ सी सा’ और फिर नये पंचतंत्र जैस उपन्यास ‘ निरीहों की दुनिया’ छापने छपाने को राजी हुए! ऐसे लोग हमारे आपके बीच रहे हैं, सचमुच निरीह — इस शब्द के मूल अर्थ में– ईहा यानी आकांक्षा से रहित! रूहे सफर, अनाम!