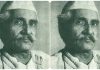– प्रणय कृष्ण –
(यह लेख वर्ष 2015 में प्रो लालबहादुर वर्मा को शारदा देवी शिक्षक सम्मान प्रदान करने के अवसर पर ‘मानपत्र’ के रूप में निर्णायक मंडल की ओर से प्रो प्रणय कृष्ण द्वारा लिखा और पढ़ा गया था। )
प्रो.लालबहादुर वर्मा को प्रथम ‘ शारदा देवी स्मृति सम्मान’ प्रदान करते हुए हम सब गर्व का अनुभव करते हैं। हिन्दी-उर्दू समाज के अप्रतिम आवयविक बुद्धिजीवी के रूप में प्रो. लालबहादुर वर्मा का हमारे बीच होना एक प्रकाश-स्तम्भ का होना है। आज के भारत में हमारे बीच शायद ही कोई ऐसा बुद्धिजीवी हो जिसने प्रो। वर्मा की तरह इतिहासकार, विचारक, आन्दोलनकारी, संगठनकर्ता, सांस्कृतिक प्रबोधनकार, अध्यापक, सम्पादक, उपन्यासकार, अनुवादक, नाटककार और सबसे बढ़कर एक नायाब इंसान और बेहतरीन दोस्त की इतनी सारी भूमिकाएं एक साथ अदा की हों। कहना न होगा कि इन सब भूमिकाओं के दक्ष निर्वाह के पीछे एक और शख्सियत की भूमिका भी है जिसे अलक्षित नहीं रखा जा सकता और वह शख्सियत हैं प्रो. वर्मा की शरीक-ए-हयात डा. रजनीगन्धा वर्मा।
प्रो. वर्मा को दुनिया पेशे से एक इतिहासकार के रूप में जानती है, लेकिन वे एक ऐसे विलक्षण इतिहासकार हैं जिन्होंने पीढ़ियों को यह सिखाने का दायित्व भी वहन किया कि इतिहास जिया कैसे जाता है, कि इतिहास का निर्माण जनता ही करती है और जनता के जीवन में हिस्सा लेना इतिहास-निर्माण में भागीदारी का ही दूसरा नाम है। इसीलिए प्रो. वर्मा ने ‘भारत का जन-इतिहास’ तैयार किया और क्रिस हर्मन की पुस्तक ‘विश्व का जन इतिहास’ का तर्जुमा करके हिन्दीभाषियों को उपलब्ध कराया।
आज जिस वक्त हमारे देश में इतिहास के नाम पर देवताओं का ऐतिहासीकरण और इतिहास-पुरुषों का दैवीकरण हो रहा है, ऐसे समय साधारण जनता को इतिहास की ताकत माननेवाले इतिहासकार लालबहादुर वर्मा का हमारे बीच होना हम सब की खुशनसीबी है। प्रो. वर्मा के विपुल इतिहास-लेखन में बारम्बार यह अमिट प्रतिज्ञा उभरती है कि इतिहास मनुष्यों का ही हुआ करता है, अतः इतिहास के बगैर न तो मनुष्यता की बात हो सकती है और न ही मनुष्यता के बगैर इतिहास की कोई बात हो सकती है। प्रो. वर्मा की लिखी ‘इतिहास के बारे में’ और ‘Understanding History’ जैसी पुस्तकों से कोई भी आम पाठक महज यही नहीं जानता कि इतिहास क्या है, उसकी पद्धतियाँ और प्रणालियाँ क्या हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा वह यह जान सकता है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए उसका मूल्य क्या है।
प्रो. वर्मा एक अग्रणी लोक-शिक्षक हैं और इतिहास की विधा को उन्होंने कभी सिर्फ अकादमिक काम नहीं माना, उसे लोक-शिक्षण और जन-चेतना की उन्नति के माध्यम की तरह बरता। ‘मानव-मुक्ति कथा’, दो खण्डों में योरप का इतिहास, दो खण्डों में विश्व का इतिहास, ‘कांग्रेस के सौ साल’, ‘अधूरी क्रांतियों का इतिहासबोध ‘ आदि मौलिक कृतियों के साथ साथ रोज़े बूर्दरो की मूल फ्रेंच पुस्तक का हिन्दी अनुवाद ‘ फासीवाद: सिद्धांत और व्यवहार ‘, आर्थर मारविक की मूल अंग्रेज़ी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद ‘ इतिहास का स्वरूप ‘ तथा एरिक होब्सबोम की कालजयी इतिहास-पुस्तक शृंखला की एक कड़ी का हिन्दी अनुवाद ‘क्रांतियों का युग’ शीर्षक से प्रकाशित करा के उन्होंने व्यापक फलक पर इतिहास के लोक शिक्षण के काम को अंजाम दिया।
वर्मा जी ने न केवल १९८५ से लेकर १९८८ तक ‘इतिहास’ पत्रिका का संपादन किया, बल्कि १९८९ से अबतक लगातार जिस राजनैतिक-सांस्कृतिक पत्रिका का वे प्रकाशन करते आ रहे हैं उसका नाम भी उन्होंने ‘ इतिहासबोध ‘ ही रखा। अकादमिक हलके में बतौर इतिहासकार उनकी कद्दावर शख्सियत का निर्माण तब शुरू हुआ जब उन्होंने १९६५ से १९६७ के बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्रो. हरिशंकर श्रीवास्तव के निर्देशन में पी. एच. डी. उपाधि के लिए ‘ भारत का सबसे छोटा अल्पमत : एंग्लो इंडियन ‘ विषय पर शोध-कार्य संपन्न किया। उसके बाद आपने पेरिस के सोरबोन्न विश्विद्यालय में विश्वविख्यात समाजशास्त्री रेमों आरों के निर्देशन में शोध-कार्य आरंभ किया। १९६७ से लेकर १९७१ तक चला यह महत्वपूर्ण शोध कार्य एक ऐसे विषय पर है जिसकी प्रासंगिकता आज सबसे ज़्यादा है। यह विषय था, ” इतिहास में पूर्वाग्रह की समस्या ‘। प्रो. वर्मा ने इतिहास की विभिन्न शोध-पत्रिकाओं मंं २० से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कराए और उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस, उत्तराखंड इतिहास कांग्रेस, अखिल भारतीय इतिहास कांग्रेस के भारतेतर इतिहास विभाग तथा अकादमी ऑफ़ सोशल साइंस के इतिहास विभाग की अध्यक्षता की।
प्रो. लालबहादुर वर्मा का जन्म १० जनवरी, १९३८ को बिहार के छपरा जिले में हुआ। आपने प्राम्भिक शिक्षा आनंदनगर, गोरखपुर से ग्रहण करने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक, लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और फिर गोरखपुर तथा सोरबोन्न विश्वविद्यालयों से पी।एच।डी। उपाधियों के लिए अध्ययन किया। १९५९ से आपने सतीशचन्द्र महाविद्यालय , बलिया से अपने अध्यापकीय सफ़र की शुरुआत की। १९६४ में आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में अध्यापन करने आ गए। यहाँ लगभग बीस साल के अध्यापन के दौर में आपने कई पीढ़ियों को प्रगतिशील जीवन-मूल्यों और मार्क्सवादी जीवन-दृष्टि में शिक्षित-प्रशिक्षित किया। यहाँ रहते हुए आपने १९७२ से लेकर १९८४ के बीच साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिका ‘भंगिमा’ का संपादन किया जो अपने समय में प्रगतिशील सांस्कृतिक मूल्यों की अनिवार्य राष्ट्रीय पत्रिका बन कर उभरी।
संस्कृति और विचार की दुनिया में पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह उर्वर दौर था जिसके केंद्र में थे युवा अध्यापक लालबहादुर वर्मा। स्टडी-सर्किल, नाटक, कार्यशालाएं, रचना-गोष्ठियों में वर्मा जी के इर्द-गिर्द युवाओं की अच्छी-खासी टोली हुआ करती जिनमें से अनेक आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मूल वृक्ष की शाखाओं की तरह फ़ैल गए हैं। प्रो. लालबहादुर वर्मा के विद्यार्थी, चाहे उनकी उम्र जो हो, उनका पेशा जो हो, आज भी अपने इस अद्भुत अध्यापक से जितना प्यार करते हैं, वह अभूतपूर्व है। एक अच्छा अध्यापक जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है, इसके सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक हैं प्रो. वर्मा। १९८५ से १९९१ के बीच आपने मणिपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। यहाँ रहते हुए आपने भारत के उत्तर-पूर्व को जिस अभिनव दृष्टि से देखा, जो अनुभव सहेजे, वे काफी समय बाद एक महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृति का आधार बने।
१९९१ से आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाने आए और यहीं से आपने १९९८ में अध्यापन से अवकाश ग्रहण किया। सतत यात्री ने आखिरकार अपना डेरा एक जगह स्थापित कर लिया – उसी इलाहाबाद में जिसे निराला, पन्त, महादेवी, फिराक ने मुख्तलिफ जगहों से आकर अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। वर्मा जी के यहाँ बस जाने से इस कतार में एक और कड़ी जुड़ी, हमारा शहर कुछ और रौशन हुआ।
प्रो. वर्मा की कार्रवाइयों का शायद सबसे बड़ा इलाका संस्कृति का इलाका है। पिछली आधी सदी से भी ज़्यादा समय से उन्होंने प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और जनवादी संस्कृति-कर्म में लगे हुए तमाम लोगों को एकताबद्ध करने की मुहिम छेड़ी हुई है। संस्कृति-कर्मियों की अनेक पीढ़ियों को उनके मार्गनिर्देशन का लाभ मिला है, उनसे प्रेरणा मिली है। १९८२ में राष्ट्रीय जनवादी सांस्कृतिक मोर्चे की स्थापना, १९९९ में साझा सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत, २००३ में ‘ मुहिम ‘ के नाम से सांस्कृतिक पहल की शुरुआत और २०१२ से अब तक लगातार सांस्कृतिक मुहिम के तहत सांस्कृतिक कार्यशालाओं, अध्ययन-चक्रों की शृंखला, आसान भाषा में समाज, संस्कृति और राजनीति के जीवंत विषयों पर पुस्तिकाओं का प्रकाशन तथा भगत सिंह और डी. डी. कोसंबी व्याख्यानमालाओं के ज़रिए उन्होंने जो अथक और अपराजेय सांस्कृतिक अभियान संचालित किया है, वह बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए भी ईर्ष्या का विषय हो सकता है।
वे खुद में एक चलती फिरती मुहिम हैं जिसके चुम्बकीय आकर्षण से हर कहीं जवां उमंगों से भरे तमाम लोग खिंचे चले आते हैं, जगह चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हो या भारत का सुदूर उत्तर-पूर्व। इस पूरे जीवन-समर के पीछे कितना संघर्ष, कितनी साधना, व्यक्तिगत और पारिवारिक ज़िंदगी की कितनी कुबानियाँ हैं, यह मानों लोगों की निगाह में ही नहीं है। प्रो. वर्मा की आत्मकथा का पहला हिस्सा ‘जीवन प्रवाह में बहते हुए’ शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है और दूसरा हिस्सा जल्दी ही प्रकाशित होगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस अत्यंत कर्मठ और कीमती जीवन की अलक्षित अंतर्धाराएं भी हम सब को दृश्यमान हो सकेंगीं. पिछले साल आपको दिल का दौरा पडा, बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन बीमारी को ठेंगा दिखाते हुए आपने इसी साल २०१५ में विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रबोधन- शृंखला शुरू कर दी। नागरिक समाज के हर आन्दोलन में उसी तरह आपकी शिरकत है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो, मानों दिल का ऑपरेशन किसी और का हुआ हो।
वर्मा जी के सांस्कृतिक अभियान का एक अहम पहलू साहित्य-सृजन भी रहा। एक संवेदनशील रचनाकार की हैसियत से उन्होंने अनेक कहानियां ही नहीं लिखीं, बल्कि दो महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। ‘उत्तर-पूर्व’ शीर्षक उपन्यास उत्तर-भारतीय, पितृसत्तात्मक, सवर्ण-बोध वाली राष्ट्रीय-चेतना से बेदखल अपनी अस्मिता के लिए जूझते उत्तर-पूर्व की महागाथा है। मणिपुर का इतिहास, संस्कृति, सामाजिक जीवन और उसके संघर्ष यहाँ मार्मिक अभिव्यक्ति पाते हैं। अकारण नहीं कि ‘थांगजम मनोरमा’ को समर्पित एक कविता से इस उपन्यास का आरम्भ होता है। आपका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है ‘मई अड़सठ’ जो फ्रांस के अभूतपूर्व छात्र आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। प्रो. वर्मा बतौर शोधकर्ता इस आन्दोलन के प्रत्यक्षदर्शी थे। जिस सोरबोन्न विश्विद्यालय में १९६७ से १९७१ के बीच आप शोधरत थे, वह आन्दोलन का प्रमुख केंद्र था। वर्मा जी के दोनों उपन्यासों में विश्वविद्यालय का जीवन वह कथा-सूत्र है जो व्यापक फलक पर घट रही घटनाओं को बांधता है। भोपाल गैस त्रासदी पर लिखा आपका नाटक ‘ज़िंदगी ने एक दिन कहा’ बहुचर्चित रहा और खेला भी खूब गया।
आपने दुनिया की कुछ युगांतरकारी साहित्यिक पुस्तकों का अनुवाद कर हिन्दी पाठक की चेतना को समृद्ध किया है. हारवर्ड फॉस्ट के चार उपन्यासों , अमेरिकी लेखक जैक लंडन के उपन्यास ‘आयरनव्हील’, अलेक्जान्द्रा कोलेंताई की आत्मकथा, गैलीलियो के जीवन पर आधारित ब्रेष्ट के कालजयी नाटक के साथ साथ विख्यात मार्क्सवादी चिन्तक जॉन होलोवे की पुस्तक ‘चेंज दि वर्ल्ड विदाउट टेकिंग पॉवर’ का ‘चीख’ शीर्षक से अनुवाद करके आपने हक़, इन्साफ, ईमान और इंसानियत के हिमायती अंतर्राष्ट्रीय साहित्य की अनेक कृतियों को हिन्दी में जज़्ब कर लिया। प्रो. वर्मा के सांस्कृतिक अभियानों, उनके भाषणों, लेखों, उनके सम्पादन में निकली पत्रिकाओं में छेडी गयी तेजस्वी बहसों और विमर्शों ने साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर जो प्रभाव छोड़े, उनके संपादन और व्यक्तिगत सान्निध्य में नए लेखक-लेखिकाओं, राजनीतिक- सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का जो प्रशिक्षण हुआ, उनके व्यक्तित्व जैसे निखरे, इन बातों का अहसास हज़ारहाँ रूपों में बिखरे हैं. आज उन्हें चुनने सहेजने का अवसर है।
इलाहाबाद की धरती पर आज प्रो. लालबहादुर वर्मा का सम्मान इंसानी दोस्ती, मुल्क की बहुरंगी संस्कृति, इन्साफ के तसव्वुर, लोकतांत्रिक और प्रगातिशील मूल्यों और मनुष्य की अदम्य जिजीविषा का सम्मान है।

शिक्षक भी, मित्र भी
– धर्मेन्द्र सुशांत –
करीब 20–21 साल पहले पटना में उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी गोकि जान उन्हें पहले चुका था। यह परोक्ष परिचय पढ़ाई के दौरान उनकी यूरोप का इतिहास और इतिहास के बारे में जैसी किताबों को पढ़ने से हुआ था, जो इतिहास का छात्र होने के कारण मेरे और मुझ जैसे हिन्दी में पढ़ने लिखने वाले न जाने कितने छात्रों का सहारा थीं।
साल अभी याद नहीं, पर 1998 – 2000 के बीच का ही कोई समय था जब पता चला कि वे पटना आने वाले हैं तो हमने ‘समन्वय’ की तरफ से उनका एक व्याख्यान आयोजित करने के लिए उनसे अनुरोध किया। समन्वय हमारी एक अनौपचारिक संस्था थी, जिसमें साहित्य, कला, सियासत, समाज आदि में दिलचस्पी रखने वाले अनेक युवा शामिल थे। जिज्ञासा और जोश तब ऐसा था कि किसी कवि, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक, कलाकार के पटना आने की भनक हमें लगती तो उनसे कुछ सुनने, जानने और बतियाने का प्रयास जरूर करते। समन्वय का अनुरोध मानकर उन्होंने भूमंडलीकरण और इसके प्रभावों पर व्याख्यान दिया और इस सिलसिले में ही उनसे हमारा प्रत्यक्ष परिचय हुआ।
अभी तक पटना में हम सैयद हसन अस्करी, रामशरण शर्मा, सिन्हा जी, आर एन नंदी और पपिया घोष जैसे इतिहासकारों को जानते थे। उनकी ख्याति से वाक़िफ़ थे और अपने शहर का होने को लेकर गौरव भी महसूस करते थे। समन्वय के युवाओं को रामशरण बाबू का स्नेह विशेष रूप से प्राप्त था। ये लोग हमारे आदरणीय थे। लेकिन वर्माजी बिल्कुल अलग किस्म के मालूम पड़े। आदरणीय तो ये भी थे लेकिन इन्होंने हमसे बराबरी का, साथी का व्यवहार रखा।
पुनाईचक के हमारे डेरे पर वर्मा जी ने पेरिस के अपने संस्मरण सुनाए। फ्रांस के ऐतिहासिक छात्र आंदोलन का, सार्त्र का जिक्र किया। उनकी बातों का मतलब यह था कि हमें अपने लिए ऐसा उद्देश्य तय करना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए जिसमें समाज के प्रति सकारात्मक उत्तरदायित्व हो। यह उपदेश नहीं था, सुचिंतित सलाह या कहें अपेक्षा थी, जिसको सबसे पहले वे खुद अपने जीवन पर लागू कर चुके थे। उनकी इस बात ने हम सभी को काफी प्रभावित किया। हम सब उनके मुरीद बन गए. तब से उनसे हमारा आत्मीय संपर्क बना रहा। दिल्ली के पुस्तक मेले में उनसे जरूर मुलाकात होती थी। एक बार मुंबई में भी हुई थी।
समन्वय के बाद हम कई साथी वामपंथी छात्र संगठन आइसा से जुड़े और उसके भी बाद राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय हुए, तब भी वर्मा जी से हमारा संपर्क बना रहा। वास्तव में उनकी जो विशेषता हमें हमेशा आकर्षित करती रही वह यह थी कि वे एक साथ अध्यापक और दोस्त दोनों थे। उनसे संवाद में उनकी विद्वत्ता कभी आड़े नहीं आती थी। वे दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे।
वह विद्वान, वामपंथी और नास्तिक थे। वैचारिक तौर पर स्पष्ट और दृढ़। साफगोई उनके स्वभाव में थी। इन गुणों वाले बहुतेरे लोग किंचित कठोर और गुरु-भाव से ग्रस्त भी हो जाते हैं, पर वे अत्यंत सहज थे, विशाल हृदय वाले थे।
हिन्दी क्षेत्र में जन बुद्धिजीवी के अभाव की चर्चा अकसर होती है। बांग्ला की महाश्वेता देवी और अंग्रेजी की अरुंधति राय का उदाहरण देते हुए बार बार यह पूछा गया है कि हिन्दी में ऐसा कोई जन बुद्धिजीवी क्यों नहीं है. यह सवाल उठाने वालों को वर्मा जी पर नजर डालनी चाहिए।
आज उनके नहीं रहने पर जितनी तादाद में और जिस तरह लोग, खास कर युवा उन्हें याद कर रहे हैं वह साबित करने के लिए काफी है कि उनसे कितनों ने प्रेरणा और प्रोत्साहन पाया है।
बेशक वे हिन्दी क्षेत्र के अनन्य जन बुद्धिजीवी और शिक्षक थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा और श्रम का उपयोग खुद को प्रतिष्ठित करने के नहीं, बल्कि जन सामान्य को विवेकवान बनाने के लिए किया। इसी कारण अध्यापक ,इतिहासकार, साहित्यकार, अनुवादक, पत्रिका संपादक, संगठक… अपनी तमाम भूमिकाओं में वे बिल्कुल अलहदा नजर आते हैं। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी।
( समकालीन जनमत से साभार )
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.