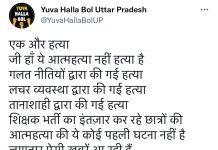(कल प्रकाशित लेख का बाकी हिस्सा )
वस्तुत: यह चौतरफा अव्यवस्था और मोहभंग का समय था। 1971 के आम चुनाव और 1972 के विधानसभा चुनाव हुए और दोनों में ही इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नवोदित कांग्रेस (इंदिरा) को प्रबल बहुमत मिला। ‘गरीबी हटाओ’ के नारे के सामने सभी विपक्षी दल धराशायी हो गए। लोकसभा की 518 सीटों में से 352 सीटें इंदिरा गांधी के उम्मीदवारों को मिली थीं। इस बीच बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के कारण हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में न सिर्फ पाकिस्तान से टूटकर बांगलादेश का उदय हुआ बल्कि भारत ने पाकिस्तान के 1 लाख सैनिक युद्धबंदी बना लिये थे। 1969 में कांग्रेस की टूट के कारण अपनी सरकार बचाने के लिए कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सांसदों का समर्थन लेने के लिए मजबूर हुईं प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी 1972 तक अपने प्रभुत्व के शिखर पर पहुँच चुकी थीं।
लेकिन यह स्थिति शीघ्र ही बदलने लगी। 1973 में ही गरीबी हटाने की बहु-प्रचारित योजनाएं कागजी साबित हो रही थीं। राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आमदनी में गिरावट सामने आई। खाद्यान्न की कमी पैदा हो रही थी। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अक्टूबर 1973 तक तेल के दामों में चार गुना बढ़ोतरी हो गयी जिससे रासायनिक खाद और डीजल के भाव आसमान छूने लगे। दैनिक जरूरत की वस्तुओं के दामों में तीस प्रतिशत तक मंहगाई हो गयी। मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए खर्च में कटौती की तो रोज़गार के अवसर घटने लगे।
आर्थिक मंदी, जरूरी वस्तुओं के अभाव (कालाबाजारी), बेरोजगारी और महंगाई के संयोग ने व्यापक असंतोष पैदा किया। भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई में अक्टूबर ’73 और जून ’74 के बीच 13,000 हडतालें हुईं। सिर्फ 1974 में उद्योग-धंधों में 3 करोड़ से अधिक श्रम-दिवस का नुकसान हुआ। मई 1974 में भारत के इतिहास की पहली अखिल भारतीय रेल हड़ताल हुई। सरकार ने इसे विफल करने के लिए ‘भारत रक्षा अधिनियम’ का इस्तेमाल किया। श्रमजीवियों और सरकारी कर्मचारियों की तनखाहों में होनेवाली नियमित सालाना वृद्धि रोक कर अनिवार्य बचत योजनाएं लागू कराई गयीं। महंगाई नियंत्रित करने के लिए किसानों से अनिवार्य अन्न वसूली का प्रयास भी बेहद अलोकप्रिय साबित हुआ। मध्यम वर्ग, किसानों, शहरी श्रमिकों और विद्यार्थियों में असंतोष गहराने लगा। सत्ता प्रतिष्ठान में इस मोहभंग की लहर को ‘उम्मीदों में क्रांति’ का विशेषण देकर अनदेखा किया गया।
राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस की टूट के बाद प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी को चुनाव में प्रबल विजय के बावजूद इंदिरा कांग्रेस के पास संगठन शक्ति का अभाव बना रहा। इसने सत्ता और जनता में असंतोषजनक फासला पैदा किया। विपक्ष की दयनीय दशा के कारण सत्ताधारी दल में निरंकुशता, गुटबंदी और स्वेच्छाचार की बढ़ोतरी होने लगी। स्वयं प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी पर अपने छोटे बेटे संजय गांधी को मारुति कार का कारखाने बनाने देने में पक्षपात का आरोप लगने लगा।
इसी बीच गुजरात में दिसम्बर ’73 और जनवरी ’74 के दौरान महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध विद्यार्थी असंतोष का विस्फोट हो गया। 168 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को 140 सदस्यों का समर्थन जरूर था लेकिन विद्यार्थियों द्वारा स्वत:स्फूर्त तरीके से गठित नवनिर्माण समिति के आन्दोलन ने इस प्रचंड बहुमत को निरर्थक बना दिया। इसमें पुलिस फायरिंग से 85 लोगों की मृत्यु हुई। तीन हजार लोग घायल हुए। आठ हजार से अधिक गिरफ्तार किये गए। सभी विरोधी दलों समेत समाज के मुखर अंशों ने आन्दोलन का समर्थन किया। जयप्रकाश नारायण ने भी नवनिर्माण समिति को अपना नैतिक समर्थन दिया। उन्हें इस आन्दोलन में ‘आशा की किरण’ दिखाई दी। क्योंकि वह दिसम्बर’73 में देश के युवजनों के नाम अपील जारी करके लोकतंत्र की बिगड़ती दशा के प्रति सरोकारी बनने का आह्वान कर चुके थे। मोरारजी देसाई तो 11 मार्च को विधानसभा भंग कराने और नए चुनावों के लिए आमरण अनशन पर ही बैठ गए। फलत: 15 मार्च को हाल में ही चुनी गयी सरकार और विधानसभा दोनों का असमय समापन हो गया!
इधर बिहार में फैल रहे जन-असंतोष के बीच दिसम्बर ’73 से विद्यार्थी आन्दोलन शुरू हो चुका था। 21 जनवरी को गैर-कांग्रेसी दलों ने महंगाई के खिलाफ बिहार बंद का आयोजन किया। पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के आह्वान पर पूरे बिहार के छात्रनेताओं का एक सम्मेलन भी हुआ जिसने 18 फरवरी को छात्र संघर्ष समिति का निर्माण किया। इसमें सभी गैर-कम्युनिस्ट संगठन शामिल थे। कम्युनिस्ट समर्थक विद्यार्थियों ने अलग से बिहार छात्र-नौजवान संघर्ष मोर्चा बनाया। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा के सवालों पर छात्रों की समिति द्वारा 18 मार्च को बिहार विधानसभा के घेराव का आयोजन किया गया। पुलिस फायरिंग से पांच प्रदर्शनकारी मारे गए और पूरे पटना में व्यापक तोड़फोड़ और हिंसा हुई।
छात्र-पुलिस टकराहटों से अन्य शहर भी प्रभावित हुए। दो दर्जन जानें गयीं। फलस्वरूप 20 मार्च तक बिहार के 11 महत्त्वपूर्ण शहरों में प्रशासन ठप हो गया और कर्फ्यू लगाना पड़ा। पटना में सेना बुलायी गयी। पूरा बिहार अराजकता की चपेट में आ गया। विरोधी दलों, समाचार पत्रों, व्यवसाय मंडल, वकील संघ आदि ने पुलिस बर्बरता की आलोचना की और सरकार से इस्तीफे की मांग की जाने लगी। इसी दौरान बिहार छात्र संघर्ष समिति ने जेपी से मार्गदर्शन का अनुरोध किया।
जेपी ने दोनों तरफ से हुई हिंसा की निंदा की। बुनियादी बदलावों के लिए अहिंसा और निर्दलीयता की जरूरत समझाई। विद्यार्थी प्रतिनिधियों ने जेपी को अनुशासन के पालन का भरोसा दिलाया। 8 अप्रैल को जेपी के नेतृत्व में सर्वोदय से जुड़े युवकों-नागरिकों का पटना में शांति स्थापना के लिए जुलूस निकला। इसमें राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े छात्रों-युवाओं की हिस्सेदारी पर मनाही थी। यह बिहार के छात्रों के लिए ही नहीं देशभर के विद्यार्थियों के बहुत बड़ी घटना थी।
जेपी का विद्यार्थियों-युवाओं के सवालों के समाधान के लिए आगे आना बहुत अप्रत्याशित उत्साह का कारण बना। इसी क्रम में जेपी ने पटना के बाहर की स्थिति जानने के लिए बिहार भर का दौरा किया। उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचने में देर नहीं लगी कि चारों तरफ असंतोष और आक्रोश का विस्तार हो रहा है लेकिन दिशाबोध नहीं है। दलों की दीवारें हैं। छात्रों और जनसाधारण में दूरियां हैं। छिटपुट हिंसा की आदत है। सही समझ और धीरज नहीं है।
बहुआयामी संकट के समाधान के लिए सत्ता-परिवर्तन की बजाय व्यवस्था-परिवर्तन की जरूरत है। इस समग्र बदलाव के लिए लोकशक्ति का निर्माण चाहिए। बिना लोकशक्ति के राजनीतिक शक्ति बेअसर साबित हो चुकी है। विचारधाराएँ निरर्थक बन गयी हैं। दल सत्ता की सीढ़ी भर रह गए हैं। लोकतंत्र का नया विमर्श चाहिए। सम्पूर्ण क्रान्ति चाहिए।
जेपी का यह निष्कर्ष 1969 और 1973 के बीच हुए सर्वोदय आत्म-मंथन के निष्कर्षों से अलग नहीं था। गांधीमार्गी सहयात्रियों से उनका खुला संवाद चला। इसीलिए वह सम्पूर्ण क्रांति की तलाश में अकेले नहीं पड़े। अनगिनत नए-पुराने गांधीमार्गी सड़क से जेल तक उनके सहयात्री बने। उन्होंने माओवादियों से मुसहरी में 1969-70 के डेढ़ बरस तक चले संवाद में भी आजादी के बाद की व्यवस्था का एक और स्वरूप देखा और ‘आमने-सामने’ पुस्तिका के जरिए नि:संकोच देश को भी बताया। फिर 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की अंतर्कथा से साक्षात्कार हुआ। आंतरिक उपनिवेशवाद और राष्ट्र-विखंडन का रिश्ता पूरी भयावहता के साथ आँखों के आगे था। देश की कानून-व्यवस्था की दुर्दशा से चम्बल के बागियों के आत्मसमर्पण के बहाने आमना-सामना हुआ।
जब उन्होंने इन सवालों को राष्ट्रीय सहमति से सुलझाने के लिए 1973 में सभी सांसदों को पत्र लिखकर जगाने की कोशिश की तो सभी आत्ममुग्ध और सत्तासाधना में लिप्त मिले। अधिकांश ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। इससे चिंतित होकर जेपी ने नागरिक शक्ति की रचना के लिए सरोकारी देशसेवकों को जोड़ना शुरू किया। इसी क्रम में ‘सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी’ और ‘यूथ फॉर डेमोक्रेसी’ के लिए आह्वान किया। अंग्रेजी पत्रिका ‘एवरीमैंस’ जुलाई 1973 से शुरू की।
इसलिए जब गुजरात और बिहार की प्रताड़ित युवाशक्ति और बेचैन नागरिक शक्ति ने उन्हें फरवरी और अप्रैल ’74 के बीच गुजरात और बिहार से पुकारा तो यह उनके लिए अप्रत्याशित नहीं था। उन्होंने खुद ही स्वीकारा कि ‘तीर पर कैसे रुकूँ मैं, आज लहरों में निमंत्रण!’ लेकिन उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी से नयी पीढ़ी को समस्याओं के व्यवस्थागत कारणों को समझाया। समाधान भी बताया। इसमें उन्होंने एक शिक्षक का कौशल दिखाया। एक पितामह का अपनत्व जताया। सत्ता-प्रतिष्ठान जेपी को नहीं समझ पाया। लेकिन समूचे बिहार और फिर क्रमश: देशभर की छात्र-युवा जमातों को जेपी की निष्काम देश-चिंता और निर्मल चेष्टा को समझने में देर नहीं लगी। इसीलिए 5 जून ’74 से आगे भारत के छात्रों-युवाओं के लिए जेपी अबूझ स्वप्नदर्शी नहीं रहे। अक्षय प्रेरणास्रोत और कालजयी लोकनायक बन गए।
भारत समेत सभी देशों में परिवर्तन का कोई भी प्रयास एक चल रही व्यवस्था से लाभान्वित जमातों, वर्गों और संगठनों के लिए असुविधाजनक होता है। फिर क्रांति का प्रयास तो खतरे की घंटी जैसा प्रभाव पैदा करता है। इसीलिए आजादी के बाद के राजनीतिक इतिहास में 5 जून 1974 को बिहार आंदोलन के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के गांधी मैदान की विराट रैली में जनसाधारण, विशेषकर नयी पीढ़ी से ‘सम्पूर्ण क्रांति’ के लिए आगे बढ़ने का आह्वान एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज यह पूछा जा सकता है कि ‘सत्तर के वर्षों में जयप्रकाश जी में ऐसी क्या खासियत थी कि उनके निष्कर्षों ने देश की दिशा बदल दी? देश ने तो 1971 के लोकसभा और 1972 के विधानसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रबल आस्था प्रकट की थी। वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ तक की सभी विरोधी पार्टियां पस्त थीं। ‘गरीबी हटाओ’ के नारे के साथ बैंकों के राष्ट्रीयकरण और महाराजाओं के प्रीवी पर्स खतम करने से लेकर पाकिस्तान के दो टुकड़े करके इंदिरा जी ने अपना चौतरफा वर्चस्व कायम कर लिया था। लेकिन यह तो तस्वीर का एक ही पहलू था।

दूसरी तरफ 1973 में बढ़ती महंगाई, व्यापक बेरोजगारी, निरर्थक शिक्षा व्यवस्था और तेजी से बढ़ते उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार का भी सच था। संसदीय मोर्चे पर एकाधिकार के कारण लोग विरोधी दलों का आसरा छोड़ कर खुद सड़कों पर आने लगे थे। नक्सलवादी घटनाओं में बढ़ोतरी थी। महंगाई से परेशान विद्यार्थियों और गृहिणियों के ‘नव-निर्माण आन्दोलन’ के कारण गुजरात में तो ताजा चुनी सरकार ही नहीं चल पायी और विधानसभा भंग करने पर ही लोग शांत हुए। इस सब के बीच जयप्रकाश जी अपने संयत तरीके से राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकने और जनता के सरोकारों के लिए निर्दलीय मंचों के जरिये नागरिक शक्ति को सबल बनाने की दिशा में देश को सजग करने में जुटे हुए थे। इससे एक नया नारा फैलने लगा – ‘अँधेरे में एक प्रकाश; जयप्रकाश! जय जयप्रकाश!!’ 1974 में कॉलेजों-विश्वविद्यालयों और कस्बों-नगरों की सभाओं में गाया जाने लगा : ‘जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। उठो जवानो! तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है।’ हर कोने से आवाज आती थी : ‘सम्पूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है!’
वस्तुत: ‘सम्पूर्ण क्रांति’ की ललकार के कई सकारात्मक नतीजे निकले। एक तो जयप्रकाश जी जैसे निष्पक्ष और निर्मल राष्ट्रनायक द्वारा आमूल-चूल बदलाव की जरूरत के ऐलान ने पूरे देश के परिवर्तनकामी व्यक्तियों, संगठनों और अभियानों के औचित्य को सिद्ध किया। दूसरे, जेपी के दो-टूक शब्दों ने छात्र-युवा आन्दोलनकारियों को तोड़फोड़ की क्षणिक आतिशबाजी के आत्मघाती तरीकों को त्यागते हुए अहिंसक क्रांति की दिशा अपनाने के लिए प्रेरित किया। तीसरे, 5 जून की घोषणा ने यथास्थितिवादी शक्तियों की ढाल बनी राजशक्ति और परिवर्तन के लिए बेचैन लोकशक्ति को आमने-सामने कर दिया। अन्यथा बिहार आन्दोलन दलों के दलदल में धंसने लगा था। चौथे, 5 जून के बाद बिहार में चल रहा जन प्रतिरोध क्षुब्ध विद्यार्थियों के एक प्रादेशिक आंदोलन की बजाय राष्ट्रनिर्माण के लिए जरूरी बदलावों के राष्ट्रीय अभियान की धुरी बनकर आगे बढ़ा। इसलिए 5 जून एक यादगार तारीख बन गयी।
लेकिन सम्पूर्ण क्रांति का संकल्प अधूरा रहा। क्यों? क्योंकि एक बरस के अंदर ही गुजरात में विधानसभा भंग करके हुए चुनावों में जून, 1975 में कांग्रेस की हार हो गयी। 12 जून 1975 को तो स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका के आधार पर चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी पाकर उनका चुनाव रद्द कर दिया। सारा देश लोकनायक जयप्रकाश की ओर देखने लगा। जयप्रकाश जी ने भी 25 जून को देश की राजधानी में विशाल जनसभा में इंदिरा सरकार के इस्तीफे की मांग के समर्थन में अहिंसक अभियान का ऐलान कर दिया। इससे घबराकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए 25 जून 1975 की रात से राष्ट्रपति के अप्रत्याशित अध्यादेश के जरिये ‘इमरजेंसी राज’ थोप दिया गया। इसके जरिये राजसत्ता के दमन-चक्र के कारण समूची लड़ाई व्यवस्था-परिवर्तन की बजाय लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने की ओर मुड़ गयी। जेपी और विपक्ष के तमाम नेता बिना मुक़दमा चलाये गिरफ्तार कर लिए गए। छात्रों और नौजवानों की देशभर में धर-पकड़ की गयी। संविधान ही तोड़-मरोड़ दिया गया। मीडिया पर सेंसर का पहरा बैठा दिया गया। न्यायपालिका के हाथ बाँध दिए गए। लोकसभा के चुनाव टाल दिए गए। जब लोकतंत्र ही नहीं बचा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक सुधारों के लिए शुरू की गयी ‘सम्पूर्ण क्रांति’ की जरूरत कैसे पूरी होती?
यह पूछा जा सकता है कि आज, आधी शताब्दी बाद 5 जून को ‘सम्पूर्ण क्रांति दिवस’ को याद करने की क्या प्रासंगिकता है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए यह प्रश्न पूछना सही होगा कि अगर जयप्रकाश जी ने 1974 में महंगाई, बेरोजगारी, निरर्थक शिक्षा और उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार से फ़ैल रहे मोहभंग और असंतोष के समाधान के लिए चुनाव सुधारों को सबसे पहली जरूरत बतायी थी तो आज की दुर्दशा के समाधान के लिए उनकी तरफ से क्या समाधान बताया जाता? निसंदेह जेपी 1975 से अवरुद्ध ‘सम्पूर्ण क्रांति’ को पूरा करने की सलाह देते। क्योंकि तब के चारों यक्ष प्रश्न अर्थात महंगाई, बेरोजगारी, निरर्थक शिक्षा और उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार आज जादा विकराल हो चुके हैं और सत्ता का खेल जादा राक्षसी हो चुका है। तबसे अबतक चुनावी खर्चों में बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है और चुनावों से बननेवाले विधायकों-सांसदों और सरकारों के सरोकारों में बहुत खराबी आ चुकी है। तब लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए कुछ लाख रुपयों की जरूरत थी, अब करोड़ों से कम में काम नहीं चलता। तब खाली देशी घरानों का पैसा लगता था, अब वैश्विक स्तर पर धंधा करनेवाले अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट घराने नेताओं की नकेल थामे दीखते हैं। तब जीतनेवाले विधायक और सांसद कुछ हद तक अपने दलों के घोषणापत्र और अपने चुनावी वायदों के प्रति जवाबदेही निभाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब तो जवाबदेही और सक्रियता अप्रासंगिक हो चुकी है। बासी घोषणापत्र ही काम में लाये जाते हैं। समूचा चुनाव प्रचार मीडिया के सहयोग से धनशक्ति का अश्लील खेल हो गया है। सरकारें भी मुट्ठीभर लक्ष्मीपुत्रों के मनबहलाव का खिलौना हो गयी हैं। राजनीति का अपराधीकरण, परिवारवाद, प्रभु जातियों का वर्चस्व और साम्प्रदायिकता चार नए महादोष जुड़ गए हैं।
लेकिन आज जयप्रकाश जैसे नि:स्वार्थ नायक नहीं हैं, न देश में लोकशक्ति और युवाशक्ति को आगे बढ़ानेवाली बेचैनी है। हाँ, उस रोमांचक दौर की स्मृतियाँ हैं जो हर 5 जून को आशा पैदा करती हैं : हमको है यकीन हम होंगे कामयाब एक दिन…
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.