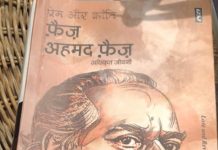— गोपेश्वर सिंह —
रामविलास शर्मा ने 1936 ई. को इस अर्थ में विशिष्ट माना है कि इस वर्ष तीन ऐसी रचनाएँ प्रकाशित हुईं जिनमें भविष्य के भारत का सपना था। इनमें पहली रचना आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू की ‘आत्मकथा’ थी। दूसरी रचना लोकनायक जयप्रकाश नारायण की ‘समाजवाद ही क्यों?’ (‘why socialism?’) थी। तीसरी रचना प्रेमचंद का निबंध ‘महाजनी सभ्यता’ है। पहली दोनों रचनाएं पुस्तक रूप में थीं और अंग्रेजी में लिखी गयी थीं। ‘आत्मकथा’ सिर्फ नेहरू की निजी कथा न होकर स्वतंत्रता आन्दोलन और स्वतंत्र भारत के आधुनिक जनतांत्रिक सपने की कथा भी है। ‘समाजवाद ही क्यों?’ (Why socialism?) भारत में समाजवादी व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देनेवाली पहली व्यवस्थित पुस्तक थी। नेहरू और जेपी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, अपने-अपने समय के युवा हृदय सम्राट तथा गांधी के बाद देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। ऐसे महानों की अति प्रसिद्ध पुस्तकों के साथ रामविलास जी ने हिंदी के लेखक प्रेमचंद के एक निबंध को याद किया है तो इसका विशेष अर्थ है।
प्रकाशन तो 1936 में और भी हुए होंगे- अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। लेकिन जब रामविलास शर्मा इन तीनों का नाम एकसाथ लेते हैं तब इसका एक खास अर्थ है और उस खास अर्थ को नेहरू और जेपी के साथ प्रेमचंद भी शक्ति देते हैं। अपने समय की आलोचना करनेवाले तो बहुतेरे लेखक मिल जाएँगे किन्तु जो लेखक वर्तमान के साथ भविष्य की भी चिंता करे, ऐसे लेखक कम होते हैं। यह नहीं कि वे वैसा जान-बूझकर करते हैं। असल में उनके पास भावी संसार का कोई मुकम्मल नक्शा नहीं होता है। इसके विपरीत प्रेमचंद ऐसे लेखक थे जिनकी नजर वर्तमान के साथ बेहतर भविष्य पर भी थी। इसलिए यह अकारण नहीं है कि नेहरू और जेपी की पुस्तकों के साथ रामविलास शर्मा प्रेमचंद के निबंध ‘महाजनी सभ्यता’ का नाम लेते हैं जो उनकी लेखकीय दृष्टि को समझने के खयाल से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
महाजनी सभ्यता यानी पूँजीवादी सभ्यता। पूँजीवाद के पहले सामंतवादी सभ्यता थी। ये दोनों सभ्यताएँ जनता के शोषण और सामाजिक भेदभाव पर आधारित थीं। जो सभ्यता शोषण और भेदभाव पर आधारित हो वह प्रेमचंद को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं थी।
उन्होंने उस सभ्यता का का स्वागत किया जिसका सूर्य पश्चिम में उग रहा था। निस्संदेह पश्चिम के उस सूर्य से तात्पर्य रूस में स्थापित समाज व्यवस्था से है। प्रेमचंद ने पूँजीवादी सभ्यता की कठोरतम आलोचना करने के बाद लिखा : “परन्तु अब नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूँजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दी है जिसका मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है और जो दूसरों की मेहनत या बाप-दादों के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है वह पतिततम प्राणी है।” (Anavaratblogspot.in)
प्रेमचंद भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के गर्भ से पैदा हुए ऐसे लेखक थे जिसके लिए स्वतंत्रता का अर्थ राजनीतिक मुक्ति के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति भी है। वे पूँजीवादी व्यवस्था के जितने खिलाफ थे, उतने ही सामंती व्यवस्था के खिलाफ भी। जाति, संप्रदाय और गरीबी के सवाल उनके शब्द-कर्म के जरूरी एजेंडे थे। पुराना क्या है जो अप्रासंगिक हो चुका है और नया क्या है जो प्रासंगिक है, उसकी जितनी साफ समझ उनके पास थी, वैसी हिंदी के उनके समकालीन किसी दूसरे लेखक के पास शायद ही हो!
प्रेमचंद यदि 1936 में ‘महाजनी सभ्यता’ का क्रीटिक तैयार करते हैं तो इसका कारण यह है कि वे पुराने समय और नए समय में फर्क करना ठीक से जानते हैं। 1919 में प्रकाशित उनके ‘पुराना जमाना : नया जमाना’ शीर्षक निबंध को देखने से पता चलता है कि 1936 में वे जहाँ पहुंचे थे उसकी तैयारी वे बहुत पहले से कर रहे थे। अपने उस निबंध में वे लिखते हैं : “आने वाला जमाना अब जनता का है, और वह लोग पछताएंगे जो जमाने के कदम-से-कदम मिलाकर न चलेंगे।” (विविध प्रसंग; भाग-1; पृ.269)
जमाने के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चलने की जो सबसे बड़ी कसौटी प्रेमचंद की थी वह थी किसानों की हालत। उनके सारे रचनात्मक और वैचारिक लेखन के मूल में किसान जीवन की वास्तविकता और उनकी चिंता सर्वोपरि है।
जैसे महात्मा गाँधी के ‘स्वराज’ के केंद्र में गाँव था और गाँव के किसान थे, वैसे ही प्रेमचंद के लेखकीय चिंतन के केंद्र में किसान हैं। ‘पूस की रात’ का हलकू हो या ‘गोदान’ का होरी या उनका वैचारिक लेखन, किसान जीवन की दशा-दुर्दशा और उसका भविष्य उनकी सजग-सचेत नजर से कभी ओझल नहीं होता।
‘पुराना जमाना, नया जमाना’ का एक अंश इस दृष्टि से देखा जा सकता है : “क्या यह शर्म की बात नहीं कि जिस देश में नब्बे फीसदी आबादी किसानों की हो उस देश में कोई किसान सभा, कोई किसानों की भलाई का आन्दोलन, कोई खेती का विद्यालय, किसानों की भलाई का कोई व्यवस्थित प्रयत्न न हो। आपने सैकड़ों मदरसे और कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटियाँ खोलीं और अनेक आन्दोलन चलाए मगर किसके लिए? सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए। और शायद अपने राष्ट्र की जो कसौटी आपके दिमाग में थी उसको देखते हुए आपका आचरण जरा भी आपत्तिजनक न था। मगर नए जमाने ने नया पन्ना पलटा है। आने वाला जमाना अब किसानों और मजदूरों का है। दुनिया की रफ्तार इसका साफ सबूत दे रही है। हिंदुस्तान इस हवा से बेअसर नहीं रह सकता। हिमालय की चोटियाँ उसे इस हमले से नहीं बचा सकतीं। जल्द या देर से, शायद जल्द ही, हम जनता को केवल मुखर ही नहीं, अपने अधिकारों की माँग करने वाले के रूप में देखेंगे और तब वह आपकी किस्मतों की मालिक होगी।” (वही, पृ.268)
प्रेमचंद जिस आधुनिक भारत का सपना देख रहे थे वह ऐसा राष्ट्र-राज्य है जिसमें किसान-मजदूर खुद अपनी किस्मत के मालिक होंगे। वे यह तो मानते हैं कि ‘वर्तमान सभ्यता का सबसे अच्छा पहलू राष्ट्रीयता की भावना का जन्म लेना है।’ (वही, पृ.259)
लेकिन सच्ची राष्ट्रीयता उनकी नजर में तब तक नहीं आ सकती जब तक कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर-बराबरी जनता में है।
वे कहते हैं : “आपका आधुनिक शिक्षा से वंचित भाई आपको इस ठाट में देखता है और यह समझता है कि यह आदमी हममें नहीं है, हम उनके नहीं हैं। फिर चाहे आप कितनी बुलंद आवाज से राष्ट्रीयता की हांक लगाएं।”(वही)
इसी के साथ वे यह जोड़ना नहीं भूलते कि यदि ‘राष्ट्रीयता’ आधुनिक सभ्यता का सबसे अच्छा पहलू है तो वे यह भी बताते चलते हैं कि ‘जनतांत्रिक’ का समावेश ‘आधुनिक सभ्यता का सबसे प्रधान गुण है।” (वही) इससे पता चलता है कि प्रेमचंद के लिए जो भविष्य का भारत है उसका ताना-बाना ‘जनतांत्रिकता’ और ‘आधुनिकता’ के रेशे से निर्मित है जिसमें ‘किसान-मजदूर अपनी किस्मत के मालिक’ हैं।
लगभग सौ वर्ष पूर्व देखा गया भारतीय राष्ट्र-राज्य का प्रेमचंद का सपना मुहावरे के अर्थ में अब भी सपना है! किसान मजदूर अब भी अपनी किस्मत के मालिक नहीं हैं! हमारी जनतांत्रिक आकांक्षाओं पर अब भी पहरेदारी है! आर्थिक और शैक्षिक गैर-बराबरी की तो बात ही मत पूछिए!
भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रेमचंद सदेह शामिल नहीं थे। कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि जनता की मुक्ति की बात करनेवाला लेखक जनता के मुक्ति-संघर्ष में सदेह शामिल क्यों नहीं होता? उस जमाने में हिंदी व विभिन्न भारतीय भाषाओं के अनेक लेखक स्वतंत्रता संग्राम में सदेह शामिल थे और उस कारण उन्हें तरह-तरह की यातनाएँ भी झेलनी पड़ीं। ऐसे सभी लेखकों से भारत के मुक्ति-संग्राम को बल मिला। उनके कर्म से भी और उनके शब्द से भी। लेकिन ऐसे भी बहुतेरे लेखक थे जो स्वतंत्रता संग्राम में सदेह शामिल न होकर मनसा-वाचा शामिल थे। उनके लिखे से भारतीय राष्ट्र-राज्य का नया रूप बन रहा था। उनका एक-एक शब्द हजारों-लाखों को प्रेरित-प्रभावित कर रहा था।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ऐसे ही लेखक थे जिनसे भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम को नयी ऊर्जा मिलती थी। प्रेमचंद भी ऐसे ही लेखक थे जो भारतीय समाज और राष्ट्र की मुक्ति के मार्ग में बाधक सभी तत्त्वों से प्रारम्भ से अंत तक अनवरत कलम से लड़ते रहे। अमृत राय ने ‘कलम का सिपाही’ नाम से उनकी जीवनी लिखी है। सही अर्थों में वे कलम के सिपाही थे। वे कलम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नेवाले हिंदी के सबसे बड़े लेखक थे।
कलम से जिस तरह जनता और राष्ट्र की मुक्ति की लड़ाई प्रेमचंद लड़ रहे थे, उसका सही पता-ठिकाना तभी चलता है जब हम उनके रचनात्मक साहित्य के साथ उनके वैचारिक लेखन को भी देखते हैं। अपने लेखन काल के प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत लगभग तीन दशक का प्रेमचंद का जो वैचारिक लेखन है वह भारत की स्वतंत्रता, स्वावलंबन, आर्थिक–सामजिक गैरबराबरी और विश्व बंधुत्व जैसी अनेक चिंताओं से मुठभेड़ का प्रतिफल है।
हम अकसर उन्हें आर्य समाजी, गाँधीवादी और मार्क्सवादी प्रभावों के सन्दर्भ में देखते-दिखाते हैं। उनके साहित्य पर इनके प्रभाव से किसी को इनकार भी नहीं है। लेकिन उनकी चेतना सबसे अधिक स्वतंत्रता आन्दोलन के मूल्यों से संचालित है।
विदेशी दासता से मुक्ति के लिए स्वशासन जरूरी था। लेकिन कैसा स्वशासन? वे सही अर्थों में जनता के शासन के पक्ष में थे और जनता का शासन तब आएगा जब बेजुबानों की ताकत जाहिर होने लगेगी। उन्हीं के शब्द देखें… “अब एक फाकाकश मजदूर भी अपनी अहमियत समझने लगा है और धन-दौलत की ड्योढ़ी पर सर झुकाना पसंद नहीं करता। उसे अपने कर्तव्य चाहे न मालूम हों लेकिन अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान है। वह जानता है कि इस सारे राष्ट्रीय वैभव और प्रभुत्व का कारण मैं हूँ। यह सारा राष्ट्रीय विकास और उन्नति मेरे ही हाथों का करिश्मा है। अब वह मूक संतोष और सर झुकाकर सबकुछ स्वीकार कर लेने में विश्वास नहीं रखता।” (वही, पृ. 264) तो प्रेमचंद इस मजदूर की हिस्सेदारी ‘स्वशासन’ में सुनिश्चित करना चाहते थे।
‘स्वदेशी आन्दोलन’ स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा एजेंडा था। स्वदेशी के बिना भारत राष्ट्र के रूप में खड़ा नहीं हो सकता था। स्वतंत्रता आन्दोलन में महात्मा गाँधी के प्रवेश के बहुत पहले स्वदेशी की मांग जोर-शोर से उठने लगी थी। महात्मा गाँधी के आने के बाद इस आन्दोलन ने और जोर पकड़ा जब वे 1915 में भारत आए। प्रेमचंद 1905 में ‘देशी चीजों का प्रचार कैसे बढ़ सकता है’ (वही, पृ.15) शीर्षक निबंध लिखकर घरेलू उद्योग-धंधों के विकास और उनकी मार्केटिंग के मार्ग में आनेवाली बाधाओं की चिंता करते हैं। वे उसी वर्ष ‘स्वदेशी आन्दोलन’ की वकालत करते हैं और उसे ‘देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन’ (वही, पृ.20) की संज्ञा देते हैं। ‘स्वराज से किसका अहित होगा?’ (1930) शीर्षक अपने निबंध में वे निर्भय होकर इस संग्राम में सम्मिलित होने की मांग करते हैं। 1931 में ‘देश की वर्तमान परिस्थिति’ की चर्चा करते हुए वे किसानों से अपील करते हैं कि ‘महात्मा जी के मार्ग’ से यदि वे हटे तो उन्हें पछताना पड़ेगा।
‘स्वदेशी आन्दोलन’ का जबर्दस्त समर्थन करने के साथ प्रेमचंद भारत और पूरी दुनिया में गोरी जातियों की सभ्यता के अन्यायपूर्ण आचरण और दमन-शोषण की आलोचना करते हैं और उनके पाखंड पर चोट करते हैं। ‘गोरी जातियों का प्रभाव क्यों कम है’ (1931) शीर्षक निबंध में वे लिखते हैं, “अगर गोरों का जीवन आदर्श होता, उसमें ऐसी खूबियां होतीं कि दूसरों के दिल में उससे भक्ति और सम्मान का संचार होता। गोरों ने आदि से ही प्रेम के बल… पर नहीं, आतंक के बल पर संसार पर प्रभुत्व जमाया है। वह कालों की नज़रों से अपने ऐबों को छिपाकर अपनी नीतिमत्ता की साख बिठाये थे।”(विविध प्रसंग, भाग-2, पृ. 77-78)
अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीति और गरीब जनता को टैक्स के जरिए लूटने की उनकी आदत के कारण प्रेमचंद को ‘स्वराज की कामना’ का भारतीय जन में ‘जन्म लेना’ स्वाभाविक जान पड़ता है।
प्रेमचंद के लिए राष्ट्र का अर्थ सिर्फ कोई निश्चित भू-भाग ही नहीं, उसके आगे भी बहुत कुछ है। उनके लिए राष्ट्र का अर्थ सबसे पहले उस भू-भाग की शोषित, पीड़ित जनता है।
‘नवयुग’ (1932) शीर्षक अपने एक निबंध में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की ओर संकेत करते हुए वे लिखते हैं : “राष्ट्र केवल एक मानसिक प्रवृत्ति है। जब यह प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है तो किसी प्रांत या देश के निवासियों में भ्रातृभाव जागरित हो जाता है। तब उनमें रूढ़ियों से पैदा होनेवाले भेद, पुराने संस्कारों से उत्पन्न होनेवाली विभिन्नताएँ और ऐतिहासिक तथा धार्मिक विषमताएँ, एक प्रकार से मिट जाती हैं।” (वही, पृ.98) जब तक ‘विविधताएँ’ और ‘विषमताएँ’ किसी राष्ट्र में मौजूद हैं तब तक वह सही अर्थों में राष्ट्र नहीं है। जनता का जिस तरह शोषण है, गरीबी का जैसा साम्राज्य है, गाँवों की जो हालत है, उसपर वे ‘दमन की सीमा’ (1932) शीर्षक निबंध में गंभीर और तल्ख़ टिप्पणी करते हैं। ब्रिटिश सरकार, प्रशासन और जमींदारों को कठघरे में खड़ा करते हुए कहते हैं : “देहात से, सुधार और सहयोग और शिक्षा और स्वास्थ्य और सभी आयोजनाएँ, जिनसे राष्ट्र बनता है, जिनसे उसका विकास होता है, लापता है।” (वही, पृ.92)
औरों के लिए ‘राष्ट्र’ और ‘राष्ट्रीयता’ का जो भी अर्थ हो, प्रेमचंद के लिए उसका ठेठ भारतीय अर्थ है। उनकी दो टूक राय है, “राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्ण-व्यवस्था, ऊँच-नीच के भेदभाव और धार्मिक पाखण्ड की जड़ खोदना है।” (वही, पृ.476)
जातिभेद की समस्या को भारतीय राष्ट्रीयता की केन्द्रीय समस्या मानते हुए ऐसे लोगों पर प्रेमचंद जोरदार हमला करते हैं जो जाति की श्रेष्ठता और धार्मिक विद्वेष की भावना से भरे हुए हैं। राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के नकली प्रवक्ताओं को ‘क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं?’ (1934) शीर्षक निबंध लिखकर कठघरे में खड़ा करते हैं। वे लिखते हैं : “हम अभी तक केवल मुंह से राष्ट्र-राष्ट्र का गुल मचाते हैं, हमारे दिलों में अभी वही जाति भेद अन्धकार छुपा हुआ है। और यह कौन नहीं जानता कि जाति भेद और राष्ट्रीयता दोनों में अमृत और विष का अंतर है।” (वही, पृ.470) इसलिए जो पुजारी, पुरोहित और पंडे जातिभेद करते हैं उन्हें वे ‘टके पंथी’ और ‘हिन्दू जाति का कलंक’ कहकर संबोधित करते हैं।
(बाकी हिस्सा कल)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.