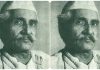मैं तड़के उठ जानेवाले लोगों में नहीं। लेकिन मंगलवार की सुबह कुछ और ही थी। मंगलवार को एकदम सबेरे ही जाग गया था, और मैं ही क्यों, मेरा पूरा परिवार जगा हुआ था। हम सबको ओलंपिक के हॉकी सेमी-फाइनल के लिए भारत और बेल्जियम के बीच होने जा रहे मैच को देखना था। लाखों भारतीय दर्शकों की तरह हम भी कंप्यूटर के पर्दे पर चल रहे मैच को देख शुरुआत में आनंद और उछाह के भाव से भरे थे फिर हमें चिन्ता ने सताया और आखिर को तकलीफ के अहसास ने घेर लिया। पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम मैच हार गयी लेकिन इस हार में अपमान का दंश नहीं था। ये हार ऐसी ना थी कि ब्रिटेन के खिलाफ मैच में हार्दिक सिंह ने जो शानदार एकलौता गोल दागा था, उस गोल की सुखद याद को मिटा दे। अर्जेंटीना के खिलाफ हुई हार ऐसी ना थी कि वह आस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज करनेवाली हमारी महिला हॉकी टीम के चक दे लम्हे के गर्व-बोध को धुंधला कर सके। जर्मनी के खिलाफ जीत के जज्बे ने इस कांस्य पदक को स्वर्णिम रंग दे दिया है।
यह अनुभव मुझे लगभग पचास साल पहले के वक्त में ले गया, मेरे स्कूली दिनों में। मेरे स्कूल एसजीएम खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीगंगानगर में ग्रामीण इलाके के सिख लड़कों की भरमार थी और स्कूल की प्रसिद्धि का एकमात्र कारण था खेलों के मामले में उसका अव्वल होना। उन दिनों राजस्थान की तरफ से खेलने वाले ग्यारह खिलाड़ियों की टीम में 6 से 8 लड़के अकेले मेरे स्कूल से हुआ करते थे। मेरे कॉलेज, एसजीएन खालसा कॉलेज, की भी हॉकी और एथलेटिक्स में ऐसी ही धाक थी। तब मैं भी थोड़ी-बहुत हॉकी खेलता था, हालांकि स्कूल की टीम-सी से आगे ना बढ़ सका लेकिन इतनी हॉकी आ गयी थी कि 1982 के एशियाई खेलों के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने हॉकी के कमेंटेटर्स का पैनल बनाया तो उसमें एक नाम मेरा भी था।
उस वक्त अपने आसपास के बाकी लोगों की तरह मुझे भी हॉकी का चस्का था। यों भारतीय हॉकी का स्वर्णयुग बीत चुका था लेकिन तब भी उसमें इतना जोर बचा हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की धमक बनी रहे। हमने ध्यानचंद का नाम भर सुना था लेकिन उनके बेटे अशोक कुमार उस वक्त हमारे हीरो थे। बलबीर सिंह के बारे में मुझे कोई खास जानकारी ना थी लेकिन इतना याद रह गया है कि मशहूर सेंटर हॉफ अजीतपाल सिंह से हाथ मिलाने का जब मौका मिला तो मैं किस कदर विस्मित हुआ था।
भारतीय हॉकी के गौरव का एक यादगार लम्हा वो भी था जब 1975 के वर्ल्डकप के सेमी-फाइनल में क्वालालम्पुर में असलम शेरखान ने मैच के एकदम आखिरी लम्हे में गोल दागा। भारत इस मैच में विजयी रहा। उस वक्त मेरे शहर में टेलीविजन नहीं हुआ करता था। हॉकी का जादू हमारे मन में जसदेव सिंह की रेडियो कमेंट्री के जरिए उतरता था। उनकी आवाज को सुनकर आपको खुद ही मन ही मन अपनी तरफ से रंग, दृश्य और हॉकी स्टिक से कमाल करते खिलाड़ियों के एक्शन जोड़ने होते थे। मेरी पीढ़ी के लिए भारतीय हॉकी टीम राष्ट्रीय गौरव का झंडा बुलंद करने वाली शय थी। बेशक, ऐसा सोचना जोखिम भरा था लेकिन फिर कुछ जोखिम ऐसे होते हैं कि उन्हें उठाने को जी ललचाता है। भारतीय हॉकी को राष्ट्रीय गौरव का झंडाबरदार मानने का जोखिम उठाना ऐसा ही था।
हॉकी से क्रिकेट
ज्यादातर दोस्तों की तरफ हॉकी को लेकर मेरी दीवानगी देर तक कायम ना रही, हॉकी की जगह जल्दी ही क्रिकेट ने ले लिया। क्रिकेट को लेकर मेरी दीवानगी की शुरुआत 1974-75 के जाड़ों में हुई जब क्लाइव लॉयड के नेतृत्व में वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आयी थी। इस दौरे में गार्डन ग्रीनिज, विवियन रिचर्ड्स और एंटी रॉबर्ट्स ने अपने टेस्ट करिअर की शुरुआत की। मेरी खास पसंद थे गुंडप्पा विश्वनाथ, बृजेश पटेल और बी.एस. चंद्रशेखर। ये तीनों ही कर्नाटक से थे। बेशक भारत ये सीरिज हार गया लेकिन उसका गर्व कायम था। साल 1976 में एस्ट्रोटर्फ की शुरुआत के साथ भारतीय हॉकी की तेज ढलान शुरू हुई, ऐसी ढलान जिससे फिर उबरना ना हो सका। हां, ढलान के इसी दौर में मास्को ओलंपिक में ज्यों-त्यों करके एक स्वर्णपदक मिल गया था। यह संयोग ही कहा जाएगा कि जिस वक्त हॉकी ढलान पर थी उसी समय क्रिकेट की दुनिया में भारत का सितारा बुलंद होना शुरू हुआ और एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत ने 1983 के वर्ल्ड-कप में मुंहमांगी जीत हासिल की।
कुछ दोस्तों ने आपस में जुड़कर स्थानीय स्तर पर एक क्रिकेट टीम बना ली और इसका भारी-भरकम सा नाम रखा एलेवन स्टार क्लब। कृषि उपज विपणन मंडी (एपीएमसी) के नये बने यार्ड का अभी उद्घाटन नहीं हुआ था और यही हमारा क्रिकेट ग्राउंड बना। टेलीविजन ने मेरे शहर में बस अभी-अभी दस्तक दी थी, हालांकि अभी मेरे घर में कोई टीवी सेट नहीं आया था। सामाजिक प्रतिष्ठा के नये प्रतीकों में शुमार हो चला टीवी का पांच मीटर ऊंचा एंटीना तब लाहौर के टीवी स्टेशन के सिग्नल ज्यादा पकड़ता था और अमृतसर से आनेवाले हमारे दूरदर्शन के सिग्नल कम। क्रिकेट स्टार- इसमें मैंने कपिल देव का नाम जोड़ लिया था- हमारे नये राष्ट्रीय हीरो थे। यों क्रिकेट के मैदान में भारत की हालत अब भी छुपे रुस्तम की ही थी और जब-तब हमारी टीम प्रतिस्पर्धी टीम को धराशायी कर देती थी। यह हमारे मन में राष्ट्रीय गर्व का भाव जगाये रखने के लिए काफी था। जब मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम नहीं खेल रही होती तो मैं वेस्टइंडीज या फिर पाकिस्तान टीम की तरफ से जोर लगाता और विवियन रिचर्ड्स तथा जहीर अब्बास की प्रशंसा किया करता था। यह तीसरी दुनिया के देशों की एकजुटता और गुटनिरेपक्ष आंदोलन के चरमोत्कर्ष के दिन थे।
लेकिन इसके दो दशक बाद खेलों की दुनिया से मेरा लगाव लगभग टूट गया। कहां तो क्रिकेट को लेकर दीवानगी का आलम तारी रहता था और कहां ये दिन आ गये कि क्रिकेट को लेकर बस कभी-कभार कुछ चीजें जान-सुन लेने भर से काम चलाने लगा। हॉकी की बस धुंधली सी यादें बची थीं, उससे लगाव अब बहुत दूर की बात हो चली थी। लगान फिल्म ने बेशक धूम मचायी लेकिन क्रिकेट से मेरा लगाव पहले की तरह कायम ना हो सका। चक दे! इंडिया फिल्म ने लोगों के दिलों पर जरूर ही घड़ी भर को राज किया और आंखें भीग गयीं लेकिन आंखों का यह भीगना हॉकी के गुजरे दौर के लिए था और जैसा कि कहते हैं गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा।
खेलों से हद दर्जे का चाव रखनेवाला मेरा बेटा जब तक मुझे फिर से उस दुनिया से जोड़ता तबतक क्रिकेट का खेल एकदम ही बदल चुका था। ट्वेन्टी-ट्वेन्टी ने क्रिकेट के खेल की गति और रूप दोनों को बदला। अच्छा ये रहा कि मैंने इस बदलाव को हिकारत से नहीं देखा। मुझे टी20 मैच अच्छे लगते हैं। अब मैच में छक्के पर छक्के जड़े जा रहे हों तो भला ये किसको अच्छा नहीं लगेगा? मुझे बड़ा विस्मय होता है कि क्रिकेट के जिस रूपाकार को खालिस बल्लेबाजों के लिए रचा गया था आज उसी पर कैसे गेंदबाजों का दबदबा है। मुझे ये सोचकर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय क्रिकेट के पास एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं और ये भी कि भारतीय क्रिकेट के पास प्रतिभाओं की इफरात है।
नया सवेरा
इस सब के बावजूद एक खालीपन सा महसूस होता है। दिल में खनक नहीं होती। क्रिकेट अब मनोरंजन उद्योग का ही विस्तार जान पड़ता है। खिलाड़ियों की नीलामी की बात सुनता हूं तो कान ढंक लेने को जी होता है। आईपीएल की टीमें शहरों और इलाकों की नुमाइंदगी करती हैं और मैं उनसे अपने को जोड़ नहीं पाता। मुझे पता है कि अभी हमलोग विश्व-क्रिकेट का सिरमौर हैं लेकिन ये तथ्य मेरे राष्ट्रीय-अस्मिता बोध से जुड़ नहीं पाता। मुझे दिखता है कि भारतीय क्रिकेट के प्रेमी दर्शक देश के भीतर और बाहर हर जगह मौजूद हैं, वे क्रिकेट के अपने प्रेम में चेहरे पुतवाये हुए हैं, टी-शर्ट रँगवाये हुए हैं लेकिन मैं इस भीड़ और इंग्लिश फुटबॉल की दीवानी भीड़ में अन्तर नहीं कर पाता। मैं इसी भीड़ के शोर में अपनी आवाज नहीं मिला पाता। भारत ने टी-टेवेन्ट्वी का वर्ल्ड कप जीता लेकिन इस जीत के मायने वे नहीं जो 1983 के वर्ल्ड-कप की जीत या फिर 1975 के वर्ल्ड-कप हॉकी की जीत के थे।
लेकिन इस बार के ओलंपिक में खेल रही भारतीय हॉकी टीम के साथ मुझे कुछ जाना-पहचाना सा अहसास हुआ। कोई शक नहीं कि हॉकी का खेल भी बहुत बदला है : इसका फोर-क्वार्टर फॉरमेट, खेल की गति, ड्रिब्लिंग के जादू को पीछे धकेल उसकी जगह ले चुका ड्रैग और फ्लिक और फिर खेल के नये नियम। तो भी, हॉकी का खेल है तो वही।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज की, तो ये मेरे दिल से कुछ वैसे ही जुड़ा जैसे कि वह मैच जब 45 साल पहले अजीतपाल सिंह की टीम की हासिल जीत ने दिल को छुआ था। भारतीय महिला हॉकी के खिलाड़ियों की ‘गरबीली गरीबी’ की कहानी 1970 के दशक की भारतीय हॉकी की कहानी से जुदा नहीं। आज भी हैट्रिक बनानेवाली वंदना कटारिया के परिवार को दलित होने के नाते अपमान सहना पड़ता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में पदक ना जीते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार के बावजूद मेरे लिए वंदना वंदन योग्य हैं, भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम नये नेशनल हीरो हैं।
मेरी यह कहानी सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है। यह कहानी उस पूरी पीढ़ी की भी कहानी है जिसने उपनिवेशवाद के बाद के वक्त के एक खुरदरे लेकिन मजबूत राष्ट्रवाद को ठोस, कठोर अति-राष्ट्रवाद में बदलते देखा जो कि खास हमारे अब के वक्त की निशानी है। साल 1970 के दशक की हॉकी और 1980 के दशक के क्रिकेट में दरअसल अपना हुनर दिखाने को निकले एक संकोची व्यक्ति सा गर्व बोध था, विश्व-रंगमंच में अपना जौहर दिखाने को निकले एक ऐसे किरदार का गर्व-बोध जिसे ये संकोच सताता रहता है कि सामनेवाले को पछाड़ पाऊंगा या नहीं।
आज जो क्रिकेट के इर्द-गिर्द जनोन्माद का सैलाब उमड़ा दिखता है वह कुछ और नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक दबंगई का ही संकेतक है, एक ऐसी आक्रामकता का, जो ऊपर से तो बहुत आत्म-विश्वासी जान पड़ती है लेकिन भीतर से उतनी ही खोखली है।
क्रिकेट को आधार बनाकर उपनिवेशवाद की राजनीति की कथा लिखने वाले आशिस नंदी ने एक जगह हमें आगाह किया है कि ‘क्रिकेट के खिलाड़ी जड़ों से उखड़े, संस्कृति-हीन और अपमान के बोध से ग्रस्त भारतीयों के लिए देश के नैतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मोर्चों पर नाकामी की एकमात्र दवा के रूप में तब्दील हो गये हैं।’
ऐसे परिदृश्य में भारतीय हॉकी का उभार मेरे भीतर भरोसा जगाता है कि एक अलग तर्ज का, कहीं ज्यादा गहरा और सकारात्मक राष्ट्रवाद हमारे भीतर अब भी जिन्दा है। भले ही यह ढंक-छिप गया हो लेकिन हमारी राष्ट्रीय चेतना में यह अब भी मौजूद है, इसे मिटाया नहीं जा सका है। अगर ऐसा है तो यह कांस्य किसी स्वर्ण से कम नहीं है। या कि यह बस मेरा एक ख्वाब है?
(द प्रिंट से साभार)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.