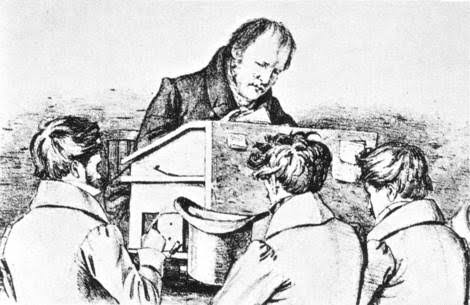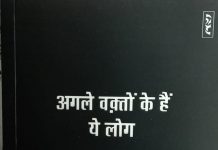— नंदकिशोर आचार्य —
शिक्षा के राजकीय यानी सरकारी नियंत्रण में चले जाने का एक आवश्यक परिणाम यह होता है कि वह विद्यार्थी के बजाय राज्य के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। दूसरे शब्दों में, उसका प्रयोजन एक ऐसा नागरिक तैयार करना हो जाता है जो राज्य यानी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल या व्यक्ति की आकांक्षा के अनुरूप हो। ऐसी स्थिति में इस बात को सहज ही भूला जा सकता है कि उसका प्राथमिक उत्तरदायित्व विद्यार्थी के प्रति है और इसका परिणाम होता है कि अपने प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थी को एक स्वतंत्र और विवेकशील व्यक्ति की तरह विकसित करने की बजाय वह उसे अपने राजनीतिक नियंत्रण की जरूरतों के अनुसार ढालने का प्रयत्न करने लगती है। इसी जरूरत के चलते वह किसी विचारधारा या दृष्टि विशेष को सार्वभौम सत्य की तरह अपने विद्यार्थी के गले उतार देना चाहती है। इस दृष्टि से वह लगभग वैसा ही काम कर रही होती है जैसा मध्यकाल में धर्मसत्ता द्वारा नियंत्रित शिक्षा करती थी।
इस दृष्टि से इतिहास की शिक्षा की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो जाती है क्योंकि कोई भी समाज अपने इतिहास के माध्यम से ही अपने को पहचानता है। मैं आज जो कुछ हूँ, वह एक इतिहास का परिणाम है– यह व्यक्ति के बारे में भी सच है और समाज के बारे में भी। हम अपने वर्तमान का क्या करते हैं, यह बड़ी हद तक इस पर निर्भर करता है कि हम अपनी स्मृति की संरचना कैसे करते हैं। इस प्रकार, स्मृति हमारे वर्तमान की भी एक संचालक शक्ति हो जाती है। विभिन्न राजनीतिक-आर्थिक स्वार्थ समाज को अपने-अपने रास्ते ले जाने को प्रयत्नशील रहते हैं, इस कारण उनके लिए यह स्वाभाविक है कि वे हमारी स्मृति की संरचना को अपने-अपने प्रयोजन के अनुरूप ढालने का उद्यम करें। यही कारण है कि इतिहास की शिक्षा– बल्कि इतिहास-लेखन को लेकर हमेशा विवाद बना रहा है।
इतिहास तथ्यों का विवरण मात्र नहीं होता। वह उन तथ्यों की पृष्ठभूमि में सक्रिय नियमों की खोज भी होता है। इसीलिए उसके अध्ययन में एक प्रकार की वैज्ञानिक दृष्टि और प्रविधि की आवश्यकता होती है। मनुष्य के जैविक विकास का भी एक इतिहास है, उसकी और उसकी पृष्ठभूमि में सक्रिय नियमों की खोज हम जीवविज्ञान में करते हैं। लेकिन उसके द्वारा विकसित सामाजिक–आर्थिक-राजनीतिक संरचनाओं एवं ज्ञान-विज्ञान तथा कला-साहित्य आदि प्रवृत्तियों का अध्ययन इतिहास के माध्यम से होता है। इन अर्थों में इतिहासकार भी एक प्रकार का वैज्ञानिक हो जाता है और इसीलिए उससे यह अपेक्षा उचित ही है कि वह अपने इस अध्ययन में एक वैज्ञानिक से अपेक्षित निष्पक्षता का संभव सीमा तक पालन करेगा- ‘संभव सीमा तक’इसलिए कि स्वयं विज्ञान के अनुसार भी पूर्ण निरपेक्षता शायद संभव ही नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि वह जान-बूझकर न तो तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने और छिपाने की कोशिश करेगा और न तथ्यों के चयन में किसी तरह के पूर्वग्रह को हावी होने देगा।
एक वैज्ञानिक तथ्यों से अपनी दृष्टि प्राप्त करता है, न कि दृष्टि के अनुरूप तथ्यों को ढालता है। कार्ल पापर ने तो इसीलिए यहाँ तक कह दिया था कि इतिहास का न तो अपना कोई लक्ष्य होता है, न अर्थ। प्राकृतिक विज्ञान भी हमें नियम तो बताते हैं, पर यह हम पर यानी मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उन नियमों से क्या करता है। लेकिन इसके लिए प्राकृतिक तथ्यों और उनसे प्राप्त नियमों को नहीं बदला जाता। मानवीय इतिहास को भी इसी तरह समझने की जरूरत है। हमारे जीवन का उद्देश्य हम तय करते हैं, इतिहास नहीं– यह बताना भी शिक्षा का एक दायित्व बनता है क्योंकि तभी वह अपने विद्यार्थी को एक स्वतंत्रचेता और विवेकशील व्यक्ति के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी निबाहने में सफल हो सकती है।
विवेक की स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त तथ्यों की पहचान और उनका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। बेकन ने कहा था कि इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, लेकिन वह तभी संभव है जब वह तथ्यों से आँखें न चुराए और न ही अपनी इच्छा के अनुरूप कल्पनाओं को तथ्य समझे या तथ्य की तरह प्रस्तुत करे। आखिर यही तो कारण है कि किसी आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास करनेवाले वैज्ञानिक भी उस सत्ता की अपनी कल्पना को प्रयोगशाला से सिद्ध तथ्य की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करते।
लेकिन तथ्यों की व्याख्या तो बाद की बात है क्योंकि पहले तो उसे तथ्यों की खोज और प्रस्तुति करनी होती है। यह अपने में बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इतिहास के और विशेष तौर पर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित तथ्य इतने अधिक धुँधले और बिखरे हुए हैं कि उन्हें अभी तक ठीक तरह शोधित और प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। भारतीय इतिहास के बारे में तो यह और भी अधिक सच है। ऐसी कई समस्याएँ और सवाल हैं कि उनसे संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी के बगैर अधूरे तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी कहा जाएगा, वह इतिहासकार का मनोवांछित अनुमान ही होगा। जब हमें पूर्ण तथ्य का ही पता नहीं है तो उसे बरामद नियम की प्रामाणिकता तो सदैव संदिग्ध ही रहेगी।
तब क्या यह शिक्षा की दायित्वहीनता नहीं होगी कि वह इतिहास के नाम पर ऐसी व्याख्याएँ विद्यार्थी के दिमाग में आरोपित कर दे जो उसे किसी राज्य यानी व्यवहार में किसी राजनीतिक दल की आकांक्षाओं के अनुरूप आचरण करने के लिए संस्कारित और प्रेरित करे– फिर इस बात से अधिक फर्क नहीं पड़ता कि वह दल वामपंथी है या दक्षिणपंथी क्योंकि दोनों ही स्थितियों में विद्यार्थी की स्मृति को अधूरे तथ्यों और उनके आधार पर किये गये अनुमानों के अनुसार विकृत करने का प्रयास तो किया ही जा रहा होगा। यह प्रयास और भी अधिक भयंकर परिणामकारी होगा यदि इस तरह संरचित स्मृति की प्रेरणा और संस्कार हिंसा के किसी भी प्रकार की ओर उन्मुख हों।
इतिहास यदि एक किस्म का मानव-विज्ञान है तो अपने अध्ययन और अध्यापन में हर स्तर पर वैज्ञानिक दृष्टि और प्रक्रिया को प्रधानता देना उसके लिए अनिवार्य होगा। इसके बिना ज्ञान यानी सत्य को जानने की एक प्रक्रिया के रूप में वह न केवल अपने दायित्व के प्रति गैर-ईमानदार हो रहा होगा बल्कि मानवीय भविष्य के प्रति भी भयंकर खिलवाड़ कर रहा होगा, जिसके लिए उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकेगा। स्पष्ट है कि यहाँ इतिहास से तात्पर्य इतिहासकार या इतिहास-लेखन से है क्योंकि उसके द्वारा लिखा जा रहा इतिहास ही विद्यार्थियों के लिए इतिहास होता है।
इतिहास के उच्च स्तर के अध्ययन में तो फिर भी इस बात की संभावना रहती है कि तथ्यों के अधूरेपन या उनकी विभिन्न व्याख्याओं की ओर ध्यान दिलाया जाता रहे और कुछ हद तक इतिहास लेखन की प्रविधियों से परिचित व्यक्ति के लिए यह संभव हो कि वह उन तथ्यों और व्याख्याओं का परीक्षण अपने स्वतंत्र विवेक की कसौटी पर करता रह सके और नये तथ्यों से परिचित होने पर उनमें संशोधन भी करता रह सके, जैसा कि एक वैज्ञानिक करता है। लेकिन इन प्रविधियों से अपरिचित विद्यार्थी तो जीवन भर के लिए अपने को अनुमानों पर आधारित व्याख्याओं से इस तरह जोड़ लेता है कि भविष्य में नये तथ्यों के स्थापित हो जाने के बावजूद वह उनके लिए अपने दिमाग के दरवाजे उसी तरह बंद रखता है जिस तरह वैज्ञानिक अन्वेषण के बावजूद बहुत-सी बातों के प्रति हम अंधविश्वासी बने रहते हैं। आखिर पत्थर की मूर्ति दूध पी सकती है, इसपर लाखों आधुनिक माने जानेवाले लोगों ने अभी कुछ ही अरसा पहले कितनी आसानी से विश्वास कर लिया था।
विद्यार्थी के दिमाग को खुला रखा जाए, यह शिक्षा की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसलिए उसे इतिहास के अध्यापन में अधूरे तथ्यों और व्याख्याओं को निश्चयात्मकता के साथ प्रस्तुत करने से बचना आवश्यक है।
यह उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध भौतिकीविद् हाइजेनबर्ग के शोध के बाद तो भौतिक विज्ञान भी निश्चयात्मकता में अंध आस्था नहीं रखता जबकि वहाँ तथ्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध नहीं रहती– अनिश्चयात्मकता केवल उन्हें पूरी तरह समझने और व्याख्या के स्तर पर ही रहती है। इतिहास में तो तथ्य भी अधूरे रहते हैं और व्याख्याएँ काफी हद तक अनुमान ही होते हैं। इसीलिए कई उत्तर-संरचनावादी दार्शनिक तो इतिहास में भी कल्पना की वैसी ही भूमिका मानते हैं, जैसी साहित्य या कलाओं में होती है। इसलिए इतिहास के अध्ययन-अध्यापन के समय इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसका कोई भी तथ्य कल्पना से पूरी तरह मुक्त नहीं है और उसकी कोई भी व्याख्या अंततः एक संभावना ही है, अंतिम सत्य नहीं।
इसलिए इतिहास के अध्यापन में विवादास्पद मसलों को प्रस्तुत करते समय इस बात को स्पष्ट कर दिया जाना जरूरी है कि पूर्ण तथ्यों के अभाव में कुछ भी निश्चयात्मकता के साथ नहीं कहा जा सकता। किसी एक पक्ष को निर्विवाद मान्यता देकर हम तथ्यों की अवहेलना कर अनुमानों के आधार पर जातीय स्मृति को विकृत कर रहे होंगे। आखिर विज्ञान भी अपने अनसुलझे सवालों के बारे में विद्यार्थियों को यही तो बताता है कि तत्संबंधी ज्ञान अभी अधूरा है और इस अधूरेपन के कारण वह उस सवाल को अभी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। विद्यार्थी इसे विज्ञान की असफलता के रूप में नहीं बल्कि उसकी प्रामाणिकता के लक्षण के रूप में लेता है और इससे उसकी चिंतन प्रक्रिया की एक प्रकार की वैज्ञानिक दीक्षा भी हो जाती है। यही तरीका इतिहास के अध्यापन में भी अपनाया जाना जरूरी है।
इसका एक सुपरिणाम यह भी होगा कि प्रारंभ से ही बच्चे को सत्य के जटिल स्वरूप का आभास होने लगेगा और वह हर चीज को स्याह-सफेद के खानों में बाँटकर देखने की आदत से छुटकारा पा सकेगा जो उसकी चिंतन प्रक्रिया के वयस्कता की ओर बढ़ने का प्रमाण होगा। लेकिन यह तभी संभव लगता है जब ज्ञान की प्रक्रियाओं की अपना स्वायत्तता को स्वीकार किया जाए और उन्हें राजकीय नियंत्रण के बहाने सत्तारूढ़ दलों की राजनीति का मोहरा न बनाया जाए।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.