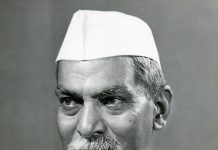(मूर्धन्य समाजवादी चिंतक सच्चिदानन्द सिन्हा ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में आगाह करने के मकसद से एक पुस्तिका काफी पहले लिखी थी। इस पुस्तिका का पहला संस्करण 1985 में छपा था। यों तो इसकी मांग हमेशा बनी रही है, कई संस्करण भी हुए हैं, पर इसकी उपलब्धता या इसका प्रसार जितना होना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम हुआ है। इस कमी को दूर करने में आप भी सहायक हो सकते हैं, बशर्ते आप इसका लिंक अपने अपने दायरे में शेयर करें, या samtamarg.in पर जाकर पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने अपने फेसबुक वॉल पर भी लगाएं। कहने की जरूरत नहीं कि उपभोक्तावादी संस्कृति के बारे में लोगों को सचेत किये बगैर बदलाव की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।)
कृत्रिमता ही जीवन
कृत्रिम शहरी वातावरण में, जो उपभोक्तावादी संस्कृति का परिवेश है, फूलों की गंध, हरियाली, सूरज, चाँद और खुला आकाश मनुष्य के अनुभव और सौंदर्यबोध के दायरे से बाहर चले जाते हैं। इनकी जगह कृत्रिम रूप से प्रकाशित एवं सँवारा गया वातावरण, नकली घास और फूल तथा कृत्रिम सुगंधित द्रव्य पेश किये जाते हैं। कृत्रिम जरूरतों के दबाव में आदमी की स्वाभाविक शारीरिक और मानसिक भूख दब जाती है। फिर तरह-तरह के चटखारों से कृत्रिम भूख जगायी जाती है। चूँकि इस भूख का मनुष्य की प्रकृति से कोई संबंध नहीं होता, इसे किसी भी चीज के लिए किसी भी हद तक उकसाया जा सकता है। शायद इस संस्कृति की अंतिम परिणति उस समाज में होगी, जहाँ जीव विज्ञान की ‘जनेटिक इंजीनियरिंग’ जैसी उपलब्धियों का प्रयोग कर मनुष्य के स्वाभाविक सौंदर्य-बोध को भ्रूणावस्था में ही समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह स्वभावगत सौंदर्य-बोध के नष्ट होने से भोंड़े फैशनों के प्रतिरोध का अंतिम आधार भी खत्म हो जाएगा और तब सुंदर का सीधा अर्थ शक्तिशाली कंपनियों द्वारा निर्मित और प्रचारतंत्र द्वारा प्रसारित प्रसाधन और परिधान का उपभोग करना ही हो जाएगा।
उपभोक्तावादी संस्कृति का यह प्रधान गुण है कि वह अनावश्यक वस्तुओं को मनुष्य के लिए आवश्यक बना देती है और इस तरह मनुष्य की सीमित आवश्यकताओं को सीमाहीन। चूँकि आवश्यकताएँ सीमाहीन बन जाती हैं लोग दिन-रात, सारी जिंदगी एक न एक वस्तु जुटाने में लगे रहते हैं। आदमी पर एक तरह से गुलामी हावी हो जाती है। परंपरागत शोषक समाजों में भी विशिष्टता जाहिर करने के लिए कुछ अनावश्यक वस्तुओं के उपभोग की ओर रुझान था। लेकिन लोगों की वस्तुपरक दृष्टि को नष्ट करने का आज जैसा विज्ञापन और प्रचार का कोई अभियान न होने के कारण इसके प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टि और निषेध भाव भी बना रहता था। अधिकांश परंपरागत धर्मों में अति ठाटबाट या असंतुलित उपभोगवृत्ति को निंदनीय माना जाता था। चूँकि उपभोक्तावादी संस्कृति का आधार व्यावसायिकता है, उसने उपभोग को ही धर्म के रूप में खड़ा कर दिया है और इस तरह उपभोग की वृत्ति बेरोकटोक आगे बढ़ती जाती है।
उपभोक्ता संस्कृति का विकास
अब प्रश्न उठता है कि यह उपभोक्तावादी संस्कृति कैसे विकसित हुई? इस समस्या पर विचार करने पर हम पाएँगे कि यह मूल रूप से पूँजीवादी उत्पादन और वितरण प्रणाली की उपज है। समाज के हर क्षेत्र के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया में पूँजीवादी समाज ने मनुष्य की सहज उपभोगवृत्ति का व्यवसायीकरण कर इस संस्कृति को जन्म दिया है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, शोषण पर आधारित हर समाज में शोषकों में कुछ बे-जरूरत की वस्तुओं के उपभोग की ओर रुझान रहा है, जिससे वे समाज पर अपनी विशिष्टता की धाक जमा सकते थे। लेकिन ऐसा तब होता था जब शोषण या लूट-खसोट से प्राप्त धन से शासकों का वैभव उफनने लगता था और वे अपने अतिरिक्त धन को देश-विदेश से उपलब्ध परंपरागत शान-शौकत की वस्तुओं पर खर्च करते थे। इस प्रक्रिया की शुरुआत शासकों में धन की विपुलता से होती थी और फिर उन वस्तुओं की तलाश होती थी या उन्हें बनवाया जाता था जिनका उपभोग शासकवर्ग को गौरवान्वित कर सके।
पूँजीवादी व्यवस्था में प्रक्रिया बिलकुल उलट हो गयी है। इसमें पहले खर्चीले शोध के जरिए हर रोज नये तरह के उपभोग के सामान ईजाद किये जाते हैं, जिनमें कुछ बिलकुल नयी किस्म के होते हैं और कुछ पुरानी उपभोग की वस्तुओं का स्थान ग्रहण करते हैं। इसके बाद इन्हें प्रचारित कर इनके लिए बाजार पैदा किया जाता है। फिर इस प्रचार से प्रभावित लोग इन्हें प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधन की तलाश करते हैं। इसके लिए अकसर वर्षों के लिए अपना श्रम बंधक रखकर निम्नमध्यम वर्ग और निम्नवर्ग के लोग ‘हायर-परचेज’ के आधार पर सामान खरीद लेते हैं और फिर अपनी आमदनी में से किस्तों में सूद के साथ पैसा भरते रहते हैं। मोटरगाड़ियाँ, फ्रिज, टीवी आदि अकसर इसी तरह मध्यम वर्ग और पश्चिम में मजदूर वर्ग के घरों को सुशोभित करते हैं। इस तरह भविष्य की कमाई गिरवी रखकर भी वस्तुओं की भूख मिटायी जाती है।
वास्तव में मनुष्य स्वयं इन वस्तुओं को लेकर खुद बंधक बन जाता है। वह आजादी के साथ अपने जीवन के विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि उसके सक्रिय जीवन का हर वर्ष पेशगी में उन कंपनियों या बैंकों को दिया जा चुका होता है जिनकी सेवा कर वह खरीदी गयी वस्तुओं का कर्ज चुकाएगा। इस तरह मनुष्य उपभोग की वस्तुओं का बँधुआ मजदूर बन जाता है।
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.