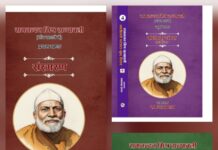— राममनोहर लोहिया —
कभी–कभी मैंने हार के दर्शन या निराशा के कर्तव्य जैसे शब्द इस्तेमाल किये तो मुझसे कहा गया कि निराशा के कर्तव्य पर बोलो। मुझको काफी समय से तीन तरह की निराशा है: एक, राष्ट्रीय निराशा, दूसरी, अंतरराष्ट्रीय निराशा, और तीसरी मानवी निराशा।
सबसे पहले राष्ट्रीय निराशा की बात लीजिए।
पिछले 1,500 बरस में हिंदुस्तान की जनता ने एक बार भी किसी अंदरूनी जालिम के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। यह कोई मामूली चीज नहीं है। इसपर लोगों ने कम ध्यान दिया है। कोई विदेशी हमलावर आए, उस वक्त यहाँ का देशी राज्य मुकाबला करे, वह बात भी अलग है। एक तो राजा अंदरूनी बन चुका है, देश का बन चुका है लेकिन जालिम है उसके खिलाफ जनता का विद्रोह नहीं हुआ यानी ऐसा विद्रोह जिसमें हजारों, लाखों हिस्सा लेते हैं, बगावत करते हैं। कानून तोड़ते हैं, इमारतों वगैरह को तोड़ते हैं या उनपर कब्जा करते हैं, जालिम को गिरफ्तार करते हैं, फाँसी पर लटका देते हैं। ये बातें पिछले 1,500 बरस में हिंदुस्तान में नहीं हुईं।
ऐसी घटनाओं के न होने के कारण और नतीजे एक-दूसरे को मजबूत करते रहे हैं। तफसील में न जाकर, मैं खाली इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान की जनता का आज इस 1,500 बरस के अभ्यास के कारण झुकना उसकी हड्डी और खून का एक अंग बन गया है। इसी झुकने को हमारे देश में बड़ा सुंदर नाम दिया जाता है कि हमारा देश तो बड़ा समन्वयी है, हम सभी अच्छी चीजों को अपने में मिला लिया करते हैं। वास्तव में, समन्वय दो किस्म का होता है। एक दास का समन्वय, और दूसरा, स्वामी का समन्वय। स्वामी या ताकतवर देश या ताकतवर लोग जब समन्वय करते हैं तो परखते हैं कि कौन-सी परायी चीज अच्छी है, उसको किस रूप में अपना लेने से अपनी शक्ति बढ़ेगी और, तब वो अपनाते हैं। नौकर या दास गुलाम परखता नहीं है। उसके सामने जो भी नयी चीज, परायी चीज आती है, अगर वह ताकतवर है तो उसको वह अपना लेता है। वह एक झक मारकर अपनाना हुआ।
अपने देश में पिछले 1,500 बरस से जो समन्वय चला आ रहा है, वह ज्यादा इसी ढंग का है। मैं नहीं कहता कि एकाध ऐसे भी उदाहरण नहीं मिलेंगे जो दूसरे किस्म के हों, लेकिन अधिकतर इसी ढंग का समन्वय हुआ। इसका नतीजा यह होता है कि आदमी अपनी चीज के लिए, स्वतंत्रता भी जिसका एक अंग है, अपनेपन, अपने अस्तित्व, के लिए मरने–मिटने के लिए ज्यादा तैयार नहीं रहता, वह झुक जाता है और उसमें स्थिरता के लिए भी बड़ी इच्छा पैदा हो जाती है। चाहे जितना गरीब हो, चाहे जितना रोगी हो, शरीर चाहे सड़ रहा हो, लेकिन फिर भी जान के लिए कितना जबरदस्त प्रेम आप अपने देश में पाओगे। कोई भी काम करते हुए हमारे लोग घबड़ाते हैं कि जान चली जाएगी। चाहे जितने गरीब हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक-एक, दो-दो कौड़ी से मोह है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आदमी जितना ज्यादा गरीब होता है, उसका उतना ही पैसे के प्रति ज्यादा अनुराग हो जाया करता है। एक विचित्र-सी अवस्था हो गयी है कि शरीर खराब, जेब खराब, लेकिन फिर भी पैसे और जान के लिए इतनी जबरदस्त ममता और अनुराग हो गया है कि आदमी कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं रहता।
जहाँ जोखिम नहीं उठाओगे, वहाँ फिर कुछ नहीं रह जाता है, क्रांति असंभव–सी हो जाती है। मुझको ऐसा लगता है कि अपने देश में क्रांति, असंभव शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, प्रायः असंभव हो गयी है। लोग आधे-मुर्दा हैं, भूखे और रोगी हैं लेकिन संतुष्ट भी हैं। संसार के और देशों में गरीबी के साथ-साथ असंतोष है और दिल में जलन। यहाँ थोड़ी-बहुत जलन इधर-उधर हो तो हो, लेकिन कोई खास मात्रा में जलन या असंतोष नहीं है।
इन सब के कारण ढूँढ़ना इस विषय के अंतर्गत नहीं आता लेकिन एक मोटा-सा कारण और शायद सबसे बड़ा कारण है जाति-प्रथा। यह हमारे देश की एक विशिष्ट बात है, जो दुनिया में कहीं और नहीं। यह भी हमारे देश की एक विशिष्ट बात है कि गुलामी में हम सबसे आगे हैं। मैं नहीं कहता कि इन दोनों विशिष्टताओं का, जाति-प्रथा और गुलामी का एक-दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। मेरी अपनी राय में तो है, ऐसा संबंध है लेकिन उस बहस को अभी छोड़कर खाली जाति-प्रथा के इस गुण-अवगुण को जान लेना जरूरी है कि गैरबराबरी को जाति-प्रथा मंत्र की भी ताकत दे देती है। दूसरे देशों में गैरबराबरी को सिर्फ बंदूक की ताकत मिली रहती है। और देशों में तो गैरबराबरी को शासक लोग कायम रखते हैं ताकत के सहारे या लालच के सहारे। वहाँ की जनता उस गैरबराबरी को स्वीकार लेती है, मानती है इसलिए कि या तो उसकी कुछ आमदनी बढ़ती रहती है या इस कारण से कि उसे डर लगता है कि उसपर ताकत का इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए वह आधा-परदा गैरबराबरी स्वीकारे रहती है और जब वह नहीं स्वीकारती, तो उस गैरबराबरी के खिलाफ बगावत भी कर दिया करती है। लेकिन अपने देश में लालच और बंदूक या हथियार के तरीकों के अलावा मंत्र का तरीका भी है। यानी मंत्र की, शब्द की, दिमागी बात की, धर्म के सूत्र की इतनी जबरदस्त ताकत है कि जो दबा है, गैरबराबर है, आधा-मुर्दा है, छोटी जाति का है, वह खुद अपनी अवस्था में संतोष पा लेता है। ऐसे किस्से हैं जो बतलाते हैं कि किस तरह से जाति-प्रथा ने प्रायः पूरी जनता को, प्रायः 43 करोड़ को, यह संतोष दे दिया है।
मैं समझता हूँ, हिंदुस्तान में सचमुच दिलजला आदमी पाना मुश्किल है, जैसा कि यूरोप में होता है। यूरोप में तो आदमी अकड़ जाता है। अंदरूनी जुल्म के खिलाफ उस तरह का उखड़ा हुआ आदमी यहाँ पाना मुश्किल है। मैं इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि बाहरी जुल्म के खिलाफ तो हमारे यहाँ भी उखड़े हुए आदमी रहे हैं। लेकिन अंदरूनी जुल्म के खिलाफ नहीं। किसी एक उपन्यासकार का मैंने एक वाक्य पढ़ा है। वैसे यह सही है कि उपन्यासकार विद्वान नहीं हुआ करते या जरूरी नहीं कि वे विद्वान हों, लेकिन कभी-कभी वे बिना ज्ञान के या विद्या के चीजों को पकड़ लेते हैं। उसने कहा हिंदुस्तान में तो क्रांति असंभव है, क्योंकि और जगहों पर जहाँ क्रांति होती है वहाँ गैरबराबरी सापेक्ष होती है, यानी बिल्कुल संपूर्ण गैरबराबरी नहीं होती, और जिस देश में बिल्कुल बराबरी हो जाए या संपूर्ण गैरबराबरी हो जाए तो वहाँ इंकलाब नहीं होगा। जिस देश में गैरबराबरी की खाई बिल्कुल गहरी हो जाए, दिमागों में घर कर ले, समाज के गठन में भी हो जाए, प्रायः संपूर्ण गैरबराबरी, तो वहाँ की जनता क्रांति के लिए बिल्कुल नाकाबिल हो जाती है।
हिंदुस्तान में वह अवस्था हो गयी है। मैं कुछ और ज्यादा ठोस शब्दों में कहूँ। एक तरफ आर्थिक गैरबराबरी और दूसरी तरफ समाज की या मंत्र की गैरबराबरी ने मिलकर यह अवस्था पैदा कर दी है कि साधारण जनता, बहुसंख्यक जनता के दिमाग में वह उखड़ापन नहीं रह गया है। उसमें संतोष आ गया है और क्रांति की संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। यह है राष्ट्रीय निराशा। साल, दो साल, दस साल, बीस साल, पचास साल की बात नहीं, यह किसी एक कांग्रेसी नेता या महात्मा गांधी या और किसी की भी बात नहीं, यह है पिछले 1500 बरस की बात। यह कूड़ा बहुत दिनों का जमा हुआ है या दिमाग पर एक विशेष प्रकार का जंग चढ़ा हुआ है और वह भी बड़ा पुराना है, कोई 1500 बरस का। यह कोई मामूली निराशा की चीज नहीं हुई।
(23 जून 1962 को नैनीताल में समाजवादी युवजन सभा के शिविर में दिया गया भाषण)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.