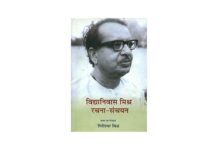— किशन पटनायक —
(यह लेख अप्रैल 1996 में लिखा गया था)
चुनाव के अध्ययन का एक शास्त्र बना हुआ है। मतदान का आकार-प्रकार किस तरह बदल रहा है, विभिन्न इलाकों में राजनीतिक दलों का जन-समर्थन कैसे घट-बढ़ रहा है, आगे के नतीजे क्या हो सकते हैं- इन सारी बातों का अध्ययन इस शास्त्र के तहत हो रहा है।
जिन बातों का पर्याप्त अध्ययन नहीं हो रहा है वह भी एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। क्या सोचकर लोग वोट दे रहे हैं? मतदाताओं के स्तर पर निर्णय कैसे होता है? प्रचार, प्रलोभन और दबाव से मतदाता का निर्णय कितना और कैसे प्रभावित होता है? आदर्शवादी, सुधारवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ तक चुनाव के निर्णयों को प्रभावित करते हैं? क्या चुनाव कभी एक बेहतर समाज-व्यवस्था बनाने का माध्यम हो सकता है? इस उद्देश्य के लिए चुनाव के तरीकों और राजनीति में क्या परिवर्तन करने होंगे?
इन सवालों का जवाब विशेषज्ञ ही दे पाएंगे- जब वे उपर्युक्त प्रश्नों को अपने शास्त्र यानी अनुसंधान का विषय बनाएंगे। चुनाव अध्ययन को अधिक गहरा और व्यापक बनाना होगा।
चुनाव राजनीतिक सत्ता हासिल करने का एक सभ्य तरीका है। राजनीतिक सत्ता हासिल करने का अधिकारी कौन है? जनसाधारण का मत उसे कैसे मिल जाता है? किसको मिलना चाहिए? इन सवालों पर ज्यादा चर्चा होती है;कैसे मिलता है इसका विश्लेषण कम होता है। कभी-कभी एक बात उठती है कि अच्छे लोगों को यानी ‘सज्जनों’ को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करना चाहिए। यह देखा गया है कि अकसर ‘सज्जन’ लोग ‘राजनीति’ से अपने को दूर रखना चाहते हैं और यह भी देखा गया है कि सज्जन लोग प्रभावशाली दलों का टिकट पाने के लिए आतुर रहते हैं। वोट, राजनीति और सज्जनों के संपर्क का प्रश्न शायद भारतीय पाखंड का एक विशेष प्रसंग है। एक तबलावादक को उम्मीदवार बनाना और एक सज्जन को उम्मीदवार बनाना एक जैसी बात है। तबलावादक को लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनाने से देश की राजनीति को कोई फायदा नहीं होगा लेकिन उस आदमी के तबलावादन का स्तर घट सकता है। उसी तरह किसी सज्जन को लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनाने से भी राजनीति को फायदा नहीं होनेवाला है लेकिन उस बेचारे की सज्जनता का स्तर अवश्य घट सकता है।
हरेक कार्यक्षेत्र का अपना चारित्रिक अनुशासन होता है। उससे कार्य अच्छा होता है और उस कार्य से समाज को ज्यादा फायदा होता है। सज्जनता के कुछ सामान्य गुण होते हैं जो सबके लिए जरूरी होते हैं, मगर कार्यक्षेत्र के हिसाब से कुछ विशेष अच्छाई भी चाहिए। कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो एक कार्य के लिए अधिक जरूरी होते हैं तो दूसरे के लिए कम जरूरी। इसी प्रकार कुछ प्रवृत्तियाँ एक क्षेत्र में ज्यादा दोषपूर्ण मानी जाएंगी, एक में नहीं। एक पहलवान या धर्मोपदेशक के लिए शराबी होना खतरनाक है, जबकि एक कलाकार के लिए यह दोष क्षम्य भी हो सकता है।
सज्जनों को वोट देना है- सामान्य मतदाताओं ने कभी भी इस उपदेश को गंभीरता से नहीं लिया है। मतदान राजनीतिक सामर्थ्य के लिए ही किया जाता रहा है। लेकिन राजनीतिक सामर्थ्य क्या है, संसद सदस्यों और विधायकों से किस प्रकार के काम की अपेक्षा होनी चाहिए, दलों से क्या उम्मीद की जानी चाहिए- इसका प्रशिक्षण नहीं के बराबर है, इसकी कोई संस्कृति विकसित नहीं हुई है; जो थोड़ी-बहुत राजनैतिक संस्कृति बन पायी थी उसका भी क्षय हुआ है। फिर भी मतदाता का एक अपना निर्णय होता है। प्रचार-प्रलोभन-दबाव से घिरे हुए मतदाता जिस प्रकार मतदान करते रहे हैं उससे यह प्रतीत होता है कि मतदाता नियंत्रित भी हैं और स्वेच्छा से भी मतदान करते हैं, लेकिन प्रचलित राजनीति के अंदर मोटेतौर पर जो विकल्प दिखायी देते हैं- उन्हीं में से चुनते हैं। चुनते समय भारतीय मतदाता व्यक्ति के तौर पर तथा सामूहिक तौर पर अपनी स्वतंत्रता का प्रमाण देता आया है।
इस बात को दुबारा कहने की जरूरत है। चुनाव में उम्मीदवार बदल सकते हैं, नये व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, नये नाम के नये राजनीतिक दल भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो राजनीति पहले से किसी इलाके या राष्ट्र में प्रचलित रहती है, उस राजनीति से जो राजनीतिक चेतना बनी हुई रहती है, उसी राजनीतिक चेतना के तहत ही चुनाव होता है। चुनाव के दरमियान नयी राजनीतिक चेतना पैदा नहीं होती। मुख्य प्रतिद्वंद्वंदी पहले से तय रहते हैं। प्रचार-प्रलोभन-दबाव के तरीकों से एक सीमित दायरे में घट-बढ़ होती है। इस घट-बढ़ के होने न होने में मतदाताओं का अपना निर्णय महत्त्वपूर्ण होता है। उससे अधिक की अपेक्षा हम नहीं कर सकते।
इसलिए सर्वोदयी, कुलदीप नैयर, मेधा पाटकर जैसे समूह अगर चाहते हैं कि चुनाव पर अपना असर डालें, तो यह संभव नहीं है क्योंकि चुनाव के पहले उनकी कोई स्पष्ट राजनीति नहीं रही। चुनाव में राजनीति का ही परिणाम निकलता है, सज्जनों की दखलंदाजी का नहीं। सज्जनों को चाहिए कि वे पहले राजनीति में हस्तक्षेप करें और उसके बाद ही चुनाव में। सज्जन वे हैं, जो देश की वर्तमान हालत से चिंतित हैं और सोचते हैं कि चुनावों के भ्रष्ट तरीकों के कारण देश को सही नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है।
जो लोग चुनाव को मौलिक ढंग से या किसी एक खास दिशा में प्रभावित करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वे चुनाव के काफी पहले से राजनीति को प्रभावित करने का या खुद राजनीति में सक्रिय होने का तरीका अपनाएं।
लोकतांत्रिक राजनीति का अभी तक जो अनुभव है उससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों में पूँजीवादी समूह अत्यंत कारगर ढंग से राजनीति पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। चुनाव के मौसम में ये लोग बहुत ज्यादा परेशान या सक्रिय नहीं रहते। उनका संबंध राजनीति से रहता है, चुनाव से नहीं। राजनीति को वे नियंत्रित कर लेते हैं तो निश्चिन्त होकर चुनाव का काम जनसाधारण पर छोड़ देते हैं। अमरीका और पश्चिम यूरोप इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। वहाँ की राजनीति दो दलों के बीच इस कदर विभाजित हो गयी है कि तीसरे दल की बात तो दूर, उसकी जगह भी नहीं दिखायी पड़ती। दोनों दल धनी वर्गों के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित हैं। शुरू में ऐसा नहीं था।
1950 के दशक तक यूरोप के श्रमिक दलों तथा सामाजिक लोकतांत्रिक (सोशल डेमोक्रेट) कहलानेवाले दलों ने समाजवाद की राजनीति को एक शक्ति के रूप में खड़ा किया था। अमरीका में भी राष्ट्रपति पद के लिए एक लोकतांत्रिक समाजवादी उम्मीदवार खड़ा होता था। वह हारता था लेकिन चुनाव लड़ता था। राजनीति में उसका महत्त्व होता था। बाद के दिनों में पूँजीवाद का राजनीति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाने पर अब समाजवाद के नाम पर अमरीका में कोई राजनीति नहीं हो सकती। यूरोप के समाजवादियों द्वारा पूँजीवादी व्यवस्था को स्वीकार कर लेने के बाद वहाँ का लोकतंत्र सफल हो गया है।
हमारे पढ़े-लिखे लोगों को सफल लोकतंत्र का मॉडल द्विदलीय व्यवस्था में दिखायी देता है- जहाँ समूची राजनीति दो दलों के बीच सीमित रहती है। ब्रिटेन का श्रमिक दल जब से पूँजीवाद का समर्थक हो गया है तब से वहाँ की लिबरल पार्टी की भूमिका खतम सी हो गयी है और इसी तरह की द्विदलीय राजनीति चलती है। इस व्यवस्था में दोनों दलों का चरित्र और विचार एक जैसा होता है- जीत-हार होती है या फिर बारी बदलने के लिए विपक्ष को जिता दिया जाता है। कुछ विचारकों की राय है कि इस व्यवस्था में नागरिक को असहमति का अधिकार नहीं रह जाता है। उसका मतलब हम यह निकाल सकते हैं कि जब एक तीसरी राजनैतिक शक्ति अमरीका या ब्रिटेन में पैदा होगी तभी वहाँ के नागरिकों के लिए असहमति का अधिकार अर्थपूर्ण होगा।
भारत की राजनीति अभी तक दो-दलीय व्यवस्था में जकड़ी नहीं गयी है। मुख्य दलों की मजबूती घटी है। चुनाव दलों के बीच नहीं, मोर्चों के बीच प्रतिद्वंद्विता का रूप लेने लगा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, भाजपा और उसके सहयोगी दल, जनता, कम्युनिस्ट और उनके सहयोगी दल- तीन मोर्चे प्रमुख हैं। इनसे भी राजनीति पूरी नहीं होती है। इनमें सो कोई भी मोर्चा स्पष्ट बहुमत नहीं पा सकता। अस्थिरता अंतर्निहित है। इसलिए विश्वविद्यालयों की किताबों के अनुसार यह सफल लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। अस्थिरता से अराजकता पैदा हो सकती है। किंतु आशावादी विचारक कहेगा कि एक नयी राजनैतिक शक्ति पैदा हो सकती है।
ऐसी हालत में भारत का मतदाता अमरीका के नागरिक की तुलना में ज्यादा स्वाधीन है, उसके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। यानी भारत का मतदान कम नियंत्रित है। संभवतः इसी कारण (यानी नियंत्रण को पूरा करने के लिए) भारत के चुनाव में हिंसा या माफिया तत्त्व की भूमिका बढ़ती जा रही है। मतदाता को घूस देने और धमकी देने के तरीकों पर पाबंदी लग जाए तो भारतीय मतदाता की आजादी सचमुच बहुत बढ़ जाएगी।
दूसरी ओर राजनीति पर यानी प्रमुख राजनैतिक दलों पर धनी वर्ग का नियंत्रण इतना बढ़ता जा रहा है कि प्रमुख मोर्चों के बीच चरित्र और विचार की कोई विशेष भिन्नता परिलक्षित नहीं होती। मूल आर्थिक नीति सबकी समान है। वैचारिक भिन्नता या कार्यक्रम की भिन्नता सिर्फ क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर या जाति और संप्रदाय की बातों को लेकर रह गयी है। इस अर्थ में भारत की तुलना विकसित पूँजीवादी देशों से की जा सकती है- कि यहाँ भी सभी प्रमुख राजनीतिक दल पूँजीवाद द्वारा नियंत्रित हो गये हैं। कम्युनिस्ट और समाजवादी भी निजीकरण तथा विदेशी पूँजी के समर्थक हो चुके हैं। चुनाव में किसी भी मोर्चे के घोषणापत्र में धनी वर्ग के शोषण के प्रतिकार का वायदा नहीं होता। इसका अर्थ है कि किसी की सरकार हो, आर्थिक विषमताएँ बढ़ेंगी।
(जारी)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.