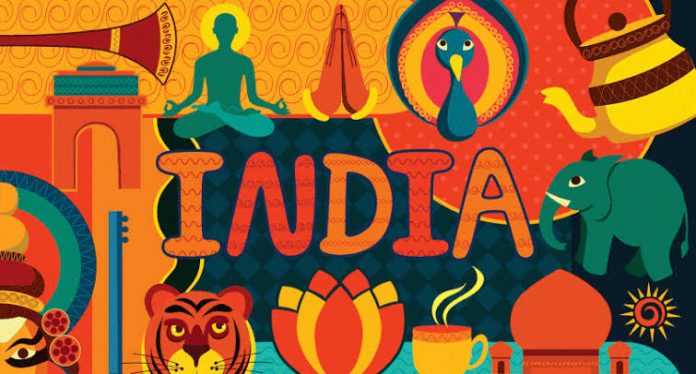—योगेन्द्र यादव —
क्या हम अब भी गुलाम हैं? साल जब हौले-हौले आजादी की 75वीं वर्षगांठ की तरफ कदम बढ़ा रहा है तो हमें अपने से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि : क्या विचारों के मामले में हमने स्वराज हासिल कर लिया है? अपना तेज और ताप गॅंवा चुके ‘ख़ान मार्केट के अभिजनों’ की आक्रामक प्रश्न-परीक्षा ने इस सवाल को एक नया संदर्भ दिया है, एक ऐसे सवाल में तब्दील किया है जिसका जवाब फौरी तौर पर देना जरूरी है।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, राजनीतिक सिद्धांतकार प्रोफेसर सुदीप्त कविराज का हाल का एक व्याख्यान सीधे-सीधे इन्हीं सवालों पर केंद्रित था। व्याख्यान का शीर्षक था ‘एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द सेल्फ ’ और व्याख्यान का आयोजन अग्रणी समाजशास्त्री प्रोफेसर पार्थ मुखर्जी की स्मृति में किया गया था जो पिछले साल दिवंगत हुए।
अमूमन, प्रोफेसर कविराज सरीखे मार्क्सवादी धारा के विद्वान से आप ऐसे सवालों पर सोच-विचार की उम्मीद नहीं लगाते। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का मसला उठानेवाले लोगों को मार्क्सवादी खारिज करने के भाव से देखते हैं। प्रोफेसर कविराज ने अपने व्याख्यान में जो कुछ कहा उस पर, उनका एक पूर्व-छात्र होने के नाते, मुझे जरा भी आश्चर्य न हुआ।
कार्ल मार्क्स के विचार और भारतीय राजनीति को समझने में इसकी उपादेयता के प्रश्न से अपने बौद्धिक जीवन की शुरुआत करनेवाले प्रोफेसर कविराज ने हमेशा मार्क्सवादी रूढ़ियों से अपने को दूर रखा है और मार्क्सवादी विचारधारा की यूरो-केंद्रिक मान्यताओं पर सवाल उठाये हैं, स्वयं कार्ल मार्क्स भी प्रोफेसर कविराज की ऐसी प्रश्न-परीक्षा के दायरे में रहे हैं। बीते कुछ वक्त से प्रोफेसर कविराज ने संस्कृति और विचारों के इतिहास को अपने अध्ययन का विषय बनाया है जिसमें महाभारत तथा बंगाल की वैष्णव-परंपरा पर चिंतन-मनन भी शामिल है।
ज्यादातर वामपंथियों के विपरीत प्रोफेसर कविराज ने व्याख्यान में इस बात को बड़े स्पष्ट और मुखर रूप से स्वीकार किया कि हम लोग राजनीतिक उपनिवेशवाद की जकड़ से भले ही बाहर निकल आए हों और आर्थिक उपनिवेशवाद की समस्या के समाधान के भी उपाय किये हैं लेकिन सांस्कृतिक और बौद्धिक उपनिवेशवाद की जकड़ में हम अब भी हैं।
प्रोफेसर कविराज के शब्दों में कहें तो हमारा ‘आत्म’ एक उपनिवेशित आत्म है और यह आत्म अपना अध्ययन यों कर रहा हो जैसे कि कोई किसी पराये और अनजाने का करता है। हम अपने समाज के बारे में विचार-विश्लेषण की जिन कोटियों के सहारे सोचते हैं वे हमारे समाज से नितांत अलग किस्म के समाज को समझने-विचारने के लिए बने। और हम, अंग्रेजी भाषा में सोचते हैं यानी एक ऐसी भाषा में जो इस देश के आमजन की भाषा नहीं है जबकि हम इस अंग्रेजी से उन्हीं आमजनों के बारे में सूत्रीकरण करते और सिद्धांत रचते हैं।
इन सब बातों के साथ एक बात यह भी है कि पश्चिम के अकादमिक जगत का सांस्थानिक तौर पर प्रभुत्व बना हुआ है और यह प्रभुत्व ज्ञान के मामले में जो एक ‘बड़ी दीदी-छोटी दीदी’ जैसा ऊॅंच-नीच बना हुआ है उसके अंतरालों को पाटने का काम किया करता है।
नया वक्त और पुराना सवाल
व्याख्यान में प्रोफेसर कविराज ने जो सवाल उठाये वे कम से कम दो सौ साल पुराने हैं। औपनिवेशिक विश्वदृष्टि को चुनौती देना भूदेव मुखोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद तथा बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय सरीखे 19वीं सदी के भारतीय चिंतकों का एक प्रमुख सरोकार रहा। औपनिवेशिक विश्वदृष्टि से बाहर निकलने का सवाल तकरीबन तमाम राष्ट्रवादी चिंतकों, खासकर महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो तथा मौलाना आजाद के लिए बहुत अहम रहा। एक मायने में देखें तो गांधी का ‘हिन्द स्वराज’ इसी सवाल से टकराने का एक उद्यम था। के.सी. भट्टाचार्य का मौलिक निबंध ‘स्वराज इन आयडियाज’ ऐसे राष्ट्रवादी सरोकारों का ही एक आईना है।
आजादी के बाद के दौर में, सांस्कृतिक तौर पर स्वायत्त होने के सरोकार जैसे ही मंद पड़े, भारत में सोच-विचार की दुनिया में पश्चिमी रंग-ढंग और इसी नाते एक नकलची बुद्धिजीवी-जगत का आकार बड़ी तेजी से बढ़ा। हालांकि, ऐसे दौर में भी राममनोहर लोहिया, किशन पटनायक, निर्मल वर्मा, रमेशचंद्र शाह और धर्मपाल सरीखे चिंतकों ने सांस्कृतिक आजादी के सवाल को जिंदा रखने के उद्यम किये।
आशीष नंदी की किताब ‘इंटीमेट एनिमी’ (1983) ने इस सवाल पर बौद्धिक जगत में छायी चुप्पी को तोड़ने में मदद की। इसी वक्त पश्चिमी बौद्धिक जगत के सरोकारों में भी एक खास बदलाव आता है, एडवर्ड सईद के ओरियंटलिज्म के प्रकाशन के साथ पश्चिमी बौद्धिक जगत में एक चलन यह निकल पड़ता है कि पूरब के बाशिंदों और पूरब की दुनिया को अब तक अगर पश्चिम के जगतजेताओं ने ज्ञान के अपने ही आईने में उतारकर उनकी छवि उकेर रखी है तो अब ऐसे आईने को तोड़ा जाए और पूरब के बारे में बनायी छवियों की सच्चाई के बारे में सवाल उठाये जाएं। इस बिंदु के बाद से उत्तर-औपनिवेशिक ज्ञान-कांड की रचना एक बार फिर से पश्चिमी जगत के बौद्धिकों की अगुवाई में चलती है और आज औपनिवेशिक सांस्कृतिक प्रभुत्व की आलोचना-प्रत्यालोचना की मुख्यधारा के रूप में स्थापित है।
हम बौद्धिक वि-उपनिवेशीकरण की आज की इस चुनौती से कैसे निपटें? हाल में ऐसी दो पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है जिसमें इस सवाल पर सोच-विचार और समाधान का उपक्रम दिखता है। हॉं, यहॉं यह कह देना भी उचित होगा कि इन दो पुस्तकों का प्रकाशन विचारधारा के लिहाज से आपस में एकदम विपरीत पड़नेवाले छोरों से हुआ है। दोनों ही पुस्तकों में प्रोफेसर कविराज की इस चिंता से सहमति दिखती है कि भारत के मायने-मतलब तलाशने का हमारा आज का जो बौद्धिक चलन है वह बड़ी हद तक यूरो-केंद्रिक है और सोच-विचार के ऐसे ढर्रे की मरम्मती की बड़ी सख्त जरूरत है।
दोनों ही पुस्तकों में इस बात पर सहमति दिखती है कि उत्तर-औपनिवेशिक ज्ञानकांड का जो दखल अभी हम देख रहे हैं वह भारत को विचारों का स्वराज उपलब्ध कराने के अर्थ में अपर्याप्त है और इस नाते दोनों ही पुस्तकों में हमारी ज्ञान-रचना के चौखटे को उपनिवेश-बद्धता की जकड़ से मुक्त करने की जरूरत बतायी गयी है। लेकिन, दोनों पुस्तकें एक खास मायने में एक-दूसरे से भिन्न हैं—इस प्रश्न पर कि बौद्धिक रूप से उपनिवेशीकृत होने का मतलब क्या होता है, दोनों पुस्तकों की दृष्टि बुनियादी तौर पर एक-दूसरे से भिन्न है।
स्वदेशी चेतना की खोज
जिन दो पुस्तकों का ऊपर जिक्र आया है उनमें एक का नाम है इंडिया दैट इज भारत : कोलोनियिलिटी, सिविलाइजेशन, कंस्टीट्यूशन (ब्लूमस्बरी इंडिया, 2021)। इस किताब के लेखक इंजीनियरिंग के पेशे से वकालत के पेशे में आए जे. साई दीपक हैं। यों, जे. साई. दीपक ‘हिन्दू राष्ट्रवाद’ के विचार को खारिज करते हैं और भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ से खुद को दूर छिटकाते हुए दीखते हैं लेकिन उनकी पुस्तक इस राजनीतिक खेमे (बीजेपी-आरएसएस) के लिए एक गहरी बौद्धिक बुनियाद गढ़ने का काम करती है।
उनके तर्क का लब्बोलुआब यह है कि भारतीय समाज और इसका अतीत तथा वर्तमान (जिसमें जाति-जनजाति जैसी अवधारणाऍं भी शामिल हैं) के बारे में जो भी आधुनिक ज्ञान मौजूद है वह औपनिवेशिक ज्ञान-कांड से प्रभावित और प्रेरित है। इसी समझ ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के संस्थागत ढॉंचे को आकार दिया है, जिसमें राष्ट्र-राज्य सरीखा विचार भी शामिल है।
भारत के अतीत और वर्तमान को लेकर जे. साई दीपक का यह पाठ बेशक सही है लेकिन नया कत्तई नहीं और ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि हमेशा याद रखा जाए और बारंबार दोहराया जाए। जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया है—पश्चिमी बौद्धिक जगत से भारत के बारे में पिछले तीन दशक से जो समाज-सिद्धांत निकलकर सामने आए हैं, उनका जोर भी वैसी ही बातों पर है जिसकी पैरोकारी जे. साई दीपक कर रहे हैं।
लेकिन उपनिवेशवाद की बौद्धिक जकड़ की व्याख्या के मामले में जे. साई दीपक इसके अन्य व्याख्याकारों से एक अहम अर्थ में भिन्न हैं। जे साई दीपक का जोर इस बात पर है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद नाम का घोड़ा मुख्य रूप से ईसाई राजनीतिक धर्मशास्त्र की ताकत और समझ की चाबुक से हॉंका जा रहा था और हॉं, ब्रिटिश उपनिवेशवाद से पहले एक उपनिवेशवाद और था जिसका नाम ‘मध्यपूर्वी उपनिवेशवाद’ है।
सो, जे. साई दीपक के मुताबिक बौद्धिक उपनिवेशवाद की जकड़ से निकलने का मतलब है उपनिवेशवाद की दोहरी जकड़बंदी से बाहर निकलना। इस दोहरी जकड़बंदी से निकलने के बाद ही स्वदेशी भारतीय चेतना की उपलब्धि होगी जो कि समूहगत अस्मिताओं के रूप में सुरक्षित-संरक्षित है। ऐसा करने के लिए जरूरी होगा कि हम भारत को सभ्यतागत-राजसत्ता (सिविलाइजेशन-स्टेट) मानें ना कि राष्ट्र-राज्य (नेशन-स्टेट) और इसी के अनुरूप अपने विधिक-संवैधानिक ढॉंचे को सभ्यतागत चेतना के मेल में ले आएं।
जे. साई दीपक की इन बातों को सीधी-सरल हिंदी में कहें तो वह यों होगा : अंग्रेजों और मुसलमानों की दोहरी दासता से उबरने के लिए हमें एक सच्ची और प्रामाणिक हिंदू विश्वदृष्टि को फिर से हासिल करना होगा और ऐसी विश्वदृष्टि से ही अपने संविधान का पुनर्लेखन करना होगा।
वि-उपनिवेशकरण की इस व्याख्या से मुझे समस्या इतनी भर नहीं कि मैं इसके राजनीतिक निहितार्थों को समझते हुए हरचंद इस व्याख्या के खिलाफ हूॅं बल्कि मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि ऐसी व्याख्याएं दरअसल उपजती ही एक ऐसे दिमाग में हैं जो बुरी तरह औपनिवेशिक दासता में जकड़ा हो।
गौर करें कि जे साई दीपक ने ‘मध्य-पूर्व’ शब्द का इस्तेमाल किया है और सोचिए कि क्या कोई और शब्द इससे भी ज्यादा औपनिवेशिक दासता से ग्रस्त हो सकता है भला?’ प्रश्न कीजिए कि मध्य-पूर्व में जो ‘पूर्व’ शब्द आया है वह कहॉं खड़े होकर देखने पर ‘पूर्व’ दिखता है, वह किनकी नजरों में ‘पूरब’ है और जो ‘मध्य’ शब्द आया है वह किसका मध्य है?
इसी तरह जे साई दीपक की यह मान्यता भी दिक्कत-तलब है कि काल-विभाजन की एक सुस्पष्ट रेखा खींची जा सकती है और इस रेखा को आधार मानते हुए कहा जा सकता है कि इस रेखा के पार जाते ही औपनिवेशिक दासता शुरू होती है और इस पार रहते हुए कहा जा सकता कि हॉं, विदेशी आक्रांताओं से मुक्त शुद्ध स्वदेशी भारतीय चेतना का समय यहॉं तक विस्तृत है। यह मान्यता भी औपनिवेशिक इतिहास-लेखन और औपनिवेशिक ज्ञान-कांड की ही देन है। और, यह कमाल तो खैर औपनिवेशिक दासता से बुरी तरह जकड़ा कोई दिमाग ही दिखा सकता है कि वह हमारे अपने वक्त की सभ्यतागत चेतना को परिभाषित करने में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की किसी भी भूमिका से इनकार करके चले।
मैंने जे. साई दीपक की पुस्तक को इस सोच से पढ़ने के लिए उठाया था कि चलो, बीजेपी/आरएसएस के खेमे से कोई ऐसा तो आया जिसके साथ पर्याप्त गंभीरता से बौद्धिक मुठभेड़ की जा सकती है। लेकिन, सच कहूॅं, तो मुझे निराशा हाथ लगी। बेशक जे साई दीपक चतुर हैं लेकिन वि-औपनिवेशिकता (डिकोलोनियलिटी) के किसी भी वैकल्पिक सूत्रीकरण से पर्याप्त गंभीरता के साथ मुठभेड़ कर पाने में वे असमर्थ हैं।
मेरे मन में आया कि काश! साई दीपक विऔपनिवेशिकता की अपनी परियोजना की शुरुआत करने से पहले थोड़ी जानकारी और इकट्ठी कर लेते, जरा टोह-टटोल लेते कि भारत में इस मुद्दे पर जो बहसें चली हैं उनमें क्या-क्या कहा गया है।
जे. साई दीपक की किताब की एक बेढंगी बात यह भी है कि वह लिखी तो गयी है विउपनिवेशीकरण के मुद्दे पर लेकिन उसमें गांधी के ‘हिन्द-स्वराज’, लोहिया के ‘मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म’ या आशीष नंदी के इंटीमेट एनिमी का कहीं जिक्र ही नहीं है। सुनते हैं कि जे साई दीपक इस किताब को तीन खंडों में लिखनेवाले हैं और उन्होंने अपने त्रिपिटक का यह पहला ही पिटारा खोला है तो फिर उम्मीद करें कि पहली किताब की रचना में जो कोने-अंतरे वे देखने-खंगालने से चूक गये उन पर अपनी अगली दो किताबों में वे जरूर रोशनी डालेंगे। जहॉं तक उनकी इस पहली किताब का सवाल है, वह यह सिखाने में कामयाब किताब मानी जाएगी कि अपना वि-उपनिवेशीकरण किस तरह न करें।
परंपराओं से संवाद
विचाराधाराई जमीन पर जे साई दीपक के एकदम उलट पड़ती दिशा में खड़े आदित्य निगम की किताब डिकोलोनाइजिंग थियरी : थिकिंग एक्रॉस ट्रेडिशन्स (ब्लूम्सबरी इंडिया, 2020) विषय के अपने निरूपण में कहीं ज्यादा गझिन और महीन है और अपने स्वर को किसी भी बड़बोलेपन से सचेत रूप से बचाते हुए वि-उपनिवेशीकरण का एक वैकल्पिक प्रस्ताव करती है।
प्रोफेसर कविराज की भांति आदित्य निगम भी मार्क्सवादी चिंतन-परंपरा की उस धारा के हैं जिसने अपने को मार्क्सवादी रूढ़ियों से मुक्त रखा। आदित्य निगम यूरो-केंद्रिकता की आलोचना में अपनी ऊर्जा का क्षय नहीं करते क्योंकि यह काम तो पर्याप्त हो रखा है। किताब में आदित्य निगम का ध्यान इस बात पर है कि अपने सैद्धांतिक औजारों का हम विउपनिवेशीकरण कैसे करें।
आदित्य निगम की किताब जे साई दीपक की किताब से पहले छपी लेकिन उसमें जे साई दीपक की किताब में उठाये गये तर्कों का पूर्वानुमान है और इसलिए ऐसे तर्कों का उत्तर भी मौजूद है। निगम ने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी किताब में तर्क दिया है कि किसी शुद्ध, सोलहो टंच खरे स्वदेशी परिप्रेक्ष्य की खोज एक छलावा है। हमारे पास सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत-सूत्रीकरण के विकसित स्वदेशी उपकरण नहीं हैं और न ही हमारे वर्तमान को गढ़नेवाली आधुनिकता से ही हम हाथ झटकने के अंदाज में पीछा छुड़ा सकते हैं।
आदित्य निगम का प्रस्ताव कहीं ज्यादा ठोस और मजबूत है। हमें अगर सिद्धांत-रचना की दुनिया में विउपनिवेशीकरण की शुरुआत करनी है तो यह शुरुआत अपने `आज` और `अब` से करनी होगी। जो पाश्चात्य सामाजिक सिद्धांत हमें विरासत से हासिल हैं उनकी विरचना और पुनर्रचना को हमें अपना प्रस्थान बिंदु बनाना चाहिए। इस काम के सहायक उद्यम के रूप में हमें उन उत्तर-औपनिवेशिक समाजों से भी सीखना होगा जिनका अनुभव हमारे अनुभवों से मिलता-जुलता रहा है। इसके साथ ही हमें अपनी निज की अवधारणाएं गढ़नी होंगी।
मिसाल के लिए, निगम ने पौराणिक विचार-परंपरा और सादृश्य आधुनिकता (पैरा-मॉडर्न) जैसी अवधारणाओं को एक पुनर्रचना के तौर पर अपनी किताब में प्रस्तुत किया है। ऐसी अवधारणाएं हमारे समय की सच्चाइयों के कहीं ज्यादा अनुकूल पड़ती हैं। बहुविध परंपराओं से संवाद से उनका यही आशय है।
मुझे सबसे ज्यादा पसंद आयी वह बात जो चलते-चिट्ठे कही गयी है और किताब के एकदम आखिर के हिस्से में कही गयी है, कि : ‘तो, फिर हम अपने सवाल कैसे गढ़ें और उनके समाधान के लिए कैसे बढ़ें, यह सवाल मुझे सबसे महत्त्वपूर्ण जान पड़ता है।’ मेरी दिली ख्वाहिश है कि इन पंक्तियों में जो मूलगामी किस्म का सुझाव पेवस्त है, लेखक उस दिशा में प्रयत्नशील हों। एक ऐसी भी स्थिति होती है कि सिद्धांत गढ़न के मोर्चे पर बात हिल-डुल करके फिर से उसी जाम में फॅंस जा रही हो लेकिन ऐसे मौके पर व्यावहारिक समस्या-समाधान से राह निकल आती है।
निगम की किताब का पाठ कुछ यों करें तो फिर नजर आएगा कि वि-उपनिवेशीकरण की चुनौती दरअसल प्रदत्त और उपनिवेशीकृत सिद्धांतों के सहारे पैदा उम्मीदों की नहीं बल्कि वास्तविक जीवन की उन समस्याओं को पूछने और उठाने की चुनौती है जो आम जन अपनी भाषा में रोजाना ही पूछा और उठाया करते हैं।
सिद्धांत या फिर अवधारणाएं तभी अच्छी हैं जब उनको बरतने वाला अपनी भाषा में अपने वस्तु-जगत का बोध बना सके और उसमें आगे की राह निकाल सके। सार रूप में कहें तो वि-उपनिवेशीकरण खुद से जुड़े सवाल पूछने और अपने लिए कारगर उपाय तलाशने के सांस्कृतिक और साभ्यतिक आत्म-विश्वास का नाम है।
(द प्रिंट से साभार)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.