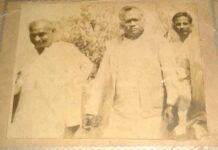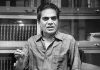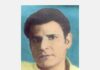भारतीय राष्ट्रवाद और इकबाल
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में विदेशी हुकूमत से मुक्ति पाने की इच्छा ने सभी वर्गों के शिक्षित भारतीयों को प्रभावित किया था। इस इच्छा के पीछे हम सभी भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इस बात का अहसास था। हम सभी एक देश के, एक मुल्क के बाशिंदे हैं, यह चेतना लोगों को विदेशियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उद्यत कर रही थी। ये शिक्षित भारतीय विभिन्न प्रांतों, संप्रदायों और पंथों के निवासी और अनुयायी थे। लेकिन बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में राष्ट्रभक्ति की समान भूमिका पर हिंदू तथा मुस्लिम संप्रदायों में एकता कायम करने की तीव्र इच्छा अब सिर्फ शिक्षित लोगों तक ही सीमित नहीं रहकर साधारण लोगों के दिलों को भी स्पर्श कर चुकी थी। 1919 से और एक भावना आम लोगों को प्रणोदित करने लगी थी और वह थी धार्मिक भावना।
महात्मा गांधी ने एक ओर धर्म को राजनीति से जोड़ दिया तो दूसरी ओर तुर्की साम्राज्य को विभाजित करने की गुप्त संधियों का रूसी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा रहस्योद्घाटन किए जाने पर हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी धार्मिक प्रक्षोभ की लहर दौड़ पड़ी। प्रथम महायुद्ध में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तुर्की और खिलाफत के बारे में अंग्रेजों ने उनको कई आश्वासन दिये थे। अब ये सारे आश्वासन झूठे साबित हो गए। इस वंचना से मुसलमानों में आग भड़क उठी। परंपरावादी मुस्लिम नेताओं ने प्रक्षुब्ध मुसलमान समुदाय को राजनीति में खींचा।
जिन्ना जैसे नेता पश्चिमी सभ्यता तथा विशुद्ध देशभक्ति से प्रेरित होकर राजनीति में आए थे। उनकी राष्ट्रीयता का स्रोत पश्चिम के आदर्शों में था, लोकतंत्र, देशभक्ति, उदारवाद, व्यक्ति-स्वातंत्र्य तथा संवैधानिक आंदोलन का रास्ता। स्वयं लोकमान्य तिलक में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया था। 1914 के पश्चात् विशुद्ध राष्ट्रीय लोकतंत्रवाद उनका सूत्र बन गया था, कट्टरता कम होने लगी थी, साथ ही उग्रता भी। इस समय तिलक और जिन्ना मिलकर कार्य करने लगे थे। लखनऊ करार का उन्होंने समर्थन किया था।
इस बीच जब महात्मा गांधी का उदय हुआ और मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद खिलाफत, पंजाब के अत्याचार और स्वराज्य के प्रश्न पर असहयोग तथा अहिंसात्मक प्रतिकार का आह्वान करने लगे तो न सिर्फ श्रीनिवास शास्त्री और तेजबहादुर सप्रू जैसे हिंदू उदारवादी नेता इससे विमुख होने लगे, जिन्ना साहब जैसे मुसलमान नेता भी बेचैनी महसूस करने लगे। उनके मन में धार्मिक तथा उग्र असहयोगवादी नेतृत्व के प्रति अत्यधिक दूरी का भाव उत्पन्न होने लगा। वे महात्मा, मौलाना, स्वामी, मौलवी आदि की भीड़ में कुछ अटपटा महसूस करने लगे, कानून तोड़कर जेल जाने की नयी प्रणाली की वजह से उनका दम घुटने लगा। बुद्धि और दिमाग को अपील करने की अब बात नहीं रही। अब प्रक्षोभ की भावना कांग्रेस के सभा-अधिवेशनों पर अपनी छाप स्थापित कर चुकी थी। खादी वेशधारी, दाढ़ी-चोटी वाले प्रतिनिधियों का इन सभा-समितियों में बाहुल्य हो गया।
धीरे-धीरे पश्चिम की विचारधारा से प्रभावित उदारवादी नेता मध्यधारा की नयी राजनीति से अलग-थलग पड़ गए। धर्म और राजनीति का मिश्रण तात्कालिक दृष्टि से इतना लाभदायक जरूर हुआ कि लाखों लोग इसी बूते पर राजनीति में शिरकत करने लगे, देहदंड और जेल की यातनाएं सहने के लिए खुशी से राजी होने लगे।
मगर जैसे ही संघर्ष और आंदोलन का सिलसिला टूट गया, तुर्की में कमाल अतातुर्क ने जब खिलाफत और खलीफा ही को समाप्त कर विशुद्ध प्रादेशिक और भाषाई राष्ट्रावाद के आधार पर तुर्की को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना दिया तो खिलाफत आंदोलन की सारी हवा निकल गयी। उधर अरबों में भी धार्मिक भ्रातृभाव और इस्लामी चेतना की जगह अरब चेतना जगने लगी। नए प्रादेशिक राज्यों तथा अरब भाषाई राष्ट्रीयता के प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा व्यक्त की। लेकिन हिंदुस्तान में धार्मिक पुनर्जागरण का, सांप्रदायिक चेतना का भूत जो एक बार जग गया था, वह अब शांत होने के लिए तैयार नहीं था। नयी सांप्रदायिक चेतना और सत्ता के हस्तांतरण की संभावना ही ने हिंदू–मुसलमान संप्रदायों तथा अन्य समुदायों में विग्रह की भावना पैदा कर दी। अब केवल मौलाना मोहम्मद अली ही नहीं, अनेक मुसलमान तथा हिंदू राष्ट्रवादी नेता भी संप्रदाय के संकुचित हित को सर्वोपरि मानने लगे। यह परिवर्तन सर मोहम्मद इकबाल जैसे विचारकों में पहले आया और सबसे आखिर में जिन्ना साहब में।
शुरू में इकबाल में भौगोलिक (हिंदुस्तानी) राष्ट्रभक्ति की भावना अत्यंत प्रखर थी। उनका तराना-ए-हिंदी मशहूर और लोकप्रिय होकर स्वतंत्रता संग्राम के नौजवानों के होंठों पर था :
“सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा,
हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा,
परबत वह सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का,
वह संतरी हमारा, वह पासबां हमारा,
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोसतां हमारा।”
इकबाल साहब ने ‘हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत’ नाम की जो कविता लिखी थी, वह भी काफी प्रसिद्ध थी। इस शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्र, वतन उनके लिए ‘खुदा’ की तरह था।
बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक के अंत में अपनी यूरोप की यात्रा के बाद जब इकबाल साहब लौट के वापस आए तो उनकी विचारधारा में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो चुका था। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी विज्ञान और उसके प्रभाव से रँगे ‘भौतिकवादी’ आधुनिक जीवन से उन्हें नफरत-सी हो गयी। वे राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता, समाजवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र और तत्सम संस्थाओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे। अकेले इस्लाम ही में आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय पाया जा सकता है, ऐसी उद्घोषणा उन्होंने की। (स्टडी आफ इकबाल्स फिलासफी : बशीर अहमद घर पृ.169)
इस्लाम मानवजाति को राष्ट्रीयता और वंशवाद के परे ले जाता है, अब ऐसी इकबाल की धारणा बन गयी। “आदर्श इस्लामी राज्य वैचारिक राज्य होगा। ऐसे वैचारिक राज्य में वंश, रंग, भौगोलिक विभाग के भेद न सिर्फ महत्वहीन हैं, बल्कि हानिकारक भी।” (उपरोक्त, पृ. 339-40)
“इस्लाम राज्य तांत्रिक दृष्टि से जनतंत्र पर आधारित नहीं होगा। यह जनता की, अवाम की सार्वभौमिकता में विश्वास नहीं करता। इस्लामी राज्य सही माने में ईश्वरीय होता है, धार्मिक होता है। इस अर्थ में नहीं कि धर्मगुरुओं का, पोप-पादरियों का, भट्ट-ब्राह्मणों का उसमें राज्य होगा। इस्लाम में ईश्वरीय राज्य का मतलब मनुष्यों का शरीयत के सामने संपूर्ण समर्पण है।”(उपरोक्त पृ.333)
1912 में मोहम्मद इकबाल को ब्रिटिश हुकूमत ने नाइटहुड का खिताब दिया। अब वे राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगे और 1927 में पंजाब विधान परिषद के सदस्य हो गये। 1930 में वे इलाहाबाद में होनेवाले मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने घोषणा की कि “पंजाब, सरहदी सूबा, सिंध तथा बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बनाना चाहिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर या बाहर। स्वतंत्रता की प्राप्ति और पश्चिमोत्तर भारत में एकत्रित राज्य, मेरी राय में, मुसलमानों की, विशेषकर पश्चिमोत्तर हिंदुस्तान के मुसलमानों की नियति है।” इसी में कुछ लोग भावी पाकिस्तान के बीज देखते हैं। मगर इकबाल का पूरा भाषण पढ़ने पर उनका पश्चिमोत्तर राज्य अभी संपूर्णतया सार्वभौम, प्रभुसत्ता-संपन्न राज्य नहीं था, यह स्पष्ट हो जाता है। हां, उनकी निगाह में समान केंद्र, अत्यंत सीमित अर्थ में ही सही, आवश्यक था।
दिसंबर 15, 1932 को नेशनल लीग के तत्वावधान में इकबाल का इस्तकबाल किया गया। अपने भाषण के दौरान, इकबाल ने कहा- “चार-पांच साल पहले मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के नाते मैंने यह सुझाव दिया था कि शायद पश्चिमोत्तर इंडियन मुस्लिम राज्य का निर्माण एक समाधान के रूप में कार्य कर सकता है। मेरे सुझाव को उस समय नहीं स्वीकार किया गया था; लेकिन आज भी मेरी राय है कि इस मसले का यही एकमात्र हल है। मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। देखें कि अनुभव मेरे द्वारा सुझाए गए समाधान की सार्थकता सिद्ध करता है या उसकी निरर्थकता।’’ (उपरोक्त, पृ.75)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.