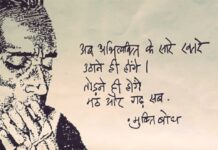— सुज्ञान मोदी —
दुनिया भर के सत्पुरुषों ने निर्भयता की सीख दी है। दुनिया के सारे महान कार्य निर्भयी महापुरुषों ने ही किए हैं। अपने जीवन में जब मुमुक्षु स्वरूपज्ञान की साधना में लगता है, तब उसके लिए सबसे जरूरी निर्भयता ही होती है। बिना निर्भयता के तो वह साधना मार्ग में आनेवाली छोटी-छोटी चुनौतियों का भी सामना नहीं कर पाएगा। निर्भयता को समझने के लिए हमें सबसे पहले भय को समझना होगा। भय या डर होता ही क्यों है? किन चीजों का भय सबसे अधिक होता है। इस भय के क्या दुष्परिणाम होते हैं। और इस भय पर विजय कैसे पाया जा सकती है? इसे समझना होगा।
सामान्य जीवन में सर्वत्र भय ही भय
श्रीमद् जी ने विशेषकर गृहस्थों के जीवन में आनेवाली समस्याओं का अत्यंत सूक्ष्मता से चिंतन और विश्लेषण किया है। वे कहते हैं कि बाल्यवास्था से लेकर वृद्धावस्था तक सामान्य मनुष्य का सारा जीवन प्रायः भय में ही बीतता है। 23वें वर्ष में श्रीमद् के शब्द हैं—
“बाल्यावस्था तो नासमझी में व्यतीत हो गई। कल्पना करो कि 46 वर्षकी आयु है, अथवा इतनी आयु है कि वृद्धावस्था का दर्शन कर सकें, परंतु उसमें शिथिल दशा के सिवाय हम दूसरी कुछ भी बात न देख सकेंगे। अब केवल एक युवावस्था बाकी बची। उसमें भी यदि मोहनीय की प्रबलता न घटी तो सुख की निद्रा न आएगी, निरोगी नहीं रहा जाएगा, मिथ्या संकल्प-विकल्प दूर न होंगे, और जगह-जगह भटकना पड़ेगा और यह भी तब होगा जबकि ऋद्धि होगी, नहीं तो पहले उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। उसका इच्छानुसार मिलना न मिलना तो एक ओर रहा, परंतु शायद पेटभर अन्न मिलना भी दुर्लभ हो जाए। उसी की चिंता में, उसी के विकल्प में, और उसको प्राप्त करके सुख भोगेंगे। इसी संकल्प में, केवल दुख के सिवाय दूसरा कुछ भी न देख सकेंगे। इस अवस्था में किसी कार्य में प्रवृत्ति करने से सफल हो गए तो आँख एकदम तिरछी हो जाएगी। यदि सफल न हुए तो लोगों का तिरस्कार और अपना निष्फल खेद बहुत दुख देगा।”
यहीं पर आगे कहते हैं— “प्रत्येक समय मृत्यु का भयवाला, रोग का भयवाला, आजीविका का भयवाला, यदि यश हुआ तो उसकी रक्षा करने का भयवाला, यदि अपयश हुआ तो उसे दूर करने का भयवाला, यदि अपना लेना हुआ तो उसे लेने का भयवाला, यदि कर्ज हुआ तो उसकी हाय-तोबा का भयवाला, यदि स्त्री हुई तो उसके ……..का भयवाला, यदि न हुई तो उसे पाने का विचारवाला, यदि पुत्र पौत्रादिक हुए तो उनकी चिंता का भयवाला, यदि न हुए तो उन्हें प्राप्त करने का विचारवाला, यदि कम ऋद्धि हुई तो उसे बढ़ाने के विचारवाला, यदि अधिक हुई तो उसे गोदी में भर लेने का विचारवाला, इत्यादि रूप से दूसरे समस्त साधनों के लिए भी अनुभव होगा। क्रम से कहो अथवा अक्रम से, किंतु संक्षेप में कहने का तात्पर्य यही है कि सुख का समय कौन-सा कहा जाए— “बाल्यावस्था? युवावस्था? जरावस्था? निरोगावस्था? रोगावस्था? धनावस्था? निर्धनावस्था? गृहस्थावस्था? या अगृहस्थावस्था?”
भय कहाँ नहीं है? और किसे नहीं है? ‘भावनाबोध’ में महायोगी भतृहरि के उपदेश समझाते हुए परमकृपालु श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं—
भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालद्भयं,
माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भयम्।
शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतांताद्भयं,
सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्॥
अर्थात् भोग में रोग का भय है। कुल में पतन का भय है। लक्ष्मी में राजा का भय है। मान में दीनता का भय है। बल में शत्रु का भय है। रूप से स्त्री को भय है। शास्त्र में वाद का भय है। गुण में खल का भय है। काया पर काल का भय है। इस प्रकार सभी वस्तुएँ भय वाली हैं। एकमात्र वैराग्य में ही अभय है!
हम किसी के भय का कारण न बनें
जब संसार में सबको भय ही भय है। अन्य प्राणियों की तो छोड़ें, जब मनुष्य जैसे चेतनासंपन्न प्राणी को इतना भय है, तो हम किसी भी प्राणी के भय का कारण क्यों बनें? एक जीव के सामने जब दूसरे जीव की बलि दी जाती है तो उसमें कितना भय उत्पन्न होता है। इसलिए सत्पुरुषों ने शाकाहार पर इतना जोर दिया है। संसार में तो भय की समाप्ति तभी होगी जब कोई किसी के भय का कारण न बने। ‘मोक्षमाला’ में राजा श्रेणिक और शाकाहार का बोध देनेवाले अभयकुमार की कथा आती है। इस कथा के अंत में इसका मर्म समझाते हुए श्रीमद् जी उपदेश करते हैं— “[सभी प्राणियों को] अभयदान आत्मा के परम सुख का कारण है।”
सबको अभयदान देने के लिए हमारे हृदय में सार्वजनीन प्रेम, करुणा और दया का प्राबल्य होना चाहिए। इसलिए श्रीमद् जी ने दयाधर्म का उपदेश करते हुए कहा है कि इसी से सभी प्राणी भयरहित रह सकते हैं। मोक्षमाला में आठों प्रकार की दया— “द्रव्यदया, भावदया, स्वदया, परदया, स्वरूपदया अनुबंधदया, व्यवहारदया और निश्चदया” का माहात्म्य समझाते हुए श्रीमद् कहते हैं— “इन आठ प्रकार की दया को लेकर भगवान ने व्यवहारधर्म कहा है। इसमे सब जीवों के सुख, संतोष और अभयदान, ये सब विचारपूर्वक देखने से आ जाते हैं। …जहाँ किसी प्राणी को दुख, अहित अथवा असंतोष होता है, वहाँ दया नहीं, और जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। अर्हंत् भगवान के कहे हुए धर्मतत्त्व से सभी प्राणी भयरहित होते हैं।”
श्रीमद् प्रभु कहते हैं—
धर्मतत्त्व जो पूछ्युं मने तो संभळावू स्नेहे तने,
जे सिद्धांत सकळनो सार सर्वमान्य सहुने हितकार ॥1॥
भाल्युं भाषणमा भगवान, धर्म न बीजो दया समान;
अभयदान साथे संतोष, द्यो प्राणिने दळवा दोष ॥2॥
अर्थात् सर्वमान्य धर्म जो धर्म का तत्त्व मुझसे पूछा है, उसे तुझे स्नेहपूर्वक सुनाता हूँ। वह धर्म-तत्त्व सकल सिद्धांत का सार है, सर्वमान्य है, और सबके लिए हितकारी है। भगवान् ने अपने उपदेश में कहा है कि दया के समान दूसरा धर्म नहीं है। दोषों को नष्ट करने के लिए अभयदान के साथ प्राणियों को संतोष प्रदान करो।
विचारवान को केवल अज्ञान का भय
निर्भयता तो वांछनीय है ही। और पूर्ण निर्भयता की स्थिति में ही साधक सत्य साधना के पथ पर सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज जो हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है, जो देश-काल और परिस्थिति है, उसमें पूर्ण निर्भयता प्राप्त करना थोड़ा कठिन दिखता है। तो ऐसी अवस्था में मुमुक्ष क्या करें?
27वें वर्ष में श्रीमद् जी कहते हैं— “मुमुक्षु जीव को दो प्रकार की दशा रहती है : एक ‘विचार-दशा’ और दूसरी ‘स्थितिप्रज्ञ-दशा’। स्थितिप्रज्ञ-दशा तब जाकर प्रगट होती है जब विचार-दशा लगभग पूरी अथवा संपूर्ण हो जाती है। उस स्थितिप्रज्ञ-दशा की प्राप्ति होना इस काल में कठिन है; क्योंकि इस काल में प्रधानतया आत्म-परिणाम का व्याघात रूप ही संयोग रहता है, और उससे विचार-दशा का संयोग भी सद्गुरु के सत्संग के अंतराय से प्राप्त नहीं होता। ऐसे काल में कृष्णदास विचार-दशा की इच्छा करते हैं, यह विचार-दशा प्राप्त होने का मुख्य कारण है। और वैसे जीव को भय, चिन्ता, पराभव आदि भाव में निज बुद्धि करना योग्य नहीं है। तो भी धीरज से उन्हें समाधान होने देना, और चित्त का निर्भय रखना ही योग्य है।”
इसी बात को और समझाते हुए आगे कहते हैं— “मुमुक्षु जीव को अर्थात् विचारवान जीव को इस संसार में अज्ञान के सिवाय दूसरा कोई भी भय नहीं होता। एक अज्ञान की निवृत्ति की इच्छा करने रूप जो इच्छा है, उसके सिवाय विचारवान जीव को दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होती, और पूर्व कर्म के बल से कोई वैसा उदय हो तो भी विचारवान के चित्त में ‘संसार काराग्रह है, समस्त लोक दुख से पीड़ित हैं, भय से आकुल हैं, राग-द्वेष के प्राप्त फल से प्रज्वलित हैं’— यह विचार निश्चय से रहता है। और ‘ज्ञान-प्राप्ति का कुछ अंतराय है, इसलिए यह कारागृहरूप संसार मुझे भय का हेतु है, और मुझे लोक का समागम करना योग्य नहीं’— एक यही भय विचारवान को रखना योग्य है।”
कर्मफलभोग मानकर दुख सहने की तैयारी से निर्भयता
क्या दुख से, वेदना से कोई बच सका है? जब इससे कोई बच नहीं सका है तो फिर भला इसका भय क्या करना! दुखों, अपमानों और रोगादि को प्रारब्ध और संचित आदि कर्मों का फलभोग मान लेने से इनके प्रति भय की तीव्रता कमती है। आसन्न एवं अवश्यंभावी दुखों के प्रति स्वीकारभाव पैदा कर लेने से मुमुक्षु निर्भयी हो जाता है। श्रीमद् जी ने विभिन्न स्थानों पर आत्मार्थियों को यही उपदेश किया है।

एक आत्मार्थी को वे पत्र में लिखते हैं— “सुदृढ़ स्वभाव से आत्मार्थ का प्रयत्न करना। आत्म-कल्याण प्राप्त करने में प्रायः प्रबल परिषहों के बारम्बार आने की संभावना है, परंतु यदि उन परिषहों को शांत चित्त से सह लिया जाए तो दीर्घकाल में हो सकने योग्य कल्याण बहुत अल्पकाल में ही सिद्ध हो जाता है। तुम सब ऐसे शुद्ध आचरण से रहना कि जिससे तुमको काल बीतने पर, विषम दृष्टि देखनेवाले मनुष्यों में से बहुतों को, अपनी उस दृष्टि पर पश्चात्ताप करनेका समय आए। धैर्य रखकर आत्म-कल्याण में निर्भय रहना। निराश न होना। आत्मार्थ में प्रयत्न करते रहना।”
आजीविका, लोकलाज, गृहस्थी का भविष्य और परिजनों के प्रति ममत्व, यही सब भय के प्रमुख स्रोत हैं। इन सबके प्रति निर्भय होने का सबसे आसान मार्ग श्रीमद् जी बताते हैं कि भविष्य को भुलाकर वर्तमान में साधनारत रहो। एक आत्मार्थी को सांत्वना देने हेतु निर्भयता का यह महत्वपूर्ण सूत्र समझाते हुए श्रीमद् जी कहते हैं—
“तुम्हारी आजीविका संबंधी स्थिति बहुत समय से मालूम है; यह पूर्वकर्म का योग है। जिसे यथार्थ ज्ञान है, ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता; इसलिए तुमने जो आकुलता के कारण इच्छा प्रगट की है, उसे निवृत्त करना ही योग्य है। हम जानते हैं कि तुम्हारी इस प्रकार की स्थिति है कि जिसमें धीरज रखना कठिन है। ऐसा होने पर भी धीरज में एक अंश की भी न्यूनता न होने देना, यह तुम्हारा कर्तव्य है, और यही यथार्थ बोध पाने का मुख्य मार्ग है। …किसी भी प्रकार का भविष्य का सांसारिक विचार छोड़कर वर्तमान में समतापूर्वक प्रवृत्ति करने का दृढ़ निश्चय करना ही तुम्हें योग्य है। भविष्य में जो होना होगा, वह होगा, वह तो अनिवार्य है, ऐसा मानकर परम पुरुषार्थ की ओर सन्सुख होना ही योग्य है।
आगे इसी पत्र में कहते हैं— “किसी प्रकार से भी लोकलज्जारूपी इस भय के स्थान ऐसे भविष्य को विस्मरण करना ही योग्य है। उसकी चिंता से परमार्थ का विस्मरण होता है और ऐसा होना महा आपत्तिरूप है; इसलिए इतना ही बारम्बार विचारना योग्य है कि जिससे वह आपत्ति न आए। बहुत समय से आजीविका और लोकलज्जा का खेद तुम्हारे अंतर में इकट्ठा हो रहा है, इस विषय में अब तो निर्भयपना ही अंगीकार करना योग्य है। फिर से कहते हैं कि यही कर्तव्य है। यथार्थ बोध का यही मुख्य मार्ग है। इस स्थल में भूल खाना योग्य नहीं है। लज्जा और आजीविका मिथ्या हैं। कुटुम्ब आदि का ममत्व रखोगे तो भी वही होगा जो होना होगा।”
निर्भयता के लिए सत्पुरुष का सत्संग आवश्यक
अब प्रश्न है कि विचार-दशा में विचारवान केवल अज्ञान का ही भय रखे और कुसंगति से बचे। ऐसा विचार निश्चित हो जाने पर भी जीवन की कठिन चुनौतियाँ तो जब-तब सामने आती ही रहती हैं और उसकी चिंता भी साधक को सताती ही रहती है। तो ऐसे दुख और ऐसी वेदना की घड़ी में मुमुक्षु क्या करे? इसका समाधान देते हुए एक स्थान पर श्रीमद् कहते हैं—
“महात्मा श्रीतीर्थंकर जो निर्ग्रन्थ को प्राप्त हुए, उन्होंने परिषह सहन करने का बारम्बार उपदेश दिया है। उस परिषह के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए ‘अज्ञानपरिषह’ और ‘दर्शनपरिषह’— इन दो प्रकार के परिषहों का प्रतिपादन किया है। अर्थात् किसी उदय-योग का प्राबल्य हो और सत्संग-सत्पुरुष का योग होने पर भी जीव को अज्ञान के कारणों को दूर करने में हिम्मत न चल सकती हो, घबराहट पैदा हो जाती हो, तो भी धीरज रखना चाहिए; सत्संग-सत्पुरुष के संयोग का विशेष-विशेष रूप से आराधन करना चाहिए।”
ऐसे सत्पुरुष जिनका संयोगमात्र ही हमें निर्भय कर दे, ऐसे सत्पुरुष की पहचान क्या है? इसे समझाते हुए एक अन्य स्थान पर अपने 27वें वर्ष में श्रीमद् जी कहते हैं—
“जिन सत्पुरुषों ने जन्म, जरा, और मरण का नाश करनेवाला, निजस्वरूप में सहज-अवस्थान होने का उपदेश दिया है, उन सत्पुरुषों को अत्यंत भक्ति से नमस्कार है। उनकी निष्कारण करुणा से नित्य प्रति निरंतर स्तवन करने से भी आत्मस्वभाव प्रगठित होता है। ऐसे सब सत्पुरुष और उनके चरणारविंद सदा ही हृदय में स्थापित रहो! जिसके वचन अंगीकार करने पर, छह पदों से सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहज में ही प्रगटित होता है, जिस आत्म-स्वरूप के प्रगट होने से सर्वकाम जीव संपूर्ण आनंद को प्राप्त होकर निर्भय हो जाता है, उस वचन के कहनेवाले ऐसे सत्पुरुष के गुणों की व्याख्या करने में हम असमर्थ ही हैं। क्योंकि जिसका कोई भी प्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्मभाव को, उसने किसी भी इच्छा के बिना, केवल निष्कारण करुणा से ही प्रदान किया है। तथा ऐसा होने पर भी जिसने दूसरे जीव को “यह मेरा शिष्य है, अथवा मेरी भक्ति करनेवाला है, इसलिए मेरा है” इस तरह कभी भी नहीं देखा—ऐसे सत्पुरुष को अत्यंत भक्ति से फिर-फिर से नमस्कार हो!
एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि निर्भयता ही स्वयं इन सत्पुरुषों की भी पहचान होती है। उनके शब्द हैं—“जिनसे मार्ग चला है, ऐसे महान पुरुषों के विचार, बल, निर्भयता आदि गुण भी महान ही थे।”
मृत्यु के भय को जीतकर ही पूर्ण निर्भयता
श्रीमद् ने मुमुक्षुओं के लिए निर्भयता को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना है। लेकिन मनुष्य को सबसे अधिक भय मृत्यु का ही होता है। ऐसा जानते हुए उन्होंने सत्य साधकों को मृत्यु का भय भी जीतने का आह्वान किया है। ‘मोक्षमाला’ में वर्णित 32 योगों में 29वाँ योग उन्होंने यह बताया है कि ‘मृत्यु के भय से भी भयभीत नहीं होना।’
एक और स्थान पर इसे समझाने के लिए कहते हैं कि अनित्यबोध से मृत्यु का भय जीतकर ही पूर्णकाम हुआ जा सकता है। उनके शब्द हैं— “हमने जो पूर्ण-कामता के विषय में लिखा है, वह इस आशय से लिखा है कि जिस प्रमाण से ज्ञान का प्रकाश होता जाता है, उसी प्रमाण से शब्द आदि व्यावहारिक पदार्थों से निस्पृहता आती जाती है; आत्म-सुख के कारण परितृप्ति रहती है। अन्य किसी भी सुख की इच्छा न होना, यह पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। ज्ञानी अनित्य जीवन में नित्यता प्राप्त करता है, ऐसा जो लिखा है वह इस आशय से लिखा है कि उसे मृत्यु से भी निर्भयता रहती है। जिसे ऐसा हो जाए उसे फिर अनित्यता रही है, ऐसा न कहें, तो यह बात सत्य ही है।”
एक अन्य स्थान पर कहते हैं—“अज्ञान से और निजस्वरूप के प्रति प्रमाद से, आत्मा को केवल मृत्यु की भ्रांति ही है। उस भ्रांति को निवृत्त कर, शुद्ध चैतन्य निज अनुभव-प्रमाणरूप में परम जाग्रत होकर, ज्ञानी सदा ही निर्भय रहता है। इसी स्वरूप के लक्ष से सब जीवों के प्रति साम्यभाव उत्पन्न होता है, और सर्व परद्रव्यों से वृत्ति को व्यावृत्त कर, आत्मा क्लेशरहित समाधि को पाती है।”
अंत में यही निवेदन कि श्रद्धा और भक्ति से बढ़कर निर्भयता का कोई दूसरा साधन नहीं। अपने 17वें वर्ष से पूर्व ही रचित प्रभु प्रार्थना में श्रीमद् ने भगवान को भयभंजन कहकर ही उनका आराधन किया है। इसके एक पद में श्रीमद् कहते हैं—
भद्रभरण भीतिहरण, सुधाझरण शुभवान।
क्लेशहरण चिंताचूरण, भयभंजन भगवान।।
सत्पुरुषों का योगबल जगत का कल्याण करे!
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.