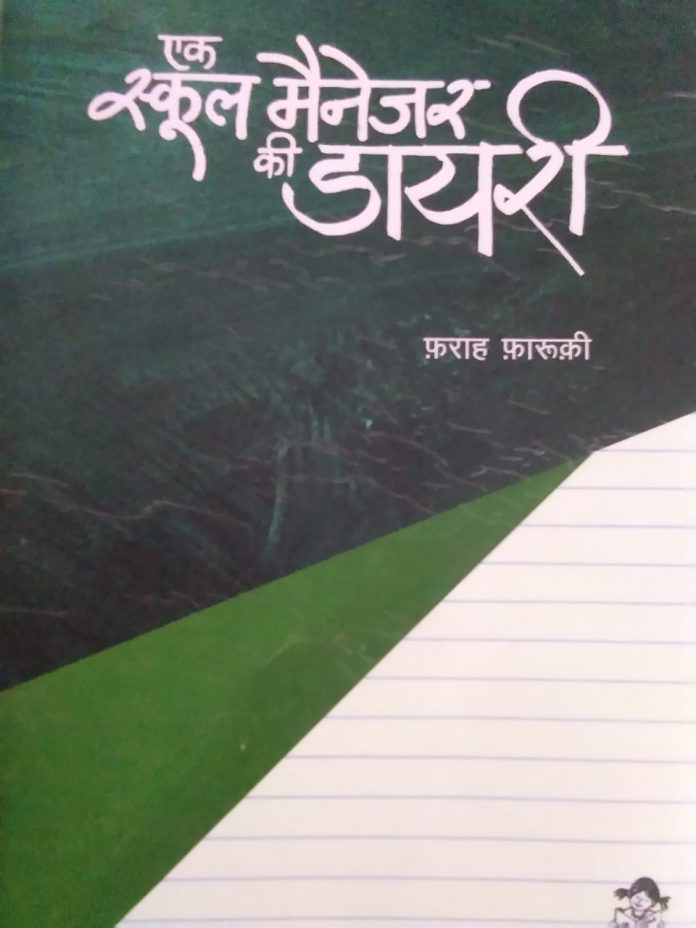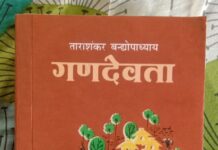— संजीव ठाकुर —
हमारे विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से मानविकी में जो शोध किए जाते हैं वे कहीं से भी स्तरीय नहीं कहे जा सकते। घिसे-पिटे विषयों पर कहीं से सामग्री काटकर कहीं जोड़ देने का काम अधिकांश शोधार्थी करते रहते हैं। उनमें मौलिक चिंतन का अभाव तो रहता ही है, दृष्टि धुंधली होने के कारण विषयों की सूक्ष्म पकड़ भी गायब रहती है। बरसों से चले आ रहे अकादमिक ढर्रे और जड़ भाषा के कारण भी अधिकांश शोध-कार्य सिर्फ डिग्री लेने के उद्देश्य को पूर्ण करते दिखाई देते हैं। इसके विपरीत कुछ शोध-कार्य ऐसे जरूर मिल जाते हैं जिनमें मौलिक ढंग से सोचने, सूक्ष्मता से देखने और रचनात्मकता से लिखने की कोशिश दिखाई देती है। शिक्षाविद फ़राह फ़ारूक़ी की किताब एक स्कूल मैनेजर की डायरी दूसरी तरह के शोध के उदाहरण के रूप में रखी जा सकती है। यह किताब चूँकि कोई डिग्री पाने की गर्ज से नहीं लिखी गई है – अपने अनुभवों और परीक्षणों को तरतीब देने के उद्देश्य से लिखी गई है : रचनात्मक बन पड़ी है।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह स्कूल और स्कूली शिक्षा की पड़ताल करती हुई किताब है। हमारे देश में स्कूलों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा दिखाई देती है। एक तरफ अधिक पैसे लेकर शिक्षा देनेवाले निजी स्कूल हैं तो दूसरी तरफ कम या बिना पैसे लिए शिक्षा देनेवाले सरकारी स्कूल। हालत यह है कि सरकारी स्कूलों में प्रायः निर्धन, साधनहीन और पिछड़े तबके के बच्चे पढ़ने जाते हैं। इन बच्चों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मध्य और उच्च वर्गीय परिवारों के बच्चों की तुलना में एकदम अलग होती है। बहुत से बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ घर के काम भी करने पड़ते हैं, माता-पिता के साथ रोजी-रोटी कमाने में भी शामिल होना पड़ता है। काफी बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। ऐसे ही बच्चों को भेड़-बकरियों की तरह हाँकनेवाले किसी स्कूल में फ़राह फ़ारूक़ी मैनेजर बनकर जाती हैं और स्कूल के इतिहास, भूगोल के साथ-साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों की स्थितियों पर गौर फरमाती हैं। प्रबंधन समिति, प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी और उनके पालकों की मनःस्थिति को समझते हुए उनको जोड़ने की कड़ी का काम करती हैं। फ़राह फ़ारूक़ी चाहतीं तो सिर्फ मैनेजर की भूमिका का निर्वाह करती रहतीं लेकिन शिक्षा और समाज के प्रति संवेदनशील होने के कारण उन्होंने इससे ऊपर उठकर स्कूल की बेहतरी के लिए काम करना स्वीकार किया। प्रबंधन-समिति और प्रधानाचार्य को जोड़ने का काम किया, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच के रिश्ते को मजबूत करने का काम किया और पालकों की स्थितियों को ध्यान में रखकर उन्हें स्कूल से जोड़ने का काम किया।

पुरानी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके के एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के जालों को साफ करने में काफी मशक्कत की ज़रूरत थी। फ़राह फ़ारूक़ी ने ईमानदारी से कोशिश की और कुछ ही समय में जाले साफ हुए, स्कूल में ताज़ा हवा का झोंका आने लगा।
फ़राह फ़ारूक़ी ने समस्या के सभी पहलुओं पर गौर किया और उन्हें सुलझाने की कोशिश की। ठीक स्कूल के सामने सार्वजनिक मूत्रागार हो या स्कूल के मैदान को सार्वजनिक संपत्ति समझने वाले लोग। शिक्षकों की आपसी गुटबंदी हो या छात्र-छात्राओं का आपसी व्यवहार। शिक्षक-शिक्षिका के पढ़ाने का ढंग हो या विद्यार्थियों के सीखने का तरीका। स्कूल बिल्डिंग की खस्ता हालत हो या सरकारी लालफीताशाही। फ़राह फ़ारूक़ी ने इन सब पर ध्यान दिया और उनपर खुली बुद्धि से विचार किया। स्कूल का हिस्सा बनकर स्कूल की कमियों को आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से परखा और प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, माता-पिता का सहयोग लेकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया।
फ़राह फ़ारूक़ी ने इस किताब में शिक्षकों की आतंकी सत्ता से विद्यार्थियों की आजादी की बात की है तो शिक्षकों की समस्याओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया है। स्कूल में आनेवाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों को रोजी-रोटी कमाने की चिंता से मुक्त रखने और उन्हें सिर्फ पढ़ाई करने की सुविधा मिलने की बात करती भी वह दिखाई देती हैं। इसके लिए राज्य की भूमिका को वह महत्त्वपूर्ण मानती हैं। उन्होंने लिखा है- “ऐसे कामों से बच्चों को दूर रखने के लिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। लेकिन यह हस्तक्षेप तभी मायने रखेगा जब यह इन बच्चों के आर्थिक-सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए किया जाए और इनकी आर्थिक जिम्मेदारी में हिस्सेदारी ली जाए।”(पृ. 62)
जिस स्कूल में फ़राह मैनेजर रहीं उसमें अवकाश के समय मजहबी तालीम के लिए बच्चे एक कमरे में जमा होते थे और कुरान और हदीस के प्रेरक-प्रसंग सुनते-सुनाते थे। इस क्रिया-कलाप को फ़राह अत्यंत सकारात्मक निगाह से देखती हैं। इतनी सकारात्मक निगाह से कि एक जगह वह कह जाती हैं- “इसी तरह एक कम उम्र टीचर को बच्चों ने हिदायत दी कि वे सर पर स्कार्फ या दुपट्टा पहना करें। इनकी मज़हब की समझ इन्हें यह हिम्मत बख्शती है।” (पृ. 93) फ़राह जिसे हिम्मत कह रही हैं क्या वह वाकई हिम्मत है? या मज़हब की गलत समझ से उपजा दुस्साहस? क्या यही दुस्साहस धार्मिक रूप से कट्टर लोगों में नहीं पाया जाता? और क्या यह मज़हबी तालीम बच्चों को कट्टरता की ओर नहीं ले जाती? फ़राह खुद ऊपर लिख चुकी हैं- “मज़हब जहाँ उम्मीद के चिराग जलाता है वहीं कई बार गलत व्यवहार को नाजायज स्वीकृति भी देता है।”(पृ. 93) आगे चलकर वह यह भी कहती हैं- “मेरे खुद के, किसी शैक्षिक संस्थान में मज़हबी तालीम होने पर बहुत से सवाल और एतराज रहे हैं।”(पृ. 105) बावजूद इसके वह किसी शिक्षिका के साथ की गई बदतमीज़ी को ‘हिम्मत’ कैसे कह सकती हैं?… सच तो यह है कि मज़हबी तालीम के पूरे विवरण में फ़राह अंदर-अंदर इस तालीम के पक्ष में ही खड़ी दिखाई देती हैं।
इस कमी के कारण इस किताब का महत्त्व कम नहीं हो जाता है. यह किताब सरकारी स्कूलों के अनेक पहलुओं को सामने लाने का काम करती है। स्कूल में पढ़नेवाले बच्चों के बहाने उनके माता-पिता और स्कूल के आसपास बसे समाज की दिक्कतों का वर्णन भी इस किताब में किया गया है। स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के अच्छे-बुरे पक्षों को भी इसमें रेखांकित किया गया है। ईमानदारी से कोशिश करने पर कुछ तो बदलाव आता ही है, यह संदेश भी इस किताब में निहित है।
कुल मिलाकर यह किताब सरकारी स्कूलों की स्थिति पर अनौपचारिक शोध का अच्छा उदाहरण कही जा सकती है। इसमें बीच-बीच में शोध के कुछ तत्त्व भले ही झाँकते मिल जाएँ, ज्यादातर यह किताब संस्मरण और डायरी का मिला-जुला रूप पढ़ने का सुख देती है। उर्दू-हिन्दी को मिलाकर बुनी गई इस किताब की भाषा बहुत रचनात्मक लगती है। कहीं-कहीं लिंगदोष और संबोधन में बिंदु का प्रयोग (भाइयों, कमबख्तों, मजदूरों, दोस्तों) इस किताब के संपादक के भाषा-ज्ञान पर प्रश्न-चिह्न लगाने का काम जरूर करते रहते हैं।
किताब – एक स्कूल मैनेजर की डायरी
लेखक – फ़राह फ़ारूक़ी
प्रकाशक – एकलव्य फाउंडेशन, भोपाल
मूल्य – 220 रुपए
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.