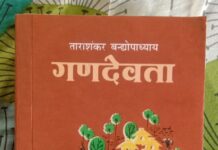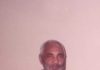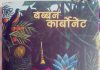— हिमांशु जोशी —
आज देश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। इसे देख आपको लगता नहीं कि इसका कारण कहीं न कहीं बच्चों पर जबर्दस्ती गृहकार्य (होमवर्क) और अंग्रेजी थोपने वाली हमारी शिक्षा व्यवस्था है।
एक ही ढर्रे पर चलती जा रही शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को विभिन्न अवसर प्रदान करने में अक्षम है।
हमारी शिक्षा व्यवस्था डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, शिक्षक तैयार करने तक ही सीमित रह गई है। बच्चों को चित्रकार, कलाकार, कथाकार, कलमकार, किसान, प्लम्बर, मैकेनिक, खिलाड़ी बनाने के बारे में हम सोचते तक नहीं।
देश अब सरकारी और प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के रूप में दो भागों में बंट रहा है। हम सरकारी स्कूलों को समस्या के तौर पर देखने लगे हैं पर सरकारी शिक्षकों की समस्याएं हमें नहीं दीखतीं।
चर्चित उपन्यास ‘फिर वही सवाल’ के लेखक दिनेश कर्नाटक शिक्षा में बदलावों की इन्हीं चुनौतियों पर बात करने के लिए अपनी नई किताब शिक्षा में बदलाव की चुनौतियां लेकर हमारे सामने आए हैं। काव्यांश प्रकाशन से छपकर आई इस किताब का आवरण चित्र डॉ मनोज रांगड़ और विनोद उप्रेती द्वारा तैयार किया गया है। खिड़की के अंदर से बाहर झांकते बच्चे के इस चित्र में हमें बच्चों द्वारा अपने भविष्य को लेकर संजोयी गई बहुत सी उम्मीदें दिखती हैं। पिछला आवरण चित्र बच्चों के लिए ‘कुछ कर के सीखना’ सन्देश देता महसूस होता है।

अनुक्रम से मालूम चलता है कि यह किताब शिक्षा के सवालों पर आधारित 29 लेखों का संग्रह है। लेखों के अलग-अलग विषय पर केंद्रित होने की वजह से आप किताब का जो पन्ना खोल कर पढ़ते हैं, उसी में रम जाते हैं।
पहले लेख ‘शिक्षा के स्वरूप का सवाल था जे. कृष्णमूर्ति’ के जरिए लेखक ने हमारे देश में शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा छेड़ी है। लेख की भाषा सरल है और जे. कृष्णमूर्ति के विचार पढ़ने के बाद हम काफी हद तक यह समझने में सफल हो जाते हैं कि आज बच्चों में सृजनशीलता की भावना को प्रेरित किया जाना आवश्यक है।
‘क्या हम अपने विद्यार्थियों को जानते हैं’ लेख में लेखक ने बड़ी ही खूबसूरती से बैंकों और ‘प्रथम’ संस्था से मिली सीख को विद्यार्थियों पर आजमाने की सलाह दी है। लेखक अपने शिक्षकीय अनुभव के बारे में बताते हैं जो बड़ा ही रोचक लगता है। इस लेख में लेखक ने अपने विद्यार्थियों के बारे में जो आंकड़े जुटाए हैं, वैसे आंकड़े शायद ही अधिक शिक्षक जुटाने की जहमत उठाते हों।
देश की मौजूदा परिस्थितियों को समझने के लिए यह लेख पढ़ा जाना बेहद जरूरी है। इसकी कुछ पंक्तियां- ‘जहां 9वीं कक्षा तक सभी बच्चे आपस में घुल मिलकर रहते थे। वहीं 10वीं में मुस्लिम बच्चे एकसाथ बैठने लगते थे।’
‘अर्थात 39 बच्चे ऐसी बदतर स्थितियों में रह रहे थे जिनके रहते पढ़ाई में ध्यान देने की बात करना उनके साथ नाइंसाफी होगी।’
लेख के अंत में लेखक 1932 में गिजूभाई द्वारा किए गए प्रयोगों को भी याद करते हैं।
अगले लेख में लेखक ने अपने स्कूली दिनों और आज के दिनों में पब्लिक स्कूलों और सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों के बारे में लिखा है। इनके बच्चों के बीच बढ़ रहे अंतर को हम इस बात से समझ सकते हैं : ‘इससे देश में दो तरह की दुनियाओं का निर्माण हो रहा है। उस अनिवार्य संघर्ष की पृष्ठभूमि बनती जा रही है, जिससे हम देश के कई हिस्सों में जूझ रहे हैं।’
‘जानने और समझने की चुनौती’ लेख में लेखक एम्स, आईआईटी का हवाला देते हुए लिखते हैं कि ‘हमारे देश में जिन सेवाओं को हमारे हुक्मरान जिम्मेदारी से चलाना चाहते हैं, वे पूरी मुस्तैदी से चल रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं।’
जब तक पाठक इसे समझते हैं तब तक सरकारी स्कूलों में स्कूल बस की व्यवस्था वाला प्रश्न पाठकों के सामने शिक्षा व्यवस्था का पूरा चेहरा ही बेनकाब करता दीखता है। साथ ही साथ लेखक ने स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाए जाने पर भी कुछ महत्त्वपूर्ण लोगों के कथनों के सहारे अपने विचार व्यक्त किए हैं।
अगला लेख ‘सिर्फ अंग्रेजी मीडियम से बात बनने से रही’ है और अब तक आप हर लेख के शीर्षक से भी प्रभावित होने लगेंगे, यह शीर्षक किताब के लेखों पर सटीक बैठते दिखते हैं। इस लेख में लेखक ने प्राइवेट स्कूलों के खुलने से भारतीय समाज को होनेवाले नुकसान के बारे में बताया है। ‘मानव सूचकांक में ऊपर की पांतों में आनेवाले लोकतांत्रिक देशों में माना जाता है कि एक सामान्य आदमी के बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा मिलनी चाहिए जैसी उस देश के सबसे बड़े आदमी के बच्चे को मिलती है’ पंक्ति इस पर स्थिति स्पष्ट कर देती है। इस लेख में लेखक ने अंग्रेजी मीडियम पर सवाल उठाने के साथ सरकारी अध्यापकों को अध्यापन के सिवाय अन्य सरकारी कामों में लगाए जाने के बारे में भी लिखा है।
‘एक गाँधीवादी के शिक्षा में प्रयोग’ लेख गाँधीवादी योगेश चन्द्र बहुगुणा द्वारा खोले गए स्कूलों के ऊपर है, यहां आप उनके द्वारा स्कूलों में किए गए प्रयोगों के बारे में पढ़ते हैं। लेख में ‘अतीत के बिखरे पन्ने’, ‘माई हार्ट टू द चिल्ड्रन’, जैसी किताबों पर लिखने के साथ ही अतीत में हुए स्कूलों के प्रयोगों पर भी लिखा गया है। इस लेख के अंत में लेखक ने आज की शिक्षा व्यवस्था में कई आवश्यक बदलाव भी सुझाए हैं।
किताब पढ़ते अब आपके मन में यह विचार जरूर आने लगेगा कि स्कूलों में अपना जीवन रमा देनेवाले लेखक जैसे शिक्षकों से ही अगर शिक्षा व्यवस्था की नीतियां बनवानी शुरू कर दी जाएं तो देश के स्कूलों की हालत बदलते देर नहीं लगेगी।
इस किताब में लेखक ने शिक्षा से जुड़े लगभग सभी महत्त्वपूर्ण विषय सम्मिलित कर लिये हैं, अगला लेख ट्यूशन पर है।इसकी शुरुआती पंक्तियां ही एक ऐसा सच हमारे सामने ले आती हैं, जिससे परिचित होने के बाद भी आमजन कुछ नहीं करता। ‘देखते ही देखते हमारे देश में बच्चों को पढ़ाना एक महंगा काम बन गया है। जिस रकम से आम लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे उसे ‘शिक्षा के व्यापारी’ बड़ी धूर्तता से उनसे छीन ले रहे हैं।’
किताब शिक्षा को लेकर आंख खोलनेवाले विचार हमारे सामने रखती रहती है। ‘बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उन्हें अपने मां-बाप पढ़ते हुए नहीं दिखाई देते’ इसका प्रमाण है।
लेखक ने ‘बच्चे प्रश्न करने से क्यों डरते हैं’ जैसा लेख अपनी पोटली से निकालते हुए, उनके अंत में उसे लिखने का समय भी लिखा है। इस लेख को पढ़ते पाठक अपने स्कूली दिनों को याद करने लगेंगे। ‘कैसा हो, यदि पाठ्यपुस्तकें ही न हों’ लेख में श्रम की शिक्षा को अनिवार्य किए जाने का विचार वास्तव में शिक्षा जगत में क्रांति ला सकने वाला विचार है।
पृष्ठ संख्या 58 पर लेखक द्वारा बच्चों से भय के बारे में सवाल, उनके भय के कारणों को हमारे सामने लाता है। ये सवाल-जवाब स्कूली बच्चों को समझने में बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। पृष्ठ 64 पर और किताब में कई अन्य जगह भी लेखक ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की समस्याएं लिखी हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है।
‘पुस्तकालय के मेरे अनुभव’ लेख की शुरुआत में लेखक ने बड़ी ही खूबसूरती से किताबों से जुड़ी अपनी बचपन की यादों को लिखा है। ‘उन दिनों घर में किताबों की तादाद बढ़ने पर सिर्फ किताबों की वजह से छत पर एक कमरा बनवाया ताकि वे वहां सुरक्षित रहें’ पंक्ति लेखक के किताबों के प्रति शौक को दर्शाने के साथ, पाठकों के मन में भी किताबों के प्रति रुचि जगाती है।
पृष्ठ 70 और 71 की घटना पढ़ने में तो अजीब है पर हमारे समाज की वास्तविकता भी है लेकिन इन्हें पढ़ आप लेखक के जज्बे को जरूर सलाम करेंगे। ‘शिक्षक का पेशा’ लेख में लेखक ने चर्चित उपन्यास ‘राग दरबारी’ का उदाहरण देकर समाज में शिक्षक का महत्त्व बताया है। लेखक किताब में शिक्षा के सुधार पर कई बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का हवाला देते हैं। यह लेख शिक्षकों की स्वायत्तता पर केंद्रित है, जिसे धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। पृष्ठ 75 पर लेखक शिक्षकों के प्रति मीडिया के नकारात्मक रवैये की तरफ भी ध्यान खींचते हैं।
‘स्कूल का काम घर क्यों आए’ लेख में लेखक ने गृहकार्य पर शहरी और ग्रामीण बच्चों के हालात का वर्णन बेहतरीन तरीके से किया है। जनवरी 2019 में लिखे इस लेख में गृहकार्य के स्वरूप को बदलने के लिए बड़े ही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। लेखों को आगे पढ़ते, मनुष्य मारपीट क्यों करता है! जैसे प्रश्न का जवाब बड़ा ही स्पष्ट दिखाई देता है। ‘एक ऐसा तैयार जवाब जिसके लिए न तो दिमाग पर जोर देने की जरूरत होती है, न किसी तरह का उपाय करने की।’ इस जवाब को शिक्षक द्वारा बच्चों की पिटाई से जोड़कर लेखक बच्चों की पिटाई पर पाठकों को एक शिक्षक की मानसिकता समझाने में कामयाब रहे हैं।
पृष्ठ 91 पर लेखक ने भारत के वर्तमान हालात पर एक सटीक टिप्पणी की है, जिसे पढ़ना जरूरी है। ‘शिक्षा के नाम पर लूट’ लेख में इस लूट पर मीडिया और सरकार की भूमिका पर चर्चा की गई है। इस लेख में स्कूलों में लूट के नए-नए तरीके पढ़ पाठक भी अचंभित होने लगेंगे। ‘अगर देशभर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों से ली गई फीस के औचित्य की जांच की जाए तो या देश का सबसे बड़ा घोटाला या संगठित लूट होगी’ पंक्ति से लेखक ने इस विषय की गम्भीरता की तरफ इशारा किया है।
स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मेट्रो को तरह मजबूत करने का उदाहरण पढ़ने में नया और प्रभावी जान पड़ता है। अंग्रेजी थोपने को लेकर किताब के एक लेख में लिखी पंक्ति ‘हकीकत तो यह है भाषा व्यवहार तथा जरूरत से सीखी जाती है। हमारे पर्यटन केंद्रों के अनपढ़ गाइड तथा वेटर इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं।’ अंग्रेजी थोपने के हिमायती लोगों की आंखें खोल सकती है।
‘शिक्षा में हम किस ओर जाना चाहते हैं’ लेख में बच्चों को आरंभिक कक्षाओं में फेल न करने के निर्णय पर विस्तार से लिखा गया है। किताब के हर लेख महत्वपूर्ण हैं और शिक्षा के क्षेत्र की हर समस्याओं, चुनौतियों से पाठकों को अवगत कराने में कामयाब रहे हैं। ‘तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच’ लेख में विज्ञान पढ़ने और बिल्ली के रास्ता काटने पर परेशान होने की पंक्ति, बहुत से पाठकों को खुद से जुड़ी महसूस होगी।
‘सरकारी स्कूल का निजीकरण क्यों’ लेख में लेखक ने निजी क्षेत्र के उद्देश्यों को भलीभांति परिभाषित किया है। पृष्ठ 136 की पंक्ति ‘संकट योग्य शिक्षकों के रिक्त पदों, संसाधनों की कमी तथा हिंदी मीडियम व अंग्रेजी मीडियम वाली दो तरह की शिक्षा प्रणाली से है’ शिक्षा तंत्र की लगभग सभी कमियों को उजागर कर देती है। इसी पृष्ठ पर यूनेस्को की एक रिपोर्ट का जिक्र भी है, जिसके जरिए लेखक ने अपने विचारों को मजबूती प्रदान की है। यहां लेखक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में निजीकरण की कोशिश के दुष्परिणाम हमारे सामने ले आते हैं।
किताब के आगे के लेख छात्रों के लिए शारिरिक श्रम और कहानी के महत्त्व पर लिखे गए हैं। ‘शारीरिक श्रम तथा कहानियाँ’ लेख पढ़ आपको अपने स्कूली दिन याद आ जाएंगे और यह भी समझ आएगा कि यदि तब शारीरिक श्रम स्कूली शिक्षा में शामिल रहा होता तो आज आप बहुत से जरूरी घरेलू कार्य खुद निपटा सकते थे।
जैसे फिल्मों में एक न एक सीन बहुत जबरदस्त होता है, ठीक वैसे ही इस किताब के अंतिम भाग ‘शिक्षा प्रश्नोत्तरी’ से पहले का लेख “शिक्षा पर ‘प्रथम’ की चौंकानेवाली रिपोर्ट” भी है। इस लेख को पढ़ आप शिक्षा क्षेत्र में चल रहे ‘खेल’ को समझने लगेंगे।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.