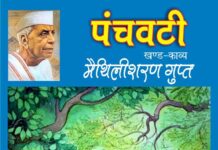— राजकिशोर —
खतरा अभी धुँधला-सा है, पर धीरे-धीरे बढ़ेगा। ग्लोबीकरण हिन्दी को, जैसी वह आज हमारे सामने है, अंततः खा जाएगा। दरअसल, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी तुलना मुहावरे में आने वाली ‘बकरे की माँ’ से ही की जा सकती है जिसे ‘खैर मनाने’ की इजाजत नहीं है। यह अभागी भाषा जन्म से ही संघर्ष करती रही है- कभी अपने रंग-रूप के सवाल पर तो कभी अपनी राजनीतिक हैसियत के सवाल पर। वह एक नदी पार करती ही है कि उसके सामने दूसरी नदी आ जाती है। कभी नाले और कभी रेगिस्तान भी। उसका रोना-पीटना इतना हो चुका कि अब रोने-पीटनेवालों को ही ‘हिंदी वाले’ बताकर डाँट दिया जाता है- क्यों बेकार टेसुए बहा रहा है! हिंदी की चिंता करनेवाले हिंदी के लोगों द्वारा ही ‘हिंदी वाले’ माने जाते हैं!
क्या समाज में मौजूद आर्थिक वर्गों की तरह हिंदी की स्थिति भी ‘हैव्स’ और ‘हैव-नॉट्स’ के लिए अलग-अलग नहीं हो गई है? एक वर्ग हिंदी का दूध पीता है और दूसरा उसके लिए चारा जुटाता है।
यहाँ हिंदी के सामने मौजूद जिस खतरे की बात की जा रही है, उसका संबंध हिंदी के हास्यास्पद अंग्रेजीकरण से है। नहीं, हिंदी पर अंग्रेजी भाषा के प्रभाव की बात नहीं हो रही है। यह प्रभाव तो तब से पड़ रहा है जब से वह अंग्रेजी के संपर्क में है। और यह कोई अस्वाभाविक या अनुचित घटना भी नहीं है। दो चीजें मिलती हैं तो वे एक-दूसरे को प्रभावित करती ही हैं। यह प्रकृति का भी नियम है और संस्कृति का भी। मजबूत कमजोर को ज्यादा प्रभावित करता है, यह भी उपर्युक्त नियम का ही एक हिस्सा ठहरा। सो, हिंदी ने अंग्रेजी से बहुत कुछ लिया और अंग्रेजी ने हिंदी से सिर्फ कुछ संज्ञाएं लीं।
यह गैरबराबरी फिर भी ‘क्षम्य’ की कोटि में आती है, क्योंकि हिंदी क्या लेती है और क्या नहीं लेती है, यह उसका अपना चुनाव है। किसी ने हिंदी को बाध्य नहीं किया कि वह अंग्रेजी के इन-इन शब्दों या विन्यासों को ग्रहण करे। जिसे इस तरह की स्वतंत्रता है कि वह चाहे तो गुलाम हो और चाहे तो गुलाम न हो, वह भी ‘स्वतंत्र’ की कोटि में ही आएगा। हमारे समय की बहुत-सी गुलामियाँ इसी कोटि की हैं। वे आरोपित नहीं की जातीं, लपक कर स्वीकार की जाती हैं। हिंदी ने पिछली शताब्दी में जब ऐसा किया था, तब उसे शायद इस बात का एहसास नहीं था। वह सुबह हो जाने के काफी देर बाद जगी थी और अपने को संपन्न करने के लिए अतिरिक्त उद्योग कर रही थी। इस प्रक्रिया में उसने अंग्रेजी से काफी उधार लिया।
आज वह स्थिति नहीं है। हिंदी एक समृद्ध नहीं तो संपन्न भाषा जरूर है। वह बारीक से बारीक अभिव्यक्ति में सक्षम है- हालांकि उसकी इस सक्षमता का लाभ उठाते हुए कुछ ही लेखक, पत्रकार और रंगकर्मी दिखाई देते हैं। अपनी-अपनी शक्ति या अपनी-अपनी रुचि। वैसे, हिंदी को खतरा तो इससे भी है, पर यह आंतरिक खतरा है। मेरा अनुमान है कि इसके मूल में हिंदी की हीन सामाजिक स्थिति है। इस सामाजिक स्थिति के कारण जो हिंदी के उन्नायक और समर्थक हैं, वे भी अपनी नई पीढ़ी को अंग्रेजी की भेंट चढ़ाए जा रहे हैं। जो भाषा अपने घर में ही लुटी जा रही हो, उस भाषा में हीरे-मोती चमकाने के लिए कौन अपने हाथ चोटिल करे, जो किसी को, बिना तीन-तिकड़म के, कुछ दे नहीं सकती। यहाँ तक कि कुछ करने का आत्मसंतोष भी नहीं। हिंदी जब उठेगी, तो उसकी यह हीनता दूर होगी। तब उसका मेला फिर से जुड़ने लगेगा। वह एक भरी-पूरी भाषा बनेगी ही नहीं, दिखेगी भी। लेकिन हिंदी को इस समय बाहर से जो खतरे हैं, उन्होंने उसे बचने दिया तभी ऐसे अच्छे दिन आ सकेंगे।
इन बाहरी खतरों में पहला विज्ञापन कंपनियों और उनसे विज्ञापन बनवाने वाले निर्माताओं-व्यापारियों से है। इन सभी को विश्व भर में एक ही भाषा आती है- मुद्रा की भाषा। धन के लिए ये और चीजों के साथ-साथ- जैसे लोकतंत्र और मानव अधिकार- भाषा को भी कुचल-मसल सकते हैं।
इनके जीवन दर्शन को पेप्सीवालों ने एक पंक्ति में परिभाषित कर दिया है- ये दिल मांगे मोर। हिंदी माध्यम से विज्ञापन करनेवाला हिंदी समाज के उसअधकचरे वर्ग को संबोधित करना चाहता है जिसे न हिंदी ठीक से आती है न अंग्रेजी। वैसे तो लफंगापन दोनों में से किसी एक भाषा में भी अच्छी तरह व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन दुचित्ते आदमी का लफंगापन भी द्विभाषी होगा। सो, विज्ञापन कंपनियां ऐसे संदेश और नारे लिखने में अपनी उम्दा प्रतिभाओं को लगा रही हैं जो हिंदी और अंग्रेजी के अवैध और अप्रिय समागम से पैदा होती हैं।
संपन्न हो रहे- और उतना नहीं भी हो रहे- हिंदी परिवारों के बेटे-बेटियों को जब अंग्रेजी माध्यम के एक से एक अधकचरे स्कूलों की ओर दौड़ाया जा रहा हो, तो हिंदी के शीश पर अंग्रेजी का मूसलाघात होना निश्चित है। हिंदी की अस्मिता को दूसरा खतरा अभी पनप ही रहा है, खुलकर सामने नहीं आया है। या, यों कहिए कि कुछेक अखबारों में यह पनप रहा है और एफएम रेडियो और टेलीविजन पर खुलकर आने के लिए पर तौल रहा है।
हिंदी अखबार बीच-बीच में अंग्रेजी के मोती बिखेरता चलता है, जैसे ‘प्राइवेट कंसलटैंट्स की मदद से’, ‘जेल में कैदियों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है’ आदि। अभी इस तरह के प्रयोगों की अधिकता नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है, क्योंकि अखबार के मालिकों की यही इच्छा है। उनमें से कुछ अपने अंग्रेजी अखबारों में भी हिंदी के जुमलों और मुहावरों को जगह-जगह पर चमकते हुए देखना चाहते हैं। इसके पीछे एक सुचिंतित दर्शन है : हर चीज की पवित्रता को नष्ट कर देना, ताकि अवैध धन से अवैध इच्छाओं और स्वप्नों को पूरा किया जा सके।
आखिर कोई भी चीज भाषा में ही व्यक्त होती है। सो, भाषा को बरबाद कर दो, तो बरबाद होने से कौन-सी चीज बची रहेगी? लेकिन ऐसे संस्थानों में जो लोग काम कर रहे हैं, वे सभी के सभी आत्महीन या संस्कृतिविहीन नहीं हैं। वे अपनी भाषा को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह उनके स्वभाव की माँग है। फिर अचानक आदेश याद आता है तो वे कुछ ऐसे शब्द जहाँ-तहाँ छिड़क देते हैं जो साबित कर सकें कि वे विद्रोही नहीं हैं।
तीसरा खतरा? यह विशिष्ट वर्ग की बातचीत में फड़फड़ाता है। इस समय हिंदी में बहुत-सी बातचीत ऐसी होती है जिसमें सर्वनाम (मैं, तुम, आप), कारक (पर, में, से, का) और क्रियाएँ ही (हूँ, था, होगा) हिंदी की होती हैं : ज्यादातर संज्ञाएं और विशेषण अंग्रेजी के होते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत वाक्य देखिए : ‘पार्टी में जो रिजिडिटी आ गई है, उसे रिमूव किए बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते।’ अक्सर इंजीनियर, माल बेचनेवाले और कंप्यूटर, धुलाई मशीन, फ्रिज आदि को सुधारने के लिए आनेवाले मिस्त्री इसी तरह की भाषा बोलते हैं। साहित्य और राजनीति में कोई गंभीर बहस छिड़ती है तो अंग्रेजी शब्दों के भारी छिड़काव के बिना वह आगे नहीं बढ़ती। पता नहीं क्या बात है कि प्रतिबद्धता पर कमिटमेंट, स्थिति पर सिचुएशन, सरल पर सिंपल और जटिल पर कॉम्प्लेक्स भारी पड़ता है। यही विद्वान जब लिखते हैं तो भारी-भरकम संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आलोचना या विचार के क्षेत्र में यह कूट भाषा ही अब स्वाभाविक हो गई है, जिसके लिए कभी रमेश कुंतल मेघ पर हँसा जाता था। लेकिन बोलते समय खासकर बातचीत में, यह भाषा नकली और प्रयासित जान पड़ती है, अतः उसे प्रामाणिक बनाने के लिए सीधे अंग्रेजी शब्दों का सहारा लिया जाता है।
अगर कहा जाए कि ये उपनिवेशीकरण के लक्षण हैं, तो अखबार और टीवी के फैलाव के मौजूदा वातावरण में, जब किसी अभागे पी-एच.डी. को किसी क्षेत्रीय संस्करण में मुश्किल से डेढ़-दो हजार रुपल्ली मिलती है और किसी किस्मतवाले ग्रेजुएट को किसी टीवी चैनल में चालीस-पचास हजार भी मिल सकते हैं, यह बात दूर की कौड़ी लग सकती है। ऐसे शंकालु मित्रों से निवेदन है कि हिंदी फैल रही है, लेकिन अपनी ही कीमत पर, जैसे कोई अपना ही खून रगड़कर अपना चेहरा लाल कर ले, अंग्रेजीवाले वर्ग की ताकत और अमीरी बढ़ाने के लिए।
जहाँ हिंदी के मजदूर को पैसा कम मिलता है, वहाँ वह देशी अपसंस्कृति का शिकार होता है, जहाँ ज्यादा मिलता है, पश्चिमोन्मुख अपसंस्कृति का। उदाहरण दिए बिना बात पूरी न हो रही हो, तो दो उदाहरण प्रस्तुत हैं। पहला उदाहरण 1901 के एक्ट नंबर तीन का ‘हिंदुस्तानी’ अनुवाद है, जो 1910 के आसपास तत्कालीन ब्रितानी सरकार द्वारा जारी किया गया होगा : “दफा 116– …अगर वह तादाद जिसका पहले तखमीना किया गया हो गैर-काफी पाई जाए तो जायज है कि वक्तन-फवक्तन तखमीना के तितम्मे बनाए जाते रहें और रकम जायद जैसा कि ऊपर हुक्म हुआ है वसूल की जाय।” (हिंदी-उर्दू-हिंदुस्तानी : हिंदू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता और अंग्रेजी राज, 1800-1947, कृपाशंकर सिंह)। इस पुस्तक में दी गई सूचना के अनुसार, अक्टूबर 1913 की ‘सरस्वती’ में कामता प्रसाद गुरु ने इसका सहज हिंदुस्तानी अनुवाद यों किया था– “अगर वह रकम जिसका अंदाजा पहले किया गया है, अधूरी पाई जाए, तो उचित है कि समय समय पर दूसरे अंदाजा किए जावें और अधिक रकम वसूल की जाय जैसा कि ऊपर हुक्म हुआ है।”
दूसरा उदाहरण भारतीय संविधान के अधिकृत हिंदी अनुवाद से है : “392 –कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति- (1) राष्ट्रपति किन्ही ऐसी कठिनाइयों को, जो विशिष्टतया भारत शासन अधिनियम, 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों को संक्रमण के संबंध में हो, दूर करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि यह संविधान उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में ऐसे अनुकूलों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह आवश्यक या समीचीन समझे : …।” इसका हिंदी या हिंदुस्तानी अनुवाद करने के लिए कामता प्रसाद गुरु जैसी ही प्रतिभा चाहिए। स्पष्ट है कि हिंदी को शासकों ने एक समय फारसी का उपनिवेश बनाने की कोशिश की थी, बाद में स्वाधीनता मिलने पर संस्कृत का। अब अंग्रेजी की बारी है। वह भले ही लिखित हिंदी से ज्यादा छेड़छाड़ न कर सके, पर बोली जानेवाली हिंदी को तो उसने अभी ही अपने बस में कर लिया है- “आपके ट्रांसफर का ऑर्डर हो गया है, आप जाकर बैंगलोर ऑफिस ज्वॉइन कीजिए और ज्वाइनिंग रिपोर्ट भेजिए।”
क्या फारसी और संस्कृत के बाद अंग्रेजी से शासित होना अनिवार्य है? पहले कोई जाति गुलाम होती है या उसकी भाषा? जिस जाति का अपनी भाषा के स्वरूप पर कोई अधिकार न रह जाए, क्या वह जाति भी स्वतंत्र कही जाएगी? ये बड़े प्रश्न हैं, लेकिन इतनी बड़े भी नहीं कि हम उन पर विचार ही करते रह जाएं और हिंदी की ट्रेन छूट जाए!
(स्व. राजकिशोर ने यह लेख ‘हिंदी की चिंदी’ शीर्षक से लिखा था)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.