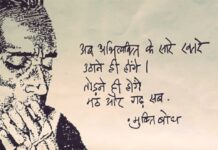— संजय गौतम —
मेरे कमरे में एक खिड़की भी है। ‘भी’ इसलिए कि सभ्यता के इस उन्नत चरण में बहुतों को खिड़की भी नसीब नहीं है। खिड़की तो बहुत बड़ी चीज है, एक छोटा सा रोशनदान भी नहीं, जहां से सूरज की कोई किरण आकर कमरे में बैठ सके। धूल की कोई रेख दीवार पर अपना निशान छोड़ सके। हवा आकर आदमी को थपकी दे सके। पानी की बौछारें आकर शीतल स्पर्श से उसे जगा सकें। जब यहां की बाड़ियों को देखता हूँ तो मुर्गी के दरबे की याद आती है। सुबह-सुबह हम मुर्गी के दरबों को खोलते थे तब मुर्गियां फड़फड़ाती हुई बाहर निकलती थीं चारे की तलाश में। रोज सुबह रोजी-रोटी के लिए महानगर की ओर उमड़ती हुई भीड़ को देख कर दरबे में से फड़फड़ा कर निकलती हुई मुर्गियों का दृश्य याद आ जाता है।
दरबे में से निकल कर आदमी पूरी हवा इकट्ठे अपने भीतर भर लेने के लिए गहरी-गहरी सांस लेता है, थोड़ी फुर्ती महसूस करता है, उसके हाथ-पांव के जोड़ ढीले होने शुरू होते हैं तभी सीटी मारती हुई लोकल ट्रेन दिखाई पड़ जाती है और वह दौड़ कर लटक जाता है, चलून दादा, भीतर चलून, ठेलून दादा, ठेलून, बाइरे लोग झूलचे, ओ दादा ठेलून ना, बाइरे लोग पोरी जाबे, तब जाकर अन्दर की भीड़ थोड़ा कसमसाती है और धीरे-धीरे जगह बन जाती है। अगले स्टापेज पर फिर यही प्रक्रिया और फिर जगह बन जाती है। ठेलते-ठेलते पूरी भीड़ ट्रेन के डिब्बे में पीठ से पीठ, पेट से पेट, मुंह से मुंह, गर्दन से गर्दन मिलाकर इस तरह खड़ी हो जाती है कि हवा भी अगर इस पार से उस पार जाना चाहे तो सहम कर लौट जाएगी। स्टेशन पहुंचने पर पूरी भीड़ ऐसे बाहर निकलती है, जैसे बहुत देर तक उबले पानी से भरी हुई केतली का ढक्कन खोल दिया गया हो और पूरी की पूरी भाप इकट्ठे निकलने को आतुर हो। यहां उतर कर आदमी अपने-अपने चारे की तलाश में महानगर के कोने-अंतरे में बिखर जाता है। रात भर सीलन भरे दरबे में गुजारने वाला आदमी बहुमंजिली इमारतों के वातानुकूल कमरों में राहत की सांस लेता है। बाजार की गलियों में डलिया भर दुकान लिये पटरी पर बैठ जाता है। रिक्शे की हैण्डिल हाथों में थाम लेता है या फिर कचड़ों के ढेर में खाने की चीजें खोजता-फिरता है। फिर बसों में भूसे सा ठुंसता, भाप की तरह निकलता, लोकल ट्रेन के डिब्बों में तीलियों सा अटा पड़ा अपने दरबे में पहुंचता है और पट से पड़ जाता है। दिनभर की थकान नशा बनकर उसे उतनी गहरी नींद में पहुंचा देती है जहां किसी भी चीज की जरूरत नहीं रह जाती है। और सबके पास तो यह दरबा भी नहीं है, जहां वह लौट सके।

भाई, घर हो या दरबा, कोई ऐसा ठौर होना चाहिए जहां आदमी लौटने के बारे में सोच सके। जहां से चलने के बारे में सोच सके। अनन्त आकाश की ऊँचाई नापते हुए हजारों मील की दूरी तय करने वाले पक्षी भी सांझ होते-होते अपने घोंसले में लौट आने को आतुर हो जाते है। खास मौसम में विदेश से आने वाले पक्षी भी मौसम बीतते ही उसी मार्ग से अपने देश लौट जाते है। लेकिन बहुत बड़ी जनसंख्या सड़कों की पटरियों पर, स्टेशन के प्लेटफार्म पर या दिन रात बाजारों में इधर- उधर भटकती रह जाती है। उसके पास लौटने की कोई जगह नहीं। इस मामले में वह आदिम है कि उसके पास कोई छांव नहीं, कोई ठौर नहीं। अभी भी हमारे साथ हमारा वह आदिम समाज यात्रा कर रहा है, अपने समूचे दुर्भाग्य के साथ। आदिम समाज के पास जंगल था, पेड़ थे, फल-फूल थे, लेकिन इन आदमियों के पास तो कुछ भी नहीं है। इनके अगल-बगल में बहुमंजिली इमारतें, होटलों की जूठन, ब्यूटी पार्लरों के सुगन्ध की धुंध और पुलिस का डण्डा, जो इन्हें भेड़ों की तरह कभी इधर तो कभी उधर हांकता रहता है। समाज के कितने रंग-रूप एकसाथ समानान्तर यात्रा करते रहते हैं लेकिन सभ्यता के इतिहास में अंकित होते हैं सिर्फ उन्नत साधन-सम्पन्न लोग, उनकी सभ्यता का रूप और उनका गुरूर। यही सभ्य लोग इतिहास को अपने साथ खींचते हुए उसकी पूर्णता का दावा करते हैं। समाज के वंचित लोंगो की पीड़ा को दर्ज किये बिना सभ्यता के इतिहास का पूरा चेहरा बन सकता है क्या?
अपने चचेरे भाई के यहां गया था। मेघ की भूमिका में। यक्ष का सन्देश लेकर नहीं। उसकी प्राणाधिक प्रिया की चिट्ठी लेकर। डेढ़ फुटे सीलन भरे रास्ते से घुसिए तो एक आंगन जैसी जगह में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ दरबे के आकार में छह फुट ऊँची छत की बाड़ी बनी हुई है। किसी में भी दरवाजा नहीं है। सबकी बाड़ी पर गल चुकी लुंगी का परदा उन्हें आड़ दे रहा है। किसी-किसी घर में सपनों का मायाजाल रचता टीवी चल रहा है। घरों के बाहर ही पानी निकलने की खुली नाली बजबजा रही है। थोड़ा किनारे हट कर है एक हैण्डपम्प और सामने ही बिना दरवाजे का लैट्रिन, उस पर टाट का एक झिगड़ा सा परदा झूल रहा है।
पूछ-पाछ कर भाई के बाड़ी का परदा हिलाता हूँ तो देखता हूं वह उदभ्रांत सा खपरैल की छत को निहार रहा है। मुझे देखते ही सकपका जाता है। आइए भईया आइए कहते हुए जैसे उसकी सांस टूटी जा रही है, गला सूखा जा रहा है। घर में जगह की कमी देखते हुए वह जैसे एकाएक सिकुड़ गये अपने दिल को फैला कर जगह बना रहा है। चौकी का बिस्तर ठीक करते हुए कहता है बैठिए भइया, और फिर संकोच से हंसते हुए कहता है, यही है अपनी राम मड़इया। मैं उसकी हिचक दूर करने की कोशिश करता हूँ—यहां यही बहुत है रे, चल बैठ और बता कैसा है तू। वह मेरी बात का जबाब दिये बिना ही बाहर दौड़ जाता है और फिर बर्फी और पानी मेरे सामने रख देता है। तब उसे थोड़ा इतमीनान हो जाता है। मैं उससे बैठने को कहता हूँ तो एक कोने में बैठ जाता है, फिर धीरे से पूछता है, आज इधर कैसे भइया। ऐसे ही चला आया, घर गया था तुम्हारी पत्नी ने यह चिट्ठी दी है और चिट्ठी उसके हाथ में पकड़ा देता हूं। अभी पढ़ ले। वह चिट्ठी खोलता है।‘ तू अकेले रहता है या और कोई साथ में,’ ‘नहीं भईया तीन लड़के हैं, सब कारखाने में शिफ्टवाइज ड्यूटी करते हैं और बना-खाकर यहीं सो रहते हैं।’
चिट्ठी पढ़ते हुए उसकी हंसती हुई आखों में थोड़ी उदासी छा जाती है। पूछता हूँ ‘क्या बात है?’ ‘अरे, कुछ नहीं वही सब जो हर बार रहता है’ और चिट्ठी मेरे हाथ में पकड़ा देता है। मैं सहसा विस्मित हो जाता हूं। इस बीस-बाइस के पति-पत्नी में ऐसा कुछ भी एकान्त नहीं जो मुझसे छिपाना चाहे और पत्र खोलकर सरसरी तौर पर देखता हूं। अत्यन्त टेढ़े-मेंढ़े अक्षरों में वही घर चूने, लड़के के बीमार रहने, बाबूजी (ससुर) के गाली देते रहने, जेठानी के ताना मारते रहने और कुल मिलाकर साथ लिवा चलने का कातर आग्रह। उसके उदास चेहरे को देखकर थोड़ा मजाक के मूड में आता हूं ‘सावन शुरु हो गया है, घर चला जा, हो आ, उसने मुझसे कहा था, भाई साहब जरुर भेज देना आखिर उसकी भी तो चाह है न। मेंहदी रचाये बैठी है’। वह उसी गम्भीर मूड में कहता है, ‘पूजा के पहले कैसे जाएंगें भइया। अभी पैसे का बहुत ठाला है, मिल ही बन्द हो गयी थी, कैसे-कैसे तो खुली है।’
मुझे उसका अल्हड़ किशोर चेहरा याद आ जाता है। गांव के बगीचे में आती-पाती खेलता हुआ लड़का किस दुनिया में खो गया। बुढ़ापे की चिन्ता की रेखाएं अभी से उसके माथे को निशाना बनाये हैं। सालों-साल से घर-परिवार से वंचित पिछड़े क्षेत्रों के लाखों किशोर युवा प्रौढ़ चार-छह सौ की नौकरी या इधर-उधर अण्डा-पावरोटी बेचते दिन भर की थकान से चूर-चूर हो “सोनागाछी” के दलदल में राहत की सांस पाने के लिए आतुर दिखाई पड़ते हैं तो इसमें किसका दोष ?

रोज नये-नये क्षेत्रों में कुकुरमुत्ते की तरह उमगते हुए “सोनागाछी” का, इन रागवंचित युवाओं का या उस केन्द्रित अर्थव्यवस्था का, जो अत्याधुनिक विकसित शहरों को माडल बनाने की धुन में पिछड़े क्षेत्रों के सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत के शोषण से लेकर वहां की जनसंख्या का भी खून चूसती चली जा रही है। रोज-ब-रोज ट्रेनों से लदकर देश के कोने-कोने की जनसंख्या उमड़ती चली आ रही है, चारे की तलाश में बिलबिलाने के लिए……..।
हां, तो मैं कह रहा ता कि मेरे कमरे में किड़की भी है। उस खिड़की से सूरज की ललछौंहीं किरण तो कमरे में आकर नहीं बैठती, क्योंकि यह उस दिशा में है ही नहीं। हम अपनी दिशा चुनने के लिए स्वतंत्र रह भी कहां गये है। हम तो जाने-अनजाने ऐसे खांचे में खड़े कर दिये गये हैं, जहां से मनचाही दिशा की ओर देख ही नहीं सकते हैं। हां, सामने वाले घर की खिड़की पर एक चित्ती धूप रोज सुबह आकर अटक जाती है और मैं उसे देखता रहता हूँ। दोनों घरों के बीच में एक नीम का गाछ भी है। खिड़की खोलिए तो घरों की नालियों के बजबजाते हुए सड़ियल पानी से दुर्गन्ध का एक भभका कमरे में घुस आता है। घुसकर नथूनों को सनसना जाता है। जी होता है खिड़की तुरंत बंद कर दें, लेकिन नहीं, साथ ही आती है नीम के गाछ से गुजरती हुई हल्की सी हवा। देर तक इसी छोटे से गाछ को देखता रहता हूँ तो गन्दगी से थोड़ा उबर जाता हूँ।
हां, उस खिड़की से मुझे थोड़ा सा आकाश भी दिखाई पड़ता है, चांदनी रात हो तो उजेला भी दीखता है और अंधियारी रात में तारे भी टिमटिमाते हुए दीख पड़ते है। शाम को घर की अंगीठियों से उठता हुआ धुआं दीखता है और पड़ोस की छत पर गप्पे मारती हुई औरतें और हंसते-खिलखिलाते, उछलते-कूदते बच्चे भी। इन्हीं के सुख से भरे हुए चेहरों को खिड़की के रास्ते पाकर मैं उल्लासपूरित होता हूँ। यह खिड़की बाहर के लोगों को मेरे होने,न होने के बारे में सूचना देती रहती है। और मेरा संबध थोड़ा बहुत प्रकृति से, समाज से जोड़ने का एकमात्र साधन है।
ग्यारह बज रहे हैं। अभी होटल से बेरस खाना निगलते हुए घर लौटा हूँ। खिड़की खोल दी है। सामने किसी घर में रोशनी नहीं है। सब गहरी नींद में हैं। घना अंधेरा है। उठ-उठकर छा रहे पागल बादल गहरे। नीम का गाछ भी बादलों की छांव में गहरा काला हो गया दिखाई पड़ता है। मानो हवा की हल्की थाप से सोना चाहता हो लेकिन सावन का शीतल स्पर्श उसे जगाये दे रहा हो। मैं भी अपने कमरे की बत्ती बुझा देता हूँ। अंधेरा अच्छा लगता है। बाहर भी-भीतर भी। खिड़की की ओर आंख टिकाकर लेट जाता हूँ। आंखो में नींद नहीं। तेज बारिश की टप-टप सुनाई पड़ती है। बारिश की तेज बूंदों से नाली के जमे हुए पानी में हलचल होती है। अभी तक अलसायी हुई तीखी गन्ध पूरे कमरे में गैस की तरह भर जाती है। इन्द्रियां सनसना जाती हैं तो भी खिड़की बन्द करने का मन नहीं होता। बारिश का गान सुनना अच्छा लगता है।…..
प्रगाढ़ आलिंगन में अपनी प्रिया को कसकर उसके गालों पर हलकी थपकी देकर कहता हूं, देखो बाहर कैसी अच्छी बारिश हो रही है। चलो हम दोनो चलें छत पर, थोड़ा भीग आयें वह हंसकर कहती है, धत् तुम्हें तो भीगने की ही लगी रहती है। बड़े चले हैं भीगने वाले। बीमार पड़ जाओगे तब सब रोमैंटिकता झड़ जायेगी, चलो सो जाओ चुपचाप। वह अपने घने काले बालों को मेरे चेहरे पर उलट देती है। लगता है, सचमुच बादल ने हम दोनों को अपनी छांव दे दी है। मेरे भीतर लहरों का गहरा उद्वेलन होता है। आलिंगन को और प्रगाढ़ कर लेता हूं। उसकी बंद पलकों को देर तक निहारता रहता हूं। निहारते-निहारते उद्वेलन और गहरा होता जाता है। कई-कई बार चूमता हूं। होंठों को गहराई से चूमता हूं…..नींद उचट जाती है, ओह बगल में तो कोई नहीं। है सिर्फ अंधेरा, भीतर भी-बाहर भी। घनघोर गरजते हुए बादलों के बीच से बिजली की चमक सहसा कमरे को नंगा कर जाती है। दरी, दरी पर लेटा मैं, बगल में ब्रीफकेस, निर्जीव सा बैग और कुछ किताबें, एक कोने में स्टोव, बर्तन….. फिर गहरा अंधेरा छा जाता है। बारिश का गान और तेज हो जाता है। मैं उतान छत की ओर निविड़ अंधकार में उदभ्रांत सा देखता रहता हूँ। भीतर से एक आवाज बुद-बुद करते हुए उठती है, फिर विलुप्त होती जाती है। घन घमंड नभ गरजत घोरा…… करवट बदल पूरे जी जान से सोने की कोशिश करता हूँ।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.