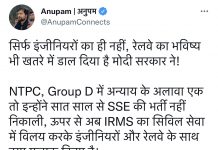— देविंदर शर्मा —
कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह देश ने प्रवासी मजदूरों का घर-वापसी पलायन देखा, उसके बाद आयी आवधिक श्रम-बल सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि खेत मजदूरों की संख्या में 3 फीसद का इजाफा हुआ है। यह गिनती वर्ष 2019-19 में 42.5 फीसद से बढ़कर 2021-22 में 45.5 फीसद हो गयी। जिस कृषि क्षेत्र को इन तीन सालों में जान-बूझकर दीन-हीन बनाकर रखा गया है, वह आज भी 40.66 लाख करोड़ रु. का सकल मूल्य संवर्धन (ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए) की कूबत रखता है। यह आँकड़ा इस क्षेत्र की मजबूती और लचीलापन दर्शाता है। और कुछ नहीं, अगर कृषि क्षेत्र में सिर्फ मूल्य समानता ही बना दी जाए अर्थात उच्चतर कीमत की गारंटी, तो कृषि क्षेत्र कहीं ज्यादा बेहतर कर दिखाए, उत्पादन और मूल्य संवर्धन, दोनों में।
कृषि उत्पाद की कीमतें नीचे रखने की वजह से जाहिर है कृषि क्षेत्र से होने वाली आय कम दिखाई देती है। इस तथ्य को स्वीकार करने के बजाय बड़ी चालाकी से यह दलील देकर आभास दिया जाता है कि ‘चूँकि देश की कुल आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा केवल 19 प्रतिशत है, इसलिए जो बोझ इसे जिलाए रखने में ढोना पड़ रहा है, उसमें खासी कटौती की जानी चाहिए।’ विद्रूपता भरी यह दलील पुरानी पड़ चुकी आर्थिक सोच का दोहराव है, जो किसानों को खेती से बाहर धकेलने पर आमादा है। मुख्यधारा के अर्थशास्त्री उस वैश्विक आर्थिक साजिश को आगे बढ़ाए रखना जारी रखे हुए हैं जो कृषि की बलि चढ़ाने को आतुर है ताकि आर्थिक सुधारों को व्यवहार्य बनाया जा सके। इसे बदलना ही होगा।
आइए पहले ग्रॉस वैल्यू आउटपुट (जीवीओ यानी सकल उत्पादन मूल्य) को समझें। अगर किसी वस्तु की औसत कीमत बढ़ती है तो उसकी ग्रॉस वैल्यू (सकल मूल्य) में भी बढ़ोतरी होती है। विकसित देश इस समीकरण का इस्तेमाल करके भारत की ताड़ना करते हैं कि वह विश्व व्यापार समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। गेहूँ और चावल के न्यूनतम खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के साथ, अमीर विकसित देश किसी उत्पाद के कुल मूल्य का निर्धारण उत्पादन की कीमत से गुणा करके निकालते हैं। फिर इससे यह हिसाब लगाते हैं कि भारत एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट (सकल माप समर्थन फार्मूले) के तहत 10 प्रतिशत सबसिडी देने की तयशुदा सीमा से कितना ऊपर जाकर कृषकों को राहत देता है।
अन्य शब्दों में, वे यह गणना करते हैं कि भारत उत्पाद के कुल मूल्य का कितना हिस्सा कृषि क्षेत्र को बतौर सहायता प्रदान करता है। बात यह है कि यदि उत्पादन पहले जितना रहे और कीमत ऊपर उठती है तो उसका जीवीओ भी ऊपर जाएगा।
परंतु, क्योंकि हम कृषि उत्पाद की कीमतें कम रखते हैं लिहाजा जीवीओ भी नीचे बना रहता है। वर्तमान में, जिंस की खेत में लगने वाली कीमत सामान्यतः नीचे रहती है, यहाँ तक कि घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से 20-30 फीसदी से कम। गेहूँ और चावल, और कुछ हद तक कपास, कुछेक दालों और चंद सब्जियों के अलावा थोक मूल्य नीचे ही रहता है। मुझे मालूम है कि उत्पाद के सकल मूल्य का निर्धारण चंद मंडियों में लगने वाली तात्कालिक कीमत का औसत निकालकर, फिर इसमें अन्य कुछ खर्च जोड़कर, तय किया जाता है। तार्किक यह है कि अगर बाजार मूल्य बनिस्बत ऊँचा रहे, जो कि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न हो, तब जीवीओ भी तुलनात्मक रूप से ऊँचा रहेगा।
साल 2014-15 में कर्नाटक सरकार ने किसानों को तुअर दाल पर 450 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया, नतीजतन रिकार्ड खरीद हुई। इस प्रक्रिया में, तुअर दाल उत्पादक की आय में 22,500 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई। कल्पना करें कि यदि देश भर में तुअर दाल की कीमतों में इतने स्तर की वृद्धि हो जाती, तो इस जिंस विशेष की जीवीओ कहीं ज्यादा हो जाती। इसी प्रकार, गेहूँ का मौजूदा न्यूनतम खरीद-मूल्य, जो कि इस साल 2125 रुपए प्रति क्विंटल है, यदि उसको देश भर में कानूनन गारंटी से लागू कर दिया जाए तो न केवल पंजाब, हरियाणा बल्कि पूरे देश के किसान को उच्चतर मूल्य मिल पाएगा। इससे गेहूँ उत्पादन का जीवीओ खुद-ब-खुद काफी उच्च गिना जाएगा। यदि शेष फसलों की कीमतों में आनुपातिक वृद्धि कर दी जाए तो यही बात उनपर भी लागू होती है।
जो अन्य पैमाना अर्थशास्त्री लागू करते हैं, वह है ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए (सकल मूल्य संवर्धन)। जीवीए और जीवीओ के बीच अंतर यह है कि फसल उगाने में आयी लागत और कच्चे माल की कीमत को जीवीओ से घटाना पड़ता है। वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन से हुए जीवीओ की गणना 50.71 लाख करोड़ रुपए की है। इस बात के मद्देनजर कि कृषि क्षेत्र के जीवीए–जीवीओ अनुपात देश भर में सबसे अधिक यानी 80.19 प्रतिशत है, यहाँ तक कि जमीन-जायदाद, व्यावसायिक एवं वित्तीय सेवाएँ, होटल और व्यापार क्षेत्र से भी अधिक, तो यह बताता है कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता कितनी अधिक है।
कुछ अर्थसास्त्रियों की सोच है कि क्योंकि कृषि के उत्पादन करने में औद्योगिक वस्तुओं की खपत वैश्विक औसत से कम होती है, मसलन खाद, कीटनाशक और कृषि-उपकरण और उत्पादन का आँकड़ा ज्यादातर भूमि-स्रोतों पर आधारित है, सो खेती का जीवीए अधिक रहता है। फिर क्या हुआ? कृषि यदि बाहरी औद्योगिक चीजों का कम इस्तेमाल करने के बावजूद इतनी उत्पादकता दे रही है तो कल्पना करें कि यदि सभी 23 फसलों से शुरुआत करके, न्यूनतम खरीद मूल्य को कानूनन रूप से लागू करते हुए, जिंस का उच्चतर और गारंटीशुदा मूल्य बना दिया जाए तो भारतीय कृषि की तस्वीर एकदम बदल जाएगी और यह आर्थिक विकास की मुख्य धुरी बन जाएगी।
वैश्विक स्तर पर, दुनिया अब खाद्य व्यवस्था के रूपांतर की ओर बढ़ रही है जिसका मंतव्य है कृषि से पैदा होनेवाले ग्रीनहाउसउत्सर्जन को कम करना। इसके लिए ऐसी कृषि-पर्यावरणीय खेती व्यवस्था की ओर जाने की जरूरत पड़ेगी जो कम बाहरी संसाधनों का इस्तेमाल करती हो। मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों को यह जरूर मालूम होना चाहिए कि जैव विविधता तंत्र ने वर्ष 2030 तक कीटनाशकों के उपयोग में दो-तिहाई कटौती करने का आह्वान किया है। यहाँ पर उनके लिए सबक है।
किसी भी सूरत में, जो बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा मुख्यतः इसलिए कम बना रहा क्योंकि किसानों को इन तमाम सालों में उनके हक का बनता मूल्य मिलने से महरूम रखा गया है। यदि कृषि का जीवीए देश भर में सबसे अधिक निकलकर आ रहा है तो मुझे उस बात में तर्क समझ नहीं आता जब अर्थशास्त्री कृषि को, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ समझकर, हेय दृष्टि से देखते हैं। तथ्य तो यह है, यह खेती ही है जो अर्थव्यवस्था को चट्टान की तरह मजबूती दिये हुए है। यहाँ तक कि जब कोरोना लाकडाउन के बाद पहली तिमाही में देश की आर्थिकी में 24 प्रतिशत की सिकुड़न दर्ज हुई थी, तब कृषि ही एकमात्र क्षेत्र था जिसने बहुत बढ़िया कर दिखाया था। वास्तव में यह कृषि का निरंतर अच्छा प्रदर्शन ही है जिसने उम्मीदें जिलाए रखी हैं।
एक जीवंत खेती व्यवस्था में इतनी ताब है कि देश को दरपेश रोजगार संकट को अपने भीतर समा सके। दरअसल, कृषि बोझ होने के बजाय एक संकटमोचक है। आज जब देश में कुल जनसंख्या का 45.5 फीसद कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, तो जोर इस ओर देने की जरूरत है कि खेती से चलनेवाली आजीविका को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और मुनाफादेह बनाया जाए। कृषि क्षेत्र को जानबूझकर सार्वजनिक निवेश से महरूम रखना, किसानों को न्यूनतम खरीद मूल्य की गारंटी न देना और एक भरोसेमंद मंडी व्यवस्था न बनाने को समय की माँग बना दिया गया है। इसके निदान के लिए मौजूदा आर्थिक सोच को पलटने की जरूरत है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.