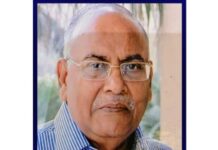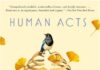– सत्यनारायण साहु —
मैंने 19 जून की शाम को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में क़ब्रिस्तान हजरत पंज पिरान बस्ती में एक अविस्मरणीय और आत्ममुग्ध कर देने वाला क्षण देखा। प्रसिद्ध प्रोफेसर इम्तियाज अहमद को अंतिम संस्कार करने से पहले, अंतिम समारोह का संचालन करने वाले एक मौलाना ने उपस्थित लोगों से एक सवाल का जवाब देने के लिए कहा। यह था : “कोई वारिस है- क्या मृतक के पास उत्तराधिकारी हैं? अगले ही पल, प्रोफेसर अहमद के सभी छात्रों ने,, जो इस शोक की घड़ी में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे, एक स्वर में जवाब दिया : “हम सब वारिस हैं- हम सभी उनके उत्तराधिकारी हैं!” इसके बाद उन्होंने परंपरा के अनुसार, सामूहिक रूप से पृथ्वी को अपने शिक्षक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रसिद्ध प्रोफेसर की कब्र पर रखा और जिन्होंने छात्रों, विद्वानों और शोधकर्ताओं की पीढ़ियों को आकार दिया।
प्रोफेसर अहमद के अनुकरणीय योगदान इस बात से परिलक्षित होते हैं कि छात्रों ने उनके उत्तराधिकारियों के लिए कॉल का जवाब कैसे दिया। वह अब व्यावहारिक व्याख्यान, लेख और किताबें साझा करने और सबसे ऊपर, आकर्षक बातचीत करने के लिए हमारे साथ नहीं हैं। 19 जून को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में उनका निधन हो गया। उन्होंने दशकों तक जेएनयू में पढ़ाया। राजनीतिक समाजशास्त्र पर उनके अग्रणी काम की एक समृद्ध विरासत है।
समान नागरिक संहिता पर उनका रुख
उनके दुखद निधन से ठीक एक दिन पहले, मैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और प्रसिद्ध वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सुहास बोरकर के साथ समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चर्चा कर रहा था। हमने उनकी प्रेरक और तर्कसंगत स्थिति पर चर्चा की, जिसमें एक समान संहिता के बजाय, उन्होंने महसूस किया कि भारत को अपने व्यक्तिगत कानूनों के तहत सामना किए जाने वाले किसी भी अन्याय को दूर करने के लिए नागरिक कानूनों का सहारा लेने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने यह रुख तब स्पष्ट किया था जब भारतीय जनता पार्टी ने 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शाह बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के महत्त्वपूर्ण फैसले को निरस्त करने के लिए संसद में एक कानून पारित करने की पृष्ठभूमि में समान नागरिक संहिता की मांग की थी। अदालत ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला बानो को दीवानी कानून के तहत गुजारा भत्ता दिया था।
उस साल प्रोफेसर अहमद ने (जानी-मानी राजनीतिक कार्यकर्ता और पूर्व लोकसभा सदस्य दिवंगत प्रमिला दंडवते की मौजूदगी में) जेएनयू के कावेरी हॉस्टल के खचाखच भरे डाइनिंग हॉल में शाह बानो फैसले और सरकार के जवाबी कदम पर एक व्याख्यान भी दिया था। समान नागरिक संहिता की भाजपा की मांग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक विवाह, तलाक और अन्य मुद्दों की एक सामान्य परिभाषा नहीं होगी, जो विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के दायरे में आते हैं, तब तक इस तरह की संहिता बनाना असंभव होगा। 38 साल पहले उन्होंने जो कहा था, उसका अभी भी बहुत महत्त्व है- और भाजपा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जनता की राय जुटाना जारी रखा है, जिससे यह उसकी चुनावी रणनीति का केंद्र बन गया है। अब भारत के विधि आयोग, जिसने पहले एक रिपोर्ट में यूसीसी का विरोध किया था, ने एक नए अध्यक्ष, न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी के तहत, सरकार को एक नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हितधारकों से इनपुट मांगे हैं।
प्रोफेसर अहमद ने तर्क दिया कि विवाह हिंदुओं के लिए एक संस्कार है, यह मुसलमानों के लिए एक अनुबंध है, जिसे साथी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से औपचारिक रूप देते हैं। उन्होंने कहा कि तलाक को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद जगजाहिर हैं। इसलिए, उन्होंने कहा, विवाह और तलाक से संबंधित मुद्दे एक मानक परिभाषा के बिना असंगत रहेंगे जिसमें हर कोई शामिल है। इसके बिना, समान नागरिक संहिता के बारे में सभी बातें अत्यधिक विवादास्पद रहेंगी और सांप्रदायिक कलह को तेज करेंगी, यहां तक कि हिंसा भी भड़क उठेगी।
यूसीसी अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों द्वारा थोपे जाने वाले भयावह रूप में प्रतीत होता है जैसे कि उनकी पवित्र मान्यताओं को कुचलने के लिए। यही कारण है कि अहमद ने पार्टियों, नागरिक समाज और कानूनी बिरादरी सहित एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान के विचार का समर्थन किया, ताकि विभिन्न धर्मों के लोगों को सूचित किया जा सके कि उन्हें नागरिक कानूनों का विकल्प क्यों चुनना चाहिए। दरअसल, शाह बानो ने एक निजी मामले से उपजी शिकायतों के लिए न्याय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था।
चव्हाण और बोरकर ने विचारों की सराहना की, लेकिन दुखद रूप से, 2014 के बाद से, जेएनयू अधिकारियों ने इस तरह की वार्ता और चर्चाओं को प्रतिबंधित कर दिया है जैसा कि प्रोफेसर अहमद ने 1985 में दिया था। अब, छात्रों के लिए जेएनयू में हॉस्टल मेस में वक्ताओं को आमंत्रित करना लगभग असंभव है, क्योंकि भारत की बहुस्तरीय जटिलताओं के बारे में विचारों और विचारों को साझा करने की संस्कृति को अतीत में धकेल दिया जा रहा है।
आज, भाजपा लगातार यूसीसी को चुनावी चिंताओं के केंद्र में रख रही है और इसे अपने बहुसंख्यक एजेंडे में शामिल कर रही है। इसका मुकाबला करने और इसे हराने के लिए, प्रोफेसर अहमद का रुख महत्त्वपूर्ण है। उनके विचारों को अत्यधिक शानदार माना जाता था, और इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में चित्रित किया गया था, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय मुसलमानों के बीच सामाजिक स्तरीकरण के बारे में उनके मौलिक विचारों का हवाला दिया था।
विद्वत्ता के साथ संवेदनशीलता और सरोकार
प्रोफेसर अहमद की संवेदनशीलता ने उन्हें उम्र की बाधाओं से परे लोगों का प्रिय बना दिया। उत्कलमणि गोपबंधु दास पर 2015 के मेरे लेख को पढ़ने के बाद उन्होंने एक बार मुझे फोन किया, जिसमें मैंने 1872 के जापान कोड ऑफ एजुकेशन का उल्लेख किया था, जिसने बच्चों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना दिया। मैंने इस निर्णय और 1905 तक जापान की सैन्य और आर्थिक वृद्धि के बीच संबंध बताया था। वास्तव में, मैंने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की इस कोड पर उनकी पुस्तक, ‘पहचान और हिंसा’ से टिप्पणियों का उल्लेख किया।
महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि गोपबंधु दास के सहयोगी ने 1912 में जापान कोड ऑफ एजुकेशन पर चर्चा करने में सेन से पहले काम किया था। पुरी जिला शैक्षिक सम्मेलन में दिए गए एक भाषण में, दास ने समकालीन ब्रिटिश सरकार से शिक्षा में क्रांति लाने के लिए ओड़िशा और पूरे भारत के लिए इस तरह के कोड को पेश करने की मांग की।
प्रोफेसर अहमद, गोपबंधु दास के भाषण का स्रोत चाहते थे और जापानी कोड के अपने विद्वत्तापूर्ण ज्ञान और इसे पूरे देश में दोहराने की उनकी इच्छा के लिए प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह असाधारण है कि भारत के पूर्वी हिस्से में तैनात कोई व्यक्ति जापान और उसके शानदार उदय से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी से इतनी अच्छी तरह से लैस था। मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या गोपबंधु दास ने कभी जापान का दौरा किया था, और मुझे याद है कि उन्होंने उन्हें बताया था कि उन्होंने शायद ही कभी ओड़िशा छोड़ा था, हालांकि उन्होंने एक बार लाहौर का दौरा किया था।
अहमद और एफजी बेली का ओड़िशा के गांव का अध्ययन
जब मैंने 1979 में राजनीति विज्ञान में मास्टर के लिए जेएनयू में दाखिला लिया, तो प्रोफेसर अहमद ने मेरे बैच को राजनीतिक समाजशास्त्र पढ़ाया। पहली कक्षा में ही प्रत्येक छात्र को अपना परिचय देने के लिए कहा गया था, और जब मैंने कहा कि मैं ओड़िशा में पढ़ा हूं, तो उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या मैं कंधमाल जिले के बिसीपारा गांव के बारे में जानता हूँ। जब मैंने कहा कि मैं एक बार इससे गुजर भी चुका हूँ, तो उन्होंने कक्षा को सूचित किया कि प्रोफेसर एफजी बेली, एक ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञानी (स्कूल ऑफ अफ्रीकन एंड ओरिएंटल स्टडीज) ने 1950 के दशक में इसकी सामाजिक संरचना का अध्ययन किया था। उस अध्ययन ने जांच की कि कैसे राज्य, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के नए रूप पारंपरिक शक्ति और यथास्थिति को बदल रहे थे। यह प्रोफेसर अहमद की विशाल शैक्षणिक प्रोफ़ाइल के बारे में मेरा पहला अनुभव था, जिसे मैंने जेएनयू में अपने समय के दौरान अधिक से अधिक खोजा था।
धर्मनिरपेक्षता और समग्र संस्कृति के लिए आशावादी
दुर्भाग्य से, नफरत फैलाने वालों ने प्रोफेसर अहमद को उनकी धार्मिक पहचान, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और प्रगतिशील विचारों के लिए निशाना बनाया। वह तर्कसंगत और आलोचनात्मक रूप से सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए धर्मों और समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि की अपनी गहरी समझ का उपयोग करेंगे। एक बार, उन्होंने मुझे बताया कि महाभारत टीवी धारावाहिक शिक्षाप्रद था क्योंकि इसने दुनिया के विचारों को रोशन किया था और कामना की कि महाकाव्य से अधिक सबक प्राप्त करने के लिए अन्य एपिसोड प्रसारित किए जाएं।
उनकी विरासत छात्रों और शिक्षाविदों की आगे की पीढ़ियों को बनाए रखेगी और प्रेरित करेगी। पिछले साल 28 मई को फॉरवर्ड प्रेस के पत्रकार अभय कुमार के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने आशावादी रूप से कहा था, “भारत बहुत जल्द धार्मिक उन्माद के इस दौर से उबर जाएगा।” उन्होंने कहा, “धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और मिलीजुली संस्कृति कायम रहेगी… यह कठिन समय जल्द ही बीत जाएगा।”
अभय कुमार कहते हैं, “प्रोफेसर अहमद के काम और विचारों से परिचित किसी भी व्यक्ति को इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि वह भारत में जो अच्छा है उसका प्रतीक है – धर्मनिरपेक्षता, समग्र संस्कृति, तर्कसंगतता और समानता की तलाश। मुझे, और मेरे पहले और बाद में उनके छात्रों की पीढ़ियों को इस तरह के एक महान शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया था- मैं उनके लिए इससे बेहतर श्रद्धांजलि के बारे में नहीं सोच सकता।
(लेखक राष्ट्रपति केआर नारायणन के विशेष कार्याधिकारी रह चुके हैं)
अनुवाद : रणधीर गौतम
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.