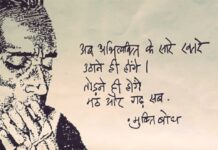— ध्रुव शुक्ल —
तेजी से बदलती दुनिया में जुल्म और लूट के नये रिवाजों के बीच करोड़ों लोग बेबस जीवन गुजार रहे हैं। अचानक कहीं आग लग जाती है और कहीं गोली चल जाती है। लोग निर्वासित होकर भाग रहे हैं। उन्हें राहत शिविरों में जगह नहीं मिल रही। शासक कह रहे हैं – आल इज वेल।
दुनिया में बसे देशों का जीवन मज़हबों के रचे पाखण्ड, राजनीतिक जनमत की लूट और नये कामुक बाज़ार की अश्लीलता और तानाशाही के क्लेशों में घुट रहा है। शासक कह रहे हैं – आल इज वेल।
लोगों की आस्था, विश्वासों और हुनर से छल करके उनकी स्वतंत्रता छीनने वाली शक्तियां आतंक, युद्ध और महामारियों की रचना कर रही हैं। जीवन के सत्य को पीछे छोड़कर कृत्रिम और नकली दुनिया बसायी जा रही है। शासक कह रहे हैं – आल इज वेल।
जीवन में क्रूरता बढ़ रही है। आये दिन लोग प्रेमिका, पड़ोसी और दोस्तों की लाशें बोरों में भरकर फेंक रहे हैं। असहाय बूढ़े, स्त्रियां और बच्चे निर्दयता के आगे बेबस हैं। अदालतों में न्याय स्थगित है। शासक कह रहे हैं – आल इज वेल।
समवेदना सिकुड़ती जा रही है। राह चलते लोग खुलेआम होते अत्याचार का सामना करने से कतरा रहे हैं। वे दूर खड़े होकर अपने मोबाइल पर हत्या की फिल्म बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी कायरता का प्रचार कर रहे हैं। शासक कह रहे हैं – आल इज वेल।
नस्ल और जातियों के पिछड़ेपन में डूबे लोग समाज होने का दंभ पालकर अपना स्वार्थ साधने के लिए बड़ी-बड़ी पंचायतें तो लगाते हैं पर उन्हें अपना पूरा देश और दुनिया नहीं दीख रही। शासक कह रहे हैं – आल इज वेल।
लोगों को बैर पालने के लिए उकसाया जा रहा है, विषमता मिटाने के लिए नहीं। प्रेम के सेतु ढहाये जा रहे हैं। साथ जीने-मरने के अरमान कम होते जा रहे हैं। लोग अकेले होकर जी नहीं पा रहे। शासक कह रहे हैं — आल इज वेल।
जीवन की छोटी-छोटी पगडण्डियों के खिलाफ बनी नयी लम्बी सड़कें बीच राह में धॅंस रही हैं। सूखती जा रही नदियों पर बने पुल टूट रहे हैं। बढ़ते तापमान में बर्फ़ पिघल रही है। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। पर्वतों पर चढ़ने वाले विजेता ऊंची चोटियों पर कचरा छोड़कर लौट रहे हैं। पृथ्वी पर घूरों की ऊंचाई पर्वतों की बराबरी कर रही है। – शासक कह रहे हैं – आल इज वेल।
शासक ही अपनी-अपनी सेना रचकर एक-दूसरे पर चढ़ाई करके जीवन को कुचल रहे हैं और शासक ही कह रहे हैं – आल इज वेल।
——
राजनीतिक दलों का कमला सर्कस
अपने देश के राजनीतिक दलों की हालत देखकर कमला सर्कस की याद आती है। बरसात के दिनों में हमारे शहर सागर के कजलीवन के मैदान में इस सर्कस का बहुत बड़ा तम्बू गाड़ा जाता था। सर्कस देखने के लिए तम्बू के सामने मचे कीचड़ को पार करके जाना पड़ता था। इस सर्कस में आगे बैठने के लिए कुर्सी क्लास और पीछे बैठने के लिए जनता क्लास के नाम से ही टिकट बेचे जाते थे।
जनता लकड़ी के पटियों से बनी गैलरी में बैठती थी। कभी पटिए खिसक कर गिरते तो जनता के हाथ-पांव टूट जाते, सिर भी फूट जाते। कुछ ज़्यादा पैसे का टिकट खरीदकर कुर्सी पर सुरक्षित बैठे लोग बेगाने-से लगते।
सर्कस की शुरुआत ऊपर झूलों पर झूलते करतबियों से होती। वे बिना चूके एक-दूसरे को अपने हाथ देकर और अपने शरीर को लय-ताल में साधकर झूलते। कभी कोई हाथ देने से चूक जाता तो नीचे बॅंधी जाली पर गिरता और फिर ऊपर चढ़कर सबके साथ झूलने लगता। गांधी और नेहरू के ज़माने के राजनीतिक लोग ऐसे ही थे। वे मिलकर उन सपनों में झूला झूल रहे थे जिन्हें आज़ादी के बाद देश की ज़मीन पर और जीवन में साकार किया जाना था। वे असहमत होकर भी एक-दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते थे।
आज का राजनीतिक सर्कस ज़मीन पर कुछ और ही दीख रहा है। जिसमें हाथी अपनी सूंड नीची करके रिंग मास्टर के आगे खड़े हैं। हाथी ही नहीं, अपने-अपने पिंजरों से निकलकर बेबस गुर्राते शेर रिंग मास्टर के कोड़े की तरफ़ देखकर चुपचाप अपने-अपने स्टूल पर बैठ जाते हैं। फिर रिंग मास्टर के ही इशारे पर अपने पिंजरों में वापस चले जाते हैं। इस राजनीतिक सर्कस के हाथी और शेर दिनों-दिन दुबले होते जा रहे हैं। वे तृण-मूल को तरस रहे हैं।
सर्कस में दो पहिए की साइकिल बंदर चलाते हैं। पटियों पर बैठी जनता उन्हें देखकर हॅंस देती है। फिर पीछे से सिर्फ़ एक पहिए की खूब ऊंची साइकिल पर बैठकर कोई करतबिया आता है और बंदर भभकती लालटेन के धुंधले उजाले में अपनी दो पहिए की साइकिल का पंचर सुधारने लगते हैं। उस एक पहिए की ऊंची साइकिल के नीचे चार पहिए वाला लोकतंत्र उस बौने जोकर की तरह लगता है जो छोटी-सी खिलौना गाड़ी में मुर्गी को जोतकर आता है। उस पर हॅंसते हुए लोगों की हॅंसी कितनी बेबस जान पड़ती है। यह राजनीतिक कमला सर्कस देखकर लगता है कि अब कोई जग को खुलकर हॅंसा नहीं पा रहा। सब मिलकर रुला रहे हैं।
ए भाई, जरा देख के चलो
आगे ही नहीं, पीछे भी,
दायें ही नहीं, बायें भी,
ऊपर ही नहीं, नीचे भी….
—–
बाज़ार के रास्ते पर धर्म और राजनीति
देश में कहीं भी देखो तो धर्म और राजनीति के मंच और पण्डाल ऐसे सजे-धजे दिखते हैं जैसे कोई बम्पर सेल लगी हो।
एक ज़माने में बीच बजरिया में अपनी दूकान पर शुभ-लाभ लिखकर बैठे महाजन की सादगी लोगों के मन में उसके प्रति ईमान का भाव जगाती थी। कपास के फूलों जैसे सुकोमल और उज्ज्वल संत-संन्यासियों के प्रति मन श्रद्धा से भर उठता था। लोकहित की भावना से भरे उजली खादी पहने नेता जब घर-घर जाकर मतदान का आग्रह करते तो उन पर विश्वास होता था।
अब बाज़ार की चकाचौंध में महाजन संदेह के घेरे में है। वह प्राकृतिक साधनों और देश की संपदा का बेजा इस्तेमाल करके और अपना घर भरके जीवन से कभी दूर न होने वाली विषमता बढा रहा है। छद्मवेशधारी साधु जनों के आसपास अंधश्रद्धा का ॲंधेरा छाया हुआ है। अब साधुओं के सान्निध्य में ज्ञान के नाम पर केवल अदृश्य भाग्य की झूठी दिलासा ही मिलती है। कर्म के नाम पर केवल अर्थहीन पूजा का पाखण्ड और भक्ति के नाम पर फिल्मी पैरोडियों का शोर सुनने को मिलता है। राजनेताओं की विश्वसनीयता दिनों-दिन घटती जा रही है। नेता अब किसी के घर नहीं आते, वे लकदक परिधान बदल-बदलकर रोड-शो करते हैं, दूर से हाथ हिलाते हैं। उजड़े हुए अतीत के मोह में फॅंसे और वर्तमान से बेख़बर नेता अभी तक न आये अच्छे दिनों का सपना दिखाते रहते हैं।
बाज़ार की लूट में मुफ़्तखोरी का लालच एक बहुत बड़ा औजार है। वह एक चीज़ का मुफ़्त लालच देकर दो चीज़ें बेच देता है – बाय टू, गेट वन फ्री। तथाकथित धार्मिकों ने भी बाज़ार से सीखकर यही रास्ता अपना लिया है – मंदिरों के कारिडोर किसी बड़े मॉल जैसे लगने लगे हैं। जहां देव प्रतिमा दर्शन, आरती, अभिषेक के लिए हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं। आप दर्शन और पूजा खरीदिए और भगवान भरोसे का भाग्य मुफ़्त में ले जाइए। राजनीति में भी यही हाल है। आप जाति और सम्प्रदाय के दो नेता चुनिए और अपने खाते में एक हज़ार रुपये मुफ़्त में डलवा लीजिए।
जीवन में अपने-अपने धर्म का ज्ञान, नेतृत्व में सद्भाव का प्रतिमान और बाज़ार में मुनाफे का ईमान डगमगा रहा है। यह नकली प्रतिभा गढ़े जाने का समय है। अब रोबोट मीडिया के स्वयंभू चौथे खम्भे पर चढ़कर न्यूज़ पढ़ने लगे हैं। कुछ दिनों में हरि-कथा भी बॉंचने लगेंगे। नेतागिरी भी करने लगेंगे। कई देशों के नेता तो बाज़ार की शक्तियों द्वारा नियुक्त रोबोट जैसे ही लगने लगे हैं।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.