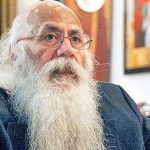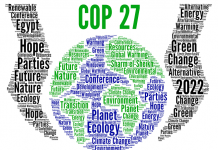— अरुण कुमार —
आज की अनिश्चितता भरी और तेजी से बदलती दुनिया में पांच साल बाद क्या होगा कौन जानता है! किसे मालूम था कि 2020 में कोविड महामारी आएगी और 2022 में यूक्रेन युद्ध होगा? फिर भी प्रधानमंत्री ने भारत के लिए 2047 का एक लक्ष्य तय किया है, कि भारत तब तक विकसित देश बन जाएगा। भारत जीडीपी के मामले में जर्मनी और जापान से आगे निकलने वाला है, बशर्ते वह वह जीडीपी की अपनी मौजूदा दर को बनाए रखे।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट चन्द्रयान-3 की सफल लैंडिंग निस्संदेह देश की एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन उससे भारत एक विकसित देश नहीं बनता।
देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि सबको अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा सेवा मुहैया कराना। यह तभी किया जा सकता है जब ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों तथा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में काफी इजाफा हो।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की सफलता यह दिखाती है कि भारत इससे भी ज्यादा बहुत कुछ कर सकता है बशर्ते वह लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखे। इसरो की सफलता यह भी दर्शाती है कि भले हम चांद पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन रोजमर्रा के मसलों की अनदेखी कर रहे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना, विकसित देश बनने के लिए जरूरी है, जैसे कि सभी के लिए स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई की सुविधा।
अगर 2024 की राह में कुछ अप्रिय घटित नहीं होता है तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता रहेगा। महामारी से पहले घोषित वृद्धि दर 8 फीसद से 3.9 फीसद पर आ गयी थी, और औसतन 6 फीसद रही है।
अगर वृद्धि दर 2047 तक 6 फीसद के आसपास लगातार बनी रहती है तो भारत का सकल घरेलू उत्पादन मौजूदा 3.7 खरब (ट्रिलियन) डॉलर से बढ़कर 4.05 गुना हो जाएगा, यानी 15 खरब डॉलर। लेकिन तब भी वह अमेरिका (25 खरब डॉलर) और चीन (18 खरब डॉलर) से बहुत पीछे होगा। फिर, यह मान लेने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी अगले चौबीस वर्षों में अपने आकार में इजाफा करेंगी, और इस तरह वे भारत से काफी आगे बनी रहेंगी।
अनुमान है कि 2047 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.65 अरब हो जाएगी। लिहाजा उस समय प्रतिव्यक्ति आय होगी 9,000 डॉलर। उच्च आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में आने के लिए, अभी विश्व बैंक के पैमाने के मुताबिक, प्रतिव्यक्ति आय होनी चाहिए 14,000 डॉलर। लिहाजा, भारत बहुत हुआ तो निम्न मध्य आयवर्ग से ऊपर उठकर उच्च मध्य आयवर्ग वाले देशों की श्रेणी में आ सकता है। अगर वृद्धि दर औसतन 8 फीसद लगातार बनी रहे, तभी जाकर 2047 तक भारत की प्रतिव्यक्ति आय 14,000 डॉलर पर पहुंच पाएगी।
8 फीसद की वृद्धि दर तो बहुत दूर, 6 फीसद की वृद्धि दर भी 24 वर्षों तक लगातार बनाए रखना काफी मुश्किल होगा। महॅंगाई की मौजूदा ऊंची दर, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती और आपूर्ति से संबंधित अड़चनें 6 फीसद की वृद्धि दर की राह में बड़ी बाधा बनेंगी। फिर, वृद्धि की राह को सुगम बनाने के लिए, असंगठित क्षेत्र को हाशिए पर ले जाने वाली मौजूदा नीतियों को काफी बदलना होगा।
और अगर भारत की प्रतिव्यक्ति आय 2047 में 14,000 डॉलर पर पहुंच भी जाती है, तो क्या भारत विकसित देश बन जाएगा? कुवैत और ब्रूनेई जैसे तेल उत्पादक देशों की प्रतिव्यक्ति आय लंबे समय से काफी अधिक है। वे धनी देश तो हैं पर विकसित देश नहीं। क्योंकि विकसित देश वह है जो टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ा हुआ है और इस मामले में अपने को लगातार प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में समर्थ है। वह अपनी समस्याएं सुलझाने में गतिशील रहता है और वैश्विक पटल पर बराबरी की शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है।
भारत इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि यह उच्च तकनीक वाले उत्पादों के आयात पर काफी निर्भर है। बेशक इसने अधिकतर विकासशील देशों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन इसका कार्य व्यापार अमूमन मध्यम और उससे नीचे की श्रेणी की तकनीक के जरिए होता है। भारत अधिकांशतः कम कीमत वाली चीजें निर्यात करता है, आयात ज्यादा कीमत वाली चीजों का करता है। नतीजतन भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है।
जिन देशों के पास उत्कृष्टतम तकनीक है वे उसे साझा नहीं करते। लिहाजा भारत को इसे अपने दम पर विकसित करना पड़ेगा।
तकनीकी गतिशीलता के पीछे कई बातें होती हैं। पहली, जैसा कि “शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट” (एएसईआर) बताती है, देश में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी ओर, उच्च शिक्षा के कुछ ही संस्थान अधुनातन अनुसंधान में मुब्तिला हैं।
खराब स्कूली शिक्षा के फलस्वरूप जो आधार तैयार होता है वह कमजोर होता है, जो विद्यार्थी निकलते हैं वे अधुनातन अनुसंधान के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं होते। अपेक्षित दर्जे से कमतर अनुसंधान का अर्थ है कि शिक्षक और स्कूली शिक्षा के लिए ज्ञानात्मक आधार, दोनों कमतर गुणवत्ता के बने रहते हैं।
दूसरे, भारत की गरीबी को देखते हुए (भारत जी-20 का सबसे गरीब देश है), प्रतिभाओं के विकास और प्रतिभावान शोधकर्ताओं तथा शिक्षकों से काम लेने के लिए, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था पर होने वाला खर्च एक अहम सवाल है।
तीसरे, अच्छे शिक्षण और शोध के लिए प्रतिबद्धता भी, ज्ञान सृजन के प्रोत्साहन के लिए बहुत मायने रखती है। चौथा, टेक्नोलॉजी खुद तकनीकी और सामाजिक स्तरों पर ढेर सारी संभावनाएं निर्मित करती है, और इसके चलते भविष्य का ठीक-ठीक नक्शा बनाना असंभव होता है।
वर्ष 2000 से पहले, लोग चिट्ठियां लिखते थे और तार भेजते थे, लेकिन अब वह लगभग इतिहास की बात है। लोग पैसा निकालने या जमा करने के लिए बैंक जाते थे लेकिन अब वे इसे इंटरनेट और एटीएम के जरिए करते हैं। ई-कॉमर्स का फैलाव हुआ है और स्थानीय दुकानदारों को इससे नुकसान हुआ है।
वर्ष 2022 में ‘लार्ज लर्निंग मॉडल’ ने एक अप्रत्याशित चुनौती पेश कर दी। यह मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सृजन करने के लिए बुनियादी गणना प्रक्रिया है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फलक को इस हद तक बदल दिया है कि इसके डेवलपर्स अद्भुत क्षमताओं के मालिक बन गये हैं और जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे वे खुद भी अब मॉंग करने लगे हैं कि आगे इसके विकास पर रोक लगा दी जाए क्योंकि इसने मानवता के सामने अस्तित्वगत खतरा पैदा कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वचालन (आटोमेशन) और यंत्रीकरण न केवल अर्धकुशल बल्कि कुशल कामगारों के लिए भी मुश्किलें पेश कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि, कौशल वाले बहुत-से रोजगार, जैसे कि शिक्षकों के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।
तकनीकी तरक्की के लिए यह जरूरी है कि अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में निवेश किया जाए। लेकिन यह जोखिम भरा है क्योंकि इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं है और इस बात की भी संभावना है कि जो भी हासिल हो वह तकनीकी परिवर्तन की तेज रफ्तार के कारण प्रचलन से बाहर हो जाए। ऐसे में निवेशक किये गए अपने निवेश का फल पाने से वंचित रह जा सकते हैं।
विकासशील देशों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में निवेश और भी जोखिम भरा है। इस मामले में उनके प्रयासों को नवीनतम तकनीक के आयात से धक्का पहुंच सकता है। यह भारत में बहुत बार हुआ है कि आर एंड डी का पौधा पनपने से पहले ही मुरझा गया। नब्बे के दशक के आरंभ में बड़े डिजिटल एक्सचेंजों के आयात से सेंटर फॉर डिवेलपमेंट के प्रयासों को धक्का लगा था। आर एंड डी के प्रोत्साहन में इस बात की भूमिका अहम है कि नीति क्या है। नीति ही स्थायी माहौल और सरकारी आवंटन मुहैया कराती है। यह आवश्यक है कि देश के पास एक रणनीतिक दृष्टि हो जो यह चिह्नित करने में मदद करे कि किन क्षेत्रों को बाहरी दबावों से बचाया जाए और किन क्षेत्रों को उनकी नियति पर छोड़ दिया जाए।
रणनीतिक दृष्टि के लिए राजनीतिक सर्वसम्मति की जरूरत होती है। ऐसे माहौल में जहॉं भाई-भतीजावाद का बोलबाला है, शक और अविश्वास के चलते आम सहमति बन पाना मुश्किल होता है। एक नया विज़न जरूरी है, जो तकनीकी परिवर्तनों का खमियाजा भुगत रहे हाशिए के तबकों की चिंताओं की सुध ले।
ऊपर बताया गया है कि किन वजहों से काफी अनिश्चितता पैदा होती है और आगे की योजना बनाना कठिन होता है, ऐसे में हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तीव्र परिवर्तनों का मुकाबला करना सीखें।
तकनीक ज्ञान है। तकनीक की तरक्की के लिए नया ज्ञान पैदा होना जरूरी है। यह अधिकांशतः उच्च शिक्षा के संस्थानों में और उत्पादन के दौरान होता है। अमूमन उत्पादन के संस्थान, उच्च शिक्षा के संस्थानों का मुंह जोहते हैं, इस बात के लिए कि वे नया ज्ञान पैदा करें जिसका व्यावसायिक लाभ उठाया जा सके। मसलन कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीके का विकास या तीव्रतर कंप्यूटर और मोबाइल फोन के लिए एडवांस्ड सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स।
समाज के लिए यह जरूरी है कि वह नवाचार और नए ज्ञान सृजन के अनुकूल वातावरण बनाए। यह तभी हो सकता है जब शोधकर्ताओं को नए विचार पेश करने की आजादी हो, यानी उन्हें ऐसी स्वायत्तता दी जाए कि वे अपनी धुन में लगे रह सकें, भले वे विफल साबित हों। चंद्रयान-3 की सफलता के पीछे चंद्रयान-2 की विफलता से मिला सबक था।
नौकरशाही के नियंत्रण के जरिए स्वायत्तता के पर कतरने से शोधकर्ता कुंठित व निराश होते हैं और उनकी पहल का दम घुट जाता है, जिससे नए ज्ञान सृजन को धक्का पहुंचता है। दुर्भाग्य से, उच्च शिक्षा और अनुसंधान की बहुत कम संस्थाएं शिक्षकों और शोधार्थियों को अपेक्षित स्वायत्तता देती हैं।
अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में भले भारत का प्रदर्शन बढ़िया है लेकिन सामान्य तौर पर देखें तो तस्वीर इससे भिन्न है, और इससे भारत को एक विकसित देश बनाने का काम और कठिन हो जाता है, प्रतिव्यक्ति आय बढ़ जाए तब भी।
(The Leaflet से साभार)
अनुवाद : राजेन्द्र राजन
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.