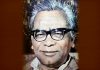— चंद्रभूषण —
सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित रिपोर्टों को 21वीं सदी के कुछ आम रुझानों के साथ जोड़कर देखें तो पूर्वी लद्दाख से सियाचिन तक चार साल लगे भारत और चीन के युद्ध-तत्पर जमावड़े के लिए सिर्फ जमीन के कुछ बेहद ठंडे, बंजर टुकड़ों पर परस्पर टकराती दावेदारियां ही जिम्मेदार नहीं हैं। चीन की तरफ से पलटनों और हर्बे-हथियारों का लांग-टर्म मूवमेंट भी सिर्फ तिब्बत तक सीमित नहीं है। तीन विशाल पश्चिमी प्रांत शिनच्यांग, चिंघाई और तिब्बत क्षेत्रफल में इस देश का 38 फीसदी हिस्सा बनाते हैं। तीनों में ही जबरदस्त सैन्य तैयारियां देखी जा रही हैं।
चीन के लिए पूर्वी लद्दाख और सियाचिन की जमीनें खुद में कोई बेशकीमती चीज नहीं हैं। सियाचिन का महत्व उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण राजमार्गों के चौराहे जैसा है। आगे उसकी योजना इसे तिब्बत और शिनच्यांग से गुजरती हुई, पाकिस्तान से होते हिंद महासागर से जुड़ रही रेल लाइनों और तेल-गैस पाइपलाइनों का जंक्शन बनाने की भी है। उसे डर इस बात का है कि भारत अपनी बेहतर सामरिक स्थिति का इस्तेमाल कहीं इस योजना को नाकारा बनाने और चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) में अड़ंगे लगाने में न करे।
यह कॉरिडोर पाक अधिकृत कश्मीर से गुजर रहा है, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान ने बिना अपना अधिकार स्पष्ट किए ही चीन को सौंप दिया है। भारत का इस पर सवाल उठाना न्यायसम्मत है। चीन की कोशिश इस मुद्दे पर लंबे समय के लिए पोजिशनिंग करने की है, जिसके लिए उसने बहाना यह खोज रखा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें और पुल बनाकर भारत ने यथास्थिति का उल्लंघन किया है। दूरगामी रूप से देखें तो यह पश्चिम की ओर अपना दखल बढ़ाने की एक लंबी चीनी चिंता का हिस्सा है, जिसके एक पहलू- हिंद महासागर में सीधी निकासी को हम अच्छी तरह जानते हैं।
अभी पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में जापान, ताइवान या सीधे अमेरिका से टकराव की स्थिति में कच्चे तेल जैसी रणनीतिक महत्व की चीजों की सप्लाई बंद हो जाने का डर चीन को सारी दिक्कतों के बावजूद पाकिस्तान के बीच से एक व्यापारिक गलियारा खोलने के लिए मजबूर कर रहा है। उसकी योजना इस गलियारे के बहुविध इस्तेमाल की है, लेकिन ईरान से तेल और कतर से गैस की पाइपलाइनें अपने यहां लाना उसका सबसे बड़ा मकसद है।
अभी अमेरिका के लिए किसी टकराव की स्थिति में चीन को घुटनों पर लाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए उसे सिंगापुर के पास मलक्का जलडमरूमध्य का रास्ता चीनी तेल टैंकरों के लिए कुछ समय तक बंद कर देना होगा। खाड़ी की पाइपलाइनें खुल जाने पर नाकेबंदी का यह काम बहुत कठिन हो जाएगा। बहरहाल, चीन की व्यापक रणनीति में सीपीईसी को एक सीमा से ज्यादा वजन देना गलत होगा। उसकी असल समस्या है हू लाइन या हेइहे-तंगछुंग लाइन, जो अपने निर्धारण के समय, 1935 से ज्यों की त्यों बनी हुई है।
भौगोलिक जनसांख्यिकी विशेषज्ञ हू ह्वानयुंग ने 1935 में चीन के नक्शे पर पूर्वी रूस के करीबी चीनी शहर हेइहे और बर्मा के नजदीकी चीनी शहर तंगछुंग को जोड़ती एक तिरछी रेखा खींचकर बताया था कि इस रेखा के पूरब में देश के 36 प्रतिशत क्षेत्रफल में 96 प्रतिशत चीनी आबादी रहती है, जबकि इसके पश्चिम में मौजूद देश के कुल 64 प्रतिशत रकबे में मात्र 4 फीसद चीनियों का वास है। तब से अब तक गुजरे 85 वर्षों में मंगोलिया के अलग देश बन जाने से पश्चिमी इलाके का रकबा 57 प्रतिशत रह गया है और आबादी तमाम कोशिशों के बावजूद 6 प्रतिशत हो पाई है, जबकि हू लाइन से पूरब के 43 फीसद इलाके में 94 प्रतिशत चीनी रह रहे हैं।
यहां एक बात और जोड़ दें कि कीमती खनिज और गरीब अल्पसंख्यक समुदाय भी ज्यादातर हू लाइन के पश्चिम में ही हैं। इधर पड़ने वाले चीनी प्रांत कौन से हैं? कुछ छूटे-फटके इलाकों को छोड़ दें तो इस 57 फीसदी चीनी क्षेत्रफल में से 52 फीसदी, यानी चीन का आधा से ज्यादा एरिया उसके चार पिछड़े प्रांतों तिब्बत, चिंघाई, शिनच्यांग और इनर मंगोलिया का है। चीन का शीर्ष नेतृत्व पिछले कुछ सालों में कई बार कह चुका है कि उनके लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हू लाइन पार करने का, यानी इस लाइन के दोनों तरफ आबादी का संतुलन बनाने का है।
पश्चिम में कई रेलवे लाइनें इस सोच के तहत ही बिछाई गई हैं, जिनमें दो पर बुलेट ट्रेनें भी चलने लगी हैं। चीन का लगभग सारा कच्चा तेल तारिम बेसिन से निकाला जाता है, जो कश्मीर के उत्तर में पड़ने वाले उसके पश्चिमी सीमाप्रांत शिनच्यांग में पड़ता है। उसकी योजना सीपीईसी से आने वाली तेल-गैस पाइपलाइनों को यहीं के काशगर शहर में लाकर उसके बने-बनाए पेट्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाने की है।
चिंघाई में मौजूद नमक की झीलों में लीथियम और दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं, जिसके लिए इनपर पूरी दुनिया की नजर रहती है। इस सबके बावजूद चीन की पुरबिया बहुसंख्यक आबादी इधर आने से बचती है, क्योंकि यहां की मूल निवासी तिब्बती, उइगुर, हुई और मंगोल जनता उसके प्रति सहज नहीं है। फिर भी, संतुलन तेजी से बदल रहा है और अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के न्यिंगची उपप्रांत में घूमते हुए मेरी मुलाकात नए-नए बसे घुमंतू पशुचारी समुदायों के अलावा चीनियों से ही हो पाई। तिब्बत के पारंपरिक नैन-नक्श यहां दस-बीस में से एक व्यक्ति में ही दिखते हैं।
जैसे-जैसे चीन में निर्यात आधारित आर्थिक वृद्धि का सूरज ढल रहा है, वैसे-वैसे अपना घरेलू बाजार बढ़ाना उसके लिए जरूरी होता जा रहा है। इसका सीधा तरीका अपने प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम दोहन और घनी आबादी वाले इलाकों से लोगों को हटाकर उन्हें विरल आबादी वाले इलाकों में बसने का है। पश्चिम के रेगिस्तानी, पठारी और अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले क्षेत्र इन दोनों कामों के लिए बहुत मुफीद हैं। यहां खदानों, तेल कुओं, सोलर फार्मों और तेजरफ्तार गाड़ियों के जरिये लोगों को लुभाने के लिए चीन जो कुछ कर सकता था, कर चुका है। इससे आगे का रास्ता अंध-राष्ट्रवाद का है।
यानी ऐसा प्रचार कि उसका अश्वमेध का घोड़ा पश्चिमी मुल्कों ने और उनके निकट सहयोगी भारत ने पकड़ रखा है। उसे छुड़ाने के लिए सारे चीनी एकजुट हो जाएं। इस नीति के तहत ही आज दुनिया न्यिंग्ची, न्गारी, खोतान और गोलमुद जैसे शहरों के नाम जानने लगी है, जो देखते देखते तिब्बती और तुर्क इलाकों से बदलकर चीनी शहर बन गए हैं। यह भारत के उत्तर में अचानक एक नया देश बस जाने जैसा है, जिससे उसे सिर्फ दो-चार दिन के लिए लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि हर मौके पर हर रोज जूझना पड़ सकता है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.