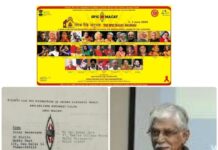— प्रेमकुमार मणि —
आम्बेडकर पर भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी को मैंने देखा-सुना. मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई आपत्तिजनक बात की गई है. बहस भारतीय संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे होने पर आयोजित विशेष चर्चा के दौरान हो रही थी. मैंने जितना देखा-सुना है, उसके आधार पर कह सकता हूँ संसद की बहस बेजान है. इसे आयोजित करने का कोई मतलब नहीं है. लेकिन संसद को और कोई काम भी तो नहीं है!
आज जब इसे लेकर धरना-प्रदर्शन और शोर- शराबा की खबरें देखीं तब पलट कर शाह के वक्तव्य को देखा. तकनीक के ज़माने में यह संभव है. मैंने जितना देखा, शाह बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकारें आम्बेडकर पर उदासीन बनी रहीं. जबकि भाजपा ने उन्हें प्रतिष्ठित स्थान देने पर ध्यान दिया. इसी प्रसंग में उन्होंने कहा कि केवल आंबेडकर-आम्बेडकर नाम लेने से कुछ नहीं होता. विपक्ष का कहना है कि आम्बेडकर का कई बार नाम लेना उन्हें अपमानित करना हुआ. मैंने जो क्लिप देखा उसमें दो बार नाम लिया गया है. मुझे बताया गया है किसी क्लिप में पांच या छह बार नाम दुहराया गया है. यानि मामला दो और छह का है. तकनीकि छेड़-छाड़ से दो को छह या छह को दो करना संभव है, इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि कौन सही है. लेकिन अपनी सुविधा केलिए मैं छह वाले को ही सही मान लूँ तो क्या अर्थ निकलता है, इस पर बात करना चाहूंगा. शाह उन आंबेडकरवादियों को लक्ष्य कर रहे थे, जो नाम तो लेते हैं आंबेडकर का, लेकिन उन्हें ले कर कोई काम नहीं करते. इसमें छह या दस बार भी नाम लेने में बुरा क्या है? लक्ष्य आंबेडकर नहीं, उनके नाम की माला जपने वाले हैं. शायद इसे ही मुहावरे में बात का बतंगड़ बनाना कहते हैं. विपक्ष यही कर रहा है. वह इतना घोंचू है कि यह भी नहीं समझ रहा कि इस रूप में वह भाजपा के राजनीतिक जाल-फांस में उलझ कर रह गया है. आंबेडकर और अपने संबंधों पर कांग्रेस जितना बहस करेगी वह उलझती जाएगी. इस मुद्दे पर न केवल कांग्रेस बल्कि लालू प्रसाद जैसे लोकदलियों और वामपंथियों को भी ध्यान देना चाहिए.
आंबेडकर विमर्श को हमें इतिहास के पार्श्व में ले जाकर देखना चाहिए. आंबेडकर 1930 के दशक में भारतीय सामाजिक जीवन में चर्चित हुए. उनकी सामाजिक गतिविधियां पहले से चल रही थीं. वह विद्वान राजनेता थे. महाराष्ट्र से थे, जहाँ सामाजिक नवजागरण की एक समृद्ध परंपरा पहले से ही थी. बल्कि जिस बंगला नवजागरण की चर्चा इतिहास में होती है उससे कहीं अधिक मजबूत नवजागरण की परंपरा महाराष्ट्र में थी. आंबेडकर इसकी शृंखला में थे. वह इस विचार के थे कि बदलाव पहले समाज में हो, फिर राजनीति में; या फिर दोनों साथ-साथ हो. राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकांश लोग इस मत के थे कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधार के आंदोलन को स्थगित किया जाना चाहिए. आंबेडकर उस सामाजिक समूह से थे जो दोहरी गुलामी झेल रहा था. सामाजिक अवमानना की ऐसी स्थिति थी, जिनके कारण सामान्य नागरिक जीवन में उनके प्रवेश निषिद्ध थे. जैसे अमेरिका और यूरोप के कुछ मुल्कों में अफ़्रीकी नीग्रो लोगों की स्थिति थी. इस स्थिति में उनकी पहली गुलामी अपने ही कुलीन देशवासियों से थी, जिन पर ब्रिटिश राज कर रहे थे. ब्रिटिश या उसके पहले के मुग़ल-तुर्क उन पर सीधे शासन नहीं कर रहे थे. वे उनके गुलामों के गुलाम थे. इसलिए उन्हें सामाजिक बदलाव की जरूरत पहले थी. इस परिप्रेक्ष्य में उनकी समझ और उनके विचार औरों से भिन्न थे. जैसे कोरेगांव प्रसंग को तिलक ने अपनी गुलामी का प्रतीक माना, जबकि आंबेडकर ने अपनी मुक्ति का. क्योंकि कोरेगांव (1 जनवरी 1818 को पेशवा सैनिकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया युद्ध जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई. इस लड़ाई के बाद पेशवा राज का अंत हो गया. कंपनी सेना में लगभग दो तिहाई दलित महार सैनिक थे. इससे यह प्रमाणित हुआ कि महार भी मार्शल प्रजाति है.) की जीत अंग्रेजी सेना के साथ दलित अस्मिता की भी जीत थी. यह आंबेडकर की इतिहास-दृष्टि थी.
आंबेडकर ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने उसमें दलित-प्रसंग को जोड़ा. कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ 1916 में ही एक समझौता किया हुआ था कि ब्रिटिशराज द्वारा स्थापित धारासभाओं में उनके लिए अलग स्थान सुरक्षित किये जाएंगे. साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद लंदन में आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आंबेडकर ने दलितों केलिए भी पृथक आरक्षण की मांग की. वहाँ उपस्थित गांधी ने इसका विरोध किया. गांधी का मानना था कि इससे हिन्दुओं की एकता का बिखराव होगा. आंबेडकर का कहना था कि जब मुसलमानों को पृथक आरक्षण देने से राष्ट्र का बिखराव नहीं हो रहा है तब दलितों को अलग आरक्षण देने से हिन्दुओं का बिखराव कैसे होगा. ब्रिटिश हुकूमत ने दलितों को पृथक निर्वाचन सूची के साथ आरक्षण का प्रावधान स्वीकार कर लिया. गाँधी को यह कतई विश्वास नहीं था कि उनके विरोध की अनदेखी कर ब्रिटिश सरकार ऐसा निर्णय लेगी. गाँधी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया. इसके विरोध में उन्होने यरवदा जेल में 20 सितम्बर 1932 से आमरण अनशन किया, जो छह रोज चला. इसके दबाव के बीच दलितों और कांग्रेस ( बल्कि कहें सवर्ण हिन्दुओं ) के बीच एक समझौता हुआ. पृथक निर्वाचन सूची की जगह संयुक्त निर्वाचन सूची पर ब्रिटिशराज द्वारा तय सीटों के मुकाबले अधिक सीटों पर आरक्षण स्वीकार करने सम्बन्धी यह समझौता हुआ था.
लेकिन कांग्रेस और आंबेडकर के बीच रस्साकशी बनी रही. 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में आंबेडकर के खिलाफ मशहूर क्रिकेटर पी बालू को कांग्रेस ने खड़ा किया. बालू को लेकर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी है. वह जीनियस क्रिकेटर थे, जो दलित परिवार से आते थे. आंबेडकर उनके फैन थे. आंबेडकर के महत्त्व से अनजान बालू चुनाव तो लड़े, किन्तु हार गए. हालांकि कांग्रेस ने अपने स्तर से आम्बेडकर को हराने का पुख्ता प्रबंध किया हुआ था. 1952 के पहले आमचुनाव में आंबेडकर को हराने में कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने एकजुट भूमिका निभाई. 1956 में आंबेडकर का निधन हो गया. निधन दिल्ली में हुआ था. प्रधानमंत्री नेहरू और दूसरे बड़े नेता दिल्ली में थे, लेकिन कोई उनके आवास पर झांकने नहीं गया. जगजीवन राम के प्रयास से उनका पार्थिव शरीर हवाई जहाज से मुंबई भेजा गया. यह कांग्रेस की उनके प्रति अपनायी गई उदासीनता थी. आम्बेडकर का आकलन इस रूप में भी होना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के बीच वह एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होने कांग्रेस और गांधीवाद का वैचारिक स्तर पर विरोध किया. उनकी किताब ‘कांग्रेस और गाँधी ने अछूतों केलिए क्या किया ‘ देखा जाना चाहिए.
संविधान सभा में आंबेडकर का प्रवेश एक पृथक प्रसंग है. पहली बार तो वह मुस्लिम लीग के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल के सहयोग से बंगाल प्रान्त से प्रवेश पा सके थे. विभाजन के बाद वह चुनाव क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में आ गया. आंबेडकर ने पाकिस्तान जाने से इंकार किया. ऐसी स्थिति में वह कांग्रेस के पटेल खेमे द्वारा दुबारा चुनाव जीतकर संविधान सभा में पहुंचे और उन्हें संविधान प्रारूप समिति का चेयरमैन बनाया गया. संविधान निर्माण में बी एन राउ और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने इस महत्वपूर्ण दायित्व को सम्पादित किया. 1948 में शारदा कबीर के साथ विवाह के बाद वह अधिक रचनात्मक स्थिति में थे. इसका प्रभाव उनके कार्यों पर देखा जा सकता है. संविधान निर्माण में महती भूमिका अदा करने के साथ उन्होंने दो महत्वपूर्ण किताबें ( बुद्धा एंड हिज धम्म और रेवोलुशन एंड काउंटर रेवोलुशन इन अन्सिएंट इंडिया ) लिखी. नदी घाटी योजनाओं पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए और सबसे बढ़ कर हिन्दू स्त्रियों से सम्बंधित हिन्दू कोड बिल का प्रारूप तैयार कर उसके लिए संघर्ष किया. राष्ट्रनिर्माण केलिए आंबेडकर द्वारा की गई सेवायें इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके विवेचन केलिए पूरी किताब चाहिए. दलित मुक्ति के प्रश्न पर उनका संघर्ष अप्रतिम है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर राष्ट्र को दी गई उनकी अन्य सेवा भी महत्वपूर्ण है. सबसे बढ़ कर वह अपने दौर के विशिष्ट विचारक-चिंतक है,जो वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखते थे.
आज कांग्रेस और दूसरे प्रगतिशील कहे जाने वाले लोगों को उनकी चिन्ता होने लगी है. लेकिन जब वह थे, तब इन्हीं लोगों ने मिल-जुल कर उनकी फजीहत की थी. कांग्रेस ने तो उनकी उपेक्षा की ही, सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों ने भी उनकी भरपूर उपेक्षा की थी. हालांकि वैचारिक स्तर पर वह उनके अधिक नजदीक थे. मजबूत विपक्ष के निर्माण केलिए समाजवादी राममनोहर लोहिया से आंबेडकर ने मिलने की इच्छा जताई थी. लोहिया ने अपने दो शिष्यों को मिलने भेज दिया. यह आंबेडकर की भरपूर तौहीन थी. लोहिया की दृष्टि में आम्बेडकर जलन के प्रतीक थे. ( देखा जाय लोहिया की किताब ‘ जातिप्रथा ‘) कम्युनिस्ट तो उन्हें दिग्भ्रमित ही समझते थे. इन तमाम उपेक्षा-भाव को झेलते वह सक्रिय रहे. समाजवादियों के खेमे से 1980 के बाद मधु लिमये ने उनपर व्यवस्थित काम किया और उनके विचारों के साथ एक विचार-सेतु स्थापित करने की कोशिश की. 1970 के दशक में जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा और कुछ बाद जाकर कर्पूरी ठाकुर आदि ने आंबेडकर को समझने और आत्मसात करने की कोशिश की. इस समय उन्हें गुजरे हुए दो दशक हो गए थे. लेकिन कांग्रेस अब भी उनसे शत्रु भाव ही रखती थी. इसी विचारभूमि पर कांशी राम ने 1980 के दशक में आम्बेडकरवाद की बहुजन राजनीति विकसित की और कांग्रेस व गांधीवादी वैचारिकी को उत्तरभारत से उखाड़ फेंका.
आरएसएस और भाजपा की विचारधारा भिन्न रही है. उनका हिंदुत्व मोटे तौर पर द्विज-केंद्रित है. ( कांग्रेस होशियार द्विजों का दल है जबकि भाजपा गंवार द्विजों का) लेकिन सावरकर जैसे हिंदूवादी विचारक जब वृहत्तर हिंदुत्व का खाका बनाते हैं,तब दलितों के बिना वह पूरा नहीं होता. इसलिए दलित-मुक्ति के प्रश्न पर हिंदुत्ववादी शक्तियां कांग्रेस, सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों की तुलना में अधिक उदार रही है. हाँ, हिन्दुत्ववादियों के बीच की द्विजवादी ताकतें निःसंदेह दलित और आंबेडकर विरोधी रही हैं. आज जब आंबेडकर को लेकर विचार किया जा रहा है तब इन तमाम प्रश्नों पर भी विचार किया जाना चाहिए. आंबेडकर अपनी वैचारिकी में नेहरू से अधिक वैज्ञानिक परिदृष्टि रखते थे. उनका इतिहास-बोध भी उनसे अधिक परिष्कृत था.
राजनीतिक-सामाजिक विमर्श करने की उनकी विशिष्ट प्राविधि थी. अनीहिलेशन ऑफ़ कास्ट जैसी पुस्तिका और रेवोलुशन एंड काउंटर रेवोलुशन इन अन्सिएंट इंडिया जैसी अधूरी रह गई किताब में उनकी इतिहास दृष्टि को देखा जा सकता है. वह लोकल को भी ग्लोबल भाव से देखने की कोशिश करते थे. उन्होंने हिंदुत्व और भारत को गाँधी और सावरकर से कहीं अधिक गहरे तौर पर समझा था. अपनी वैचारिकी में वह गाँधी और नेहरू की अपेक्षा रवीन्द्रनाथ टैगोर के अधिक निकट दीखते हैं. आंबेडकर की मुसीबत यह है कि दलित उन्हें अपने घेरे से बाहर नहीं जाने देना चाहते और दूसरे उन पर माला चढ़ा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं. भारतीय लोकतंत्र पर उनकी यह टिप्पणी कि लोकतंत्र केलिए विवेक की जगह भक्ति-प्रदर्शन खतरनाक संकेत है, याद करने लायक सबक है. मैं नहीं चाहूंगा कि आंबेडकर को लेकर भी एक भक्ति-फ्रंट खुल जाय. मैं उनके विचारों को महत्त्व देने के पक्ष में हूँ.