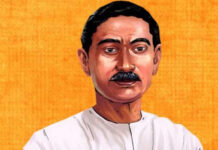— प्रो. रणधीर गौतम —
जब भारतीय समाजवाद विचारधारा के रूप में बड़ी चुनौतियों आक कर रहा है तब समाजवादी विरासत के महान सेनानियों की स्मृति का सामना का महत्व बढ़ जाता है। आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के बाद मधु लिमये, राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर जैसे नायक ऐसी स्थिति में प्रकाशपुंज की तरह हैं। आज राजनीति एक नए संकट में है। एक तरफ छद्म-राष्ट्रवाद और दूसरी ओर घनघोर जातिवादी राजनीति, यहाँ तक की बहुत सारे समाजवादी बुद्धिजीवी यहाँ तक मानते हैं कि छद्म-राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए जातिवादी राजनीति को प्रोत्साहित करना जरूरी है। यह आश्चर्यजनक है। ऐसे में हमें कर्पूरी जी याद आते हैं जो समाजवादी मूल्यों को राजनीति में समदर्शी होकर स्थापित करने का प्रयास करते थे। कर्पूरी जी जातिवादी बहुलवाद के खिलाफ भी संघर्ष करते हुए दिखते हैं- इस मामले में उनका एक कथन याद आता है- “न लाठीतंत्र से, न जातितंत्र से, हमको तो लोकतंत्र से ही राजनीति करनी है”।
कई समाजवादियों के प्रभाव के साथ समाजवादी रामनंदन मिश्रा जी कर्पूरी जी के मार्गदर्शक के रूप में माने जा सकते हैं। लगभग 1930 के दशक में ही रामनंदन मिश्रा ने कर्पूरी ठाकुर में बिहार की राजनीति का भविष्य देखा था। उन्होंने ही उनका ‘कपूरी’ नाम बदलकर कर्पूरी ठाकुर रखा। रामनन्दन मिश्रा एक समाजवादी स्वतंत्रता संग्रामी थे और जयप्रकाश नारायण जी के साथ जेल में बंद रहे थे।
आज हिंदी पट्टी के ‘डायनेस्टिक पॉलिटिक्स’, और ‘कम्युनल पॉलिटिक्स’ के दौर में कर्पूरी ठाकुर जैसे नायकों का विचार आशावाद का संचार करता है। कर्पूरी जी के लिए राजनीति एक साधना थी, जिसमें बिहार का नवनिर्माण और समाजवादी सपनों को पूरा करना एक मुख्य मकसद था।
राजनेताओं से आज जब राजधर्म के पालन की बात की जाती है तब एक छोटा सा उदाहरण याद आता है- एक बार जब कर्पूरी ठाकुर के पिता के साथ कुछ तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने दुर्व्यवहार किया तो पुलिसिया कार्रवाई करते हुए वहां के प्रशासन ने उन लोगों को पकड़ कर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। कर्पूरी जी को जैसे ही यह जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत वहां के प्रशासन को उन लोगों को छोड़ देने का आदेश दिया।
कर्पूरी ठाकुर का नाम याद आते ही, भिखारी ठाकुर भी याद आते हैं जिन्होंने बिहार में भोजपुरी को सांस्कृतिक पहचान दी। इसी तरह कर्पूरी जी ने भी अपने राजनीति की कला के माध्यम से बिहार की राजनीति को एक नयी पहचान दी। दोनों ही नाई जाति से आते थे. आज लगभग हर नेता जब राष्ट्रीय पटल पर आने की चाह रखता है, तब हमको कर्पूरी जी याद आते हैं जिन्होंने अपना साधना क्षेत्र बिहार को रखा। सत्ता-सुख से अधिक उनके लिए जनसेवा का महत्त्व था।
तमाम विसंगतियों के बावजूद लालू जी के बारे में जिस प्रकार कहा जाता है कि उन्होंने वंचितों को स्वर्ग तो नहीं दिया लेकिन स्वर दिया, उसी तरह कर्पूरी जी के बारे में कहा जा सकता है की उन्होंने बिहार में वंचितों को राजनितिक भविष्य दिया | कर्पूरी जी की राजनीति को हम लोग तीन भागों में देख सकते हैं- पहले 1930 से 1967, बनता हुआ समाजवादी, दूसरा 1967 से 1979, ओबीसी और ‘डिप्राइव्ड क्लास’ की आवाज, और फिर 1979 से 1988, जनांदोलन के समर्थक।
वैसे तो जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार कर्पूरी जी का जन्म सन् 1924 माना जा सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से उनका जन्म मिथिलांचल के समस्तीपुर जिले में 24 जनवरी, 1921 को हुआ था. बचपन से ही उन्होंने गरीबी, जातिवाद और साम्राज्यवाद की चुनौतियों से स्वयं को घिरा पाया. वे ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलन में भाग लेकर और फिर बाद में जयप्रकाश नारायण ‘के आजाद’ दस्ता में भाग लेकर क्रांतिकारिता के संस्कार को अपने अंदर विकसित करते रहे. 1942 में जब जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हुए तो वे पूरे भारत में एक महानायक के रूप में जाने जाने लगे. जैसे ही यह जानकारी कर्पूरी ठाकुर को मिली तो कर्पूरी जी जयप्रकाश नारायण से मिलने नेपाल पहुंच गए. बाद में कर्पूरी जी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में भी शामिल हुए और 23 अक्टूबर 1943 को उन्हें जेल में भी डाल दिया गया. जब भी समाजवादियों की सभा या कार्यशाला होती कर्पूरी जी एक विद्यार्थी की तरह नोट ले रहे होते थे, यह उनके भीतर वैचारिकी निर्माण के प्रति ललक को दिखलाता है।
इसी तरह जब चुनाव लड़ने की बात हुई तो जयप्रकाश की धर्मपत्नी प्रभावती जी
ने कर्पूरी जी को प्रोत्साहित किया। शुचिता इतनी थी कि सबसे एक रूपये या दो रूपये चंदा लेते थे और अधिकतर कुछ पैसे ही। लेकिन प्रभावती जी ने सबसे बड़ा पाँच रूपये चंदा दिया। उनके बारे में आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री जी कहते हैं- ‘वह बोलते थे! क्या बोलते थे, जन-जन को अपनी बातों से कोई उनको ध्यान से सुने तो जीवन का फलसफा ही बदल जाए। पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूँ लोकनायक के बाद जननायक नाम ही उनके साथ जुड़ेगा.’
कर्पूरी जी जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कक्षा 10वीं के बोर्ड में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया, इसकी बड़ी तारीफ हुई, लेकिन कुछ लोग कर्पूरी जी का मजाक भी बना रहे थे। यहाँ तक कि उस समय के दसवीं डिवीजन को उन्होंने ‘कर्पूरी डिवीजन’ के नाम से खिल्ली उड़ाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सच्चे अर्थों में कर्पूरी जी के मिट्टी के दर्शन और इसकी ताकत को समझते थे। उन्हें पता था भाषाई गुलामी सबसे बड़ी गुलामी होती है। उनके इस प्रयास को समता मूलक समाज के निर्माण में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा सकता है। उच्च शिक्षा में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। उच्च शिक्षा में लाखों लोगो को आने का मौका मिला।
कर्पूरी जी एक प्रखर समाजवादी थे। उनका समतामूलक समाज की स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने गरीबी, विषमता को बहुत नजदीक से देखा था; अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि तक शोषण के खिलाफ वह अनवरत संघर्षरत रहे। उन्होंने दुनिया भर से समाजवादी आंदोलन की ऐतिहासिक समझ जुटा कर उसको सामाजिक जीवन में भी उतारने का प्रयास किया. एक तरफ वे ‘सबलटर्न क्लास’ से जुड़े नायक थे जिसकी जमीनी सच्चाई की समझ उनके पास थी, वहीं दूसरी तरफ वे समाजवाद के इतिहास व महत्व को जानते थे। कर्पूरी जी के ऊपर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के विचारों का गहरा प्रभाव था. कर्पूरी जी के दैनिक व्यवहार में ‘सोशल डेमोक्रेसी’ और ‘डेमोक्रेटिक सोशलिज्म’ के उद्देश्य और व्यवहार को देखा जा सकता है। कर्पूरी जी ने समाजवादी चिंतन की धारा को आगे बढाया। उन्होंने ‘सोशल डेमोक्रेसी’ और ‘सोशल इंजीनियरिंग’ की नई सोच प्रस्तुत की। जातीय रूप से बहुत कम संख्या में होने के बावजूद उस समय अपने सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों की वजह से समाज ने सर्वमान्य नायक बनाया। यह समाज और राजनीति में उनके कद को बताता है।
‘मुंगेरीलाल आयोग’ बना करके जो छाप उन्होंने राजनीति पर छोड़ी वह ‘मंडल आयोग’ के परिणाम से बाद में निखर कर सामने आयी। पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए
निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करके, मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी बढ़ाकर, बिना अंग्रेजी के माट्रिक पास करने की मान्यता देकर और ऐसे कितने नए तरीकों से उन्होंने कई अहम् कार्य किये। इन सन्दर्भों में ‘मुंगेरीलाल आयोग’ को ‘मंडल कमीशन’ का अग्रवाहक कहे जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
कर्पूरी जी की सोच की वजह से ही ‘आरक्षण निति’ में एक नई अंतर्दृष्टि आई जिनके कारकों की भी चर्चा करना अनिवार्य है। कर्पूरी जी हमेशा प्रतिनिधि को लोकतंत्र में मानदंड माना करते थे। इस तरह कर्पूरी जी बहुत हद तक डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित थे। ‘एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एंड एजिटेट’ के सिद्धांत को वे अपने राजनीतिक मकसद का मूल मंत्र माना करते थे। कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सामाजिक न्याय के मुक्ति मार्ग प्रशस्त करने के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने अपने विचार और आचरण से समाजवाद की विरासत को आगे बढ़ाया। जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण की ‘संपूर्ण क्रांति’ में कर्पूरी जी आए और बिनोवा जी के साथ आपातकाल के दरमियान जिस तरह का पत्राचार उन्होंने किया इससे स्पष्ट होता है कि कर्पूरी जी के अंदर आंदोलनकारी प्रवृत्ति हमेशा से रही। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाले कर्पूरी तानाशाही को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे।
‘मुंगेरीलाल आयोग’ में 127 जातियों को चिन्हित करके जिस प्रकार उन्होंने ‘सामाजिक सशक्तीकरण’ का काम किया वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जब कर्पूरी जी के प्रयासों को हम देखते हैं कि कर्पूरी जी ‘संस्थगात सुधार’ नहीं कर पाए तो इसके पीछे मुख्य कारण के रूप में चुनावी राजनीति की सीमाएं थी; हालांकि बाद में लालू प्रसाद यादव भी भूमि सुधार आगे नहीं बढ़ा पाए, जबकि बट्टेदारी कानून से सबसे अधिक फायदा यादव समुदायों को ही होता। इसको समाजशास्त्रीय भाषा में हम अल्थुजर के सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं कि कई बार शासन में आने के बावजूद जो ‘आइडियोलोजिकल स्टेट एपरेटस’ (वैचारिक राज्य औजार) होता है उसकी वजह से सांस्थानिक सुधार आसानी से संभव नहीं होते. इ. जे. क्ले अपने लेख इन अंडर-डेवलपमेंट में बात करते हैं कि कभी- कभी ऐसा माना जाता है की सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, जबकि सत्ता पक्ष, ‘डोमिनेन्ट क्लास’ के साथ कोऑप्ट कर लेता है जिससे समाज बदलाव की प्रक्रिया पर विराम लग जाता है।
इसमें एक और उदाहरण देखा जा सकता है- गांधी और अंबेडकर के पूना पैक्ट को गांधी और अंबेडकर के बीच की जंग के रूप में, गांधी की जीत और अंबेडकर की हार के रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अंबेडकर को ऐसा ज्ञात था और उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा की पूना पैक्ट के फेल होने की दशा में बाद जो हिंसा होती उसमें न जाने कितने
दलित मारे जाते। तो कभी-कभी सत्ता वर्ग और रिफॉर्म के बीच एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ता है। और ये परिस्थिति हम कर्पूरी ठाकुर के साथ भी देखते है। इस तरीके से कर्पूरी जी क्रांतिकारी समाजवाद के पक्षधर थे और ‘जमीन से शासन’ को अपनी शासन शैली का ध्येय मानते थे। कई लोग जो यह आरोप लगाते हैं कि कर्पूरी जी के आंदोलन से दलित आंदोलन बिहार में कमजोर हुआ वह निराधार है। बिहार में ‘लेफ्ट-मूवमेंट’ तेज होने के कारण बिहार में दलित आंदोलन नहीं बढ़ पाया, हालांकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन बढ़ा। इसके अलावा बिहार में जगजीवन जी और भोला पासवान शास्त्री जैसे कांग्रेस के नेता थे जिनका अपना जनाधार भी था। वाम आंदोलन कमजोर होने के कारण बिहार में रामविलास पासवान का उद्भव हुआ। नक्सली आंदोलन को बिहार में न फैलने देने में कर्पूरी ठाकुर की राजनीति का भी एक योगदान हो सकता है जिसका समाज वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना शेष है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.