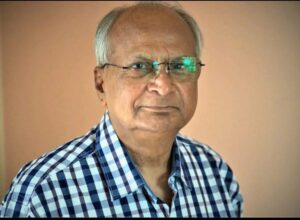— सच्चिदानंद पांडे —
अपनी उत्कृष्ट मेधा बुद्धि, बौध्दिक सौष्ठव, वैचारिक शक्ति, सामाजिक गतिकी की सही समझ, संचित ज्ञान, बुद्धिमत्ता, सूचनाओं तक पहुंच, अभिव्यक्ति की आजादी आदि गुणों से विभूषित होने के कारण बुद्धिजीवी सत्तासीनों के वर्ग हित, उनके कार्यकलापों और उनकी विचारधारा के आवरण के पीछे छुपे उनके गुप्त इरादों और झूठ-फरेब को समझने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनका दायित्व और उनकी जिम्मेदारी है कि वे आगे बढ़कर सत्तासीनों के झूठ और छल का पर्दाफाश करें और अपनी अपेक्षित भूमिका को निभाएं।
एक सजग, सचेष्ट, प्रबुद्ध बौद्धिक के रूप में देश और समाज के दहकते सवालों और सरोकारों पर, समकालीन घटनाक्रमों- पर कुछ लिख या बोल कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, विचार के क्षेत्र में समाज में व्याप्त अवांछित व रुग्ण प्रवृत्तियों पर तथ्यपरक और संतुलित प्रहार करना प्रत्येक बुद्धजीवी का कर्तव्य और दायित्व है। अगर वक्त रहते इन चुनौतियों का सामना नहीं किया गया तो हमारी सभ्यता का सारा ढ़ांचा बिखर जाएगा।
यदि हम अवांछित प्रवृत्तियों का मौन समर्थक बने रहकर उनका विरोध नहीं करते तो चाहे अनचाहे हम उनका समर्थन करते हैं। कलम उठाना जोखिम भरा और जिम्मेदारी का काम है। हमारा विचार उपचार और प्रहार दोनों का काम करता है। संक्रांति काल समस्या से भागने का नहीं सुलझाने और लड़ने का काल होता है। सही वक्त पर सही मोर्चे से भागना अपने दायित्व से पलायन करने जैसा है। बुद्धिजीवियों को हर तरह का खतरा उठाकर भी मोर्चे पर अंतिम दम तक डटा रहना चाहिए। अपने पूर्वाग्रहों से,अपनी विकृतियों से मुक्त होकर और एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए। हर ज़माने में बुद्धिजीवियों ने ऐसी भूमिका निभाई है। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनमें बुद्धजीवियों का महती योगदान रहा है। उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी क्रांति में बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से लोगों को प्रेरित किया और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। इनमें वाल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू और दिदरो जैसे दार्शनिक शामिल थे।
वॉलटेयर धार्मिक सहिष्णुता और तर्कसंगतता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने चर्च के प्रभाव और निरंकुश राजतंत्र की आलोचना की।
ज्यां-जैक्स रूसो ने सामाजिक अनुबंध और लोगों की संप्रभुता के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि सरकार जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और लोगों को शासकों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं।
मोंटेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन किया, जिससे सरकार में संतुलन और नियंत्रण स्थापित हो सके।
दिदरो ने ज्ञानकोश (Encyclopédia) नामक एक विशाल ग्रंथ का संपादन किया, जिसमें ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का समावेश था। इसने ज्ञानोदय के विचारों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन बुद्धिजीवियों के विचारों ने लोगों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया और क्रांति के दौरान उत्पन्न होने वाले क्रांतिकारी विचारों की नींव रखी। इनके विचारों ने लोगों को पुरानी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने और एक नई, अधिक न्यायसंगत समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया।
भारत के संदर्भ में भी समाज सुधार की भावना से अभिप्रेरित जनों – राजा राममोहन राय, विद्यासागर, स्वामी दयानंद आदि ने यही काम उस समय किया था जब विघटनकारी प्रवृत्तियों को उभारने और बढ़ावा देने के लिए सरकारी तंत्र अपनी पूरी ताकत लगाए हुए था। लेकिन स्वतंत्र भारत में इस काम की ओर बुद्धिजीवियों ने ध्यान नहीं दिया। कोई आंदोलन नहीं किया। वे विक्रांति करते रहे जो उनके बस का काम नहीं था। सामाजिक रूपांतरण में उनकी जो अपेक्षित भूमिका थी उससे वे विलग रहे और समाज भी उनकी ओर से निराश और उदासीन रहा।
सामाजिक चेतना में परिवर्तन एकमात्र ऐसा कार्य है जो परिवर्तनकामी बुद्धिजीवी ही कर सकता है। लेकिन हमारे यहां शिक्षा और अवसर की समानता के कागजी दावों के बावजूद सुविधा भोगी समाज अपनी सुविधाएं किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। सुविधा वंचित समुदाय का शिक्षित वर्ग जल्द से जल्द बराबरी पर आना चाहता है और स्वयं भी सुविधाभोगी समाज का हिस्सा बनकर अपने ही समाज के पिछड़े तबके का अपने हित में इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। इनके विकृत रूप आए दिन सामने आते रहते हैं। मुक्ति संग्राम में बंधन में पड़े हुए लोग उपद्रव तो कर सकते हैं परंतु अपनी स्वतंत्रता का अभियान नहीं चला सकते। आजतक दबे हुए लोगों की सिसकती जिंदगी की समानता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाई है। अवसर की समानता और शिक्षा की समानता आज भी एक सपना है जिसे देखने तक का साहस पूरे समाज में नहीं है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.