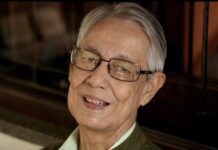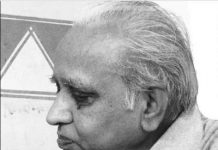— परिचय दास —
कुमार गन्धर्व का गायन अनुभव नहीं, अनुभूति है। वह शास्त्रीय संगीत नहीं, एक आत्मिक अनुनाद है। उनके स्वर जब निकलते हैं तो किसी पाठ्य परंपरा की पुनरावृत्ति नहीं करते; वे एक नये ब्रह्मांड की रचना करते हैं—जैसे शब्द नहीं, ध्वनि साकार हो गई हो। उस ध्वनि में एक विरल विरक्ति है जो शरीर और जगत दोनों से गहरी दूरी बनाती है पर आत्मा से अत्यंत निकट होती है। कुमार गन्धर्व के संगीत को यदि कोई पहली बार सुनता है तो उसे यह परंपरा से हटकर, कभी-कभी विक्षेप-सा लग सकता है पर जितना वह उसमें डूबता है, उतना ही उसे यह अनुभूति होती है कि संगीत का केंद्र वहाँ है, जहाँ कुमार बैठते हैं।
गायन उनके लिए अनुकरण नहीं, आविष्कार था। राग को उन्होंने केवल उसकी बंदिशों में नहीं, उसके मौन में भी सुना। यह मौन, जो शब्दों से अधिक अर्थपूर्ण था। जब वे कोई राग छेड़ते, तो लगता—सदियों से सोई हुई कोई पुरानी स्मृति, किसी जंगल की छाया में हौले से जाग रही हो। उसमें शास्त्रीय अनुशासन भी था, पर उससे अधिक वह था जिसे गन्धर्व ने ‘स्वतंत्रता’ कहा था—संगीत की आत्मा की स्वतंत्रता। इसीलिए वे कहते थे, “राग गाना नहीं होता, राग में होना होता है।”
उनकी आवाज़ में कहीं कोई मीठी कड़वाहट थी—एक ऐसा तीखा ताप जो श्रोता को भीतर से हिला देता था। उनके स्वर किसी रेशमी गली से नहीं गुजरते थे, वे गंगा की धार की तरह सीधे दिल में उतरते थे। उसमें काशी की उदासी थी, कबीर की दग्धता थी और किसी पुराने साधु की अनहद धुन थी। वे गाते नहीं थे वे एक भटका हुआ आत्मा थे जो ध्वनि के माध्यम से घर लौटती थी। इसीलिए उनके गायन में भाषा कभी केंद्र में नहीं रही—भाव रहा, ध्वनि रही, वह अति सूक्ष्म कंपन रहा, जिसे पकड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं।
कुमार गन्धर्व जब कबीर गाते थे तो लगता जैसे कबीर स्वयं गा रहे हों। ‘सुनता नहीं क्या कहता संत?’ में जिस प्रकार से वे शब्दों के बीच विराम रखते थे, वह विराम ही सबसे ज़्यादा कहता था। वहाँ कोई लय की चाल नहीं थी, वहाँ कोई ताली या ख्याल की बंदिश नहीं थी—वहाँ बस एक अन्तःशब्द था, जो न केवल स्वर को बल्कि श्रोता की चेतना को भी झंकृत करता था। यही कारण है कि उनका संगीत सुनते हुए कोई केवल संगीत नहीं सुनता, वह अपने भीतर उतरता चला जाता है।
उनकी तानें परंपरागत नहीं थीं। वह तानों को उनके बंधन से मुक्त करते थे, परंतु यह कोई विद्रोह नहीं था—यह एक साधु का आग्रह था, कि राग अपने आत्मा में पहुँचे। वे मालकोंस को किसी मंदिर की शांत धूप में गाते थे तो उसमें दिनकर की कांति नहीं, एक स्निग्ध संध्या की मृदु आभा होती थी। कभी तो ऐसा लगता कि कुमार किसी संगीत सभा में नहीं, किसी ब्रह्म रात्रि में गा रहे हैं, जहाँ समय रुक गया है और केवल राग बह रहा है।
शुद्धता उनके लिए एक मानसिक अवस्था थी, कोई तकनीकी आग्रह नहीं। वे किसी सुर को पकड़ने की चेष्टा नहीं करते थे बल्कि सुर को अपने भीतर उतारते थे। एक बार उन्होंने कहा था, “मैं संगीत से यह नहीं कहता कि तू कैसी है, मैं तो बस उससे मिलने निकलता हूँ।” यही मिलन, यही अन्वेषण, उनके गायन का सार था। वे जब भैरवी गाते थे, तो उसमें कोई अंत नहीं होता था—जैसे कोई ध्वनि किसी पहाड़ी नदी की तरह बहती चली जाती है और सुनने वाला उसके साथ बहता चला जाता है, न लौटने के लिए, न पहुँचने के लिए—बस बहने के लिए।
कुमार गन्धर्व की उपस्थिति मंच पर साधारण थी—कोई नाटकीय भंगिमा नहीं, कोई विशेष अंगविक्षेप नहीं पर उनके आँखों में एक भीतरी आग जलती थी। उनकी देह की दुर्बलता संगीत की शक्ति के आगे एक मौन संकेत बनकर रह जाती थी। वे फेफड़ों की बीमारी से जूझते रहे पर उन्होंने अपने गायन को कभी उस शरीर की सीमा में बंद नहीं होने दिया। जब डॉक्टरों ने कहा कि वे अब कभी गा नहीं पाएँगे, तब उन्होंने बंदिशें नहीं छोड़ीं, ध्वनि के अन्य रूपों की खोज की—उन्होंने आलाप को नए रूप में साधा, उन्होंने लोक रागों को शास्त्रीय स्वरूप दिया, उन्होंने पर्वतों, जंगलों और नदियों को अपने स्वर में बसाया।
उनके लिए लोक, केवल एक स्रोत नहीं था—वह उनका विश्वास था। वे कहते थे कि “लोक में राग का बीज छिपा होता है।” उन्होंने मालवा के निर्गुण भजनों को, झारखंड के आंचलिक सुरों को, महाराष्ट्र के लोक स्वरों को अपनी शास्त्रीय समझ से मिलाया और एक ऐसा नया रूप दिया जो न केवल नया था बल्कि पुराना भी था—उस पुरातन की स्मृति जो किसी समय की शुरुआत से हमारे भीतर पल रही थी।
वे कबीर, मीरा, तुलसी, मलूकदास, नामदेव—इन संत कवियों को केवल गाते नहीं थे, वे उन्हें जीते थे। उनके स्वर में मीरा की व्याकुलता भी थी और कबीर की निर्ममता भी। कभी वह स्वर चुपके से हृदय में उतरता था और कभी किसी तूफान की तरह मन को झकझोर देता था। वे श्रोताओं को न केवल मोहित करते थे, उन्हें जागृत भी करते थे—यह वह दुर्लभ शक्ति है जो केवल कुमार गन्धर्व जैसे साधकों को मिलती है।
कुमार गन्धर्व का संगीत समय की सीमा में नहीं बंधा। वह एक ऐसी यात्रा है, जो किसी समय विशेष में नहीं, चेतना के किसी गहरे तल में घटती है। उनके गीतों को बार-बार सुनने पर भी कुछ नया सामने आता है—कोई स्वर, जो पहली बार नहीं सुना था; कोई मौन, जो पहले नहीं समझा था। यह संगीत उस बारिश की तरह है, जो हर बार नये रंग में गिरती है, और हर बार कुछ नया उगाती है।
उनके गायन में एक विशेष प्रकार की एकाकी विरक्ति थी—मानो कोई ऋषि एकांत में बैठा, अनंत से संवाद कर रहा हो। वह संवाद श्रोताओं के लिए भी खुला होता था परंतु उसकी भाषा बहुत पारदर्शी नहीं थी। वे सरल नहीं थे पर जटिल भी नहीं थे—वे उस बिन्दु पर थे जहाँ दोनों मिलते हैं। उनकी आवाज़ कभी सीधी नहीं चलती थी, वह चक्राकार घूमती थी, फिर ऊपर उठती थी, फिर अचानक नीचे आ गिरती थी—जैसे कोई अनुभूति, जो खुद को पकड़ने नहीं देती।
गायन उनके लिए केवल एक कलात्मक कर्म नहीं था—वह एक साधना थी। वे मंच पर नहीं, अपने अंतर्मन की गुफा में बैठते थे। वे राग नहीं रचते थे, वे राग में विलीन हो जाते थे। यह विलय, यह विसर्जन, उनकी पहचान था। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वे महान हैं बल्कि वे कहते थे, “मैं तो राग को खोज रहा हूँ, वह कभी मिल जाता है, कभी नहीं।”
उनके संगीत में प्रकृति की अनुगूंजें थीं। मालवा की मिट्टी, बांसुरी की साँसें, हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट—इन सभी ने उनके गायन में स्थान पाया। जब वे गाते, तो लगता जैसे कोई वनस्पति अपने भीतर गा रही है। उन्होंने जो कहा, वह सुना भी जाता था और महसूस भी किया जाता था—जैसे शरीर से अधिक, आत्मा सुन रही हो।
उनकी मृत्यु के बाद भारतीय संगीत में एक सन्नाटा छा गया। उनके जैसा न कोई हुआ, न कोई हो सकता है—क्योंकि कुमार गन्धर्व केवल एक गायक नहीं थे, वे एक विचार थे, एक चेतना थे, एक संगीतदर्शी थे। उनके स्वर भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा पृष्ठ हैं, जो कभी धुंधला नहीं होगा। उन्होंने संगीत को नये मायने दिए, उसे आकाश दिया और श्रोताओं को वह दृष्टि दी जिससे वे केवल सुनें नहीं, देख सकें।
कुमार गन्धर्व का गायन किसी परंपरा का उत्तराधिकार नहीं, एक नवीन परंपरा का सृजन था। उनकी तानें हवा में लिखी हुई कविताएँ थीं और उनके विराम शून्य के उस पक्ष को प्रकट करते थे जहाँ केवल अनुभूति बोलती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि संगीत न तो केवल ध्वनि है, न केवल भाव—वह एक यात्रा है, जो भीतर से बाहर और फिर बाहर से भीतर लौटती है।
उनके स्वर आज भी गूँजते हैं—उन रात्रियों में जब हम अकेले होते हैं, उन क्षणों में जब हम खुद से मिलते हैं। वे हमारे भीतर गाते हैं—कभी कबीर के शब्दों में, कभी किसी अनाम धुन में, और कभी महाकाल के मौन में। कुमार गन्धर्व का संगीत समाप्त नहीं हुआ—वह एक निर्झरिणी की तरह बह रहा है—कभी किसी मन की चुप्पी में, तो कभी किसी तान की धारा में। वह बहाव ही उनका उत्तरजीवन है—एक ऐसा जीवन जो स्वरों से बना है पर शब्दों से परे है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.