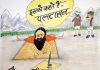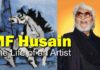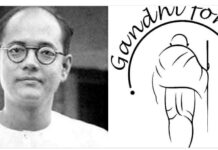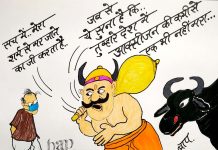— आनन्द कुमार —
यह पहचानना होगा कि तिब्बत मुक्ति-साधना आज की दुर्निया में अहिंसक रास्ते की प्रासंगिकता की ताजा कसौटी है। तिब्बत के प्रश्न पर दुनिया में पहले अज्ञान था। फिर उपेक्षा फैली। आजकल आशंका का माहौल है। क्या सत्य व अहिंसा का अनुसरण कर रहे तिब्बती हमें तिब्बत के बारे में अज्ञान, उपेक्षा व आशंका से बाहर निकाल सकेंगे?
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अपनी स्वाधीनता खोने वाला एक मात्र एशियायी राष्ट्र तिब्बत है। वह मार्क्सवादी राष्ट्रवाद में निहित विस्तारवाद का शिकार हुआ और उसकी दुर्दशा में तत्कालीन तिब्बती नेतृत्व की अदूरदर्शिता तथा भारतीय सरकार की चुप्पी का भी योगदान था। तिब्बत को कम्युनिस्ट चीन ने दो चरणों में हड़पा। 1949 में स्वायत्तता की बहुआयामी परिभाषा स्वीकारते हुए चीन ने तिब्बत के साथ एक संघि की। फिर इसी स्वायत्तता को नष्ट करने के लिए भारत से 1954 में ‘पंचशील’ जैसे सनातन महत्व के विशेषण के साथ एक आठवर्षीय संधि में हिमालयी एशिया के सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक व आर्थिक इतिहास को अनदेखा किया गया। चीन की इस कूटनीतिक व्यूहरचना का अंतिम लक्ष्य एशिया महाद्वीप में अपना वर्चस्व स्थापित करना था। लेकिन इसका आभास विश्व-शक्तियों या एशिया की प्रमुख सरकारों को नहीं हो पाया। (इन दोनों ही षड्यंत्रों को ‘प्रगति और शांति’ की दिशा में ऐतिहासिक कदम घोषित करते हुए भारत के तत्कालीन सरकारी नेतृत्व व ‘प्रगतिशील’ विशेषज्ञों ने तिब्बत की पुकार की आत्मघाती उपेक्षा की। अब सफाई दी जाती है कि 1949 में भारत अपनी ही सुरक्षा व स्थिरता की समस्याओं से जूझ रहा था। कश्मीर पर हमला, भारत विभाजन से उत्पन्न हिंसा व अराजकता, देशी रियासतों की चालबाजियां आदि के कारण नव-स्वाधीन भारत का ध्यान तिब्बत-चोन सम्बन्धों में हो रहे बदलाव से हटा हुआ था। इसी प्रकार 1954-59 में कोरिया का युद्ध, भारत को शीत युद्ध में घसीटने की पश्चिमी महाशक्तियों की कोशिशों, चीन से मैत्री के जरिए एशिया को तीसरी दुनिया व तीसरी शक्तियों का शक्ति केन्द्र बनाने का सपना तथा कम्युनिस्ट क्रांति में निहित मानवतावादी संभावनाओं में आस्था जैसे कारणों ने जवाहरलाल नेहरु की सरकार को पड़ोसी धर्म की अनदेखी करने का आधार दिया।
पड़ोसी धर्म न निभाने का क्या नतीजा निकला? 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले तिब्बत राष्ट्र की स्वाधीनता चीनी सैनिक शासन ने छीन ली और भारत, भूटान, नेपाल, बर्मा, मंगोलिया व रूस के एशियाई क्षेत्र तक फौजी अड्डे फैलाने में सफल हो गया। इसके परिणाम स्वरूप भारत से 1962 में सैनिक टक्कर हुई और भारत बुरी तरह पराजित हुआ। अपनी 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के हाथ खोने के साथ ही हम अपना अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व राष्ट्रीय आत्मविश्वास भी खो बैठे। तिव्यत पर चीनी कब्जा व भारत पर चीनी हमले के पूर्व भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र में कोई सुरक्षा समस्या नहीं थी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली भारत-तिब्बत सीमा की कुल लंबाई 5000 किलोमीटर है। लेकिन 1962 से पूर्व हमारा सुरक्षा व्यय मात्र 28 करोड़ रुपए वार्षिक था। 1962 के चीनी हमले के बाद व्यय तीन गुना बढ़कर 81 करोड़ रुपए हुआ। अब हमारा देश पूरे बजट का 15 प्रतिशत यानी 41,200 करोड़ रुपए (1998) चीन के सैनिक दबाव के प्रतिरोध में खर्च करने को विवश है। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में 200 सैनिक अड्डों में 5 लाख सैनिक जमा कर रखे हैं। चीनी सेना प्रक्षेपास्त्रों, परमाणु अस्त्रों व बमवर्षकों से लैस है। चीन ने भारत के खिलाफ मध्य तिब्बत में 5 प्रक्षेपास्त्र केन्द्र, 14 वायुसेना केन्द्र, 19 रडार केन्द्र व 81 अंतर्महाद्वीपीय मारक क्षमता वाले प्रक्षेपास्त्र तैनात कर रखे हैं। इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के बीच चीन स्थायी अवरोध भी बन गया है। पाकिस्तानी परमाणु अस्त्रों के पीछे चीनी सहयोग का सच जगजाहिर हो चुका है। क्या तिब्बत की चीनी सैनिकों से मुक्ति हुए बिना भारत सुरक्षित महसूस कर सकता है? जब भारत ही असुरक्षित हो तो एशिया में निर्भयता व शांति कहां संभव है और यह महाद्वीप चीनी आंतक से कैसे बच सकता है ?
इस तस्वीर का दूसरा पहलू हिमालय की सांस्कृतिक अस्थिरता तथा वहां के आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है। तिव्वत की राजधानी ल्हासा बौद्ध धर्म की महायान परंपरा का केन्द्र है। इसकी महत्ता वेटिकन, यरूशलम, मक्का-मदीना व काशी से कम नहीं है। आध्यात्मिक साधना, शिक्षा से लेकर व्यापार व राजनीति की धुरी के रूप में तिब्बत की भूमिका समूचे हिमालय के लिए स्रोत व संदर्भकी रही है। हिमालय का पूरा भूगोल पूर्व से लेकर पश्चिम तक व उत्तर से लेकर दक्षिण तक दलाई लामा-पंचेन लामा के नेतृत्व व शिक्षा से ओतप्रोत बौद्ध सभ्यता से सुगंधित है। भाषा-भूषा-भोजन से लेकर आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक व्यवस्था व सांस्कृतिक विशेषताएं तिब्बत की केन्द्रीयता को प्रतिबिंबित करती हैं। चीन ने तिब्बत को कब्जे में लेकर बौद्ध सभ्यता पर घातक प्रहार किया है। 1959 से अब तक के बीच चीन ने 60 लाख जनसंख्या वाले तिब्बतियों में से 12 लाख निर्दोष स्त्री-पुरुषों को अकाल मृत्यु का शिकार बनाया है। 6000 से अधिक मंदिरों, मठों व विद्या केन्द्रों का ध्वंस किया गया। तिव्वती संस्कृक्ति को समूल नष्ट करने के लिए लगभग 75 लाख चीनियों को तिब्बत में पहुँचा दिया गया है। तिब्बती समाज को धर्म व साधना से विमुख करने के लिए भिक्षुओं व भिक्षुणियों को जेलों में बंद करना इसी सैनिक राज की दूसरी कूर नीति है। इसी के समानान्तर तिव्वती स्त्रियों को चीनियों से विवाह के लिए विवश किया जाता है।
अन्यथा उन्हें गर्भपात, वंध्यीकरण व वलात्कार का शिकार बनाया जाता है। जब तिब्बत में ही मठ-मंदिर नष्ट हो रहे हैं तो शेष हिमालय में उनकी परंपरा को कैसे बल मिलेगा? दलाई लामा व उनके सवा लाख से अधिक अनुयायियों ने चीनी सैनिक कब्जे का विरोध करते हुए आत्मरक्षा के लिए तिब्बत से बाहर शरण ली है। इनमें से अधिकांश (लगभग एक लाख बीस हजार) भारत व नेपाल में शरणागत हैं। कुछ हजार तिब्बती प्रवासी यूरोप व अमेरिका में रहकर आत्मरक्षा व विश्व जनमत-जागरण में जुटे हुए हैं। लेकिन मंगोलिया से लेकर म्यांमार और आम्दो से लेकर लद्दाख अरुणाचल तक आध्यात्मिकता आधारित समाज व्यवस्था का प्रवाह कमजोर हो रहा है। अहिंसा पर हिंसा का क्रूर प्रहार जारी है। एक समूची सभ्यता व जीवन प्रणाली चीनी सैनिकों के आतंक से दम तोड़ रही है। चीनी शासन ने वनों की अंधाधुंध कटाई, खनिजों का भूगर्भ से बेलगाम उत्खनन, तथा परमाणु विस्फोटों व अन्य गतिविधियों से तिब्बत के पर्यावरण को नष्ट व प्रदूषित किया है। तिब्बत में वनों की कटाई से भारतीय मानसून की अवधि तथा जलवृष्टि की मात्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे तिब्बत से निकलने वाली मुख्य भारतीय नदियों-ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज तथा कोसी में बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है।
दलाई लामा 1959 से निर्वासन की जिन्दगी जीने को विवश किए गये हैं। जवकि पंचेन लामा की चीनी हिरासत में रहस्यमय दशा में मृत्यु हुई। उनके उत्तराधिकारी शिशु को चीनियों की जेल में रखा गया है। नए पंचेन लामा के माता-पिता तथा चयन समिति के प्रधान रिपोछे भी नहीं बख्शे गये हैं।
तिब्बत पर चीनी कब्जे के पहले समूचा हिमालय क्षेत्र शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की सदियों पुरानी परंपरा का निर्वाह कर रहा था। लेकिन चीनी सैनिक राज के शुरू होते ही तनाव, हिंसा व अलगाववाद को हवा मिल रही है। कश्मीर से लेकर मणिपुर, नागालैण्ड तथा मिजोरम तक अवैध व्यापार तथा आतंकवाद का सिलसिला प्रबल हुआ है। म्यांमार में जनतंत्र की वापसी का आन सान सू की द्वारा सफल अभियान चलाया गया। लेकिन चीनी शासकों ने तत्काल म्यांमार (बर्मा) के फौजी तानाशाहों व जंगल-माफिया के गठजोड़ की मदद करके एक स्वस्थ राजनीतिक परिवर्तन को अवरुद्ध किया।
तिब्बत की पराधीनता का असर भारत और शेष विश्व के हिन्दू व बौद्ध धर्मावलंबियों के धार्मिक अधिकारों व कर्तव्यों पर भी पड़ा है। भारतीयों का श्रेष्ठतम तोर्थ कैलाश-मानसरोवर है। लेकिन इसकी यात्रा चीनी सैनिकों के नियंत्रण में चीनी राज की शर्तों को स्वीकारने वाले तथा यात्रा शुल्क के रूप में एक मोटी रकम देने के लिए प्रस्तुत तीर्थयात्रियों के लिए ही संभव है।
इसी प्रकार बौद्धों की परंपराओं के दो शीर्षस्थ प्रतीकों दलाई लामा तथा पंचेन लामा को भी चीनी आघात का शिकार बनाया गया है। दलाई लामा 1959 से निर्वासन की जिन्दगी जीने को विवश किए गये हैं। जबकि पंचेन लामा की चीनी हिरासत में रहस्यमय दशा में मृत्यु हुई। उनके उत्तराधिकारी शिशु को चीनियों की जेल में रखा गया है। नए पंचेन लामा के माता-पिता तथा चयन समिति के प्रधान रिपोछे भी नहीं बख्शे गये हैं।
कड़ी निगरानी व कठोर सजा के बावजूद आस्थावान तिब्बती संतों व नागरिकों द्वारा चीनी राज के लगातार प्रतिरोध का सिलसिला भी बना हुआ है। चूंकि तिब्बती संस्कृति की नींव बौद्ध दर्शन पर आधारित है, अतः विशिष्ट प्रकार के अहिंसक व आध्यात्मिक तरीकों से तिब्बती जनसाधारण अपना दुःख व्यक्त करते हैं। इन तरीकों का बनता की जीवन शैली से सम्बन्ध है और चीनी सैनिक शासन अपनी क्रूरता के बावजूद रोक नहीं लगा पाता है। उदाहरणार्थ, दलाई लामा के चित्र की पूजा तथा पंचेन लामा के उत्तराधिकारी बालक की दीर्घायु की प्रार्थनाएं चीनी-तिब्बती द्वन्द्व का एक मुख्य प्रतीक बन गया है। इसी प्रकार नियमित रूप से रेडियो के जरिए विश्व के विभिन्न भागों में तिब्बत मुक्ति-साधना के समर्थन में चल रही गतिविधियों का विवरण सुनना भी एक व्यापक तरीका बना हुआ है। दलाई लामा के दर्शन कालचक्र पूजा के प्रवचनों को सुनने के लिए यात्राएं भी इसी विशिष्ट प्रतिरोध का एक प्रकार है।
तिब्बत सम्वन्धी अज्ञान का परिणाम
तिब्बत की पराधीनता का सच एक लंबे अरसे तक हिमालय से परे के संसार को नहीं मालूम था। वैसे भी ‘संसार’ का कुल अर्थ औद्योगिक तथा राजनीतिक क्रांतियों से संपन्न हुए अथवा पराधीन हुए देशों से बनी दुनिया तक ही सीमित रहा है। इस अर्थ में यूरोप केन्द्रित समझ वाले लोगों व संस्थाओं के लिए तिब्बत जैसी स्थिति वाले राष्ट्रों को जानना-पहचानना असंभव ही था क्योंकि तिब्बत आधुनिकीकरण के उजले या अंधेरे पक्ष में से किसी में भी शामिल नहीं था। जो यूरोप से अछूता रहा हो उसे अपना सरोकार कैसे माना जाए? जो ‘आधुनिक’ नहीं हुआ, वह समाज या राष्ट्र आधुनिक राजनीति व आर्थिकी के तानेबाने को चलाने वाली व्यवस्था से हमदर्दी और मदद कैसे पा सकता है? इस प्रकार अपनी गुलामी के पहले दौर में तिब्बत ‘आधुनिक’ राष्ट्रों व उनके विविध मंचों के अज्ञान का शिकार बना। यह 1949 से 1959 तक चला। फिर उपेक्षा का दौर आया। 1960, 1961 व 1965 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने तिब्बत के दुःख पर प्रतिक्रिया जरूर की। लेकिन यह प्रतिक्रियाएं चीन की घेरेबंदी व कम्युनिस्ट विरोधी कूटनीति के एक और बिन्दु के रूप में सामने आयीं। मानवीयता व करुणा के आधार पर तिब्बत के साथ हमदर्दी का भाव हिमालय क्षेत्र के सभी राष्ट्रों की जनता के बीच 1959 से बना हुआ है। लेकिन भारत समेत सभी एशियाई देशों की सरकारों ने अपने देश की जन भावनाओं की उपेक्षा करके चीनी अन्याय की अनदेखी का रास्ता अपनाया। सत्तर के दशक में तो ऐसा लगने लगा था कि तिब्बत राष्ट्र को चीन सचमुच पचा जाएगा।
किन्तु दलाई लामा की सात्विक शिक्षा, तिब्बत मुक्ति-साधना की सौम्य दृढ़ता और चीनी राष्ट्र निर्माण के अंतर्विरोधों ने क्रमशः विश्व जनमत को जागृत करना शुरू किया। माओ राज का खात्मा, चीनी राजनीति में देंग त्साओ-पिंग का उदय तथा विश्व के साथ जुड़ने की चीनी चेष्टाओं ने भी तिब्बत प्रश्न को नई प्रासंगिकता दी। 1989 में दलाई लामा को नोबल शांति पुरस्कार अर्पित करके पश्चिमी दुनिया ने अपने अज्ञान व उपेक्षा दोनों से परे जाने का शुभारंभ किया। यह दुनिया भर के आध्यात्मवादियों व अहिंसावादियों के लिए उत्साहवर्द्धक मोड़ था। यूरोपीय संसद, अमेरिकी कांग्रेस वे सिनेट, आस्ट्रेलिया की जन-प्रतिनिधि सभा व कई लैटिन अमेरिकी देशों ने 1989 से 1998 के बीच खुलकर तिब्बत के दुख को स्वर दिया है, तिब्बत मुक्ति-साधना का समर्थन किया है। ईसाई धर्मगुरुओं, हिन्दू आचार्यों, यहूदी धर्म प्रवक्ताओं तथा अनेकों धर्म-सम्प्रदायों के समर्थन वक्तव्यों से भी तिब्बत की रक्षा के अभियान को बल मिला है। इधर चीनी जनतांत्रिक आंदोलन के नेताओं का तिब्बती स्वंतत्रता सेनानियों से लगातार संवाद तथा ताईवान में दलाई लामाजी का अभूतपूर्व अभिनंदन सर्वाधिक उल्लेखनीय घटनाएं हैं।
चीनी शासन ने पिछले दशक में तिब्बत के समर्थन में उभरे विश्व जनमत का सामना करने के लिए बड़े प्रभावशाली तरीके से असत्य प्रचार का सहारा लिया। दलाई लामा के बारे में दुस्साहसी तरीकों से झूठ फैलाने से लेकर तिब्बती समाज में फूट फैलाने व पंचेन लामा परंपरा को नष्ट करने तक के प्रयास हुए हैं। चीनी शासकों के प्रभाव में विश्व का एक बड़ा हिस्सा जरूर है। फिर तिब्बती समाज चीनी राजसत्ता की प्रचार क्षमता का किसी भी स्तर पर मुकाबला नहीं कर सकते। चीनी शासकों व दलाई लामा के बीच के ‘विवाद’ में भारत जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पड़ोसी की चुप्पी से भी एक भ्रमपूर्ण स्थिति बनाने में चीनी शासक सफल रहे हैं। जब तक तिब्बत की दशा के बारे में फैले हुए अज्ञान, अर्द्धज्ञान व उपेक्षा भाव-तीनों का प्रभावशाली निदान नहीं किया जाएगा तब तक चीनी सैनिक-राज से मुक्ति की तिब्बत की पुकार पर पूरी दुनिया का ध्यान केन्द्रित करना कठिन बना रहेगा।
दो मुख्य प्रतिक्रियाएं: चीन व अमेरिका
आज दुनिया में तिब्बत को लेकर दलाई लामा व उनके अनुयायियों की ओर से चलाए जा रहे अभियानों पर दो सशक्त देशों की ओर से खुली प्रतिक्रिया हो रही है। चीनी शासक दलाई लामा की हर यात्रा व वक्तव्य पर निगाह रखते हैं, प्रतिवाद करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। भारत की सरकार विश्व मंचों पर या तो चीन के पक्ष में कतारबद्ध होती है या चुप रहती है। जबकि कैलाश मानसरोवर पर चीनी नियंत्रण से लेकर अरुणाचल पर चीनी दावे जैसी कई समस्याओं के कारण चीन तिब्बत विवाद में भारत की स्वाभाविक भूमिका होनी चाहिए। यह भारत के स्वाभिमान, पड़ोसी धर्म, आत्मरक्षा व युगधर्म चारों दृष्टियों से आवश्यक है। लेकिन 1962 की हार से उत्पन्न भयग्रंथि व पड़ोसियों के प्रति उदासीनता का दोष भारतीय विदेश मंत्रालय को चीन का पिछलगुआ बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका सरकार भी चीन में सक्रिय दिलचस्पी के कारण तिब्बत के प्रश्न पर बहुत सजगता दिखाती है। अमेरिका की दिलचस्पी के कई कारण हैं। लेकिन अमेरिका तिब्बत प्रश्न को अभी तक दलाई लामा की निगाह से देखने से बचता आया है। एक लंबी अवधि तक अमेरिकी जनता तिब्बत के प्रश्न से अनष्कान थी। इस प्रकार अमेरिकी शासन की समूची चेष्टाएँ उसकी गुप्तचर संस्था के माध्यम से आकार व अर्थ ग्रहण करती थीं।
सी.आई.ए. ने तिब्बत की गुलामी के बाद छापामार युद्ध से लेकर स्वतंत्र तिब्बत की संविधान रचना तक कई प्रयोगों में तिब्बती समाज की सहायता की है। लेकिन उसकी दिलचस्पी चीन-अमेरिका मैत्री का आरंभ होते ही घटने लगी। वैसे आज तक अनेकों व्यक्ति, विशेषकर कम्युनिस्ट धारा से सम्बन्धित विश्लेषक व संगठन, तिब्बत आन्दोलन को सी.आई.ए. का ही बखेड़ा मानते हैं। निक्सन प्रशासन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने तिब्बत में सीधी दिलचस्पी कम की। लेकिन कार्टर के राष्ट्रपति काल में मानवाधिकारों के प्रश्न को नई गंभीरता से उठाया जाने लगा। बिल क्लिंटन ने तो अपने चुनाव अभियान में तिब्बत प्रश्न को खुला महत्व दिया। इसके पीछे विगत दशक में अमेरिकी जनता में तिब्बत के लिए फैलती सहानुभूति का बड़ा योगदान है। यह सहानुभूति राजनीति से लेकर कला-फिल्म-शिक्षा-संस्कृति तक फैली है। डैनियल मोयनिहान (सेनेटर), रिचर्ड गेयरे (फिल्म कलाकार), प्रो. राकफेलर (प्राध्यापक), आदि इस बहुमुखी आंदोलन के प्रेरक हैं। इन सबने तिब्बत के प्रश्न को बुद्ध व दलाई लामा की शिक्षाओं के संदर्भ में पहचाना है। नासमझी व अवसरवादिता-दोनों अतियों से अलग सात्विक संवेदनशीलता पर आधारित प्रतिवद्धता का यह परिणाम है। फिर भी, अमेरिकी समाज व सरकार की दिलचस्पी का कोई बड़ा असर चीन पर नहीं पड़ा है। इसीलिए विगत कई वर्षों से हर बार अंतरर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोजन की सुनवाईयों में चीनी शासकों का दलाई लामा के प्रस्तावों को रद्द करते जाना जारी है।
तीसरी संभावना का विकास
इधर धीरे-धीरे एक तीसरी संभावना का भी उभार हो रहा है। चीन व अमेरिकी शासकों से अलग छोटे राष्ट्रों की जनता व शासकों का भी स्वर तिब्बत के प्रश्न पर उभर चुका है। वस्तुतः विश्व के राष्ट्रों में कुछ बड़े राष्ट्रों के इर्द-गिर्द ढेर सारे छोटे राष्ट्र फैले हुए हैं। अधिकतर बड़े राष्ट्र अपने इर्द-गिर्द के छोटे राष्ट्रों को जाने-अनजाने प्रताड़ित करते रहे हैं। बड़े राष्ट्रों के आगे छोटे राष्ट्रों की सुनवाई का कहीं प्रभावशाली मंच भी नहीं है। वैसे विश्व में छोटे राष्ट्रों का विराट बहुमत है। अंतरर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इस सच को तिब्बत के प्रसंग में दुनिया भर के छोटे राष्ट्र पहचानने लगे हैं। प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में पीड़ा ग्रस्त हुये अनेक यूरोपीय राष्ट्र भी तिब्बत की न्याय की पुकार का पूरी गंभीरता से प्रत्युत्तर देने लगे हैं। लेकिन इसमें एशिया की भूमिका नगण्य है। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मण्डेला तक किसी भी एशियाई देश के नेता से ज्यादा संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, डेनमार्क, नार्वे, आस्ट्रिया व कोस्टारिका जैसे देश इस प्रक्रिया में प्रमुख हैं। इस संभावना का अभी कोई असर नहीं है। क्योंकि इसको किसी शक्तिशाली देश की मदद नहीं है। भारत व यूरोपीय यूनियन मिलकर नैतिक नेतृत्व कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड व इटली में पर्याप्त सहमति के आसार हैं। लेकिन भारत क्या कर रहा है ? फिलहाल भारत की तरफ से पिछले कई वर्षों से तिब्बत के प्रश्न पर मानवाधिकार आयोग में चीन के ही पक्ष में मतदान किया गया है।
चीन व अमेरिका से परे विकसित हो रही मानवतावादी चिन्ता ने समूची परिस्थिति में गुणात्मक परिवर्तन शुरू कर दिया है। बुद्ध की करुणा व दलाई लामा की सार्वभौमिक उत्तरदायित्व की शिक्षाओं से आकर्षित व्यक्तियों के सहयोग से बन रही लोकशक्ति को किसी देश की राजशक्ति का संरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन मामूली स्त्री-पुरुषों की छोटी-छोटी चेष्टाओं की निरंतरता से तिब्बत समर्थन अभियान इस दौर का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास बन चुका है। इसे तिब्बत की स्थानीय एवं प्रवासित जनता से लेकर चीन की जनतांत्रिक धारा, समूचे हिमालय की आस्थावान जनता, एशिया अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रतावादी व्यक्तियों व संगठनों तथा पश्चिमी दुनिया के बुद्धिजीवियों, संस्कृतिकर्मियों, शांति आंदोलन तथा युवा पीढ़ी का प्रबल व मुखर समर्थन है। विश्व के सभी छोटे देशों की संसद में तिब्बत समर्थक सांसदों की अच्छी संख्या है। भारत, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, फ्रांस व इटली के तो मंत्रिमंडलों में भी तिब्बत मित्रों की उल्लेखनीय हैसियत है।
तब भी कुछ कमजोरियां हैं। इन कमजोरियों को कुछ लोग तिब्बती नेतृत्व की अहिंसा व संवाद के प्रति अटूट आस्था से जोड़ते हैं। कई विश्लेषणकर्ता इसमें दलाई लामा के व्यक्तित्व की कंन्द्रीयता को कारण मानते हैं। प्रायः सभी बहसों में चीन और तिब्बत की भौतिक-आर्थिक-सामरिक राजनीतिक अतुलनीयता को लेकर आशंका की जाती है। अब अज्ञान व उपेक्षा के व्यूह टूट चुके हैं। इस समय आशंकाओं का जोर है।
कई लोगों का मानना है कि तिब्बत के प्रश्न पर सक्रियता का रास्ता अपनाने पर भारत को कश्मीर के प्रश्न पर चीन की आक्रामकता का शिकार होना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि व राजनीति के कई विशेषज्ञों ने कश्मीर व तिव्वत की दशा के बुनियादी फर्को को वार-बार साफ किया है। क्या कश्मीर 1947 या उसके लगभग स्वतंत्र राष्ट्र था जिसकी अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संघियों का इतिहास है? क्या कश्मीर में धारा 370 के जरिये स्वायत्तता का पूरा संरक्षण नहीं हुआ है? क्या कश्मीर में जनमत संग्रह की संभावना का पाकिस्तान प्रेरित हमले के बाद स्वतः अंत नहीं हो गया ?
तिब्बत के बारे में नौ भ्रम
चीन तिब्बत का प्रश्न उठाने पर क्या करेगा ? यह भी आशंका है कि दलाई लामा में आस्था रखने वाले तिब्बती वास्तविक स्वायत्तता व पूर्ण स्वतंत्रता के बीच अंतर को क्या सम्मान देंगे? यह घबराहट तो है ही कि तिब्बत का प्रश्न उठाने वाले पर चीन पूरी तरह से हमला कर देगा। इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। लेकिन किसी भी मूल्यांकन में यह ध्यान रखना होगा कि चीन की चेष्टाओं, विश्व राजनीति की वास्तविकताओं तथा तिब्बत मुक्ति-साधना के इतिहास व वर्तमान के कारण चौतरफा भ्रमों का बोलबाला है। इनमें से नौ भ्रमों का या मिथ्या प्रचारों का स्पष्टीकरण जरूरी है।
सर्वप्रथम, चीन की ओर से वारंवार यह निराधार प्रचार किया जाता है कि दलाई लामा व उनके अनुयायी चीन के टुकड़े-टुकड़े करने के अंतर्राष्ट्रीय षड़यंत्र के अगुवा हैं। यह सच है कि स्वतंत्र तिब्बत चीन का अंग नहीं था और न रहेगा। लेकिन जहां तक दलाई लामा का प्रश्न है उनकी ओर से प्रस्तावित सभी समाधानों में तिब्बत और चीन के सहअस्तित्व पर ही जोर है ‘स्वायत्त स्वराज’ (अटानामस तिब्बत विद जेनुइन सेल्फ रूल) का ही आग्रह है। पिछले नौ वर्ष में दलाई लामा के वार्षिक व विशिष्ट संदेशों में यह तथ्य बार-बार दुहराया गया है।
दूसरे, यह भी पूछा जाता है कि क्या तिब्बत का प्रश्न चीन विरोधी अभियान है ? तिब्बतियों व तिब्बत मित्रों की दृष्टि में यह समूची चेष्टा ‘तिब्बत समर्थक’ आंदोलन है। यह स्वाभाविक है कि इस संदर्भ में चीनी शासन की नीतियों की खुली आलोचना की जाती है। लेकिन चीनी जनता व चीनी संस्कृति के प्रति कोई बैर-भाव नहीं फैलाया जाता। उलटे, तिब्बत के सर्वोच्च नेता दलाई लामा का मानना है कि तिब्बत के साथ न्याय करने में चीन का भी हित है।
तीसरा धम तिब्बत की मौजूदा स्थिति के बारे में है। क्या सचमुच तिब्बती संस्कृति का नाश हो रहा है? क्या यह दुनिया भर में सक्रिय कम्युनिस्ट विरोधी तथा अमेरिकन गुप्तचर संस्था सी.आई.ए. की प्रचार मशीन का फैलाया झूठ है? तिब्बत पर चीन के कब्जे के चार दशकों में अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग (इंटरनेशनल कमिशन आफ जूरिस्ट्स) जेनेवा, ने तिब्बत की दशा पर शुरू से अबतक लगातार निगाह रखी है। इसकी ताजा रपट दिसंबर 1997 में प्रकाशित की गई। इसमें तिब्बत में चल रहे दमनचक्र व संस्कृति संहार का विस्तृत विवरण है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल जैसी विश्व भर में मान्यता प्राप्त एक अन्य प्रमाणिक संस्था का भी यही निष्कर्ष है। तिब्बत को नजदीक से जानने वाले समाज वैज्ञानिकों, धर्माचायों, राजनयिकों व पत्रकारों का मूल्यांकन भी चौंकाने वाला है। वास्तविकता यह भी है कि सी.आई.ए. जैसी राष्ट्रीय राजनीतिक हितों से जुड़ी पश्चिमी देशों को एजेंसियों का तिब्बत के प्रश्न पर सदैव त्रुटिपूर्ण व उदासीन रुख रहा है। गुप्तचर संस्थाएं सिवाय अपने राज्य के किसी दूसरे का कब से हित करने लगी हैं ?
तीसरे प्रश्न के साथ ही चौथा भ्रम जुड़ा हुआ है-क्या तिब्बत के प्रश्न पर सिर्फ निर्वासित तिब्बतियों में आक्रोश है या स्थानीय तिब्बती जनता भी पीड़ा व अन्याय से क्षुब्ध है। दुनिया को भरमाने के लिए तिब्बत की स्वायत्त विकास यात्रा का मासिक व वार्षिक विवरण चीनी दूतावासों के जरिए विभिन्न देशों की भाषाओं में छापा व बांटा जाता है। तिब्बत की सरकारी यात्राएं भी करायी जाती हैं। लेकिन जनता व चीनी सैनिक शासन का रिश्ता खोलने वाले दो तथ्य विचारणीय हैं-एक, अगर तिब्बत में सब कुछ मंगलमय है तो पिछले दो दशक से बार-बार मार्शल लॉ (फौजी कानून) की क्यों जरूरत पड़ती रही है ? दूसरे, अगर तिब्बती संस्कृति की स्वायत्तता की चीन ने रक्षा की है तो दलाई लामा के चित्र रखने व पंचेन लामा के उत्तराधिकारी के चयन का दलाई लामा द्वारा अनुमोदन करने पर एतराज क्यों है ? वास्तविकता यही है कि व्यापक असंतोष व दमन का द्वन्द्व चल रहा है। पिछले एक दशक में ड़ेढ़ सौ से अधिक प्रदर्शनों व प्रतिरोधों का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। दलाई लामा में जनता की अटूट और गहरी आस्था तथा तिब्बत के चीनीकरण से उत्पन्न असंतोष का डर चीनी शासकों को बराबर रहता है। यह बुनियादी बात है कि तिब्बत का
प्रश्न 1959-60 में तिब्बत छोड़कर भारत में बसे दलाई लामा व उनके निकटतम सहयोगियों का ही सरोकार नहीं है। तिब्बत की दशा को लेकर तिब्बत देश में भी लगातार गहराता असंतोष ही इसका वास्तविक आधार है।
कई लोगों का मानना है कि तिब्बत के प्रश्न पर सक्रियता का रास्ता अपनाने पर भारत को कश्मीर के प्रश्न पर चीन की आक्रामकता का शिकार होना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि व राजनीति के कई विशेषज्ञों ने कश्मीर व तिब्बत की दशा के बुनियादी फकों को बार-बार साफ किया है। क्या कश्मीर 1947 या उसके लगभग स्वतंत्र राष्ट्र था जिसको अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों का इतिहारों है? क्या कश्मीर में धारा 370 के जरिये स्वायत्तता का पूरा संरक्षण नहीं हुआ है? क्या कश्मीर में जनमत संग्रह की संभावना का पाकिस्तान प्रेरित हमले के बाद स्वतः अंत नहीं हो गया? दूसरे स्तर पर असलियत यही है कि चीन कश्मीर में पूरी तरह से सक्रिय है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कराकोरम दरें के आस-पास 800 किलोमीटर क्षेत्र में चीन ने स्वयं इस्तेमाल लायक सड़क बनायी है। यह सड़क कश्मीर को तिब्बत के जरिये चीन से जोड़ती है। इसी प्रकार हर मौके पर चीन भारत को नसीहत देता है कि कश्मीर एक दक्षिण एशियाई समस्या है और भारत व पाकिस्तान को परस्पर बातचीत करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन की कश्मीर सम्वन्धी तटस्थता का वास्तविक अर्थ पाकिस्तानी दावों की मौन पुष्टि जैसा ही माना जाता है। फिर चीन भारत की नैतिक सक्रियता की प्रतिक्रिया में नया क्या करेगा?
छठा भ्रम यह फैला हुआ है कि भारतीय राजनीति में तिब्बत का प्रश्न कुछ महत्वहीन राजनीतिज्ञों ने व दलों ने भारत-चीन मैत्री में अड़ंगेवाजी के लिए उठाया। अब यह प्रश्न विदेशी इशारे पर उठता है। सरदार पटेल, डा. राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, डा. बाबा साहेब अम्बेडकर व श्री मोहम्मद करीम छागला श्री नेहरु के समकक्ष महत्व के राष्ट्र नायक थे। सभी तिब्बत के प्रश्न पर चीन की चेष्टाओं से असहमत व आशंकित थे। डा. राममनोहर लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री दीनदयाल उपाध्याय व श्री मीनू मसानी जरूर गैर कांग्रेसी राजनीति से जुड़े थे लेकिन इनमें से किसी की भी देशभक्ति पर संदेह करना नादानी होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि अब तक उपलब्ध सभी दस्तावेजों व संस्मरणों में तिब्बत की आजादी व भारत की सुरक्षा को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा गया है। भारत की ओर से विदेश सचिव या चीन में राजदूत रह चुके सभी विदेश नीति विशेषज्ञों ने तिब्बत के प्रश्न पर पुनर्विचार व संशोधन का वार-बार सुझाव दिया है। इनमें सर्व श्री ए. पी. वेंकटेश्वरन्, मुचकुन्द दुबे, जगत मेहता, एन. एन. झा व रंगनाथन् विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वर्तमान राजनीतिज्ञों में श्री वेंकटरमण, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री रवि राय, श्री जार्ज फर्नांडिस, श्री इंद्रजीत गुप्त, श्री जनेश्वर मिश्न एवं श्री राम जेठमलानी की चिंताएं जगजाहिर हैं।
सातवां भ्रम यह है कि तिब्बत का प्रश्न सिर्फ दलाई लामा की पीढ़ी वाले तिब्बतियों का प्रश्न है। नई पीढ़ी वाले तिब्बती तिब्बत के अंदर आधुनिकीकरण तथा तिब्बत के बाहर पश्चिमीकरण से प्रभावित हैं। अपनी अस्मिता के बजाए चीनीकरण व अमरीकीकरण के प्रति ज्यादा आकर्षित हैं। हाल ही में दिल्ली में थुप्तेन न्योडुप की आत्माहुति, स्त्रियों द्वारा पेईचिंग में संपन्न विश्व महिला सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन तथा तिब्बती युवक कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के प्रश्न पर दलाई लामा द्वारा नरमी का खुला विरोध जैसे संकेत इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए काफी हैं। यह रातही प्रचार वैसे भी स्वतंत्रता आंदोलनों की प्रक्ति का ज्ञान रखने वालों के लिए निरर्थक रहा है।
आठवां भ्रम इस आशंका के साथ जुड़ा है कि तिब्बत का प्रश्न उठाने पर चीन भारत पर पुनः 1962 जैसा हमलावर व्यवहार करेगा। इसलिए चुप रहना चाहिए। ऐसा मानने वाले यह भूल करते हैं कि स्वयं दलाई लामा बिना शर्त संवाद के आग्रही हैं। गांधीमार्ग पर चलकर सर्वानुमति की चेष्टा में हैं। फिर दलाई लामा के पक्षधर क्यों आघात व प्रहार का रास्ता खोलेंगे?
इस प्रसंग में नौवां व आखिरी महत्वपूर्ण भ्रम इस बात को लेकर है कि तिब्बत के सवाल पर सिर्फ कुछ भारतीय व अमेरिकी व्यक्तियों व समूहों के राष्ट्रवादी सरोकारों के कारण ही दिलचस्पी है; जबकि वास्तविकता दूसरी है। विगत वर्ष यूरोप के तीन सौ शहरों में नगरपालिका भवनों पर तिब्बती झण्डे फहराकर एकजुटता प्रदर्शित की गई है। यूरोपीय संसद में रेडिकल पार्टी के 45 सदस्य हैं और वे तिब्बत के प्रश्न को सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में प्राथमिकता देते हैं। जर्मनी के 35 शहरों में तिब्बत समर्थक नागरिक मंच सक्रिय हैं। इटली, फ्रांस, इंग्लैण्ड व आस्ट्रेलिया में तिब्बत मुक्ति समर्थक स्थानीय जन संगठनों के सक्रिय सहयोग से चलाए जा रहे हैं। विश्व भर में अहिंसावादी, पर्यावरणवादी तथा जनतंत्रवादी संगठनों का तिब्बत के प्रश्न पर अति सक्रिय सहयोग हो चुका है। इसीलिए पिछले 5 वर्ष में तीन बार तिब्बत समर्थक संसद सदस्यों व जनसंगठनों के पांच अंतर्राष्ट्रीय समागम भारत, लिथुआनिया, जर्मनी व अमेरिका में संपन्न हो चुके हैं। असलियत यह है कि भारत या अमेरिका की सरकार, भारत की तिब्बत मित्र संस्थाएं दोनों ही आज तिब्बत के प्रश्न पर विश्व जनमत या विश्वराजनीति का नेतृत्व नहीं कर रही हैं। अमेरिका को चीनी बाजार का लोभ है। भारत को चीनी सेना का भय है।
साभार-
तिब्बत दमन, मुक्ति-साधना और भारत का स्वधर्म,
सम्पादक राजीव वोरा
गांधी शांति प्रतिष्ठान (1998)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.