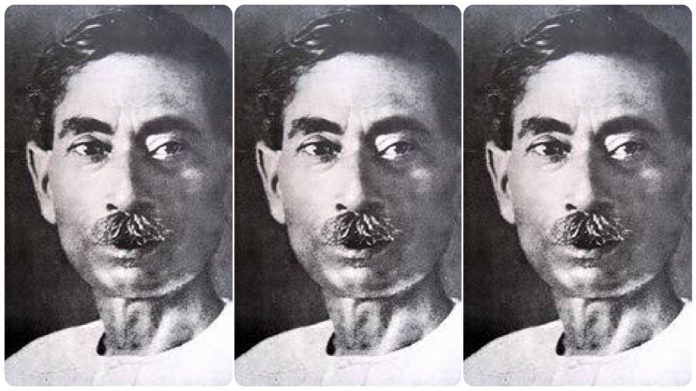दिलों में गुबार भरा हुआ है, फिर मेल कैसे हो। मैली चीज पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता, यहाँ तक कि जब तक दीवान साफ न हो, उस पर सीमेण्ट का पलस्तर भी नहीं ठहरता। हम गलत इतिहास पढ़-पढ़ कर एक-दूसरे के प्रति तरह-तरह की गलतफहमियाँ दिल में भरे हुए हैं, और उन्हें किसी तरह दिल से नहीं निकालना चाहते, मानो उन्हीं पर हमारे जीवन का आधार है।
मुसलमानों को अगर यह शिकायत है कि हिंदू हमसे परहेज करते हैं, हमें अछूत समझते हैं, हमारे हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहते, तो हिंदुओं को यह शिकायत है कि मुसलमानों ने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे तीर्थ-स्थानों को लूटा, हमारे राजाओं की लड़कियाँ अपने महल में डालीं और न जाने क्या-क्या उपद्रव किये। हिंदू मुसलमानों के आचार और धर्म की हँसी उड़ाते हैं, मुसलमान हिंदुओं के आचार और धर्म की। विजयी जाति पराजितों पर जो सबसे कठोर आघात करती है, वह है, उनके इतिहास को विषैला बना देना। प्राचीन, हमारे भविष्य का पथ-प्रदर्शक हुआ करता है। प्राचीन को दूषित करके, उसमें द्वेष और भेद का कीमा भरकर, भविष्य को भुलाया जा सकता है। वही भारत में हो रहा है।

यह बात हमारे अंदर ठूँस दी गयी है कि हिंदू और मुसलमान हमेशा से दो विरोधी दलों में विभाजित हो रहे हैं, हालाँकि ऐसा कहना सत्य का गला घोंटना है। यह बिलकुल गलत है कि इसलाम तलवार के बल पर फैला। तलवार के बल से कोई धर्म नहीं फैलता, और कुछ दिनों के लिए फैल भी जाय, तो चिरजीवी नहीं हो सकता। भारत में इसलाम के फैलने का कारण ऊँची जातिवाले हिंदुओं का नीची जातियों पर अत्याचार था। बौद्धों ने ऊँच-नीच का भेद मिटाकर नीचों के उद्धार का प्रयास किया और इसमें उन्हें अच्छी सफलता मिली, लेकिन जब हिंदू धर्म ने फिर जोर पकड़ा, तो नीची जातियों पर फिर वही पुराना अत्याचार शुरू हुआ, बल्कि और जोरों के साथ। ऊँचों ने नीचों से उनके विद्रोह का बदला लेने की ठानी। नीचों ने बौद्ध-काल में अपना आत्मसम्मान पा लिया था। वे उच्चवर्गीय हिंदुओं से बराबरी का दावा करने लगे थे। उस बराबरी का मजा चखने के बाद, अब उन्हें अपने को नीच समझना दुस्सह हो गया।
यह खींच-तान हो ही रही थी कि इसलाम ने नये सिद्धांतों के साथ पदार्पण किया। वहाँ ऊँच-नीच का भेद न था। छोटे-बड़े, ऊँच-नीच की कैद न थी। इसलाम की दीक्षा लेते ही मनुष्य की सारी अशुद्धियाँ, सारी अयोग्यताएँ, मानो धुल जाती थीं। वह मस्जिद में इमाम के पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता था, बड़े से बड़े सैयदजादे के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर भोजन कर सकता था। यहाँ तक कि उच्चवर्गीय हिंदुओं की दृष्टि में भी उसका सम्मान बढ़ जाता था। हिंदू अछूत से हाथ नहीं मिला सकता, पर मुसलमान के साथ मिलने-जुलने में उसे कोई बाधा नहीं होती। वहाँ कोई नहीं पूछता कि अमुक पुरुष कैसा, किस जाति का मुसलमान है। वहाँ तो सभी मुसलमान हैं। इसलिए नीचों ने इस नये धर्म का बड़े हर्ष से स्वागत किया और गाँव के गाँव मुसलमान हो गये।
जहाँ वर्गीय हिंदुओं का अत्याचार जितना ही ज्यादा था, वहाँ यह विरोधाग्नि भी उतनी ही प्रचण्ड थी, और वहीं इसलाम की तबलीग भी खूब हुई। कश्मीर, असम, पूर्वी बंगाल आदि इसके उदाहरण हैं। आज भी नीची जातियों में ग़ाज़ी मियाँ और ताज़ियों की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। उनकी दृष्टि में इसलाम विजयी शत्रु नहीं, उद्धारक था। यह है इसलाम के फैलने का इतिहास, और आज भी वर्गीय हिंदू अपने पुराने संस्कारों को नहीं बदल सके हैं। आज भी छूत-छात और भेद-भाव को मानते आते हैं। आज भी मंदिरों में, कुओं पर, संस्थाओं में बड़ी रोक-टोक है। महात्मा गाँधी ने अपने जीवन में सबसे बड़ा जो काम किया है, वह इस भेद-भाव पर कुठाराघात है। वर्गीय हिंदुओं में जो एक सूक्ष्म-सी ऊपरी जागृति नजर आती है, इसका श्रेय महात्माजी को है।

तो इसलाम तलवार के बल से नहीं, बल्कि अपने धर्म-तत्त्वों की व्यापकता के बल से फैला। इसलिए फैला कि उसके यहाँ मनुष्यमात्र के अधिकार समान हैं। अब रही संस्कृति। हमें तो हिंदू और मुसलिम संस्कृति में कोई ऐसा मौलिक भेद नहीं नजर आता। अगर मुसलमान पाजामा पहनता है, तो पंजाब और सीमाप्रांत के सारे हिंदू स्त्री-पुरुष पाजामा पहनते हैं। अचकन में भी मुसलमानी नहीं रही। रहा चौका-चूल्हा। पंजाब में चौके-चूल्हे का झगड़ा, हिंदुओं में भी नहीं है और शिक्षित समाज तो कहीं भी चौके-चूल्हे का कायल नहीं। मध्यप्रांत के मुसलमान भी हिंदुओं की भाँति चौके-चूल्हें की नीति का व्यवहार करते हैं। हिंदू-मुसलिम भेद के लिए यहाँ भी कोई टिकाव नहीं मिलता। हमारे देवता अलग हैं, उनके देवता अलग। । पुराणों में देवता को चाहे कुछ कहा जाय, हम तो प्रतिमा को ही देवता मानते हैं। शिव, राम, कृष्ण और विष्णु जैसे हमारे देवता हैं, वैसे ही मुहम्मद अली और हुसैन आदि मुसलमानों के देवता या पूज्य पुरुष हैं। हमारे देवता जैसे त्याग, आत्मज्ञान, वीरता और संयम के लिए आदरणीय हैं, उसी भाँति मुसलिम देवता भी हैं। अगर हम श्रीरामचंद्र को स्मरणीय समझ सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हुसैन को उतना ही आदरणीय न समझें। हम मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, मुसलमान मस्जिदों में, ईसाई गिरजाघरों में। मगर कोई जैनी या आर्यसमाजी मंदिर में पूजा करने नहीं जाता। क्या इसलिए हम जैनियों या आर्य-समाजियों को अपने से पृथक् समझते हैं?
सिख भी हमारे मंदिरों में नहीं जाते। उनके गुरुद्वारे अलग हैं, पर इसलिए हम सिक्खों से लड़ने नहीं जाते। यों तो हिंदू-हिंदू में, जाति-जाति में, वर्ग-वर्ग में भेद हैं और उन भेदों पर हम लड़ने लग जाएं, तो जीवन नरक तुल्य हो जाय। जब हम इन भेदों को भूल जाते हैं, तो मस्जिद में नमाज पढ़ना क्यों आपत्ति की बात समझी जाय? महात्मा गाँधी तो गिरजाघर में भी प्रार्थना कर लेते हैं। यहाँ भी हमें हिंदू-मुसलिम भेद के लिए कोई आधार नहीं मिलता। तो क्या वह गऊ-हत्या में है? या शिखा में? या जनेऊ में? जनेऊ तो आज कम-से-कम अस्सी फीसदी हिंदू नहीं पहनते, और शिखा भी अब उतनी व्यापक वस्तु नहीं है। हम किसी हिंदू को इसलिए अहिंदू नहीं कह सकते कि वह शिखाधारी नहीं है। बंगाल में शिखा का प्रचार नहीं। रही गऊ-हत्या। यह तो मालूम ही है कि अरब में गायें नहीं होतीं। वहाँ तो ऊँट और घोड़े ही पाये जाते हैं।
भारत खेती का देश है और यहाँ गाय को जितना महत्त्व दिया जाय, उतना थोड़ा है। लेकिन आज कौल-कसम लिया जाय तो शायद ऐसे बहुत कम राजे-महाराजे या विदेश में शिक्षा प्राप्त करनेवाले हिंदू निकलेंगे जो गोमांस न खा चुके हों। उनमें से कितने ही आज हमारे नेता हैं, और हम उनके नामों का जयघोष करते हैं। अछूत जातियाँ भी गोमांस खाती हैं, और आज हम उनके उत्थान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमने उनके मंदिरों में प्रवेश के निमित्त कोई शर्त नहीं लगायी और न लगानी चाहिए। हमें अख्तियार है, हम गऊ की पूजा करें, लेकिन हमें यह अख्तियार नहीं है कि हम दूसरों को गऊ –पूजा के लिए बाध्य कर सकें। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि गोमांस भक्षियों की न्यायबुद्धि को स्पर्श करें। फिर मुसलमानों में अधिकतर गोमांस वही लोग खाते हैं जो गरीब हैं, और गरीब अधिकतर वही लोग हैं, जो किसी जमाने में हिंदुओं से तंग आकर मुसलमान हो गये थे। वे हिंदू समाज से जले हुए थे और उसे जलाना और चिढ़ाना चाहते थे। वही प्रवृत्ति उनमें अब तक चली आती है।

जो मुसलमान हिंदुओं के पड़ोस में, देहातों में रहते हैं, वे प्रायः गोमांस से उतनी ही घृणा करते हैं जितनी साधारण हिंदू। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि मुसलमान भी गोभक्त हों, तो उसका उपाय यही है कि हमारे और उनके बीच में घनिष्ठता हो, परस्पर ऐक्य हो। तभी वे हमारे धार्मिक मनोभावों का आदर करेंगे। बहरहाल इस जाति-द्वेष का कारण गोहत्या नहीं है। और उर्दू-हिंदी का झगड़ा तो थोड़े-से शिक्षितों तक ही महदूद है। अन्य प्रांतों के मुसलमान उर्दू के भक्त नहीं और न हिंदी के विरोधी हैं। वे जिस प्रांत में रहते हैं, उसी की भाषा का व्यवहार करते हैं। सारांश यह है कि हिंदू-मुसलिम वैमनस्य का कोई यथार्थ कारण नहीं नजर आता। फिर भी वैमनस्य है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि हममें बहुत कम ऐसे महानुभाव हैं, जो इस वैमनस्य के ऊपर उठ सकें। खेद तो यह है कि हमारे राष्ट्रीय नेता भी इस प्रवृत्ति से खाली नहीं हैं। और यही कारण है कि हम एकता-एकता चिल्लाने पर भी, उस एकता से उतने ही दूर हैं।
जरूरत यह है कि जैसा हम पहले कह चुके हैं, कि हम गलत इतिहास को दिल से निकाल डालें और देश-काल को भली-भाँति विचार करके अपनी धारणाएँ स्थिर करें। तब हम देखेंगे कि जिन्हें हम अपना शत्रु समझते थे, उन्होंने वास्तव में दलितों का उद्धार किया है। हमारे जात-पाँत के कठोर बंधनों को सरल किया है और हमारी सभ्यता के विकास में सहायक हुए हैं। यह कोई छोटी और महत्त्वहीन बात नहीं है कि 1857 के विद्रोह में हिंदू-मुसलमान, दोनों ही ने जिसे अपना नेता बनाया, वह दिल्ली का शक्तिहीन बादशाह था। हिंदू-मुसलमान नृपतियों में पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं, पर वे लड़ाइयाँ धार्मिक द्वेष के कारण नहीं, स्पर्धा के कारण थीं, उसी तरह, जैसे हिंदू राजे आपस में लड़ा करते हैं। उन हिंदू-मुसलिम लड़ाइयों में हिंदू सिपाही मुसलमानों की ओर थे और मुसलमान सिपाही हिंदुओं की ओर।

प्रोफेसर मुहम्मद हबीब ऑक्सन ने अपने ‘मध्यकाल में हिंदू-मुसलिम संबंध’नाम से इस विषय पर एक विद्वत्तापूर्ण लेख लिखा है, जिसका एक अंश हम नकल करते हैं-
‘कहा जाता है कि हिंदुओं को घोड़े पर सवार होने, तीर चलाने और जुलूस निकालने तथा स्नान और पूजा-पाठ का निषेध था, पर ये किंवदन्तियाँ मौलिक प्रमाणों के गलत मुताला (अध्ययन) से पैदा हुई हैं। उस जमाने का हिंदू मजहब संगठित और शक्तिशाली था। उसके साथ मुसलमान बादशाह इसलिए रवादारी बरतते थे कि इसके सिवा दूसरी राह न थी।…उनके लिए साम्प्रदायिक संघर्ष का फल तबाही के सिवा और कुछ न होता। यह विचित्र बात है कि मध्यकालीन इतिहास के राजनीतिक या ऐतिहासिक साहित्य में हिंदू-मुसलिम द्वंद्व का कोई छोटे से छोटा प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि हिंदू इसके लिए तैयार न थे। नहीं! वे तो अपनी रणप्रियता के लिए बदनाम थे। लेकिन उस काल की किसी लड़ाई में भी हम सेनाओं को सांप्रदायिक आधार पर लड़ते नहीं पाते। अफगानी सिपाहियों का एक दस्ता तराइन की लड़ाई में राय पिथौरा के नीचे लड़ा था। मुसलमानों की एक पैदल सेना ने पानीपत की लड़ाई में मराठों की मदद की थी। असली हिंदू-मुसलिम लड़ाई तो वास्तव में कभी हुई ही नहीं।’
(नवंबर, 1931)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.