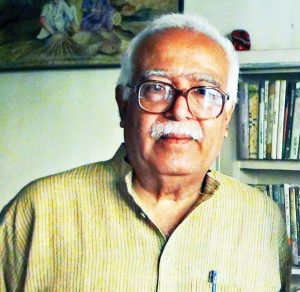
1. दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ
दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ!
इतनी काली अँधेरी है यह चादर कि जैसे
काले सन्नाटे की गुफा
कि अब रास्ते बिलाने लगे हैं
हताशा की हारी हुई राह पर
डगमग-डगमग पाँव…
काँपती है साँस की डोरी, घुटने काँपते हैं
दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ
कुछ ऐसे
कि खुद पर खुद का यकीन नहीं रहा अब
कल तक थे जो मेरे आसमान के जगमग नक्षत्र
हर कदम पर पाथेय मेरी जिंदगी के
और उपलब्धि की वैदूर्य मणियाँ
समय ने बुहारकर उन्हें एक बेछोर कूड़ेदान के हवाले किया
कभी-कभी टिम-टिम चमकती है उनमें उम्मीद कोई
अगले पल बुझती है
बुझी हुई जिंदगी के बोझ को और गाढ़ा
और अँधेरा बनाती हुई
दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ!
और समय के साथ बदल गई हैं सब चीजें
और सिलसिले जीत-हार के
यों भी समय के साथ बदल जाता है बहुत कुछ
यहाँ तक कि सुख के नग्मे और दुख के आँसू तक
इन दिनों हर राह चलते
का दुख देख भीगती हैं आँखें बह आते आँसू
गला रुँधने लगता है
पर कोई करता है किसी के साथ कुछ अच्छा
कोई भला हाथ उम्मीद की डोर लिये थपथपाता है
किसी की पीठ
तो मारे खुशी के हिलक-हिलककर रोने लगता हूँ
पता नहीं, रोने और हँसने का फर्क कहाँ चला गया?
दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ!
और अँधेरे और हताशा से घबराकर
अब जिंदगी को जिंदगी की तरह जीने के बजाय
मैं एकांत विथा में रास्ते खोजने लगा हूँ
मगर रास्ते कभी मिलते हैं और कभी एक और
निबिड़ अंधकार में छोड़ जाते हैं छटपटाने को
जहाँ न टिम-टिम तारे हैं
न उम्मीद के हर पल रोशन चाँद-सूरज के नग्मे
न पुरानी स्मृतियों के टूटे तिनके
न नदी न कगार
तो फिर जाऊँ कहाँ और कैसे,
कहाँ उतार दूँ भार इस बेमानी और अंतहीन सफर का
कि शेष हो जिंदगी का सिलसिला बेमतलब…
दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ!
और समझ में नहीं आ रहा
कि मैं क्यों यों खुद को खींचता चला जा रहा हूँ निरर्थक लंबा
जबकि जीने में कुछ दम ही नहीं बचा अब
दुख ने अपनी चादर तान दी है माँ!
और अब काली आँधियों-सा निबिड़ अंधकार है चारों ओर बस
और इस अंधकार में मेरी पुकार कहीं नहीं जाती माँ,
शायद तुम तक भी नहीं
तो फिर मैं क्यों पुकार रहा हूँ लगातार माँ!
किसलिए…?
2. हत्यारे
दुनिया के और पेशों की तरह हत्या भी एक पेशा है
बता रहा था वह हँसते हुए
तो उसकी हँसी से टपक रहा था
बूँद-बूँद
लहू
जैसे कोई भेड़िया शिकार करते हुए जंगल में अट्टहास कर रहा हो…
और मैं डर गया था।
आज भी याद आती है उसकी हँसी
और मैं भीतर तक सिहरता हूँ
हालाँकि अखबारों के रोजनामचे उसी की तसदीक करते हैं
कि हत्यारे आते हैं और बड़ी सफाई से
करके जाते हैं अपना काम
जिसके उन्हें पैसे मिलते हैं और फायदा
किसी और को
यह देश फायदे और सिर्फ फायदे की फिलास्फी का देश
बनता जा रहा है
क्या इसीलिए इतनी बढ़ रही हैं हत्याएँ?
पूछता है एक बूढ़ा दरवेश पतियाई आवाज में
एक घायल परिंद सा छटपटाता सवाल,
और मैं सन्न हूँ—
क्या जवाब दूँ उसे?
हालाँकि अपने अनुभव से जानता हूँ कि किस्म-किस्म के
बुद्धिजीवियों की तरह
किस्म-किस्म के हत्यारे हैं इस देश में
सबकी अपनी-अपनी शैली, अंदाज और तौर-तरीके
मसलन कुछ हैं जो कि शोर मचाते और गालियाँ बकते
हुए आते हैं
और फिर करके अपना काम हवा में गोलियाँ चलाते
हुए भाग निकलते हैं
कुछ चुपके से आते हैं और करते हैं अचानक
पीछे से वार
और फिर एक ही शांत क्रिया से सब खत्म…
न धूल न धुआँ न शोर-शराबा मगर वार अचूक!
कुछ जो राजनेताओं की संगत में उठते-बैठते हैं
वे लाठी भी न टूटे और साँप मर जाए
वाली शैली के हैं हत्यारे
कहीं पर निशाना कहीं वार वाले कलावंत खिलाड़ी
उनसे कुछ ही भिन्न हैं जो हमेशा दूसरों के कंधों पर
रखकर बंदूक
चलाते हैं और निशाना उनका कभी नहीं चूकता
पर सबसे शातिर हैं वे हत्यारे
जो शांत चेहरे और सधे हाथों से सामने रखे कागज पर
कुछ लिखते हैं
और देखते ही देखते कट जाती है सामने वाले की जीभ
गरदन झूल जाती एकाएक
रस्सी पर…
और फिर सब शांत!
कहीं कोई चीं-चूँ तक नहीं
मगर तीर दिल और दिशाओं के पार…
अपरंपार।
माननीयों वाले आत्मविश्वास और चुप्पी से
करते हैं वे सारा काम
और कोई पूछे तो उतनी ही बारीक छिपी हुई मुसकान
के साथ कहते हैं—
‘ओह, ऐसा हुआ क्या…? अच्छा, चच्च!
पर चलो, अब किया भी क्या जा सकता है?’
और फिर दोस्तों के साथ कला और संगीत और
शेक्सपियर के
किसी क्लासिकल ड्रामे
की बारीकियों की चर्चा करने लगते हैं।
मैं अपने अनुभव से जानता हूँ
हत्यारों की यही कोटि है सबसे नृशंस
यही अचूक
और
भीषण दुर्दांत
जिनकी एक मीठी बात में है सौ साँपों का जहर
इसीलिए उनका काटा पानी नहीं माँगता
और दुनिया के सब हत्यारे उनकी गोद में खेलते हैं।
3. एक बूढ़े मल्लाह का गीत
अपनी थकी हुई पुरानी नाव खेता
मैं देख रहा हूँ अपने इर्द-गिर्द नन्ही-नन्ही किश्तियाँ
बड़ी ही चंचल, शरीर और अलमस्त किश्तियाँ कागज की
जो लहरों पर लहर होकर बढ़ी जा रही हैं
इस बुलंद हौसले के साथ कि जैसे कभी रुकेंगी ही नहीं,
नहीं थमेंगी कहीं भी…
और नदी-नालों और समुद्रों की छाती पर हो सवार
विजेता बनकर लौटेंगी एक दिन
वे कागज की किश्तियाँ हैं
नन्हे हाथों के नन्हे इरादों से बनी
पर उनके भीतर ताजा मन, ताजी इच्छाओं
के हैं बहुरंगे पुष्पगुच्छ और मोरपंख गर्वीले
उनके खिले हुए चेहरों की हँसी
हजार घातक तूफानों पर भारी
वे प्रलय के तूफानों पर हँसकर सवारी कर सकती हैं
कि जैसे यह भी हो कोई खो-खो नुमा दिलचस्प खेल
इस अथाह समंदर की हिचकोले खाती विशाल छाती पर
मैं देख रहा हूँ नन्ही-नन्ही किश्तियाँ
और खुश हूँ
कि अब जबकि मैं समेट रहा हूँ अपनी जिंदगी का
आखिरी पाल
और हसरतों से देख रहा हूँ अपना बूढ़ा चप्पू
तब हजारोंहजार किश्तियाँ ये
हवाओं से मीठी छेड़छाड़ करती
चली जा रही हैं एक बेपरवाह धुन में
अलमस्त
असीसें निकलती हैं भीतर से
जियो…जियो मेरे अनगिनत बेटो, बेटियो
कि हमारी हारी हुई लड़ाइयाँ, खीज और टूटन…
तुम्हारे हाथों में बन जाएँ
अमोघ अस्त्र, ढाल और कवच
कि तुम विजेता होकर लौटो
वहाँ-वहाँ से भी, जहाँ हम हारे…
अपने संशय, अविश्वास और कौशल की कमी से।
नदी किनारे के हरे-भरे बूढ़े पेड़
तुम्हारे आगे हरे पत्तों का बंदनवार सजाएँ
और जब तुम लौटो अपनी गर्वीली विश्वयात्राओं से
तो बिछाएँ तुम्हारी राह में महकते फूलों के कालीन
तब यह बूढ़ा मल्लाह शायद न रहे
पर इस बूढ़े मल्लाह का बूढ़ा चप्पू
नदी के एक किनारे पर उपेक्षित पड़ा
टूटते सुर में
नए युग के नए आने वाले विजेताओं का
विजय-गीत गा रहा होगा…
गाता रहेगा धीरे-धीरे टूटकर बिखरने तक

4. भीष्म साहनी को याद करते हुए
यहीं कहीं कोई भीष्म साहनी था
जो गुजर गया…
यहीं इसी जमीन पर,
जिसे कितने ही ताकतवर पैर
कितनी तरह से कुचल रहे हैं
दूर तक एक सांस्कृतिक सन्नाटे को तोड़ते
नए तानाशाहों के जूते ठक-ठक बजते हैं।
कोई एक भोंपू सुबह से शाम तक चीखता है—
हमें नई सुबह नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए नए विचार!
उनका हर ‘सुप्रभात’
आज से पाँच हजार साल पहले हो चुका होता है!
यहीं…यहीं—इसी जमीन पर—
जहाँ धूल और धुएँ के गुबार आप देखते हैं,
जरा गौर से देखें तो हवा में वह प्रागैतिहासिक किला
नजर आ सकता है,
जहाँ काठ की तलवारों से इतिहास की झूठी
लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं
जहाँ कुछ भरे हुए पेटों की लाठियाँ
मंदिर-मस्जिद से ऊबकर
अचानक मजदूर और किसानों पर टूट पड़ती हैं
और कहीं हलकी चीख तक नहीं सुनाई देती
यहीं…
यहीं जहाँ जमीन धूल के बगूले बहुत उगलती है
यहीं कहीं दरम्याने कद का
एक दुबला सा लेखक था भीष्म साहनी
जो गुजर गया!
मैं दर्जनों बार आविष्ट चेहरा लिये उससे मिला
उसकी आँखों में हमेशा एक पैनी चमक थी,
जो हमेशा मुसकराते रहने का भरम देती थी।
मैंने उसे कभी ऊँची आवाज में बोलते नहीं सुना,
मैंने उसे कभी अभिमान से कहते नहीं सुना
कि चूँकि हम लेखक हैं, इसलिए बड़े हैं।
मैंने उसे जिंदगी भर किसी पर हिकारत से
हँसते नहीं देखा,
नहीं उछालते देखा कोई चालाक फिकरा!
कोई चालीस बरस पहले
जब मैं पहलेपहल अपने युवा गुस्से और पागलपन के साथ
उससे मिला था
खाया झुलसा और झल्लाया हुआ
तब भी, याद है—मेरी हर तीखी फब्ती के जवाब में
वह मुसकराता रहा था
फिर हँसते-हँसते उसने धीरे से
प्रेमचंद की ओर उँगली उठा दी थी—
देखो प्रकाश मनु, प्रेमचंद…!
बोलते समय जिनके किरमिच के फटे जूतों से निकली
पैर की काली उँगली बाहर झाँक रही होती थी
न प्रेमचंद को उसकी परवाह होती थी
न सुनने वालों को!
और अब मैं भीष्म नहीं, प्रेमचंद के रू-ब-रू था
और मेरा मलाल बह गया…!!
कोई भावुक खामख्याली, कोई शब्दों का खेल नहीं…
बस, छोटे-छोटे वाक्यों के टुकड़ों पर टुकड़े जमाते
उन्होंने अपनी तकरीर पूरी की थी
पूरे इत्मीनान से
जैसे कोई होशियार राज ईंट पर ईंट रखकर
एक सीधी दीवार बनाता है
और दीवारों से एक घर…
वह घर जो प्रेमचंद का घर था
मगर जो किसी भी लेखक का घर हो सकता है!
मामूली तूलिका से बड़ी लकीरें खींचता वही भीष्म साहनी
जो यहाँ था,
हलके कदमों से चहलकदमी करते हुए
अभी-अभी कैनवस से बाहर चला गया।
वही भीष्म साहनी जिसने ‘तमस’ नहीं
एक पछाड़ें खाती इनसानियत का इतिहास लिखा,
फिर ‘मय्यादास की माड़ी’ में ले जाकर
इतिहास की विडंबनाओं से गुजरे पंजाब के रिसते घाव दिखाए
वह कल तक यहीं कहीं आसपास था
जो गुजर गया।
मैंने उसे कभी अखबारों में नहीं देखा
क्योंकि अखबारों में रोज नया शगूफा छोड़ते
कुछ मल्ल किस्म के साहित्यिक महानों का स्थायी अधिवास था
जो हर चीज को ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर
ले जाने की
कला में उस्ताद थे
और जिस दिन अखबार में नहीं छपता था उनका नाम
उनकी सुबह, सुबह नहीं होती थी।
इसके लिए दोस्तों और दुश्मनों पर
मेहबानियाँ करने से लेकर
उनके पास कई किस्म के मामले ओर एजेंडे थे!
पर उन महानों के बीच धीमी मगर सुती हुई आवाज में
आहिस्ता-आहिस्ता सोचकर बोलने वाला
एक भीष्म साहनी था,
जिसकी धीमी आवाज अचानक किसी ‘तमस’ में
बुलंद हो जाती
तो तूफान आ जाता था।
वह शख्स जो कभी चमकीली सुर्खियों में नहीं रहा
हमने देखा, मरकर भी साहित्य के तमाम महाभट्टों
से ज्यादा जिंदा है…
हालाँकि वह चला गया
मगर जाकर भी कहाँ गया!
यह दीगर बात है कि जिनकी सारी जिंदगी
हर प्रगति को प्रगति से भिड़ाने में गुजरी है
इस बात से बेपरवाह कि पास ही लाल आँखें किए भेड़िए
बस, अब झपटने को ही हैं…
वे अब भी उसी तरह कूदने और जमीन खूँदने
के खेल में व्यस्त हैं
मैंने उन अहंकारियों से
उस विनम्र, दुबले और आहिस्ता-आहिस्ता
अपनी चाल से चलने वाले लेखक के बारे में पूछा
जो कभी जोर से नहीं बोला,
और कभी गरूर से नहीं बोला
तब कंधे उचकाते हुए उनमें से एक ने
कहा—
हाँ-हाँ, यहीं कहीं कोई भीष्म साहनी था,
जो गुजर गया।
जी हाँ, एक भीष्म साहनी था, जो गुजर गया।
5. कुबेर की याद में
यह खिला हुआ फूल मैं तुम्हें भेंट करता हूँ
कुबेरदत्त!
जिस दिन तुम गए उसी दिन यह खिला
पूरे जोम में पूरी लाली और रंगत के साथ
जैसे तुम थे मृत्यु की घाटी में अपनी यकबयक लंबी
छलाँग के वक्त
अपनी पूरी रंगत और आब में—
कुबेरदत्त, यह खिला हुआ फूल मैं तुम्हें भेंट करता हूँ।
जानता हूँ जहाँ तुम गए हो वहाँ से कोई नहीं लौटता
पर तुम आओगे—यकीनन आओगे
जैसे रात के ग्यारह-बारह के बीच
फोन पर तुम्हारी आवाज—माफ करना, बड़े भाई,
तुम डिस्टर्ब तो होगे पर मैं रह ही नहीं पाया
आ रही थी बहुत याद और बात थी कुछ ऐसी कि…!
आवाज में ऐसी नरमी और लज्जत
कि गुस्सा आए तो पानी हो जाए
और आदमी बहे तो कूल-किनारे तोड़कर
फिर बहता ही जाए
पता नहीं कौन बड़ा था कौन छोटा
पर तुम कहते थे तो मैं ही आहिस्ता से
बड़े वाले गद्दे पर बैठ जाता था
और सहेज लेता था जो कुछ उमड़ता था तुम्हारे भीतर
किसी खिले-अधखिले कविता के फूल की मानिंद
फिर चाहे नंदन जी का नजारा हो
या कालेवाला के विष्णु खरे की उधेड़बुन।
बड़े भाई, नंदन जी तो एकदम हत्थे से उखड़ गए
ये सवाल सिर्फ तुम्हीं पूछ सकते थे बड़े भाई,
याद करेंगे नंदन जी भी कि किसी ने लिया था इंटरव्यू
कि उन्हें उतरना पड़ गया पानी में!
आवाज आवाज थी कि गुनगुने पानी का झरना
मालूम नहीं—
पर उसमें कोई हँसी की चटुल मछली उछली थी
कि फिर एकाएक गुड़ुप…
शराब थी कि बह रही थी फोन के तार और चोगे में
और मैं कितनी शराब कितनी संवेदना कितना भीतर तक
जला हुआ लहू—
इस हिसाब में वाबस्ता
घुल रहा था उस आवाज की नरमी में
जो मुझ तक आती थी फिर रुक-रुक कर
घूँट भरने लगती थी
घूँट-घूँट जिंदगी को पिया जा रहा था
घूँट-घूँट मृत्यु छलछला रही थी।
और फिर आवाज में घुलता-छनता
खिला एक दिन कालेवाला का काला फूल
कि उस कालेवाला में विष्णु खरे के आजू-बाजू
औघड़ बाबा नागार्जुन सत्यार्थी त्रिलोचन
आल्हा-ऊदल सिंहासन बत्तीसी और न जाने कौन-कौन
गल्प और महाकाव्य—
कैसा-कैसा जुड़ता चला गया मेला
और वहाँ लोक का वैभव था वैभव का धरती-आकाश।
वाह, एक मुकम्मल इंटरव्यू बड़े भाई,
मुकम्मल एकदम
आह, मुझे कितना सुख मिला है
आज की रिकार्डिंग में बड़े भाई
काश, मैं बता पाता!
आवाज एक समंदर थी
समंदर शराब और संवेदना से दहकता
समंदर छलक रहा था बार-बार फोन के चोगे से
मेरे छोटे-से कमरे में
कमरे के फर्श पर…
और भीग रहे थे छोटे-बड़े हम चारों प्राणी
और चीजें जो कमरे में थीं
और समंदर जो फर्श पर बह आया था
उससे लहरों पर हिलता-काँपता बन रहा था
डब-डब एक चेहरा—
कुबेरदत्त!
कुबेरदत्त, फूल खिला है मेरे घर में
ठीक उसी दिन जिस दिन निगमबोध घाट पर
तुम्हें निःशेष होते देख मैं लौटा हूँ
लाल सुर्ख फूल यह गुड़हल का पूरे जोम में है
जैसे तुम थे अपनी सृजन-चेतना में पूरे रचे-बसे जब गए
इस फूल में धीरे-धीरे उतरते जा रहे हैं
बहुत खूबसूरत लिखाई वाले तुम्हारे कैप्शंस
खेल-खेल में बने तुम्हारे अमूर्त रेखांकन और कविता की पंक्तियाँ…
यह फूल अब धीरे-धीरे तुम्हारे चेहरे में बदलता जा रहा है
कुबेरदत्त,
और चेहरा नहीं, आवाज—
भीतर किसी अनकहे सच को झकझोरती आवाज
जिसमें सारी दुनिया का गम है!
आवाज का चेहरा कि चेहरे की आवाज…?
एक लाल फूल अपने पूरे जोम में खिला हुआ
यह तुम हो कुबेरदत्त!
यह फूल मैं तुम्हें भेंट करता हूँ।
जानता हूँ, तुम अब नहीं रहे
पर तुम आओगे—आओगे जरूर,
जैसे आती है तुम्हारी आवाज कहीं भीतर से
आती रहेगी हमेशा-हमेशा उसी शिद्दत से।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

















