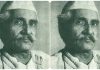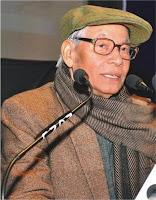 लोहियाजी से मेरा संपर्क विद्यार्थी जीवन में हुआ। 1953-54 में लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच जो राजनैतिक माहौल था, उसमें सभी प्रायः दो प्रमुख पार्टियों में विभाजित थे। एक थे साम्यवादी और दूसरे समाजवादी। मैं समाजवादी आन्दोलन से जुड़ा था। लेकिन मैं कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि कभी-कभार अपना बौद्धिक योगदान दे दिया करता था। लोगों से मिलता-जुलता था और गोष्ठियों में भाग लेता था। वहाँ विचारों का जो आदान-प्रदान होता था, वह बहुत ही उग्र और सार्थक हुआ करता था जिनमें मुख्यतः साम्यवादी दर्शन और उसके प्रतिपक्ष में समाजवादी दर्शन था। इन गोष्ठियों में विद्यार्थियों के आमंत्रण पर लोहियाजी लखनऊ विश्वविद्यालय आते थे और छात्रों का मार्गदर्शन करते थे। लोहियाजी जब वहाँ रुकते थे, तो हम लोगों को उनसे कभी-कभार छोटी-सी मुलाकात करने का मौका मिल जाता था। बाद में, मैं पढ़ाई और शोध कार्य में रम गया। फिर भी अपने मित्रों के माध्यम से समाजवादी आन्दोलन और विचारों से संपर्क बना रहा। परन्तु फिर लोहियाजी के सानिध्य का मौका नहीं मिल पाया।
लोहियाजी से मेरा संपर्क विद्यार्थी जीवन में हुआ। 1953-54 में लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच जो राजनैतिक माहौल था, उसमें सभी प्रायः दो प्रमुख पार्टियों में विभाजित थे। एक थे साम्यवादी और दूसरे समाजवादी। मैं समाजवादी आन्दोलन से जुड़ा था। लेकिन मैं कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि कभी-कभार अपना बौद्धिक योगदान दे दिया करता था। लोगों से मिलता-जुलता था और गोष्ठियों में भाग लेता था। वहाँ विचारों का जो आदान-प्रदान होता था, वह बहुत ही उग्र और सार्थक हुआ करता था जिनमें मुख्यतः साम्यवादी दर्शन और उसके प्रतिपक्ष में समाजवादी दर्शन था। इन गोष्ठियों में विद्यार्थियों के आमंत्रण पर लोहियाजी लखनऊ विश्वविद्यालय आते थे और छात्रों का मार्गदर्शन करते थे। लोहियाजी जब वहाँ रुकते थे, तो हम लोगों को उनसे कभी-कभार छोटी-सी मुलाकात करने का मौका मिल जाता था। बाद में, मैं पढ़ाई और शोध कार्य में रम गया। फिर भी अपने मित्रों के माध्यम से समाजवादी आन्दोलन और विचारों से संपर्क बना रहा। परन्तु फिर लोहियाजी के सानिध्य का मौका नहीं मिल पाया।
पहली बार जब मैंने लोहियाजी को सुना था तो वे लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देश के हालात पर भाषण दे रहे थे। लोहियाजी अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे और जर्मनी में उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोम्बार्ट के साथ शोधकार्य भी किया था। मुझे उनका भाषण अभी तक याद है और उसमें जो सूत्र था वह यह था कि भारतवर्ष विश्व के अन्य देशों के संदर्भ में आर्थिक दृष्टि से क्या स्थान रखता है। उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से सभी देशों का स्तरीकरण किया और तार्किक ढंग से समझाया कि वही देश आर्थिक रूप से आगे हैं, जो सबसे ज्यादा स्टील पैदा करते; जिसमें भारत उस वक़्त काफी पिछड़ा था। अगर आज हम उनकी बातों को समझने की कोशिश करें कि उसमें एक संदेश था कि औद्योगिक प्रक्रिया को हमें और भी सक्रिय ढंग से आगे बढ़ाना होगा।
लोहियाजी की बातें विद्यार्थियों को काफ़ी आकर्षित करती थीं। जब वे व्यक्तित्त्व के बारे में, राजनीतिज्ञों के बारे में करते थे, तो विद्यार्थी उसे काफ़ी रुचि से सुनते थे। लेकिन उसमें जो बौद्धिक पुट हुआ करता था, उसे कितने लोग आत्मसात् करते थे यह कहना मुश्किल है। समाजवादी विचारधारा में लोहियाजी का काफ़ी योगदान था जिसे समझने के लिए समाजवादी विचारधारा के ऐतिहासिक पक्ष को समझना होगा। लोहियाजी जिस वक़्त विद्यार्थी थे, उस वक़्त योरोप में जो ज्ञान की लहर और विचारों का संघर्ष था, उससे समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ और दूसरा उसके साथ-साथ क्रांतिकारी-साम्यवादी विचारधारा का भी उदय हुआ। उस वक़्त वहाँ दोनों गुटों में काफ़ी कठिन संघर्ष होता रहता था। समाजवादियों का भी यही मानना था और साम्यवादियों की भी यही मान्यता थी कि बराबरी हो, सबको नौकरियाँ मिलें और संसाधनों पर जनता का आधिपत्य हो न कि कुछ पूँजीवादियों का। लेकिन मुख्य बात जो साम्यवाद से अलग करती है कि जनतंत्र या प्रजातंत्र के बारे में दोनों की राय अलग हैं।
समाजवादी राज्य को सशक्त करने के लिए जनता को सशक्त करने के पक्षधर हैं। वहीं साम्यवाद में पार्टी और पोलित ब्यूरो का प्रावधान है। आजादी की लड़ाई में भी सभी राजनीतिक दल अलग-अलग थे, साम्यवादी अलग थे, कांग्रेसी अलग थे और कांग्रेस में भी समाजवादी अलग थे, राष्ट्रीय आन्दोलन में लोहियाजी की उतनी ही भूमिका थी, जितनी गांधी या नेहरू की। गांधी सबसे ऊपर थे और उनको सभी मानते थे। सभी अपने-अपने तरीके से संघर्ष कर रहे थे। लोहियाजी ने तो कई बार व्यक्तिगत बलिदान भी दिया। वे तो आज़ादी के बाद भी कई बार जेल गए। लोहियाजी का कहना था कि हमें आज़ादी पहले उपनिवेशवाद से लेनी है।
जो ब्रिटिश राजसत्ता की उपनिवेशिक सत्ता थी, लोहियाजी उसके पूर्ण रूपांतरण के पक्षधर थे यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों ही रूपों से। आज़ादी के बाद उनका कांग्रेस से नीतिगत विरोध था। इसी कारण कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का बिखराव हुआ। पहला मतभेद तो नीतियों को लेकर था और दूसरा मतभेद नीतियों के कार्यान्वयन को लेकर था। लेकिन समाजवादियों की यह विडम्बना है कि वे सत्ता में पूरे तौर पर कभी आ नहीं पाए जबकि नीतिगत योजना को वास्तविकता के धरातल पर उतारने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ इतने दल, इतने समूह और इतनी विभिन्नताएँ है कि किसी नीति को लागू करने के लिए कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं।
जयप्रकाश नारायण ने मॉडल दिया था, लेकिन वे उसे लागू कहाँ कर पाए। जो जनता सरकार बनी वह भी उसी नीतियों पर चलती रहीं फलस्वरूप समाजवादियों के मॉडल को लागू करने में असफल रही। दूसरी तरफ समाजवादी आन्दोलन के अनूठेपन और विकेन्द्रीकरण के कारण इसमें जुड़े सारे लोग अलग-अलग ध्रुव और अलग-अलग दिशाओं में चलते चले गए। यह आन्दोलन पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हो पाया; जितनी इसकी क्षमता थी। लोहियाजी के समाजवादी आन्दोलन में योगदान को समझने के लिए उनकी अनूठी राजनीतिक शैली को समझना होगा।
उस वक़्त समाजवादियों के तीन स्तंभ थे-जयप्रकाश, लोहिया और आचार्य नरेन्द्रदेव। जयप्रकाशजी भूमिदान और विनोबा आन्दोलन के द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण में लगे रहे; वहीं आचार्यजी बौद्धिक थे। वे पार्टी में शामिल होकर भी राजनीतिक रूप से कम और बौद्धिक रूप से ज्यादा सक्रिय थे। लोहियाजी की शैली बिल्कुल अलग थी। जो चीज उन्हें गलत प्रतीत होती, उसके खिलाफ़ वह आवाज उठाते थे और आन्दोलन करते थे। उनके प्रतिरोध करने, जेल जाने, आवाज उठाने में सक्रियता ज्यादा रहती थी। वह किसी की परवाह नहीं करते थे। गलत चीज के खिलाफ़ वे इस हद तक चले जाते थे कि उनकी बातें कुछ लोगों को नागवार गुजरती थीं। लेकिन उनका मानना था कि अगर प्रभाव पैदा करना है, तो कुछ तल्ख बोलना जरूरी है। बौद्धिक भी वे कम नहीं थे। उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में बहुत-सी पुस्तकें लिखी हैं और इसके अलावा बहुत सारा तुलनात्मक अध्ययन भी किया है।
लोहियाजी अंग्रेजी भाषा के खिलाफ़ लड़ने के लिए जाने जाते हैं; लेकिन उनकी इसके पीछे भावना थी कि देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उनकी सोच थी कि जब तक हम अपनी शिक्षा-दीक्षा विदेशी भाषा में करेंगे, तो हमारे अपने मूल विचार, दर्शन और अस्मिता उभर कर नहीं आ पाएगी। इसलिए दिमाग़ी आज़ादी के लिए वे देशी भाषाओं के पक्षधर थे। अंग्रेजी भाषा के कारण समाज में वर्गीकरण हो गया था। देश में एक अंग्रेजीदाँ अभिजात्य वर्ग का प्रभुत्व हो चुका था। उनके इस आन्दोलन का ही नतीजा था कि बाद में देश में कई सारी देशी भाषाओं को मान्यता मिली।
लोहियाजी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए विशेष अवसर के समर्थक थे। उनका मानना था कि समाज में इनको बराबर की भागीदारी देने के लिए विशेष अवसर मिलना चाहिए। जाति-प्रथा के बारे में लोहियाजी ने एक पुस्तक भी लिखी थी। उनका मानना था कि जाति को हटाने के लिए वर्ग-संघर्ष से असमानताओं को हटाना होगा। जब असमानता हट जाएगी तो जाति-प्रथा निष्क्रिय होकर अपने-आप हट जाएगी। इसे प्राप्त करने के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी और नीतियों में बदलाव के वे पक्षधर थे।
लोहियाजी ने सावित्री और द्रौपदी का बड़ा अनूठा उदाहरण दिया है कि भारतीय महिलाओं का आदर्श द्रौपदी का उदाहरण हमारे सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया, मूल्यों के विन्यास और सामाजिक व्यवस्था के संकुल से जुड़ा है। एक बार अपने एक लेख में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में दो संस्कृतियाँ हैं। एक अवध की संस्कृति है और दूसरी बृज की संस्कृति है। राम और कृष्ण दोनों के प्रतीक हैं। अवध में जहाँ संरचनावाद पर ज्यादा जोर है, वहीं बृज की संस्कृति में भागीदारी को ज्यादा महत्त्व दिया गया है। हमारी परंपरा में इतनी विविधता और विरोधाभास है कि सब अलग-अलग मूल्यों और दिशाओं का संदेश देते हैं। सावित्री एक तरफ जहाँ पारिवारिक मूल्यों और बने हुए सामाजिक नियमों का अनुसरण करती है; जो सामाजिक नियम सत्ता के लोग निर्धारित करते हैं, चाहे वह राजसत्ता हो, परिवारसत्ता या पुरुषसत्ता हो। सावित्री इन नियमों की परिधि में ही अपना अहम् बनाये रखती है।
लेकिन दूसरी तरफ द्रौपदी का सत्ता के प्रति विरोध है; वह पीड़ित है लेकिन उसके मन में आक्रोश है। वह उसका विरोध करती है, आक्रोश व्यक्त करती है और व्यंग्य बोलती है। एक प्रकार से द्रौपदी व्यक्तिगत रूप से सशक्त है। दूसरी तरफ सावित्री अपनी सीमा स्वीकार करती है। यदि महिला को सशक्त करना है तो सांस्कृतिक परिवर्तन लाना होगा; सामाजिक मूल्यों और विचारों में परिवर्तन लाना होगा जैसा कि अमर्त्य सेन ने कहा कि हमें बाहर नहीं जाना है, देश में ही सीखना है। यह विचार लोहिया-दर्शन में निहित है। अगर सावित्री को सशक्त करना है तो हमें द्रौपदी से सीखना होगा।
लोहियाजी ने गैर-कांग्रेसवाद की नीति को काफ़ी जोर-शोर से चलाया। क्योंकि उनका साम्यवादी विचारधारा से बहुत ही विलगाव था। उस वक़्त देश में राष्ट्रीय नीतियाँ बन रही थीं, पंचवर्षीय योजनाएँ बन रही थीं। राजसत्ता को अधिक सशक्त किया जा रहा था और जनता पर केन्द्रित कम था। उन्हें लगा कि राज्य की नीतियों पर साम्यवादी नीतियाँ अधिक हावी हो रही हैं। इसलिए कांग्रेस को हटाने के लिए उन्होंने विभिन्न दलों और मान्यताओं के लोगों से हाथ मिलाया। लेकिन यह उनकी तात्कालिक नीति थी, न कि कोई दूरगामी रणनीति। लोहिया के गैर-कांग्रेसवाद को समझने के लिए यह भी देखना पड़ेगा कि नेहरू के व्यक्तित्व के कारण 1950 के बाद से कितने दशकों तक कांग्रेस की राजसत्ता रही। एक पार्टी और एक व्यक्ति की प्रमुखता हो गई थी। समाजवादियों की संसद में इतनी उपस्थिति नहीं थी कि वे अपनी आवाज़ आसानी से पहुँचा सकें। इसलिए जनतंत्र को सही मायने में लाने के लिए और एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए उन्होंने गैर-कांग्रेसवाद की नीति चलाई।
लोहियाजी ने कहा था कि जिंदा कौमें पाँच साल का इंतजार नहीं करतीं। मुझे इस बात में विरोधाभास दिखाई देता है। यह कुछ ऐसी बात है जो जे० पी० के संपूर्ण क्रांति से अलग है। अगर हमें संविधान के हिसाब से चलना है, तो उसकी इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है कि चूँकि समाजवादी बहुत समय तक सत्ता में नहीं आए, इसलिए उनके विरोध का भावात्मक पक्ष कभी-कभी हावी हो जाता है। अगर उन्हें नीतियाँ निर्धारित करनी होती, राज्य चलाना होता तो यह गौण बात है। वे इस बात को खुद ही महत्त्व नहीं देते। अगर सरकार को पाँच साल से पहले जन-विद्रोह से उतार दिया जाए तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी और लोहियाजी विद्रोही नहीं, बल्कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे।
आज लोहियाजी की दृष्टि और कार्यक्रमों को देखें तो अब विश्व की राजनीति और व्यवस्था इतनी बदल गई है। यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि उनके विचार अब कितने प्रासंगिक हैं। क्योंकि प्रसंग बहुत बदल गया है, प्रासंगिकता बहुत बदल गई है। फिर भी लोहियाजी के बहुत से नीतिगत और राजनैतिक दर्शन अभी भी उतने हीं प्रासंगिक हैं। उदाहरणतः वर्गीकरण, वर्ग-शोषण, जाति और वर्ग के शोषण की व्यवस्था कम हुई है; लेकिन पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो पाया है। आज जिस तरह से देश में क्षेत्रवाद फैल रहा है, वहाँ उनकी विचारधारा अत्यंत प्रासंगिक है। भाषा के प्रश्न पर उनकी प्रासंगिकता स्वयं राजसत्ता ने स्वीकारी। आज बहुत-से राज्यों में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा है। मेरे विचार में आज लोहियाजी अंग्रेजी भाषा को उतना बहिष्कृत नहीं करते। क्योंकि भूमण्डलीकरण और लोगों का प्रवासीकरण से जनसंख्या का एक नया स्वरूप विकसित हो रहा है। आज अंग्रेजी भाषा किसी एक देश की भाषा न होकर, वैश्विक भाषा बन चुकी है। आज भारतीय लोगों की अपनी क्षमताएँ दूसरे देशों से ज्यादा है और अंग्रेजी भाषा इसमें एक बड़ा योगदान कर रही है, तो उनका भाषा-विरोध का दार्शनिक पक्ष आज भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है, अपनी मानसिक और सांस्कृतिक आज़ादी की सुरक्षा के लिए।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.