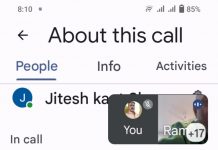— ओम थानवी —
मैं उस घोषित इमरजेंसी का घनघोर निंदक था। आज भी हूँ। कल रात ‘इमरजेंसी’ यह सोचकर देखने गया कि फ़िल्म को फ़िल्म की तरह देखूँगा। लेकिन यह सरासर बेईमान फ़िल्म निकली। निर्देशक कंगना रनौत (अब भाजपा सांसद) की अपनी राजनीतिक भड़ास। इंदिरा गांधी को आरम्भ में “सम्मानित नेता” बताकर निरंतर कलंकित करने की कोशिश।
कहना न होगा कि इस फेर में कंगना ने फ़िल्मजगत को ही कलंकित किया है। वे तथ्यहीनता की हदें लांघ गई हैं। इमरजेंसी के बहाने नेहरू, विजयलक्ष्मी, फ़ीरोज़ गांधी, पुपुल जयकर, निक्सन, जॉर्ज पोंपीदू, मुजीबुर्रहमान, मानेकशॉ, रामन्ना, जे कृष्णमूर्ति आदि के बीच “इन्दु” को संकीर्ण, ख़ुदगर्ज़, झगड़ालू ही नहीं, षड्यंत्रकारी तक बता डाला है।
यों बताया है जैसे इमरजेंसी में नहीं, शुरू से अंत तक वे तानाशाह प्रकृति की थीं। एक प्रसंग में उनके सपने में डायन आती है। प्रधानमंत्री के घर में रात सेवक से आईने के सामने कहलवा दिया कि ये तो आप हैं।
तथ्यों का कोई सिरा नहीं। शास्त्रीजी की शपथ से परदे पर इंदिरा आहत हैं; अगले दृश्य में ताशकंद में “रहस्यमय” मृत्यु; अगले दृश्य में इंदिरा गांधी की शपथ। 1971 के युद्ध से बड़ी “बांग्लादेशियों” की आमद है। पोकरण के परमाणु परीक्षण को विपक्ष को ध्वस्त करने की रणनीति बताया है। वाइट हाउस में इंदिरा के बोल कड़े हैं, पर घबराहट में मानो कांप रही हैं। दिल्ली में निक्सन का फ़ोन आता है तो खड़ी हो जाती हैं।
हाँ, अतिरंजना (जो पूरी फ़िल्म में भरी पड़ी है) के बावजूद संजय गांधी की बुराइयों का बचाव कोई नहीं कर सकता। उनका समांतर सत्तारूप कमोबेश ऐसा ही था। उनकी सनक ने ज़्यादतियों का अंबार खड़ा कर दिया। मीडिया ही नहीं, हर तरह की स्वाधीन अभिव्यक्ति को दबा दिया गया। लेकिन उनकी मौत की उड़ान को माँ की डाँट से जोड़ना छिछला काम है। यों चित्रित किया है मानो स्मृतिदृश्यों की विचलित अवस्था में उन्होंने नियंत्रण खो दिया।
संजय गांधी से भिंडरावाले आकर मिले, यह भी फ़िल्म ही बताती है। हमने तो नहीं सुना। मैं दस साल चंडीगढ़ में रह भी आया हूँ। फ़िल्म में “इंदिरा इज़ इंडिया इंडिया इज़ इंदिरा” देवकांत बरुआ नहीं कहते, इंदिरा गांधी ख़ुद अपने बारे में बुदबुदाती हैं। धीरेंद्र ब्रह्मचारी फ़िल्म में नहीं, पर जे कृष्णमूर्ति को इतना क़रीब बता दिया जो कि वे कभी न थे। और तो और एक जगह कृष्णमूर्ति भी कह रह हैं “इंदिरा इज़ इंडिया”। यह तो बेवक़ूफ़ी भरे चित्रण की इंतिहा हुई।
हिंसा का चित्रण अपार है। त्रिपुरा हो चाहे इमरजेंसी। जॉर्ज फ़र्नांडीज़ को जेल इस तरह पीटा गया, या विपक्षी नेता — राजनीतिक बंदी — जेल में तीसरे दरज़े के अपराधियों सा जीवन बिता आए कभी सुना नहीं। जेपी तो पीजीआई, चंडीगढ़ में भरती रखे गए थे। रघु राय ने वहाँ उनकी अनेक तसवीरें खींची थीं।
बायोपिक में अंत में तथ्यों की (अगर हों) तो संदर्भ-सूची
देनी चाहिए। हालाँकि झूठ ज़्यादा समय टिकता नहीं। पर अंदाज़ा लगाइए कि जिस पीढ़ी को देश के अतीत के बारे में ज़्यादा नही पता, वे इसे “इतिहास” समझकर अपना कितना नुक़सान करेंगे।
हैरानी की बात नहीं कि निर्देशक के नाते कंगना ने निराश किया है। जरा सोचिए, जेपी, वाजपेयी, मानेकशॉ गाना गाते हुए कैसे लगते होंगे। कलाकारों का चुनाव भी सही नहीं है। कंगना अच्छी अभिनेत्री रही हैं। पर चरित्र को निभाने में बिखर गईं। मेकअप वालों ने नाक मिला दी, पर क़द-काठी कहाँ से लाते। आवाज़ तो उनकी यों है जैसे होठों में फ़ेविकोल लगा हो।
अनुपम खेर ने ज़रूर जेपी की भूमिका बेहतर निभाई है। सतीश कौशिक (अब नहीं रहे) तो जगजीवन राम की भूमिका में सर्वश्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। हालाँकि उनके संवादों में जो है, वह पटकथा का झूठ है। वाजपेयी के रूप में श्रेयस तलपड़े कार्टून लगते हैं। विशाक नायर (संजय गांधी), मिलिंद सोमण (मानेकशॉ) और महिमा चौधरी (पुपुल जयकर) जम गए। एक दृश्य में अतिथि भूमिका में मेरे मित्र अरविंद गौड़ भी दिखाई दिए, जो कंगना के गुरु रहे हैं। बालकृष्ण मिश्र एमएफ़ हुसेन हैं, जिन्होंने श्रीमती गांधी को शेर पर सवार ‘दुर्गा’ चित्रित कर दिया था। आगे जाकर कांग्रेस ने ही उन्हें देश छोड़ने को विवश किया।
सबसे बड़ा सरदर्द है फ़िल्म का “संगीत”। अनवरत शोर है, मानो हर घड़ी जंग के नगाड़े बज रहे हों।
(यह फ़िल्म की समीक्षा नहीं, अपने अनुभव का फ़ौरी साझा भर है।)
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.