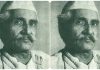— परिचय दास —
।। एक।।
शिवपूजन सहाय को याद करना केवल एक लेखक को स्मरण करना नहीं है बल्कि उस समय-खंड को छूना है जहाँ हिंदी गद्य अपनी सहजता, आत्मीयता और नैतिक दृढ़ता के साथ आकार ले रहा था। उनकी पुण्य तिथि पर स्मृति किसी पुष्पांजलि की तरह नहीं आती, वह आलोचनात्मक विवेक के साथ आती है—जैसे साहित्य स्वयं पूछ रहा हो कि मैंने अपने समय में मनुष्य के पक्ष में क्या किया। शिवपूजन सहाय उस प्रश्न का उत्तर अपने पूरे लेखन से देते हैं। वे न तो भाषा के बाजीगर थे, न विचारधारा के घोषणाकार। उनका साहित्य धीरे-धीरे मन में उतरता है और वहीं ठहर जाता है। यही ठहराव उनकी सबसे बड़ी शक्ति है।
उनका गद्य पढ़ते हुए लगता है कि लेखक पाठक से ऊपर नहीं, उसके बगल में बैठा है। उसमें उपदेश का स्वर नहीं, अनुभव की साझेदारी है। यह साझेदारी किसी एक वर्ग या जाति तक सीमित नहीं रहती; वह किसान, स्त्री, दलित, श्रमिक—सबके जीवन-संघर्षों को समान संवेदना से देखती है। शिवपूजन सहाय के यहाँ करुणा दया नहीं बनती, और यथार्थ निराशा नहीं। वे जीवन की कठिनाइयों को रोमांटिक नहीं बनाते पर उन्हें नकारते भी नहीं। यही संतुलन उन्हें उनके समकालीनों से अलग करता है।
आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो शिवपूजन सहाय उस परंपरा के लेखक हैं, जहाँ भाषा विचार की सेविका है, स्वामी नहीं। उनकी रचनाओं में अलंकार हैं पर वे प्रदर्शनकारी नहीं हैं। उनकी शैली में एक प्रकार की नैतिक सादगी है—जैसे शब्द स्वयं अपने स्थान और मर्यादा को जानते हों। वे न तो संस्कृतनिष्ठता के आग्रह में बहते हैं, न ही अनावश्यक लोकलुभावनता में। यह संतुलित भाषा ही उनके सामाजिक सरोकारों को विश्वसनीय बनाती है।
उनका साहित्य उस समय लिखा गया जब हिंदी समाज तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था—औपनिवेशिक सत्ता, राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक असमानताएँ, और नई शिक्षा-व्यवस्था। शिवपूजन सहाय इन सबको नारे में नहीं बदलते, बल्कि जीवन के छोटे-छोटे प्रसंगों में पिरो देते हैं। यही कारण है कि उनका लेखन आज भी ऐतिहासिक दस्तावेज से अधिक जीवित अनुभव की तरह पढ़ा जाता है। वे समय के इतिहासकार नहीं, समय के साक्षी हैं।
अब उनकी पुस्तकों की ओर बढ़ें तो यह स्पष्ट होता है कि उनका रचनात्मक संसार किसी एक विधा में सीमित नहीं है। कहानी, उपन्यास, संस्मरण, निबंध—हर जगह वही संवेदनशील दृष्टि काम करती है। उनके उपन्यासों में कथानक से अधिक चरित्र महत्वपूर्ण होते हैं। पात्र किसी प्रतीक की तरह नहीं, बल्कि जीवित मनुष्यों की तरह सामने आते हैं—अपनी कमजोरियों, भ्रमों और संघर्षों के साथ।
‘देहाती दुनिया’ उनके लेखन का केंद्रीय ग्रंथ माना जाता है। यह उपन्यास केवल ग्रामीण जीवन का चित्रण नहीं है बल्कि ग्रामीण चेतना का आत्मवृत्त है। यहाँ गाँव किसी रोमानी स्वर्ग की तरह नहीं दिखता, न ही केवल शोषण का अखाड़ा बनता है। शिवपूजन सहाय गाँव को उसकी पूरी जटिलता के साथ प्रस्तुत करते हैं—जहाँ प्रेम है पर भय भी है; परंपरा है, पर जड़ता भी है। इस कृति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी दृष्टि है, जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है।
‘मेरा जीवन’ जैसे आत्मकथात्मक लेखन में शिवपूजन सहाय आत्मश्लाघा से पूरी तरह मुक्त दिखाई देते हैं। वे अपने संघर्षों को महिमामंडित नहीं करते, बल्कि उन्हें सामान्य मनुष्य के अनुभव की तरह रखते हैं। यहाँ आत्मकथा किसी उपलब्धि-पत्र की तरह नहीं बल्कि आत्मालोचना की तरह सामने आती है। यह साहस दुर्लभ है, और यही इसे साहित्यिक रूप से मूल्यवान बनाता है।
उनकी कहानियों में घटनाएँ कम, स्थितियाँ अधिक हैं। कहानी किसी चौंकाने वाले मोड़ पर समाप्त नहीं होती बल्कि मन में प्रश्न छोड़ जाती है। यह प्रश्न अक्सर नैतिक होता है—हम क्या हैं, और क्या हो सकते थे। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में सामाजिक विषमता, स्त्री की स्थिति, और वर्ग-संघर्ष जैसे विषय बिना किसी वैचारिक शोर के उपस्थित होते हैं। वे पाठक को सहानुभूति के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि उसे देखने के लिए विवश करते हैं।
उनके आलोचनात्मक लेखों में भी वही संतुलन दिखाई देता है। वे किसी लेखक को खारिज करने या स्थापित करने की जल्दी में नहीं रहते। उनकी आलोचना मूल्यांकन है, निर्णय नहीं। यह आलोचना पाठक को साहित्य से जोड़ती है, न कि उसे विद्वता के बोझ से दबाती है। उनकी आलोचनात्मक भाषा में भी रचनात्मक ऊष्मा बनी रहती है।
शिवपूजन सहाय की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नैतिक गंभीरता दी, बिना उसे बोझिल बनाए। वे प्रगतिशील थे पर वैचारिक कट्टरता से मुक्त। वे परंपरा का सम्मान करते थे पर अंधभक्ति नहीं करते थे। यही द्वंद्वात्मक संतुलन उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाता है। उनकी पुण्य तिथि पर जब हम उनके साहित्य को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने किसी एक आंदोलन या विचारधारा के लिए नहीं लिखा बल्कि मनुष्य के लिए लिखा। उनका साहित्य हमें किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँचाता बल्कि सोचने की आदत देता है। और शायद यही किसी लेखक की सबसे बड़ी विरासत होती है—कि वह हमें थोड़ा अधिक मनुष्य बना दे।
आज के शोरगुल भरे समय में शिवपूजन सहाय का लेखन एक धीमी आवाज़ की तरह है, जिसे सुनने के लिए ठहरना पड़ता है लेकिन जो ठहर जाता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। उनके शब्द आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि साहित्य का मूल उद्देश्य चमकना नहीं, समझना है; जीतना नहीं, संवाद करना है। यही संवाद उनकी सबसे स्थायी स्मृति है।
।। दो ।।
शिवपूजन सहाय के रचनाकार व्यक्तित्व को यदि केवल कथाकार, उपन्यासकार या आलोचक के रूप में देखा जाए तो उनके समग्र अवदान के साथ अन्याय होगा। उनका एक ऐसा पक्ष है, जो प्रत्यक्ष रचनाओं से अधिक दूरगामी प्रभाव रखता है—साहित्यिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक संपादक का पक्ष। यह पक्ष उनके व्यक्तित्व का सबसे शांत पर सबसे निर्णायक आयाम है। वे मंच पर खड़े होकर भाषण देने वाले साहित्यकार नहीं थे; वे परदे के पीछे रहकर साहित्य की दिशा तय करने वाले विवेकशील कर्मी थे।
शिवपूजन सहाय के लिए संपादन केवल पाठ-संशोधन या भाषा-सुधार की प्रक्रिया नहीं थी। वह एक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व था। वे पत्रिका को केवल छपने वाली सामग्री का संकलन नहीं मानते थे बल्कि उसे समय की चेतना का वाहक समझते थे। संपादक के रूप में उनकी दृष्टि हमेशा व्यापक रही—वे साहित्य को समाज से काटकर नहीं देखते थे और समाज को साहित्य के नीचे दबाकर भी नहीं। यही कारण है कि उनके संपादकीय प्रयासों में संतुलन, मर्यादा और दूरदर्शिता दिखाई देती है।
उनके संपादन में एक प्रकार की नैतिक सजगता थी। वे किसी रचना को केवल इसलिए स्थान नहीं देते थे कि वह चर्चित है या किसी बड़े नाम से जुड़ी है। उनके लिए रचना का आंतरिक सत्य अधिक महत्त्वपूर्ण था। यही कारण है कि कई नए और अल्पज्ञात लेखकों को उन्होंने मंच दिया, बिना इस चिंता के कि इससे उनकी पत्रिका की ‘प्रतिष्ठा’ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनका विश्वास रचना की शक्ति में था, प्रचार में नहीं।
संपादक शिवपूजन सहाय का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने साहित्य को विचारधारात्मक अखाड़ा नहीं बनने दिया। उस समय जब साहित्यिक पत्रिकाएँ स्पष्ट राजनीतिक या वैचारिक खेमों में बँटती जा रही थीं, शिवपूजन सहाय ने संवाद की जगह बनाए रखी। वे असहमति से डरते नहीं थे, लेकिन कटुता को साहित्य का स्वभाव भी नहीं मानते थे। उनके संपादकीय निर्णयों में यह साफ दिखता है कि वे विविध स्वरों को एक साथ सुनना चाहते थे।
सांस्कृतिक दृष्टि से भी उनका संपादन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी साहित्य को केवल शहरी, शिक्षित मध्यवर्ग तक सीमित नहीं रहने दिया। लोक, ग्रामीण जीवन, पिछड़े इलाकों की संवेदना—इन सबको उन्होंने साहित्यिक वैधता प्रदान की। यह कार्य उन्होंने नारेबाज़ी से नहीं बल्कि चयन से किया। उनके द्वारा प्रकाशित रचनाएँ स्वयं यह सिद्ध करती थीं कि साहित्य का केंद्र केवल महानगर नहीं होता।
रचनात्मकता के संदर्भ में शिवपूजन सहाय का संपादक रूप विशेष ध्यान योग्य है। वे रचना को ‘तैयार माल’ की तरह नहीं देखते थे। कई बार वे लेखक के साथ संवाद करते, सुझाव देते पर कभी अपनी शैली या दृष्टि थोपते नहीं थे। यह दुर्लभ गुण है। अधिकांश संपादक या तो पूर्ण हस्तक्षेप करते हैं या पूर्ण उदासीनता दिखाते हैं। शिवपूजन सहाय बीच का रास्ता चुनते हैं—संवेदनशील मार्गदर्शन का।
उनकी यह संपादकीय विनम्रता दरअसल उनके गहरे आत्मविश्वास का प्रमाण है। जो व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, वही रचना पर अधिकार जताता है। शिवपूजन सहाय को न अपने कद को सिद्ध करने की जल्दी थी, न अपनी वैचारिक छाया फैलाने की आकांक्षा। वे साहित्य को लेखक से बड़ा मानते थे और पाठक को संपादक से।
सांस्कृतिक कर्मी के रूप में भी उनका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने साहित्य को केवल पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहने दिया। उनकी दृष्टि में साहित्य जीवन से संवाद करने का माध्यम था। इसलिए वे सामाजिक प्रश्नों, सांस्कृतिक बदलावों और नैतिक संकटों पर निरंतर सोचते रहे। यह सोच उनकी रचनाओं में जितनी दिखाई देती है, उतनी ही उनके संपादकीय विवेक में भी।
शिवपूजन सहाय का यह पक्ष हमें यह समझने में मदद करता है कि साहित्य केवल लिखने से नहीं बनता, उसे सँभालने, बचाने और दिशा देने की भी ज़रूरत होती है। वे इस कार्य को किसी पद या प्रतिष्ठा की तरह नहीं बल्कि सेवा की तरह करते थे। यही कारण है कि उनका संपादक रूप आज भी प्रेरक है—खासकर ऐसे समय में जब संपादन अक्सर बाज़ार और गुटबंदी के दबाव में आ जाता है।
उनकी समूची साहित्यिक यात्रा को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि वे एक अकेले लेखक नहीं थे, बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था की तरह कार्य कर रहे थे। उनकी रचनाएँ, उनकी आलोचना और उनका संपादन—तीनों मिलकर हिंदी साहित्य के नैतिक आधार को मजबूत करते हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि साहित्य का मूल्य केवल उसकी चमक में नहीं, उसकी जिम्मेदारी में है।
शिवपूजन सहाय का अद्वितीय साहित्यिक-सांस्कृतिक-संपादकीय पक्ष उनके
रचनाकार व्यक्तित्व का परिशिष्ट नहीं बल्कि उसका अनिवार्य विस्तार है। उनकी पुण्य तिथि पर उन्हें इसी समग्रता में याद करना सबसे उचित होगा—एक ऐसे साहित्यकार के रूप में, जिसने शब्द लिखे ही नहीं, शब्दों के लिए जगह भी बनाई।
।। तीन ।।
शिवपूजन सहाय आत्म-प्रचार से लगभग सैद्धांतिक रूप से दूरी रखते थे। अपने समय में जब साहित्यिक पहचान बनाने के लिए मंच, गोष्ठियाँ और समूह आवश्यक माने जाने लगे थे, शिवपूजन सहाय ने चुपचाप लिखना और संपादित करना चुना। कई महत्वपूर्ण अवसरों पर वे जान-बूझकर अनुपस्थित रहे क्योंकि वे साहित्य को ‘दिखने’ की नहीं, ‘होने’ की प्रक्रिया मानते थे। वे पत्र लिखने को भी साहित्यिक कर्म मानते थे।
उनके निजी पत्रों में भाषा की वही सजगता, संवेदना और विचार-गहराई मिलती है, जो उनकी प्रकाशित रचनाओं में। दुर्भाग्य से उनके पत्रों का बड़ा हिस्सा अभी भी सम्यक रूप से संपादित होकर सामने नहीं आया है।
वे किसी भी लेखक को अंतिम रूप में ‘स्थापित’ मानने के पक्ष में नहीं थे।
उनका मानना था कि लेखक को बार-बार नए संदर्भों में पढ़ा जाना चाहिए। इसीलिए वे आलोचना में अंतिम निष्कर्ष देने से बचते थे और ‘संभावना’ की भाषा का प्रयोग करते थे। वे भाषा के नैतिक पक्ष को सौंदर्य से अधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे।
उनके लिए सुंदर भाषा वही थी जो अपने विषय के साथ ईमानदार हो। वे चमकदार, अलंकृत गद्य से सावधान रहते थे, यदि उसमें जीवन का सत्य कमजोर पड़ता दिखाई देता। उन्होंने कई रचनाओं को स्वयं प्रकाशित न करने का निर्णय लिया। वे ‘ग्रामीणता’ को न तो गौरव-चिह्न बनाते थे, न ही हीनता-बोध।
उनके लिए गाँव कोई वैचारिक प्रतीक नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक विस्तार था। इसीलिए उनका ग्रामीण चित्रण न तो रोमानी है, न सुधारवादी उपदेश से भरा।
वे नई पीढ़ी के लेखकों को सलाह कम, प्रश्न अधिक देते थे। जो लोग उनसे मार्गदर्शन लेने जाते थे, वे अक्सर निराश लौटते थे—उन्हें स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते थे। बाद में वही प्रश्न उनके लेखन की दिशा तय कर देते थे।
वे साहित्यिक विवादों से सचेत दूरी बनाए रखते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि वे असहमति से डरते थे, बल्कि वे सार्वजनिक विवादों को साहित्य के लिए अपकर्ष मानते थे। उनका विरोध अक्सर मौन या चयन के रूप में प्रकट होता था।
उनकी दिनचर्या में अनुशासन नहीं, लय थी।
वे तय समय पर लिखने के बजाय मनःस्थिति के अनुरूप लिखते थे। उनका मानना था कि साहित्य घड़ी से नहीं, चेतना से चलता है।
वे अपने पाठक को अत्यंत बुद्धिमान मानते थे। इसी कारण वे रचना में सब कुछ स्पष्ट नहीं करते थे। अधूरापन, रिक्तता और मौन—ये सब उनकी रचनात्मक रणनीति का हिस्सा थे।
शिवपूजन सहाय केवल अपने प्रकाशित ग्रंथों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार, चयन और मौन में भी एक गहरे साहित्यकार थे। शायद यही कारण है कि उन्हें समझने के लिए केवल पढ़ना नहीं, ठहरना भी आवश्यक है। वे ‘महत्त्वाकांक्षा’ को रचनात्मक ऊर्जा नहीं मानते थे।
उनका विश्वास था कि महत्त्वाकांक्षा साहित्य को जल्दी थका देती है। इसी कारण उन्होंने कभी दीर्घकालिक साहित्यिक नेतृत्व या संस्थागत पदों की आकांक्षा नहीं की, जबकि उनके पास पर्याप्त योग्यता और स्वीकृति थी।
वे अपने समकालीनों की सफलता से असहज नहीं होते थे।
यह दुर्लभ गुण है। जिन लेखकों को उन्होंने मंच दिया, वे कई बार उनसे अधिक चर्चित हो गए, पर शिवपूजन सहाय ने इसे कभी प्रतिस्पर्धा या उपेक्षा के रूप में नहीं देखा।
वे रचना के ‘अप्रकाशित’ रहने को भी एक वैध अवस्था मानते थे।
उनका मानना था कि हर अच्छी रचना का सार्वजनिक होना आवश्यक नहीं। कुछ रचनाएँ लेखक की आत्मा के लिए होती हैं, पाठक के लिए नहीं।
वे ‘समकालीनता’ के दबाव से सचेत रूप से दूरी रखते थे। तत्काल प्रतिक्रिया, त्वरित लेखन या समय के शोर में शामिल होना उन्हें रास नहीं आता था। वे समय को पहले ठहरकर देखते थे, फिर लिखते थे—कभी-कभी बहुत बाद में। उनके लिए साहित्यिक नैतिकता, राजनीतिक नैतिकता से अलग थी।
वे सामाजिक अन्याय के पक्ष में नहीं थे, पर साहित्य को राजनीतिक घोषणापत्र भी नहीं बनने देते थे। यह संतुलन उन्होंने जीवन भर साधे रखा।
वे मौन को संवाद का एक रूप मानते थे।
कई बार वे किसी रचना या बहस पर कुछ नहीं कहते थे। बाद में उनकी अगली रचना या संपादकीय चयन ही उनका उत्तर बन जाता था। वे स्मृति को ‘कथ्य’ से अधिक ‘दृष्टि’ मानते थे।
इसीलिए उनके संस्मरणों में घटनाएँ कम और भाव-छवियाँ अधिक मिलती हैं। वे यादों को सूचना नहीं बनने देते थे। वे साहित्यिक पीड़ा का प्रदर्शन नहीं करते थे।
निजी संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयाँ, या उपेक्षा—इनका उल्लेख उनकी रचनाओं में संकेत रूप में आता है, पर करुण-आत्मकथ्य नहीं बनता।
वे आलोचना को रचनात्मक विधा मानते थे।
उनकी आलोचना का उद्देश्य लेखक को ‘गलत’ सिद्ध करना नहीं बल्कि पाठ को अधिक पठनीय बनाना था। इसीलिए उनकी आलोचना में आक्रामकता का अभाव है।
वे साहित्य को उत्तराधिकार की वस्तु नहीं मानते थे।
उन्होंने कभी यह चिंता नहीं की कि ‘मेरा साहित्य कैसे याद किया जाएगा’। उनका विश्वास था कि जो आवश्यक है, वह स्वयं स्मरण में बना रहेगा।
ये विरल पक्ष शिवपूजन सहाय को केवल उनके ग्रंथों से नहीं, बल्कि उनके आचरण, संयम और चयन से भी परिभाषित करते हैं। वे उन साहित्यकारों में हैं, जिनकी अनुपस्थिति भी साहित्य में एक नैतिक रिक्ति छोड़ जाती है—और यही रिक्ति उनकी उपस्थिति का सबसे सशक्त प्रमाण बन जाती है।
।। चार ।।
‘साहित्य का विवेक’ शिवपूजन सहाय की ऐसी पुस्तक है जिसमें वे साहित्य को किसी सिद्धांत, आंदोलन या अकादमिक अनुशासन की संकीर्ण परिधि में नहीं बाँधते बल्कि उसे एक नैतिक और मानवीय विवेक के रूप में परिभाषित करते हैं। यह पुस्तक आलोचना की तरह नहीं बल्कि साहित्य के साथ लगातार चलने वाली आत्मचिंता की तरह पढ़ी जाती है। यहाँ लेखक निर्णय सुनाने से अधिक प्रश्न खड़े करता है और वही प्रश्न इस पुस्तक की वैचारिक रीढ़ बनते हैं।
शिवपूजन सहाय के लिए ‘विवेक’ का अर्थ केवल बुद्धि नहीं है। यह संवेदना, अनुभव, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का संयुक्त रूप है। वे मानते हैं कि साहित्य तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक उसमें विवेक सक्रिय न हो। विवेकहीन साहित्य उनके यहाँ केवल शब्दों की सजावट बनकर रह जाता है—चाहे वह कितना ही शिल्पगत रूप से प्रभावशाली क्यों न हो। इस दृष्टि से वे सौंदर्य को भी विवेक के अधीन रखते हैं, न कि उसके विपरीत।
इस पुस्तक का केंद्रीय आग्रह यह है कि साहित्य को जीवन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। शिवपूजन सहाय बार-बार इस बात पर जोर देते हैं कि साहित्य जीवन का विकल्प नहीं बल्कि उसका संवेदनशील विस्तार है। वे उस प्रवृत्ति के आलोचक हैं, जो साहित्य को केवल कल्पना का खेल या बौद्धिक व्यायाम मानती है। उनके अनुसार, साहित्य का वास्तविक मूल्य तब सामने आता है जब वह मनुष्य की पीड़ा, संघर्ष और नैतिक उलझनों से संवाद करता है।
‘साहित्य का विवेक’ में वे लेखक की भूमिका पर विशेष रूप से विचार करते हैं। लेखक उनके यहाँ कोई उपदेशक या नायक नहीं है, बल्कि एक सजग साक्षी है। वह समाज से ऊपर खड़ा होकर निर्णय नहीं सुनाता, बल्कि समाज के भीतर रहकर उसकी जटिलताओं को समझने का प्रयास करता है। शिवपूजन सहाय लेखक की इस सजगता को उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। लेखक यदि केवल अपनी प्रतिभा या प्रसिद्धि में उलझा रहे तो उसका साहित्य खोखला हो जाता है।
पुस्तक में आलोचना की भूमिका पर भी महत्त्वपूर्ण विचार हैं। शिवपूजन सहाय आलोचना को न तो न्यायालय मानते हैं, न दंड-प्रणाली। उनके अनुसार आलोचना का उद्देश्य रचना को ‘सही’ या ‘गलत’ ठहराना नहीं, बल्कि उसे अधिक समझने योग्य बनाना है। वे आलोचकों की उस प्रवृत्ति से असहमत हैं, जिसमें लेखक को किसी खांचे में फिट करने की जल्दी होती है। उनके लिए आलोचना भी एक रचनात्मक कर्म है, जिसमें विनम्रता और धैर्य अनिवार्य हैं।
भाषा के प्रश्न पर शिवपूजन सहाय का दृष्टिकोण अत्यंत संतुलित है। वे न तो अत्यधिक संस्कृतनिष्ठता के पक्षधर हैं, न ही अति-सरलीकरण के। उनके लिए भाषा का मूल्य उसकी सच्चाई और उपयुक्तता में है। यदि भाषा विषय से ईमानदार है तो वही सुंदर है। वे चेतावनी देते हैं कि जब भाषा केवल प्रभाव पैदा करने का साधन बन जाती है, तब साहित्य अपने विवेक से दूर चला जाता है।
इस पुस्तक में साहित्य और विचारधारा के संबंध पर भी गहरी चर्चा है। शिवपूजन सहाय विचारधाराओं को पूरी तरह नकारते नहीं पर उन्हें साहित्य का अंतिम सत्य भी नहीं मानते।
उनका मानना है कि साहित्य किसी विचारधारा से प्रेरणा ले सकता है लेकिन यदि वह उसका उपकरण बन जाए, तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। साहित्य का विवेक इसी स्वतंत्रता में निहित है—विचारधारा से संवाद करते हुए भी उससे बँधकर न रहना।
वे ‘प्रगतिशीलता’ को भी इसी विवेक के संदर्भ में देखते हैं। उनके लिए प्रगतिशीलता कोई नारा नहीं बल्कि मनुष्य के प्रति गहरी जिम्मेदारी है। यदि कोई रचना सामाजिक परिवर्तन की बात करती है पर मनुष्य की जटिलता को अनदेखा करती है, तो वह उन्हें अधूरी लगती है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि साहित्य का काम समाधान देना नहीं बल्कि समस्या की गहराई को सामने लाना है।
‘साहित्य का विवेक’ में परंपरा को लेकर भी एक संतुलित दृष्टि मिलती है। शिवपूजन सहाय न तो परंपरा-पूजा के पक्षधर हैं, न परंपरा-विरोध के। वे परंपरा को एक जीवित धारा मानते हैं, जो समय के साथ बदलती रहती है। साहित्य का विवेक इसी में है कि वह परंपरा से संवाद करे, पर उसके बोझ तले दब न जाए। नई रचना तभी सार्थक है, जब वह अतीत को समझते हुए वर्तमान से टकराती है।
पुस्तक का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि यहाँ साहित्य को सत्ता और बाजार से भी जोड़ा गया है। शिवपूजन सहाय आशंका व्यक्त करते हैं कि जब साहित्य केवल पुरस्कार, प्रतिष्ठा और बिक्री के गणित में फँस जाता है, तब उसका विवेक कमजोर पड़ने लगता है। वे लेखक से अपेक्षा करते हैं कि वह इस दबाव को पहचाने और उससे सावधान रहे। साहित्य का सम्मान बाहरी स्वीकृति से नहीं, आंतरिक ईमानदारी से आता है।
इस पुस्तक में पाठक की भूमिका भी उपेक्षित नहीं है।
शिवपूजन सहाय पाठक को निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं मानते। उनके अनुसार विवेकपूर्ण साहित्य विवेकपूर्ण पाठक की भी माँग करता है। पाठक यदि केवल मनोरंजन या पुष्टि की तलाश में है तो साहित्य का गहरा प्रभाव संभव नहीं। इस प्रकार साहित्य एक त्रिकोण बनाता है—लेखक, पाठ और पाठक—और विवेक इन तीनों के बीच से गुजरता है।
समग्र रूप से ‘साहित्य का विवेक’ किसी सिद्धांत-ग्रंथ की तरह नहीं बल्कि साहित्य के साथ चलने वाली आत्मालोचनात्मक चेतना की तरह है। यह पुस्तक हमें यह नहीं बताती कि क्या लिखना चाहिए बल्कि यह पूछती है कि हम क्यों लिखते हैं और किसके लिए लिखते हैं। शिवपूजन सहाय का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वे साहित्य को नैतिक जिम्मेदारी से जोड़ते हैं, बिना उसे उपदेशात्मक बनाए।
यह पुस्तक आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाती है, जब साहित्य पर त्वरित प्रतिक्रिया, वैचारिक ध्रुवीकरण और बाज़ार का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ‘साहित्य का विवेक’ हमें ठहरकर सोचने का अवसर देता है। यह याद दिलाता है कि साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी चमक में नहीं, उसकी ईमानदार दृष्टि में है। और यही विवेक शिवपूजन सहाय के पूरे साहित्यिक व्यक्तित्व की केंद्रीय धुरी है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.