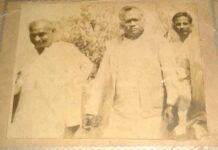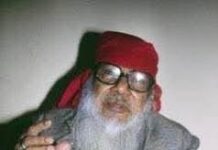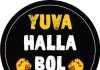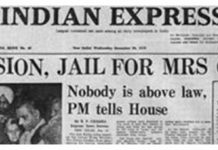— नंद भारद्वाज —
पाँच भागों और 168 उप-शीर्षकों के रूप में लिखी गयी यह जीवन-कथा कहीं डायरी शैली में है, कहीं छोटी कथाओं के रूप में तो कहीं रिपोर्ताज शैली में। इस कथा की सहज-सरल भाषा और बयान की सादगी इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जो पाठक को अपने साथ बहा ले जाती है। गांधीजी की लेखन शैली की इसी खूबी का उल्लेख करते हुए ‘हिन्द स्वराज : नव सभ्यता-विमर्श’ के लेखक वीरेन्द्र कुमार बरनवाल ने सटीक टिप्पणी की है– “गांधी पर बहुत लोगों ने लिखा, आज भी लिख रहे हैं और भविष्य में भी लिखते रहेंगे। पर गांधी पर स्वयं गांधी ही सवेश्रेष्ठ हैं। उनसे बेहतर निश्चय ही कोई नहीं।”
हिन्दी के प्रतिष्ठित कथाकार गिरिराज किशोर ने गांधी की इसी आत्मकथा को आधार बनाकर 900 पृष्ठों का जो वृहद् उपन्यास लिखा है ‘पहला गिरमिटिया’ वह निश्चय ही कथा-विन्यास की दृष्टि से एक उल्लेखनीय कृति है, जिसमें गांधीजी के वृहत्तर मानवीय चरित्र को जिस संजीदगी और सजीव ढंग से उभारा गया है, वह उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही कहा जाएगा। स्वयं गांधीजी के लिए अपनी आत्मबयान शैली में ऐसा चरित्र अंकन शायद ही संभव होता। लेकिन इस अंतर के बावजूद उनकी अपनी शैली में लिखी गयी यह आत्मकथा, उनके जीवन पर लिखी गयी सभी कथा-कृतियों से कहीं अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली है।
मोहनदास गांधी पोरबंदर के ही एक पारिवारिक परिचित व्यवसायी दादा अब्दुल्ला की मेमन फर्म के विशेष निमंत्रण और आग्रह पर बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका गये थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की दृष्टि में गुलाम हिन्दुस्तान से आनेवाले एक साधारण मजदूर और बैरिस्टर गांधी में कोई फर्क नहीं था। जब गांधी को दक्षिण अफ्रीका पहुँचकर स्वयं गोरी सरकार के इस अमानवीय बरताव का और कई अवसरों पर अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा तो दादा अब्दुल्ला की फर्म द्वारा सौंपे गये अदालती काम के साथ गांधीजी के लिए वहाँ की गोरी सरकार के बुरे और अन्यायपूर्ण आचरण के विरुद्ध हिन्दुस्तानी गरीब मजदूरों के हितों की लड़ाई उस मूल काम से भी ज्यादा जरूरी हो गयी। उन्हें न केवल अन्याय से पीड़ित हिन्दुस्तानी लोगों को उन अमानवीय कानूनों के विरुद्ध एकजुट करना जरूरी लग रहा था, बल्कि ब्रिटिश कानून और प्राकृतिक न्याय के एक सजग जन-अधिवक्ता के रूप में गोरी सरकार के तंत्र को भी मानवीय आचरण का महत्त्व समझा देना था। इसी दृष्टि से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनी वकालत शुरू करने के साथ हिन्दुस्तानी लोगों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और आजादी की चेतना पैदा करना जरूरी समझा।
गिरिराज किशोर का उपन्यास जहाँ केवल मोहनदास गांधी के दक्षिण अफ्रीकी प्रवास पर केन्द्रित और वहीं तक सीमित है, वहीं मोहनदास करमचंद गांधी कृत ‘सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा’ उनके बचपन, प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा, कस्तूरबाई से उनके बाल-विवाह, ढाई साल विलायत (लंदन) में बैरिस्ट्री की शिक्षा, स्वदेश वापसी और स्वदेश लौटकर राजकोट और बम्बई में अपनी वकालत की शुरुआत जैसे सभी महत्त्वपूर्ण जीवन-प्रसंग तो दर्ज हैं ही, जनवरी1915 में दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौट आने के बाद देश के स्वाधीनता संग्राम को जिस तरह उन्होंने पुनर्जीवित किया और उसे नयी दिशा दी, उससे भारत ही नहीं पूरे विश्व में वे एक नयी तरह की राजनीति के प्रणेता बनकर उभरे। सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आन्दोलन और असहयोग आन्दोलन के माध्यम से उन्होंने जिस तरह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बिना किसी हिंसक प्रतिरोध के भारतीय उपमहाद्वीप से लौट जाने को विवश किया, वह विश्व-इतिहास में एक अनूठी मिसाल है। अंग्रेजी हुकूमत की सारी कुटिलताओं के बावजूद उन्होंने उस हुकूमत को उसकी औकात समझा दी।
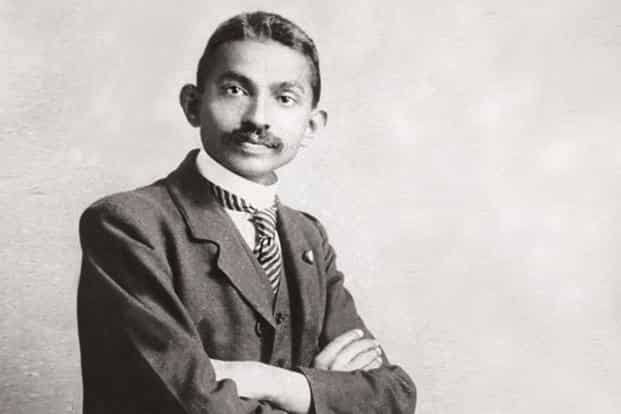 यद्यपि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आने और यहाँ पहले से चल रहे स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय होने के बाद उनके जीवन में व्यक्तिगत जीवन जैसा कुछ नहीं रह गया था, यहाँ तक कि वे दक्षिण अफ्रीका से फीनिक्स, टाल्स्टॉय फॉर्म के साथियों और जिन करीबी लोगों को साथ लेकर लौटे थे, वे अपनी पत्नी और बेटों सहित उन्हीं के साथ आश्रम निवासी ही होकर रहे, लौटकर वापस अपने निजी परिवार में नहीं गये। उनका पूरा समय देश-भ्रमण करते हुए आजादी के आन्दोलन को गतिशील बनाये रखने में ही व्यतीत हुआ।
यद्यपि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आने और यहाँ पहले से चल रहे स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय होने के बाद उनके जीवन में व्यक्तिगत जीवन जैसा कुछ नहीं रह गया था, यहाँ तक कि वे दक्षिण अफ्रीका से फीनिक्स, टाल्स्टॉय फॉर्म के साथियों और जिन करीबी लोगों को साथ लेकर लौटे थे, वे अपनी पत्नी और बेटों सहित उन्हीं के साथ आश्रम निवासी ही होकर रहे, लौटकर वापस अपने निजी परिवार में नहीं गये। उनका पूरा समय देश-भ्रमण करते हुए आजादी के आन्दोलन को गतिशील बनाये रखने में ही व्यतीत हुआ।
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधीजी ने एक-डेढ़ वर्ष तो अपने गुरु गोपालकृष्ण गोखले की सलाह पर तीसरे दर्जे की रेल-यात्राओं के माध्यम से देश के आम लोगों से संवाद करते हुए अन्दरूनी हालात को समझा और बीच-बीच में बुलावे पर कांग्रेस की गतिविधियों में भी शामिल होते रहे। गोखले की इच्छा थी कि स्वदेश लौटने के बाद वे कांग्रेस महासभा का नेतृत्व सँभालें, लेकिन उनके देहावसान के बाद कांग्रेस के दूसरे नेता आन्दोलन की बागडोर उन्हें पूरी तरह से सौंपने के पक्ष में नहीं थे और न गांधीजी को ही उसमें कोई दिलचस्पी थी। यों गुजरात के तमाम बड़े नेता वल्लभभाई पटेल, विट्ठलभाई,अनसूयाबाई, शंकरलाल बैंकर, उमर सुभानी, महादेव देसाई, इंदुलाल याज्ञिक आदि तो हमेशा उनके साथ बने ही रहते, इनके अलावा गुजरात से बाहर के नेताओं में दीनबंधु एंड्रयूज, पंडित मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, मौलाना हसरत मोहानी, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचार्य, गुरुकुल कांगड़ी के स्वामी श्रद्धानंद, अमृतसर से डॉ सत्यपाल, मोहम्मद अली जिन्ना आदि उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे और उनका पूरा समर्थन करते थे। देश में चल रहे स्वाधीनता आन्दोलन में जहाँ भी उन्हें मार्गदर्शन के लिए याद किया जाता, वे उन स्थानीय लोगों के साथ जुट जाते।
सन 1917 का चंपारण का किसान आन्दोलन, खेड़ा का मजदूर-किसान आन्दोलन, अहमदाबाद से इंदुलाल याज्ञिक की देखरेख में ‘नवजीवन’ और शंकरलाल बैंकर की देखरेख में ‘यंग इंडिया’ जैसे पत्रों की शुरुआत में गांधीजी की निर्णायक भूमिका रही। वही उन पत्रों में नियमित रूप से लिखनेवाले लेखक थे। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जारी किये गये रौलट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल में गांधी की प्रमुख भूमिका रही। इन सभी घटना-प्रसंगों और गतिविधियों पर वे ‘नवजीवन’ और ‘यंग इंडिया’ में लिखते रहे,जिससे आन्दोलन के पक्ष में देशव्यापी माहौल बना। इन्हीं पत्रों में छपे उनके तीन लेखों पर आपत्ति उठाते हुए अंग्रेज सरकार ने मार्च 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और छह साल के कारावास की सजा सुनाकर ‘यरवदा जेल’ में बंद कर दिया। इसी यरवदा जेल में रहते हुए गांधीजी ने ‘नवजीवन’ में नियमित कॉलम के रूप में अपनी ‘आत्मकथा’ को ‘सत्य के प्रयोग’ के रूप में धारावाहिक लिखना शुरू किया था, लेकिन दो साल बाद ही जब उन्हें यरवदा जेल से रिहा कर दिया गया तो जेल से बाहर आते ही वे फिर आन्दोलन के और कामों में ऐसे व्यस्त हुए कि आगे की अपनी जीवन-यात्रा पर सिलसिलेवार नहीं लिख सके और सन् 1925 तक के कुछ महत्त्वपूर्ण घटना-प्रसंगों और गतिविधियों का ही हवाला ‘आत्मकथा’ में जोड़ पाये।
उस दौर के बाद का जीवन-वृत्त अलग-अलग रूपों में अवश्य उपलबध है, और‘संपूर्ण गांधी वांग्मय’ में वह सब सुरक्षित भी है, कोई और कुशल लेखक उसे उनकी आत्मकथा या जीवनी के रूप में भी लिखता तो स्वयं गांधीजी से बेहतर शायद ही लिख पाता। इस आत्मकथा में दर्ज मोहनदास करमचंद गांधी के बचपन, कैशोर्य, युवा काल, और उनके प्रौढ़ व्यक्तित्व की जो खूबियाँ और कमजोरियाँ जिस ईमानदारी, पारदर्शिता और निर्मोही भाव से स्वयं गांधीजी ने बयान की हैं, वह निर्वैयक्तिक वस्तुपरकता इस कृति की अहमियत को कई गुना बढ़ा देती है।
Discover more from समता मार्ग
Subscribe to get the latest posts sent to your email.